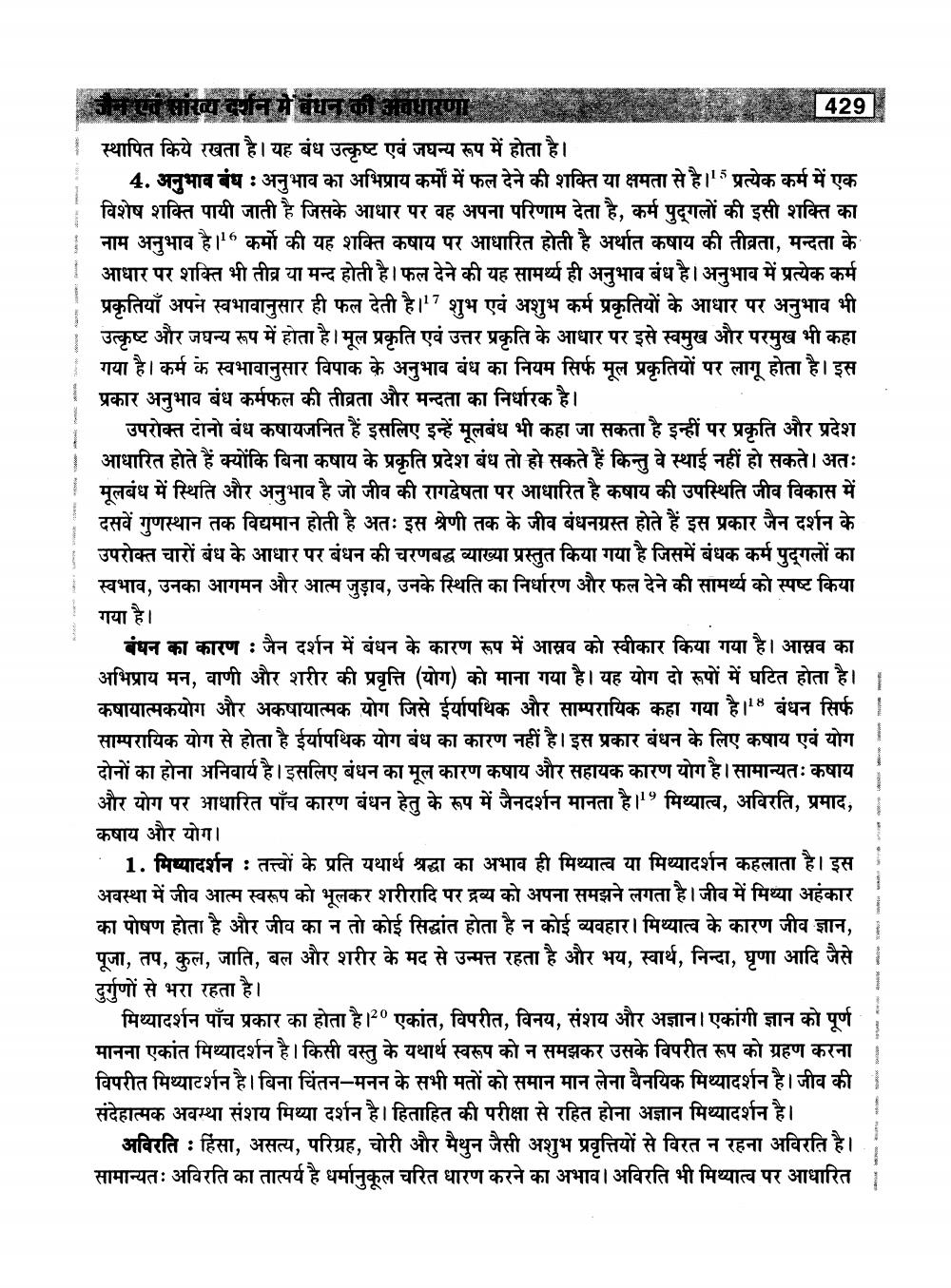________________
जैन सारत्य दर्शन में बंधन की अवधारणा
429] स्थापित किये रखता है। यह बंध उत्कृष्ट एवं जघन्य रूप में होता है।
4. अनुभाव बंध : अनुभाव का अभिप्राय कर्मों में फल देने की शक्ति या क्षमता से है। प्रत्येक कर्म में एक विशेष शक्ति पायी जाती है जिसके आधार पर वह अपना परिणाम देता है, कर्म पुद्गलों की इसी शक्ति का नाम अनुभाव है। कर्मो की यह शक्ति कषाय पर आधारित होती है अर्थात कषाय की तीव्रता, मन्दता के आधार पर शक्ति भी तीव्र या मन्द होती है। फल देने की यह सामर्थ्य ही अनुभाव बंध है। अनुभाव में प्रत्येक कर्म प्रकृतियाँ अपने स्वभावानुसार ही फल देती है। 7 शुभ एवं अशुभ कर्म प्रकृतियों के आधार पर अनुभाव भी उत्कृष्ट और जघन्य रूप में होता है। मूल प्रकृति एवं उत्तर प्रकृति के आधार पर इसे स्वमुख और परमुख भी कहा गया है। कर्म के स्वभावानुसार विपाक के अनुभाव बंध का नियम सिर्फ मूल प्रकृतियों पर लागू होता है। इस प्रकार अनुभाव बंध कर्मफल की तीव्रता और मन्दता का निर्धारक है। ___ उपरोक्त दोनो बंध कषायजनित हैं इसलिए इन्हें मूलबंध भी कहा जा सकता है इन्हीं पर प्रकृति और प्रदेश आधारित होते हैं क्योंकि बिना कषाय के प्रकृति प्रदेश बंध तो हो सकते हैं किन्तु वे स्थाई नहीं हो सकते। अतः मूलबंध में स्थिति और अनुभाव है जो जीव की रागद्वेषता पर आधारित है कषाय की उपस्थिति जीव विकास में दसवें गुणस्थान तक विद्यमान होती है अतः इस श्रेणी तक के जीव बंधनग्रस्त होते हैं इस प्रकार जैन दर्शन के उपरोक्त चारों बंध के आधार पर बंधन की चरणबद्ध व्याख्या प्रस्तुत किया गया है जिसमें बंधक कर्म पुद्गलों का स्वभाव, उनका आगमन और आत्म जुड़ाव, उनके स्थिति का निर्धारण और फल देने की सामर्थ्य को स्पष्ट किया गया है।
बंधन का कारण : जैन दर्शन में बंधन के कारण रूप में आस्रव को स्वीकार किया गया है। आस्रव का अभिप्राय मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति (योग) को माना गया है। यह योग दो रूपों में घटित होता है। कषायात्मकयोग और अकषायात्मक योग जिसे ईर्यापथिक और साम्परायिक कहा गया है। बंधन सिर्फ । साम्परायिक योग से होता है ईर्यापथिक योग बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार बंधन के लिए कषाय एवं योग दोनों का होना अनिवार्य है। इसलिए बंधन का मूल कारण कषाय और सहायक कारण योग है। सामान्यतः कषाय
और योग पर आधारित पाँच कारण बंधन हेतु के रूप में जैनदर्शन मानता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। - 1. मिष्यादर्शन : तत्त्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा का अभाव ही मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन कहलाता है। इस अवस्था में जीव आत्म स्वरूप को भूलकर शरीरादि पर द्रव्य को अपना समझने लगता है। जीव में मिथ्या अहंकार का पोषण होता है और जीव का न तो कोई सिद्धांत होता है न कोई व्यवहार। मिथ्यात्व के कारण जीव ज्ञान, पूजा, तप, कुल, जाति, बल और शरीर के मद से उन्मत्त रहता है और भय, स्वार्थ, निन्दा, घृणा आदि जैसे दुर्गुणों से भरा रहता है। __ मिथ्यादर्शन पाँच प्रकार का होता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांगी ज्ञान को पूर्ण मानना एकांत मिथ्यादर्शन है। किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को न समझकर उसके विपरीत रूप को ग्रहण करना विपरीत मिथ्याटर्शन है। बिना चिंतन-मनन के सभी मतों को समान मान लेना वैनयिक मिथ्यादर्शन है। जीव की । संदेहात्मक अवस्था संशय मिथ्या दर्शन है। हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञान मिथ्यादर्शन है।
अविरति : हिंसा, असत्य, परिग्रह, चोरी और मैथुन जैसी अशुभ प्रवृत्तियों से विरत न रहना अविरति है। सामान्यतः अविरति का तात्पर्य है धर्मानुकूल चरित धारण करने का अभाव। अविरति भी मिथ्यात्व पर आधारित ।