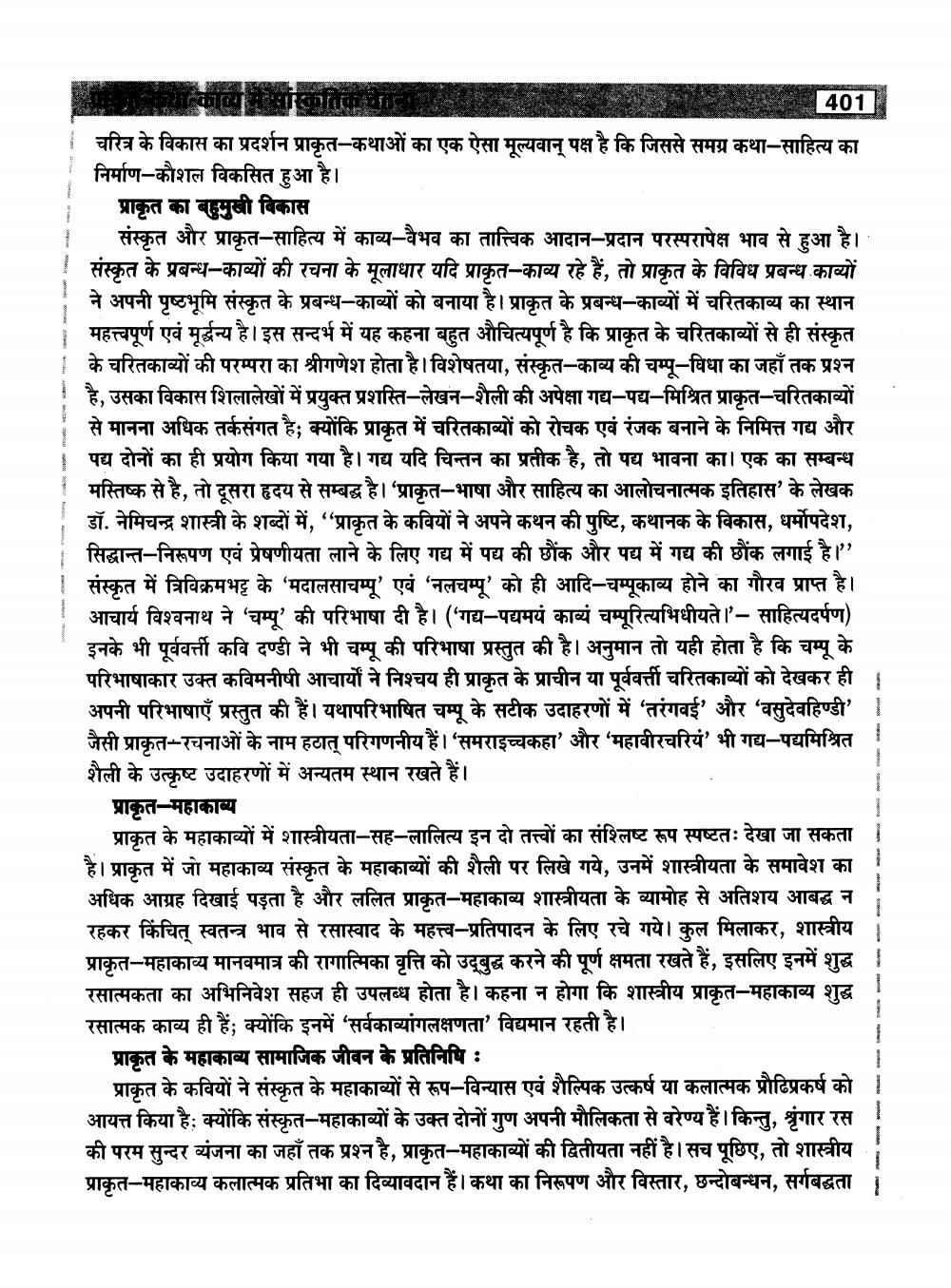________________
401
चरित्र के विकास का प्रदर्शन प्राकृत-कथाओं का एक ऐसा मूल्यवान् पक्ष है कि जिससे समग्र कथा-साहित्य का निर्माण-कौशल विकसित हुआ है।
प्राकृत का बहुमुखी विकास ___ संस्कृत और प्राकृत-साहित्य में काव्य-वैभव का तात्त्विक आदान-प्रदान परस्परापेक्ष भाव से हुआ है। संस्कृत के प्रबन्ध-काव्यों की रचना के मूलाधार यदि प्राकृत-काव्य रहे हैं, तो प्राकृत के विविध प्रबन्ध काव्यों
ने अपनी पृष्ठभूमि संस्कृत के प्रबन्ध-काव्यों को बनाया है। प्राकृत के प्रबन्ध-काव्यों में चरितकाव्य का स्थान | महत्त्वपूर्ण एवं मूर्द्धन्य है। इस सन्दर्भ में यह कहना बहुत औचित्यपूर्ण है कि प्राकृत के चरितकाव्यों से ही संस्कृत 1 के चरितकाव्यों की परम्परा का श्रीगणेश होता है। विशेषतया, संस्कृत-काव्य की चम्पू-विधा का जहाँ तक प्रश्न
है, उसका विकास शिलालेखों में प्रयुक्त प्रशस्ति-लेखन-शैली की अपेक्षा गद्य-पद्य-मिश्रित प्राकृत-चरितकाव्यों से मानना अधिक तर्कसंगत है क्योंकि प्राकृत में चरितकाव्यों को रोचक एवं रंजक बनाने के निमित्त गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग किया गया है। गद्य यदि चिन्तन का प्रतीक है, तो पद्य भावना का। एक का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, तो दूसरा हृदय से सम्बद्ध है। 'प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' के लेखक डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री के शब्दों में, “प्राकृत के कवियों ने अपने कथन की पुष्टि, कथानक के विकास, धर्मोपदेश, सिद्धान्त-निरूपण एवं प्रेषणीयता लाने के लिए गद्य में पद्य की छौंक और पद्य में गद्य की छौंक लगाई है।" संस्कृत में त्रिविक्रमभट्ट के 'मदालसाचम्पू' एवं 'नलचम्पू' को ही आदि-चम्पूकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। आचार्य विश्वनाथ ने 'चम्पू' की परिभाषा दी है। ('गद्य-पद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।'- साहित्यदर्पण) इनके भी पूर्ववर्ती कवि दण्डी ने भी चम्पू की परिभाषा प्रस्तुत की है। अनुमान तो यही होता है कि चम्पू के परिभाषाकार उक्त कविमनीषी आचार्यों ने निश्चय ही प्राकृत के प्राचीन या पूर्ववर्ती चरितकाव्यों को देखकर ही । अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। यथापरिभाषित चम्पू के सटीक उदाहरणों में 'तरंगवई' और 'वसुदेवहिण्डी' जैसी प्राकृत-रचनाओं के नाम हठात् परिगणनीय हैं। 'समराइच्चकहा' और 'महावीरचरियं' भी गद्य-पद्यमिश्रित शैली के उत्कृष्ट उदाहरणों में अन्यतम स्थान रखते हैं। प्राकृत-महाकाव्य
प्राकृत के महाकाव्यों में शास्त्रीयता-सह-लालित्य इन दो तत्त्वों का संश्लिष्ट रूप स्पष्टतः देखा जा सकता है। प्राकृत में जो महाकाव्य संस्कृत के महाकाव्यों की शैली पर लिखे गये, उनमें शास्त्रीयता के समावेश का अधिक आग्रह दिखाई पड़ता है और ललित प्राकृत-महाकाव्य शास्त्रीयता के व्यामोह से अतिशय आबद्ध न रहकर किंचित् स्वतन्त्र भाव से रसास्वाद के महत्त्व-प्रतिपादन के लिए रचे गये। कुल मिलाकर, शास्त्रीय प्राकृत-महाकाव्य मानवमात्र की रागात्मिका वृत्ति को उबुद्ध करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं, इसलिए इनमें शुद्ध रसात्मकता का अभिनिवेश सहज ही उपलब्ध होता है। कहना न होगा कि शास्त्रीय प्राकृत-महाकाव्य शुद्ध रसात्मक काव्य ही हैं; क्योंकि इनमें 'सर्वकाव्यांगलक्षणता' विद्यमान रहती है।
प्राकृत के महाकाव्य सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि : प्राकृत के कवियों ने संस्कृत के महाकाव्यों से रूप-विन्यास एवं शैल्पिक उत्कर्ष या कलात्मक प्रौढिप्रकर्ष को । आयत्त किया है। क्योंकि संस्कृत-महाकाव्यों के उक्त दोनों गुण अपनी मौलिकता से वरेण्य हैं। किन्तु, श्रृंगार रस ! की परम सुन्दर व्यंजना का जहाँ तक प्रश्न है, प्राकृत-महाकाव्यों की द्वितीयता नहीं है। सच पूछिए, तो शास्त्रीय प्राकृत-महाकाव्य कलात्मक प्रतिभा का दिव्यावदान हैं। कथा का निरूपण और विस्तार, छन्दोबन्धन, सर्गबद्धता ।