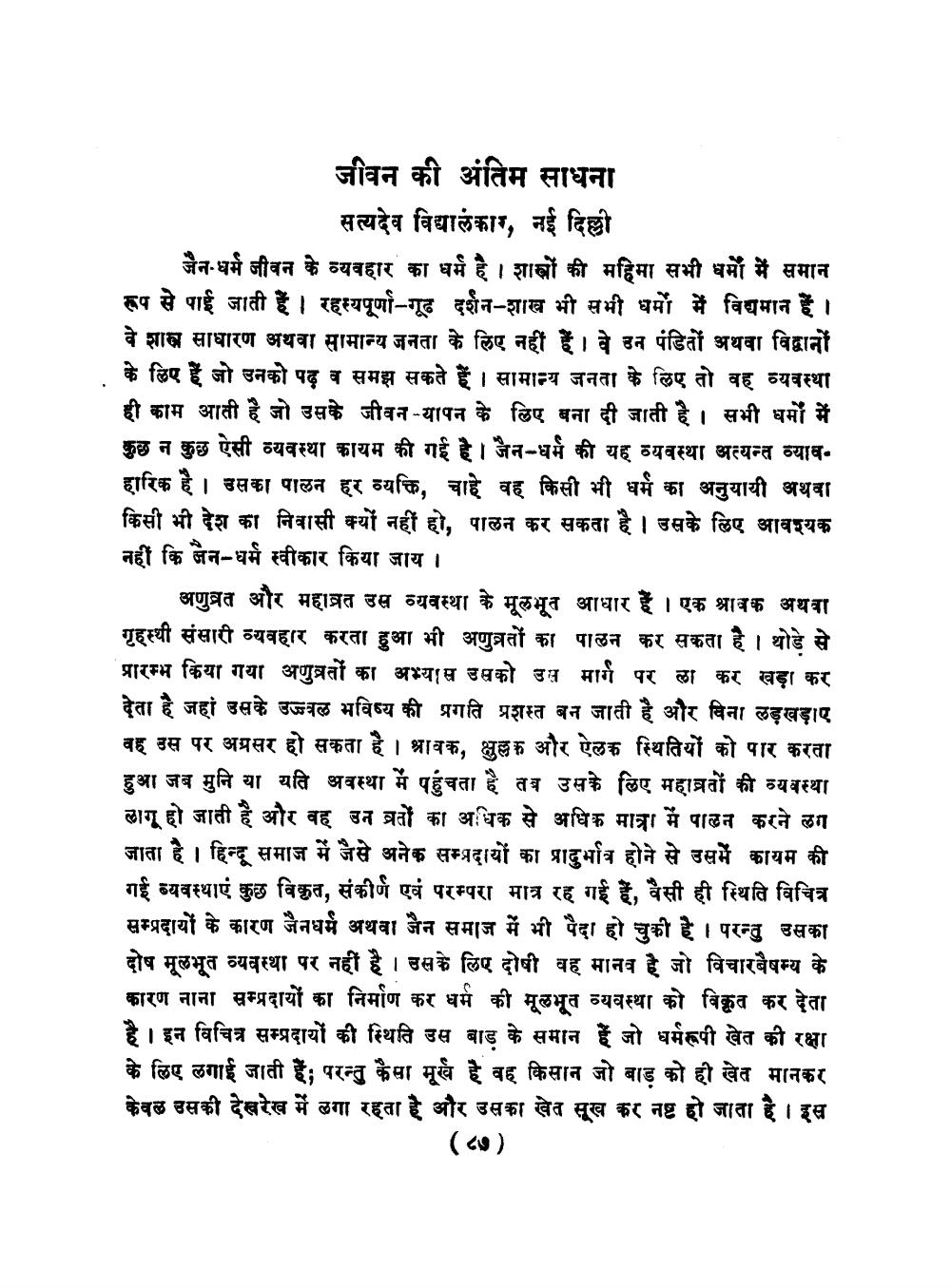________________
जीवन की अंतिम साधना
सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली जैन-धर्म जीवन के व्यवहार का धर्म है । शास्त्रों की महिमा सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती हैं। रहस्यपूर्णा-गूढ दर्शन-शाख भी सभी धर्मों में विद्यमान हैं। वे शास्त्र साधारण अथवा सामान्य जनता के लिए नहीं हैं। वे उन पंडितों अथवा विद्वानों के लिए हैं जो उनको पढ़ व समझ सकते हैं । सामान्य जनता के लिए तो वह व्यवस्था ही काम आती है जो उसके जीवन-यापन के लिए बना दी जाती है। सभी धर्मों में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कायम की गई है। जैन-धर्म की यह व्यवस्था अत्यन्त व्याव. हारिक है। उसका पालन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी अथवा किसी भी देश का निवासी क्यों नहीं हो, पालन कर सकता है । उसके लिए आवश्यक नहीं कि जैन-धर्म स्वीकार किया जाय ।
अणुव्रत और महाव्रत उस व्यवस्था के मूलभूत आधार हैं । एक श्रावक अथवा गृहस्थी संसारी व्यवहार करता हुआ भी अणुव्रतों का पालन कर सकता है । थोड़े से प्रारम्भ किया गया अणुव्रतों का अभ्यास उसको उस मार्ग पर ला कर खड़ा कर देता है जहां उसके उज्वल भविष्य की प्रगति प्रशस्त बन जाती है और विना लड़खड़ाए वह उस पर अग्रसर हो सकता है । श्रावक, क्षुल्लक और ऐलक स्थितियों को पार करता हुआ जब मुनि या यति अवस्था में पहुंचता है तब उसके लिए महाव्रतों की व्यवस्था लागू हो जाती है और वह उन व्रतों का अधिक से अधिक मात्रा में पालन करने लग जाता है । हिन्दू समाज में जैसे अनेक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव होने से उसमें कायम की गई ब्यवस्थाएं कुछ विकृत, संकीर्ण एवं परम्परा मात्र रह गई हैं, वैसी ही स्थिति विचित्र सम्प्रदायों के कारण जैनधर्म अथवा जैन समाज में भी पैदा हो चुकी है । परन्तु उसका दोष मूलभूत व्यवस्था पर नहीं है । उसके लिए दोषी वह मानव है जो विचारबैषम्य के कारण नाना सम्प्रदायों का निर्माण कर धर्म की मूलभूत व्यवस्था को विकृत कर देता है। इन विचित्र सम्प्रदायों की स्थिति उस बाड़ के समान हैं जो धर्मरूपी खेत की रक्षा के लिए लगाई जाती है; परन्तु कैसा मूर्ख है वह किसान जो बाड़ को ही खेत मानकर केवल उसकी देखरेख में लगा रहता है और उसका खेत सूख कर नष्ट हो जाता है । इस