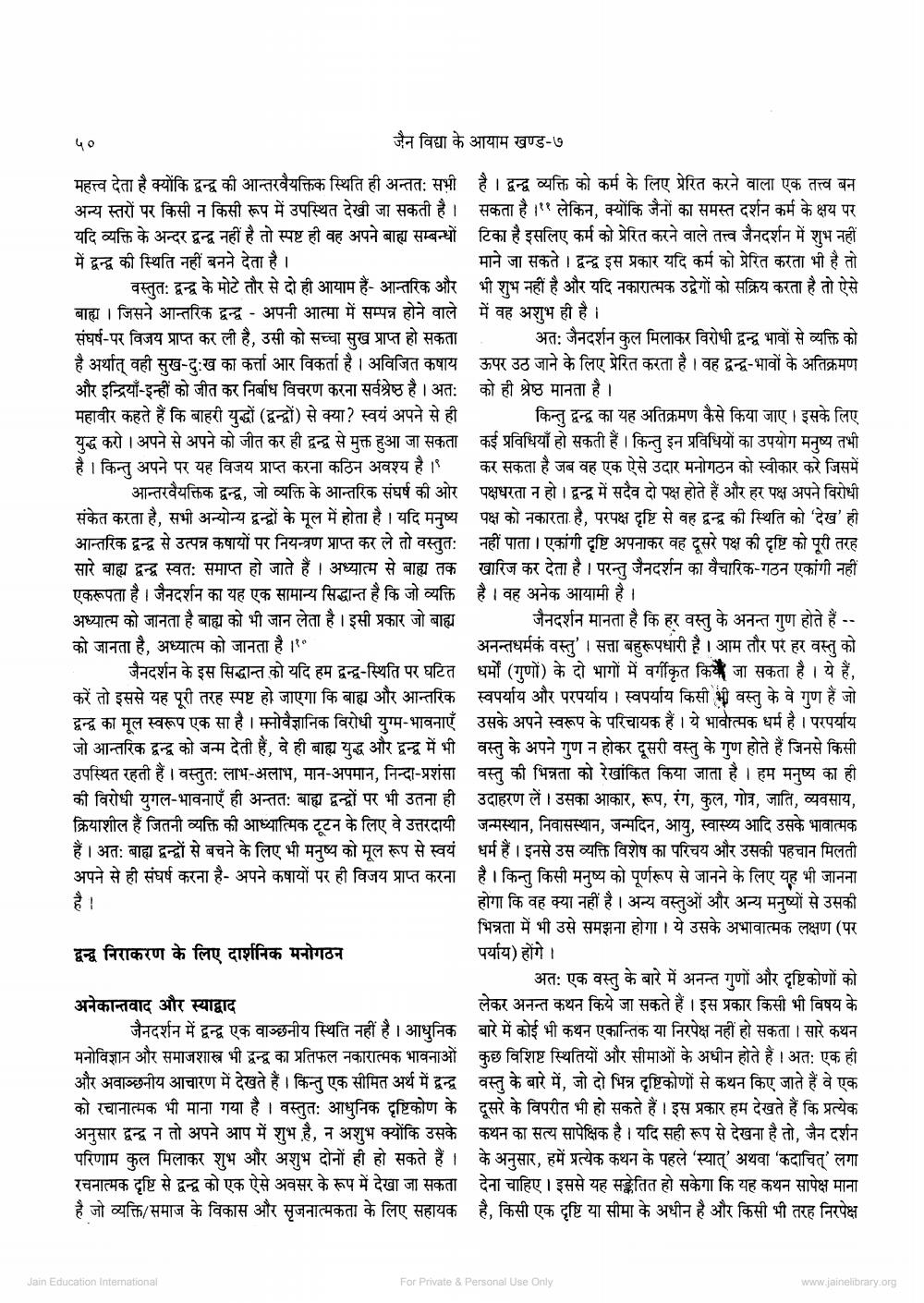________________
जैन विद्या के आयाम खण्ड-७
महत्त्व देता है क्योंकि द्वन्द्व की आन्तरवैयक्तिक स्थिति ही अन्तत: सभी है । द्वन्द्व व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करने वाला एक तत्त्व बन अन्य स्तरों पर किसी न किसी रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। सकता है ।१९ लेकिन, क्योंकि जैनों का समस्त दर्शन कर्म के क्षय पर यदि व्यक्ति के अन्दर द्वन्द्व नहीं है तो स्पष्ट ही वह अपने बाह्य सम्बन्धों टिका है इसलिए कर्म को प्रेरित करने वाले तत्त्व जैनदर्शन में शुभ नहीं में द्वन्द्व की स्थिति नहीं बनने देता है।
माने जा सकते । द्वन्द्व इस प्रकार यदि कर्म को प्रेरित करता भी है तो वस्तुत: द्वन्द्व के मोटे तौर से दो ही आयाम हैं- आन्तरिक और भी शुभ नहीं है और यदि नकारात्मक उद्वेगों को सक्रिय करता है तो ऐसे बाह्य । जिसने आन्तरिक द्वन्द्व - अपनी आत्मा में सम्पन्न होने वाले में वह अशुभ ही है। संघर्ष-पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी को सच्चा सुख प्राप्त हो सकता . अत: जैनदर्शन कुल मिलाकर विरोधी द्वन्द्व भावों से व्यक्ति को है अर्थात् वही सुख-दुःख का कर्ता आर विकर्ता है । अविजित कषाय ऊपर उठ जाने के लिए प्रेरित करता है । वह द्वन्द्व-भावों के अतिक्रमण
और इन्द्रियाँ-इन्हीं को जीत कर निर्बाध विचरण करना सर्वश्रेष्ठ है । अतः को ही श्रेष्ठ मानता है। महावीर कहते हैं कि बाहरी युद्धों (द्वन्द्वों) से क्या? स्वयं अपने से ही किन्तु द्वन्द्व का यह अतिक्रमण कैसे किया जाए। इसके लिए युद्ध करो । अपने से अपने को जीत कर ही द्वन्द्व से मुक्त हुआ जा सकता कई प्रविधियाँ हो सकती हैं। किन्तु इन प्रविधियों का उपयोग मनुष्य तभी है। किन्तु अपने पर यह विजय प्राप्त करना कठिन अवश्य है । कर सकता है जब वह एक ऐसे उदार मनोगठन को स्वीकार करे जिसमें
आन्तरवैयक्तिक द्वन्द्व, जो व्यक्ति के आन्तरिक संघर्ष की ओर पक्षधरता न हो । द्वन्द्व में सदैव दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष अपने विरोधी संकेत करता है, सभी अन्योन्य द्वन्द्वों के मूल में होता है । यदि मनुष्य पक्ष को नकारता है, परपक्ष दृष्टि से वह द्वन्द्व की स्थिति को देख' ही आन्तरिक द्वन्द्व से उत्पन्न कषायों पर नियन्त्रण प्राप्त कर ले तो वस्तुत: नहीं पाता। एकांगी दृष्टि अपनाकर वह दूसरे पक्ष की दृष्टि को पूरी तरह सारे बाह्य द्वन्द्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं । अध्यात्म से बाह्य तक खारिज कर देता है । परन्तु जैनदर्शन का वैचारिक-गठन एकांगी नहीं एकरूपता है । जैनदर्शन का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति है। वह अनेक आयामी है। अध्यात्म को जानता है बाह्य को भी जान लेता है । इसी प्रकार जो बाह्य जैनदर्शन मानता है कि हर वस्तु के अनन्त गुण होते हैं -- को जानता है, अध्यात्म को जानता है ।
अनन्तधर्मकं वस्तु' । सत्ता बहरूपधारी है। आम तौर पर हर वस्तु को जैनदर्शन के इस सिद्धान्त को यदि हम द्वन्द्व-स्थिति पर घटित धर्मों (गुणों) के दो भागों में वर्गीकृत किये जा सकता है। ये हैं, करें तो इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि बाह्य और आन्तरिक स्वपर्याय और परपर्याय । स्वपर्याय किसी भी वस्तु के वे गुण हैं जो द्वन्द्व का मूल स्वरूप एक सा है । मनोवैज्ञानिक विरोधी युग्म-भावनाएँ उसके अपने स्वरूप के परिचायक हैं । ये भावोत्मक धर्म है । परपर्याय जो आन्तरिक द्वन्द्व को जन्म देती हैं, वे ही बाह्य युद्ध और द्वन्द्व में भी वस्तु के अपने गुण न होकर दूसरी वस्तु के गुण होते हैं जिनसे किसी उपस्थित रहती हैं। वस्तुत: लाभ-अलाभ, मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा वस्तु की भिन्नता को रेखांकित किया जाता है । हम मनुष्य का ही की विरोधी युगल-भावनाएँ ही अन्तत: बाह्य द्वन्द्वों पर भी उतना ही उदाहरण लें। उसका आकार, रूप, रंग, कुल, गोत्र, जाति, व्यवसाय, क्रियाशील हैं जितनी व्यक्ति की आध्यात्मिक टूटन के लिए वे उत्तरदायी जन्मस्थान, निवासस्थान, जन्मदिन, आयु, स्वास्थ्य आदि उसके भावात्मक हैं। अत: बाह्य द्वन्द्वों से बचने के लिए भी मनुष्य को मूल रूप से स्वयं धर्म हैं । इनसे उस व्यक्ति विशेष का परिचय और उसकी पहचान मिलती अपने से ही संघर्ष करना है- अपने कषायों पर ही विजय प्राप्त करना है। किन्तु किसी मनुष्य को पूर्णरूप से जानने के लिए यह भी जानना
होगा कि वह क्या नहीं है । अन्य वस्तुओं और अन्य मनुष्यों से उसकी
भिन्नता में भी उसे समझना होगा। ये उसके अभावात्मक लक्षण (पर द्वन्द्व निराकरण के लिए दार्शनिक मनोगठन
पर्याय) होंगे।
अत: एक वस्तु के बारे में अनन्त गणों और दृष्टिकोणों को अनेकान्तवाद और स्याद्वाद
लेकर अनन्त कथन किये जा सकते हैं । इस प्रकार किसी भी विषय के जैनदर्शन में द्वन्द्व एक वाञ्छनीय स्थिति नहीं है । आधुनिक बारे में कोई भी कथन एकान्तिक या निरपेक्ष नहीं हो सकता । सारे कथन मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी द्वन्द्व का प्रतिफल नकारात्मक भावनाओं कुछ विशिष्ट स्थितियों और सीमाओं के अधीन होते हैं । अतः एक ही
और अवाञ्छनीय आचारण में देखते हैं। किन्तु एक सीमित अर्थ में द्वन्द्व वस्तु के बारे में, जो दो भिन्न दृष्टिकोणों से कथन किए जाते हैं वे एक को रचानात्मक भी माना गया है । वस्तुत: आधुनिक दृष्टिकोण के दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक अनुसार द्वन्द्व न तो अपने आप में शुभ है, न अशुभ क्योंकि उसके कथन का सत्य सापेक्षिक है। यदि सही रूप से देखना है तो, जैन दर्शन परिणाम कुल मिलाकर शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं। के अनुसार, हमें प्रत्येक कथन के पहले 'स्यात्' अथवा 'कदाचित् लगा रचनात्मक दृष्टि से द्वन्द्व को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जा सकता देना चाहिए। इससे यह सङ्केतित हो सकेगा कि यह कथन सापेक्ष माना है जो व्यक्ति/समाज के विकास और सृजनात्मकता के लिए सहायक है, किसी एक दृष्टि या सीमा के अधीन है और किसी भी तरह निरपेक्ष
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org