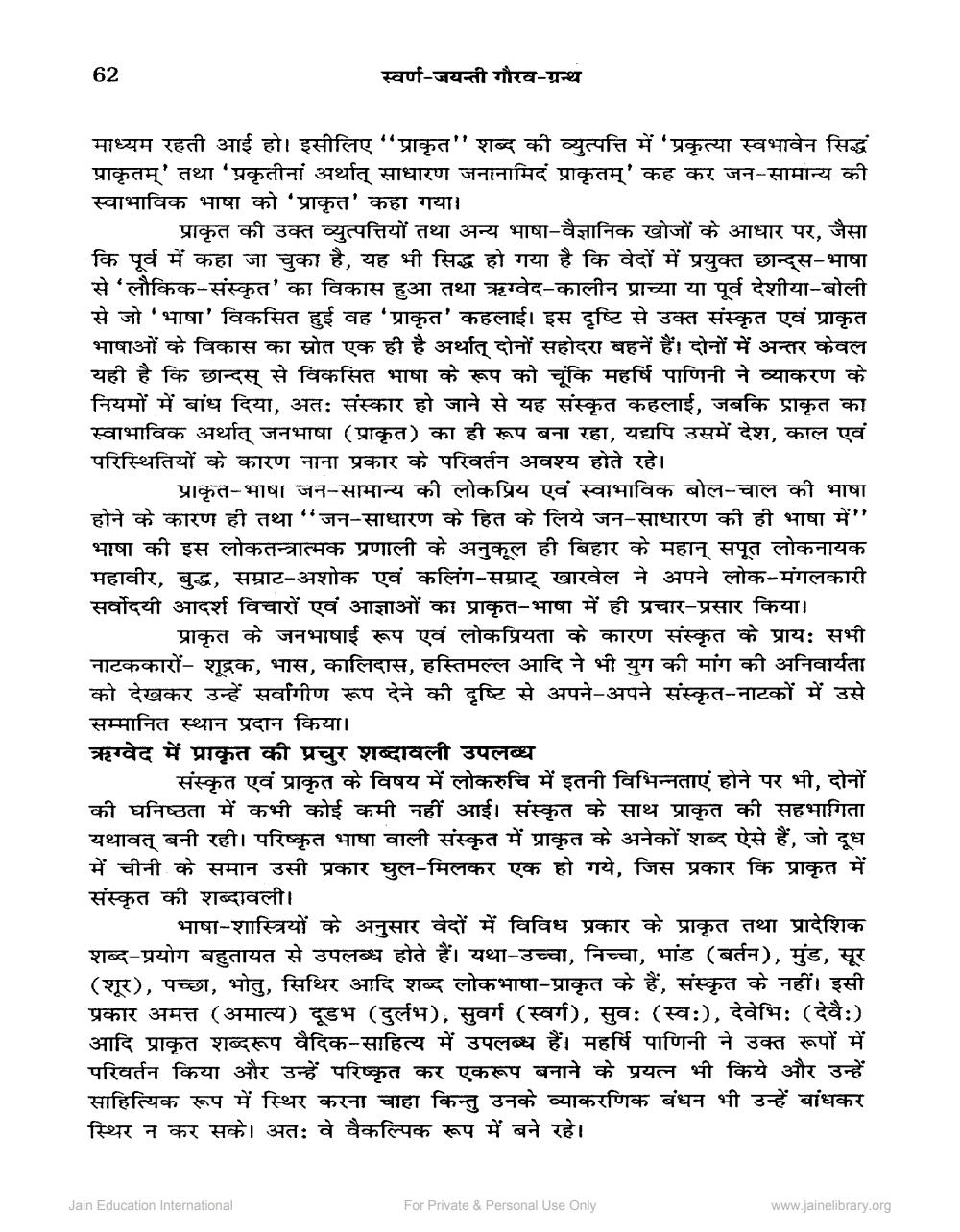________________
62
स्वर्ण-जयन्ती गौरव-ग्रन्थ
माध्यम रहती आई हो। इसीलिए "प्राकृत" शब्द की व्युत्पत्ति में 'प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृतम्' तथा 'प्रकृतीनां अर्थात् साधारण जनानामिदं प्राकृतम्' कह कर जन-सामान्य की स्वाभाविक भाषा को 'प्राकृत' कहा गया।
प्राकृत की उक्त व्युत्पत्तियों तथा अन्य भाषा-वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, यह भी सिद्ध हो गया है कि वेदों में प्रयुक्त छान्दुस-भाषा से 'लौकिक-संस्कृत' का विकास हुआ तथा ऋग्वेद-कालीन प्राच्या या पूर्व देशीया-बोली से जो 'भाषा' विकसित हुई वह 'प्राकृत' कहलाई। इस दृष्टि से उक्त संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के विकास का स्रोत एक ही है अर्थात् दोनों सहोदरा बहनें हैं। दोनों में अन्तर केवल यही है कि छान्दस से विकसित भाषा के रूप को चंकि महर्षि पाणिनी ने व्या नियमों में बांध दिया, अतः संस्कार हो जाने से यह संस्कृत कहलाई, जबकि प्राकृत का स्वाभाविक अर्थात् जनभाषा (प्राकृत) का ही रूप बना रहा, यद्यपि उसमें देश, काल एवं परिस्थितियों के कारण नाना प्रकार के परिवर्तन अवश्य होते रहे।
प्राकृत-भाषा जन-सामान्य की लोकप्रिय एवं स्वाभाविक बोल-चाल की भाषा होने के कारण ही तथा "जन-साधारण के हित के लिये जन-साधारण की ही भाषा में" भाषा की इस लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के अनुकूल ही बिहार के महान् सपूत लोकनायक महावीर, बुद्ध, सम्राट-अशोक एवं कलिंग-सम्राट् खारवेल ने अपने लोक-मंगलकारी सर्वोदयी आदर्श विचारों एवं आज्ञाओं का प्राकृत-भाषा में ही प्रचार-प्रसार किया।
प्राकृत के जनभाषाई रूप एवं लोकप्रियता के कारण संस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों- शूद्रक, भास, कालिदास, हस्तिमल्ल आदि ने भी युग की मांग की अनिवार्यता को देखकर उन्हें सर्वागीण रूप देने की दृष्टि से अपने-अपने संस्कृत-नाटकों में उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया। ऋग्वेद में प्राकृत की प्रचुर शब्दावली उपलब्ध
संस्कृत एवं प्राकृत के विषय में लोकरुचि में इतनी विभिन्नताएं होने पर भी, दोनों की घनिष्ठता में कभी कोई कमी नहीं आई। संस्कृत के साथ प्राकृत की सहभागिता यथावत् बनी रही। परिष्कृत भाषा वाली संस्कृत में प्राकृत के अनेकों शब्द ऐसे हैं, जो दूध में चीनी के समान उसी प्रकार घुल-मिलकर एक हो गये, जिस प्रकार कि प्राकृत में संस्कृत की शब्दावली।
भाषा-शास्त्रियों के अनुसार वेदों में विविध प्रकार के प्राकृत तथा प्रादेशिक शब्द प्रयोग बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। यथा-उच्चा, निच्चा, भांड (बर्तन), मुंड, सूर (शूर), पच्छा, भोतु, सिथिर आदि शब्द लोकभाषा-प्राकृत के हैं, संस्कृत के नहीं। इसी प्रकार अमत्त (अमात्य) दूडभ (दुर्लभ), सुवर्ग (स्वर्ग), सुवः (स्व:), देवेभिः (देवैः) आदि प्राकृत शब्दरूप वैदिक-साहित्य में उपलब्ध हैं। महर्षि पाणिनी ने उक्त रूपों में परिवर्तन किया और उन्हें परिष्कृत कर एकरूप बनाने के प्रयत्न भी किये और उन्हें साहित्यिक रूप में स्थिर करना चाहा किन्तु उनके व्याकरणिक बंधन भी उन्हें बांधकर स्थिर न कर सके। अतः वे वैकल्पिक रूप में बने रहे।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org