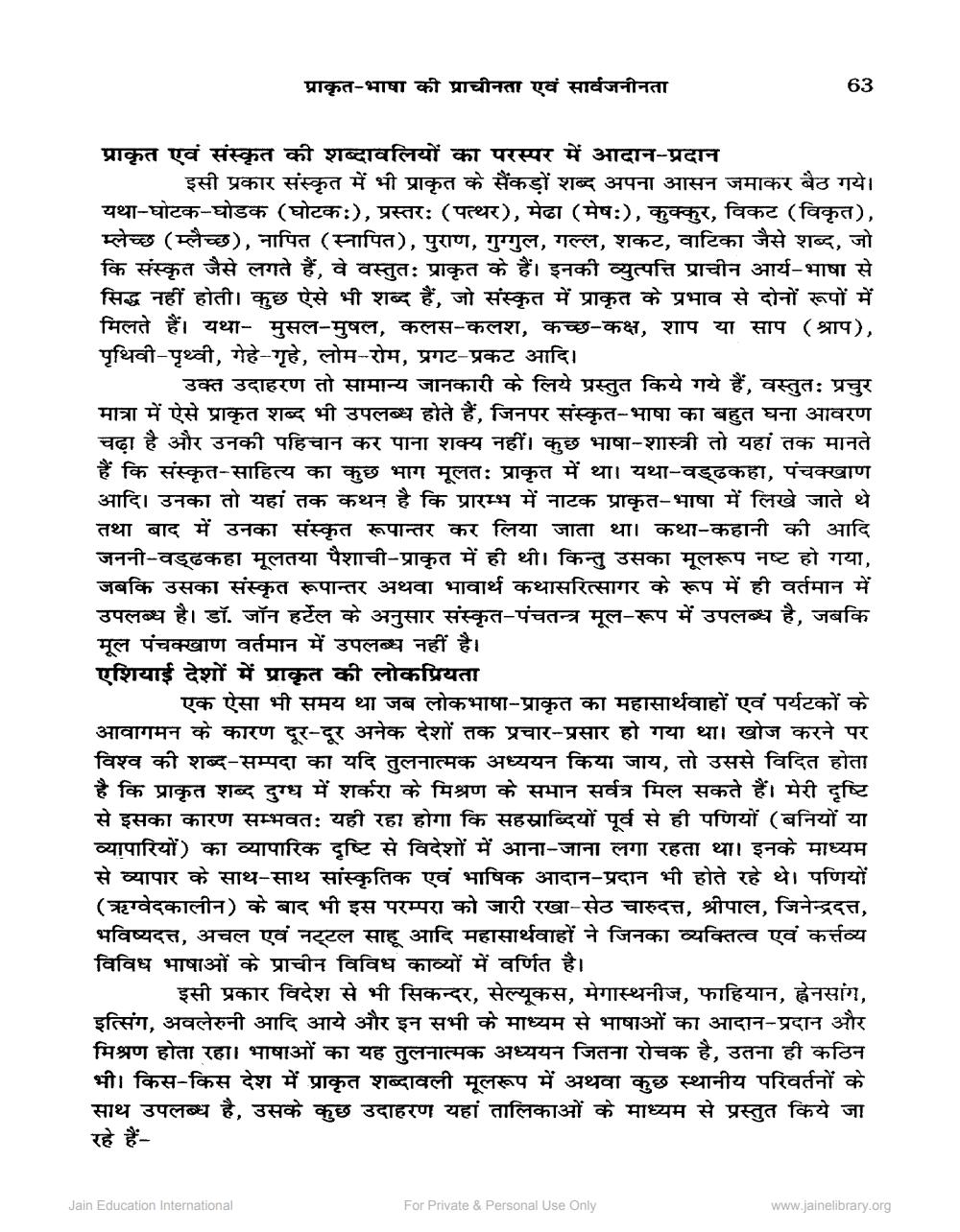________________
प्राकृत-भाषा की प्राचीनता एवं सार्वजनीनता
63
प्राकृत एवं संस्कृत की शब्दावलियों का परस्पर में आदान-प्रदान
इसी प्रकार संस्कृत में भी प्राकृत के सैंकड़ों शब्द अपना आसन जमाकर बैठ गये। यथा-घोटक-घोडक (घोटकः), प्रस्तरः (पत्थर), मेढा (मेषः), कुक्कुर, विकट (विकृत), म्लेच्छ (म्लेच्छ), नापित (स्नापित), पुराण, गुग्गुल, गल्ल, शकट, वाटिका जैसे शब्द, जो कि संस्कृत जैसे लगते हैं, वे वस्तुतः प्राकृत के हैं। इनकी व्युत्पत्ति प्राचीन आर्य-भाषा से सिद्ध नहीं होती। कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो संस्कृत में प्राकृत के प्रभाव से दोनों रूपों में मिलते हैं। यथा- मुसल-मुषल, कलस-कलश, कच्छ-कक्ष, शाप या साप (श्राप), पृथिवी-पृथ्वी, गेहे-गृहे, लोम-रोम, प्रगट-प्रकट आदि।
उक्त उदाहरण तो सामान्य जानकारी के लिये प्रस्तुत किये गये हैं, वस्तुतः प्रचुर मात्रा में ऐसे प्राकृत शब्द भी उपलब्ध होते हैं, जिनपर संस्कृत-भाषा का बहुत घना आवरण चढ़ा है और उनकी पहिचान कर पाना शक्य नहीं। कुछ भाषा-शास्त्री तो यहां तक मानते हैं कि संस्कृत-साहित्य का कुछ भाग मूलतः प्राकृत में था। यथा-वड्ढकहा, पंचक्खाण आदि। उनका तो यहां तक कथन है कि प्रारम्भ में नाटक प्राकृत-भाषा में लिखे जाते थे तथा बाद में उनका संस्कृत रूपान्तर कर लिया जाता था। कथा-कहानी की आदि जननी-वड्ढकहा मूलतया पैशाची-प्राकृत में ही थी। किन्तु उसका मूलरूप नष्ट हो गया, जबकि उसका संस्कृत रूपान्तर अथवा भावार्थ कथासरित्सागर के रूप में ही वर्तमान में उपलब्ध है। डॉ. जॉन हर्टेल के अनुसार संस्कृत-पंचतन्त्र मूल-रूप में उपलब्ध है, जबकि मूल पंचक्खाण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। एशियाई देशों में प्राकृत की लोकप्रियता
एक ऐसा भी समय था जब लोकभाषा-प्राकृत का महासार्थवाहों एवं पर्यटकों के आवागमन के कारण दूर-दूर अनेक देशों तक प्रचार-प्रसार हो गया था। खोज करने पर विश्व की शब्द-सम्पदा का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो उससे विदित होता है कि प्राकृत शब्द दुग्ध में शर्करा के मिश्रण के समान सर्वत्र मिल सकते हैं। मेरी दृष्टि से इसका कारण सम्भवतः यही रहा होगा कि सहस्राब्दियों पूर्व से ही पणियों (बनियों या व्यापारियों) का व्यापारिक दृष्टि से विदेशों में आना-जाना लगा रहता था। इनके माध्यम से व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं भाषिक आदान-प्रदान भी होते रहे थे। पणियों (ऋग्वेदकालीन) के बाद भी इस परम्परा को जारी रखा-सेठ चारुदत्त, श्रीपाल, जिनेन्द्रदत्त, भविष्यदत्त, अचल एवं नट्टल साहू आदि महासार्थवाहों ने जिनका व्यक्तित्व एवं कर्तव्य विविध भाषाओं के प्राचीन विविध काव्यों में वर्णित है।
इसी प्रकार विदेश से भी सिकन्दर, सेल्यूकस, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अवलेरुनी आदि आये और इन सभी के माध्यम से भाषाओं का आदान-प्रदान और मिश्रण होता रहा। भाषाओं का यह तुलनात्मक अध्ययन जितना रोचक है, उतना ही कठिन
कस-किस देश में प्राकृत शब्दावली मलरूप में अथवा कछ स्थानीय परिवर्तनों के साथ उपलब्ध है, उसके कुछ उदाहरण यहां तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे हैं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org