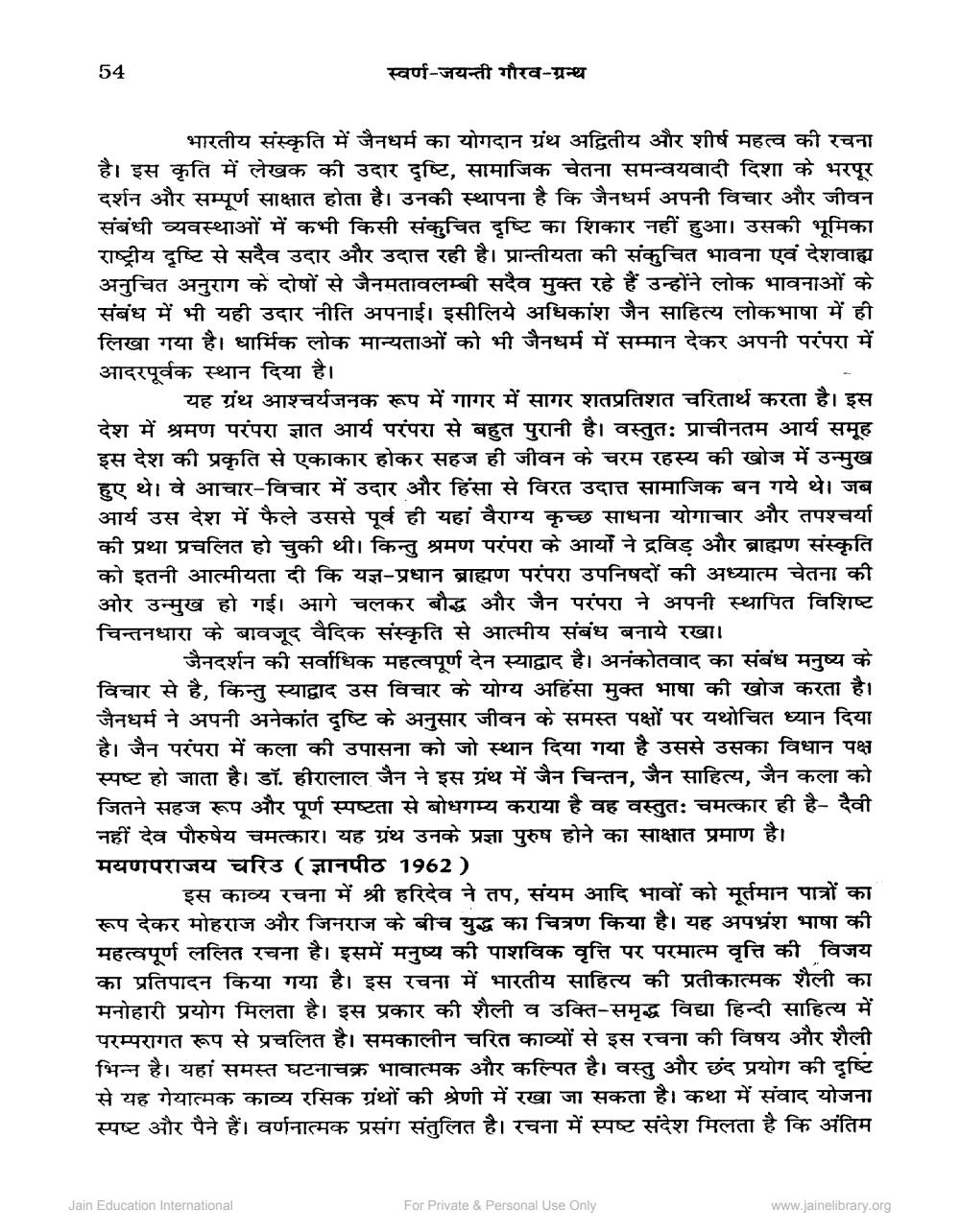________________
54
स्वर्ण जयन्ती गौरव-ग्रन्थ
भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान ग्रंथ अद्वितीय और शीर्ष महत्व की रचना है। इस कृति में लेखक की उदार दृष्टि, सामाजिक चेतना समन्वयवादी दिशा के भरपूर दर्शन और सम्पूर्ण साक्षात होता है। उनकी स्थापना है कि जैनधर्म अपनी विचार और जीवन संबंधी व्यवस्थाओं में कभी किसी संकुचित दृष्टि का शिकार नहीं हुआ। उसकी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टि से सदैव उदार और उदात्त रही है। प्रान्तीयता की संकुचित भावना एवं देशवाह्य अनुचित अनुराग के दोषों से जैनमतावलम्बी सदैव मुक्त रहे हैं उन्होंने लोक भावनाओं के संबंध में भी यही उदार नीति अपनाई । इसीलिये अधिकांश जैन साहित्य लोकभाषा में ही लिखा गया है। धार्मिक लोक मान्यताओं को भी जैनधर्म में सम्मान देकर अपनी परंपरा में आदरपूर्वक स्थान दिया है।
यह ग्रंथ आश्चर्यजनक रूप में गागर में सागर शतप्रतिशत चरितार्थ करता है। इस देश में श्रमण परंपरा ज्ञात आर्य परंपरा से बहुत पुरानी है। वस्तुतः प्राचीनतम आर्य समूह इस देश की प्रकृति से एकाकार होकर सहज ही जीवन के चरम रहस्य की खोज में उन्मुख हुए थे। वे आचार-विचार में उदार और हिंसा से विरत उदात्त सामाजिक बन गये थे। जब आर्य उस देश में फैले उससे पूर्व ही यहां वैराग्य कृच्छ साधना योगाचार और तपश्चर्या की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। किन्तु श्रमण परंपरा के आर्यों ने द्रविड़ और ब्राह्मण संस्कृति को इतनी आत्मीयता दी कि यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण परंपरा उपनिषदों की अध्यात्म चेतना की ओर उन्मुख हो गई। आगे चलकर बौद्ध और जैन परंपरा ने अपनी स्थापित विशिष्ट चिन्तनधारा के बावजूद वैदिक संस्कृति से आत्मीय संबंध बनाये रखा।
जैनदर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन स्याद्वाद है। अनंकोतवाद का संबंध मनुष्य के विचार से है, किन्तु स्याद्वाद उस विचार के योग्य अहिंसा मुक्त भाषा की खोज करता है। जैनधर्म ने अपनी अनेकांत दृष्टि के अनुसार जीवन के समस्त पक्षों पर यथोचित ध्यान दिया है। जैन परंपरा में कला की उपासना को जो स्थान दिया गया है उससे उसका विधान पक्ष स्पष्ट हो जाता है। डॉ. हीरालाल जैन ने इस ग्रंथ में जैन चिन्तन, जैन साहित्य, जैन कला को जितने सहज रूप और पूर्ण स्पष्टता से बोधगम्य कराया है वह वस्तुतः चमत्कार ही है- दैवी नहीं देव पौरुषेय चमत्कार। यह ग्रंथ उनके प्रज्ञा पुरुष होने का साक्षात प्रमाण है। मयणपराजय चरिउ ( ज्ञानपीठ 1962 )
इस काव्य रचना में श्री हरिदेव ने तप, संयम आदि भावों को मूर्तमान पात्रों का रूप देकर मोहराज और जिनराज के बीच युद्ध का चित्रण किया है। यह अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण ललित रचना है। इसमें मनुष्य की पाशविक वृत्ति पर परमात्म वृत्ति की विजय का प्रतिपादन किया गया है। इस रचना में भारतीय साहित्य की प्रतीकात्मक शैली का मनोहारी प्रयोग मिलता है। इस प्रकार की शैली व उक्ति - समृद्ध विद्या हिन्दी साहित्य में परम्परागत रूप से प्रचलित है। समकालीन चरित काव्यों से इस रचना की विषय और शैली भिन्न है। यहां समस्त घटनाचक्र भावात्मक और कल्पित है। वस्तु और छंद प्रयोग की दृष्टि से यह गेयात्मक काव्य रसिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कथा में संवाद योजना स्पष्ट और पैने हैं। वर्णनात्मक प्रसंग संतुलित है। रचना में स्पष्ट संदेश मिलता है कि अंतिम
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org