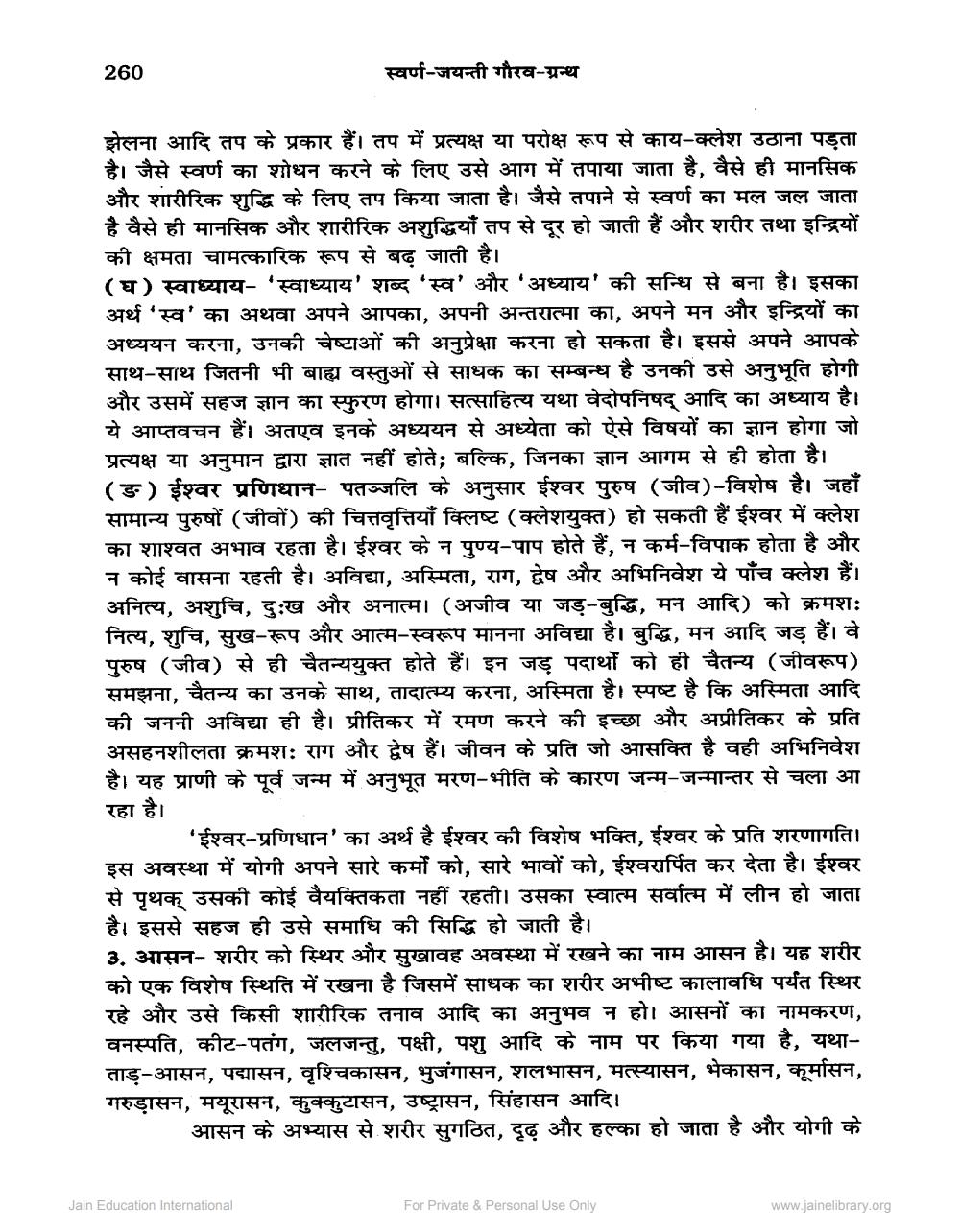________________
260
स्वर्ण-जयन्ती गौरव-ग्रन्थ
झेलना आदि तप के प्रकार हैं। तप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काय-क्लेश उठाना पड़ता है। जैसे स्वर्ण का शोधन करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही मानसिक
और शारीरिक शुद्धि के लिए तप किया जाता है। जैसे तपाने से स्वर्ण का मल जल जाता है वैसे ही मानसिक और शारीरिक अशुद्धियाँ तप से दूर हो जाती हैं और शरीर तथा इन्द्रियों की क्षमता चामत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। (घ) स्वाध्याय- 'स्वाध्याय' शब्द 'स्व' और 'अध्याय' की सन्धि से बना है। इसका अर्थ 'स्व' का अथवा अपने आपका, अपनी अन्तरात्मा का, अपने मन और इन्द्रियों का अध्ययन करना, उनकी चेष्टाओं की अनुप्रेक्षा करना हो सकता है। इससे अपने आपके साथ-साथ जितनी भी बाह्य वस्तुओं से साधक का सम्बन्ध है उनकी उसे अनुभूति होगी
और उसमें सहज ज्ञान का स्फुरण होगा। सत्साहित्य यथा वेदोपनिषद् आदि का अध्याय है। ये आप्तवचन हैं। अतएव इनके अध्ययन से अध्येता को ऐसे विषयों का ज्ञान होगा जो प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा ज्ञात नहीं होते; बल्कि, जिनका ज्ञान आगम से ही होता है। (ङ) ईश्वर प्रणिधान- पतञ्जलि के अनुसार ईश्वर पुरुष (जीव)-विशेष है। जहाँ सामान्य पुरुषों (जीवों) की चित्तवृत्तियाँ क्लिष्ट (क्लेशयुक्त) हो सकती हैं ईश्वर में क्लेश का शाश्वत अभाव रहता है। ईश्वर के न पुण्य-पाप होते हैं, न कर्म-विपाक होता है और न कोई वासना रहती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं। अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्म। (अजीव या जड-बुद्धि, मन आदि) को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख-रूप और आत्म-स्वरूप मानना अविद्या है। बुद्धि, मन आदि जड़ हैं। वे पुरुष (जीव) से ही चैतन्ययुक्त होते हैं। इन जड़ पदार्थों को ही चैतन्य (जीवरूप) समझना, चैतन्य का उनके साथ, तादात्म्य करना, अस्मिता है। स्पष्ट है कि अस्मिता आदि की जननी अविद्या ही है। प्रीतिकर में रमण करने की इच्छा और अप्रीतिकर के प्रति असहनशीलता क्रमशः राग और द्वेष हैं। जीवन के प्रति जो आसक्ति है वही अभिनिवेश है। यह प्राणी के पूर्व जन्म में अनुभूत मरण-भीति के कारण जन्म-जन्मान्तर से चला आ
रहा है।
'ईश्वर-प्रणिधान' का अर्थ है ईश्वर की विशेष भक्ति, ईश्वर के प्रति शरणागति। इस अवस्था में योगी अपने सारे कर्मों को, सारे भावों को, ईश्वरार्पित कर देता है। ईश्वर से पृथक् उसकी कोई वैयक्तिकता नहीं रहती। उसका स्वात्म सर्वात्म में लीन हो जाता है। इससे सहज ही उसे समाधि की सिद्धि हो जाती है। 3. आसन- शरीर को स्थिर और सुखावह अवस्था में रखने का नाम आसन है। यह शरीर को एक विशेष स्थिति में रखना है जिसमें साधक का शरीर अभीष्ट कालावधि पर्यंत स्थिर रहे और उसे किसी शारीरिक तनाव आदि का अनुभव न हो। आसनों का नामकरण, वनस्पति, कीट-पतंग, जलजन्तु, पक्षी, पशु आदि के नाम पर किया गया है, यथाताड़-आसन, पद्मासन, वृश्चिकासन, भुजंगासन, शलभासन, मत्स्यासन, भेकासन, कूर्मासन, गरुड़ासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, उष्ट्रासन, सिंहासन आदि।
आसन के अभ्यास से शरीर सुगठित, दृढ़ और हल्का हो जाता है और योगी के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org