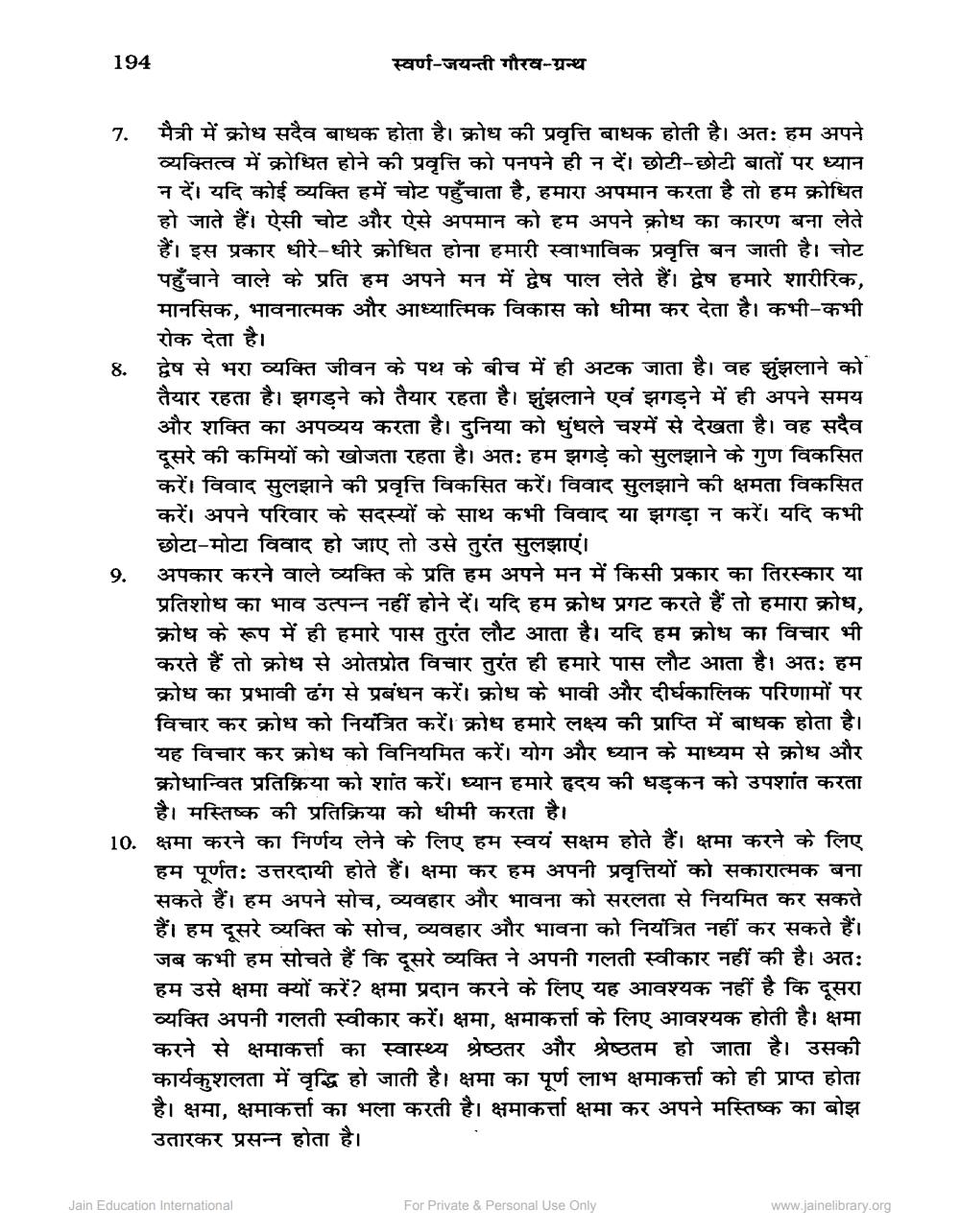________________
194
स्वर्ण-जयन्ती गौरव-ग्रन्थ
7. मैत्री में क्रोध सदैव बाधक होता है। क्रोध की प्रवृत्ति बाधक होती है। अतः हम अपने
व्यक्तित्व में क्रोधित होने की प्रवृत्ति को पनपने ही न दें। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, हमारा अपमान करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी चोट और ऐसे अपमान को हम अपने क्रोध का कारण बना लेते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे क्रोधित होना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। चोट पहुँचाने वाले के प्रति हम अपने मन में द्वेष पाल लेते हैं। द्वेष हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को धीमा कर देता है। कभी-कभी
रोक देता है। 8. द्वेष से भरा व्यक्ति जीवन के पथ के बीच में ही अटक जाता है। वह झुंझलाने को
तैयार रहता है। झगडने को तैयार रहता है। झंझलाने एवं झगडने में ही अपने समय
और शक्ति का अपव्यय करता है। दुनिया को धुंधले चश्में से देखता है। वह सदैव दूसरे की कमियों को खोजता रहता है। अतः हम झगड़े को सुलझाने के गुण विकसित करें। विवाद सुलझाने की प्रवृत्ति विकसित करें। विवाद सुलझाने की क्षमता विकसित करें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कभी विवाद या झगड़ा न करें। यदि कभी छोटा-मोटा विवाद हो जाए तो उसे तुरंत सुलझाएं। अपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति हम अपने मन में किसी प्रकार का तिरस्कार या प्रतिशोध का भाव उत्पन्न नहीं होने दें। यदि हम क्रोध प्रगट करते हैं तो हमारा क्रोध, क्रोध के रूप में ही हमारे पास तुरंत लौट आता है। यदि हम क्रोध का विचार भी करते हैं तो क्रोध से ओतप्रोत विचार तुरंत ही हमारे पास लौट आता है। अतः हम क्रोध का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। क्रोध के भावी और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार कर क्रोध को नियंत्रित करें। क्रोध हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होता है। यह विचार कर क्रोध को विनियमित करें। योग और ध्यान के माध्यम से क्रोध और क्रोधान्वित प्रतिक्रिया को शांत करें। ध्यान हमारे हृदय की धड़कन को उपशांत करता
है। मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को धीमी करता है। 10. क्षमा करने का निर्णय लेने के लिए हम स्वयं सक्षम होते हैं। क्षमा करने के लिए
हम पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। क्षमा कर हम अपनी प्रवृत्तियों को सकारात्मक बना सकते हैं। हम अपने सोच, व्यवहार और भावना को सरलता से नियमित कर सकते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के सोच, व्यवहार और भावना को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जब कभी हम सोचते हैं कि दसरे व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। अतः हम उसे क्षमा क्यों करें? क्षमा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करें। क्षमा, क्षमाकर्ता के लिए आवश्यक होती है। क्षमा करने से क्षमाकर्ता का स्वास्थ्य श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम हो जाता है। उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। क्षमा का पूर्ण लाभ क्षमाकर्ता को ही प्राप्त होता है। क्षमा, क्षमाकर्ता का भला करती है। क्षमाकर्ता क्षमा कर अपने मस्तिष्क का बोझ उतारकर प्रसन्न होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org