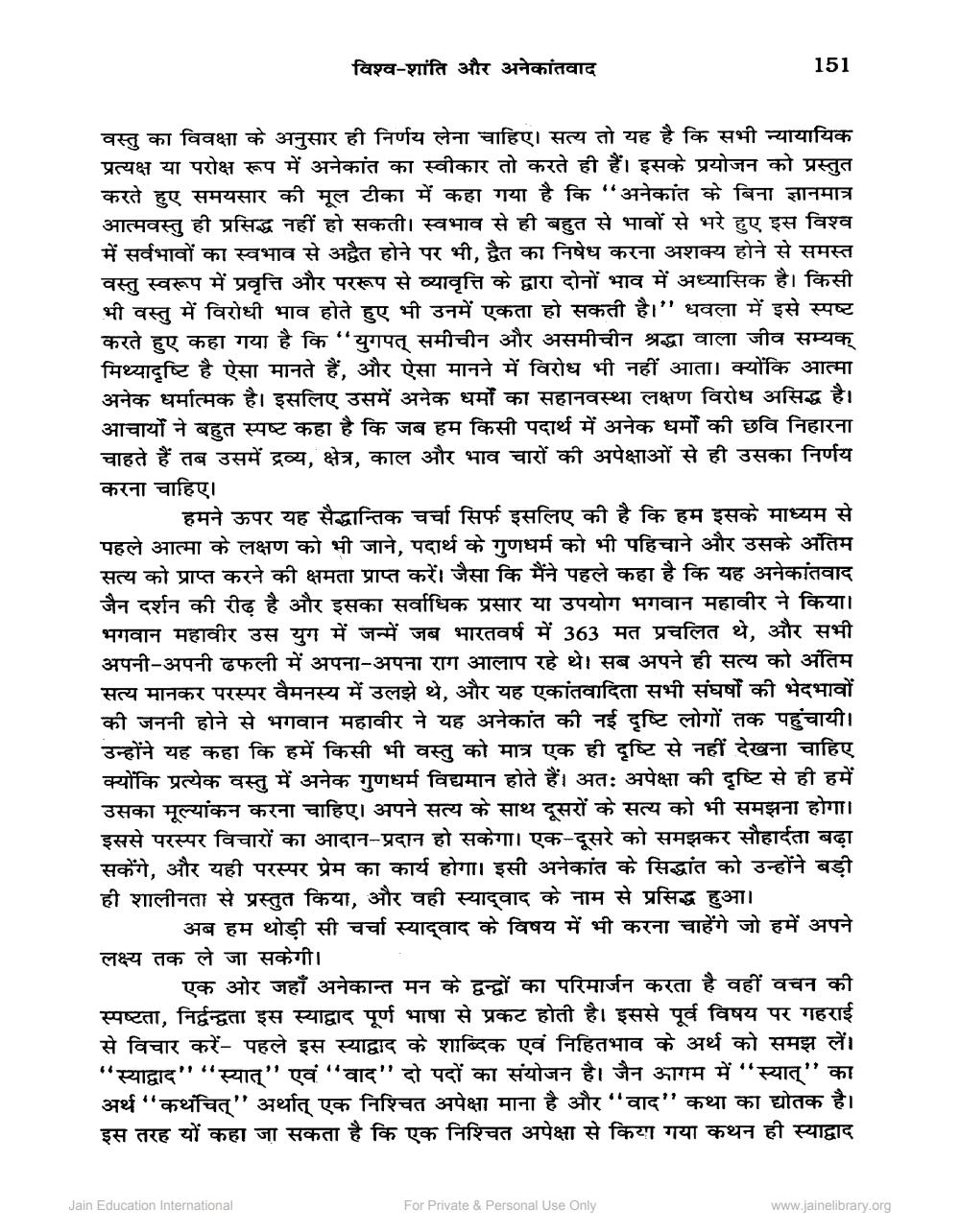________________
विश्व शांति और अनेकांतवाद
वस्तु का विवक्षा के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। सत्य तो यह है कि सभी न्यायायिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनेकांत का स्वीकार तो करते ही हैं। इसके प्रयोजन को प्रस्तुत करते हुए समयसार की मूल टीका में कहा गया है कि "अनेकांत के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्वभावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भाव में अध्यासिक है। किसी भी वस्तु में विरोधी भाव होते हुए भी उनमें एकता हो सकती है।" धवला में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया कि “युगपत् समीचीन और असमीचीन श्रद्धा वाला जीव सम्यक् मिथ्यादृष्टि है ऐसा मानते हैं, और ऐसा मानने में विरोध भी नहीं आता। क्योंकि आत्मा अनेक धर्मात्मक है। इसलिए उसमें अनेक धर्मों का सहानवस्था लक्षण विरोध असिद्ध है। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब हम किसी पदार्थ में अनेक धर्मों की छवि निहारना चाहते हैं तब उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अपेक्षाओं ही उसका निर्णय
करना चाहिए।
151
हमने ऊपर यह सैद्धान्तिक चर्चा सिर्फ इसलिए की है कि हम इसके माध्यम से पहले आत्मा के लक्षण को भी जाने, पदार्थ के गुणधर्म को भी पहिचाने और उसके अंतिम सत्य को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह अनेकांतवाद जैन दर्शन की रीढ़ है और इसका सर्वाधिक प्रसार या उपयोग भगवान महावीर ने किया। भगवान महावीर उस युग में जन्में जब भारतवर्ष में 363 मत प्रचलित थे, और सभी अपनी-अपनी ढफली में अपना-अपना राग आलाप रहे थे। सब अपने ही सत्य को अंतिम सत्य मानकर परस्पर वैमनस्य में उलझे थे, और यह एकांतवादिता सभी संघर्षों की भेदभावों की जननी होने से भगवान महावीर ने यह अनेकांत की नई दृष्टि लोगों तक पहुंचायी। उन्होंने यह कहा कि हमें किसी भी वस्तु को मात्र एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। अतः अपेक्षा की दृष्टि से ही हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अपने सत्य के साथ दूसरों के सत्य को भी समझना होगा। इससे परस्पर विचारों का आदान-प्रदान हो सकेगा। एक-दूसरे को समझकर सौहार्दता बढ़ा सकेंगे, और यही परस्पर प्रेम का कार्य होगा। इसी अनेकांत के सिद्धांत को उन्होंने बड़ी ही शालीनता से प्रस्तुत किया, और वही स्याद्वाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।
अब हम थोड़ी सी चर्चा स्याद्वाद के विषय में भी करना चाहेंगे जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जा सकेगी।
Jain Education International
एक ओर जहाँ अनेकान्त मन के द्वन्द्वों का परिमार्जन करता है वहीं वचन की स्पष्टता, निर्द्वन्द्वता इस स्याद्वाद पूर्ण भाषा से प्रकट होती है। इससे पूर्व विषय पर गहराई से विचार करें- पहले इस स्याद्वाद के शाब्दिक एवं निहितभाव के अर्थ को समझ लें । 'स्याद्वाद" " स्यात् " एवं "वाद" दो पदों का संयोजन है। जैन आगम में " स्यात् " का अर्थ " कथंचित्" अर्थात् एक निश्चित अपेक्षा माना है और "वाद" कथा का द्योतक है। इस तरह यों कहा जा सकता है कि एक निश्चित अपेक्षा से किया गया कथन ही स्याद्वाद
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org