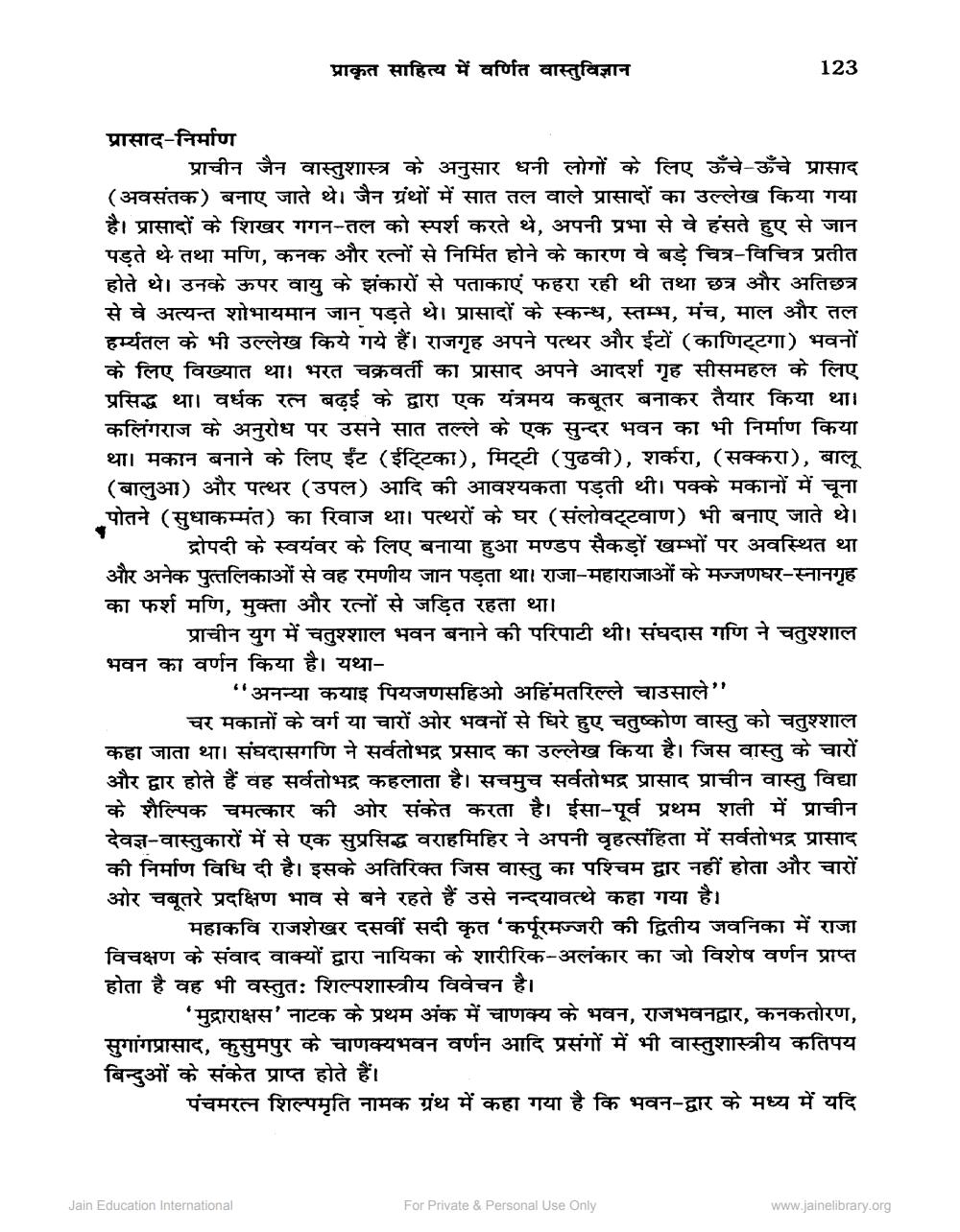________________
प्राकृत साहित्य में वर्णित वास्तुविज्ञान
123
प्रासाद-निर्माण
प्राचीन जैन वास्तुशास्त्र के अनुसार धनी लोगों के लिए ऊँचे-ऊँचे प्रासाद (अवसंतक) बनाए जाते थे। जैन ग्रंथों में सात तल वाले प्रासादों का उल्लेख किया गया है। प्रासादों के शिखर गगन-तल को स्पर्श करते थे, अपनी प्रभा से वे हंसते हुए से जान पड़ते थे तथा मणि, कनक और रत्नों से निर्मित होने के कारण वे बड़े चित्र-विचित्र प्रतीत होते थे। उनके ऊपर वायु के झंकारों से पताकाएं फहरा रही थी तथा छत्र और अतिछत्र से वे अत्यन्त शोभायमान जान पड़ते थे। प्रासादों के स्कन्ध, स्तम्भ, मंच, माल और तल हर्म्यतल के भी उल्लेख किये गये हैं। राजगृह अपने पत्थर और ईटों (काणिट्टगा) भवनों के लिए विख्यात था। भरत चक्रवर्ती का प्रासाद अपने आदर्श गृह सीसमहल के लिए प्रसिद्ध था। वर्धक रत्न बढ़ई के द्वारा एक यंत्रमय कबूतर बनाकर तैयार किया था। कलिंगराज के अनुरोध पर उसने सात तल्ले के एक सुन्दर भवन का भी निर्माण किया था। मकान बनाने के लिए ईंट (ईट्टिका), मिट्टी (पुढवी), शर्करा, (सक्करा), बालू (बालुआ) और पत्थर (उपल) आदि की आवश्यकता पड़ती थी। पक्के मकानों में चूना पोतने (सुधाकम्मत) का रिवाज था। पत्थरों के घर (संलोवट्टवाण) भी बनाए जाते थे।
द्रोपदी के स्वयंवर के लिए बनाया हुआ मण्डप सैकड़ों खम्भों पर अवस्थित था और अनेक पुत्तलिकाओं से वह रमणीय जान पड़ता था। राजा-महाराजाओं के मज्जणघर-स्नानगृह का फर्श मणि. मक्ता और रत्नों से जडित रहता था।
प्राचीन युग में चतुश्शाल भवन बनाने की परिपाटी थी। संघदास गणि ने चतुश्शाल भवन का वर्णन किया है। यथा
"अनन्या कयाइ पियजणसहिओ अहिंमतरिल्ले चाउसाले"
चर मकानों के वर्ग या चारों ओर भवनों से घिरे हुए चतुष्कोण वास्तु को चतुश्शाल कहा जाता था। संघदासगणि ने सर्वतोभद्र प्रसाद का उल्लेख किया है। जिस वास्तु के चारों और द्वार होते हैं वह सर्वतोभद्र कहलाता है। सचमुच सर्वतोभद्र प्रासाद प्राचीन वास्तु विद्या के शैल्पिक चमत्कार की ओर संकेत करता है। ईसा-पूर्व प्रथम शती में प्राचीन देवज्ञ-वास्तुकारों में से एक सुप्रसिद्ध वराहमिहिर ने अपनी वृहत्संहिता में सर्वतोभद्र प्रासाद की निर्माण विधि दी है। इसके अतिरिक्त जिस वास्तु का पश्चिम द्वार नहीं होता और चारों ओर चबूतरे प्रदक्षिण भाव से बने रहते हैं उसे नन्दयावत्थे कहा गया है।
महाकवि राजशेखर दसवीं सदी कृत 'कर्पूरमज्जरी की द्वितीय जवनिका में राजा विचक्षण के संवाद वाक्यों द्वारा नायिका के शारीरिक-अलंकार का जो विशेष वर्णन प्राप्त होता है वह भी वस्तुतः शिल्पशास्त्रीय विवेचन है।
'मुद्राराक्षस' नाटक के प्रथम अंक में चाणक्य के भवन, राजभवनद्वार, कनकतोरण, सगांगप्रासाद, कसमपुर के चाणक्यभवन वर्णन आदि प्रसंगों में भी वास्तशास्त्रीय कतिपय बिन्दुओं के संकेत प्राप्त होते हैं।
पंचमरत्न शिल्पमति नामक ग्रंथ में कहा गया है कि भवन-द्वार के मध्य में यदि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org