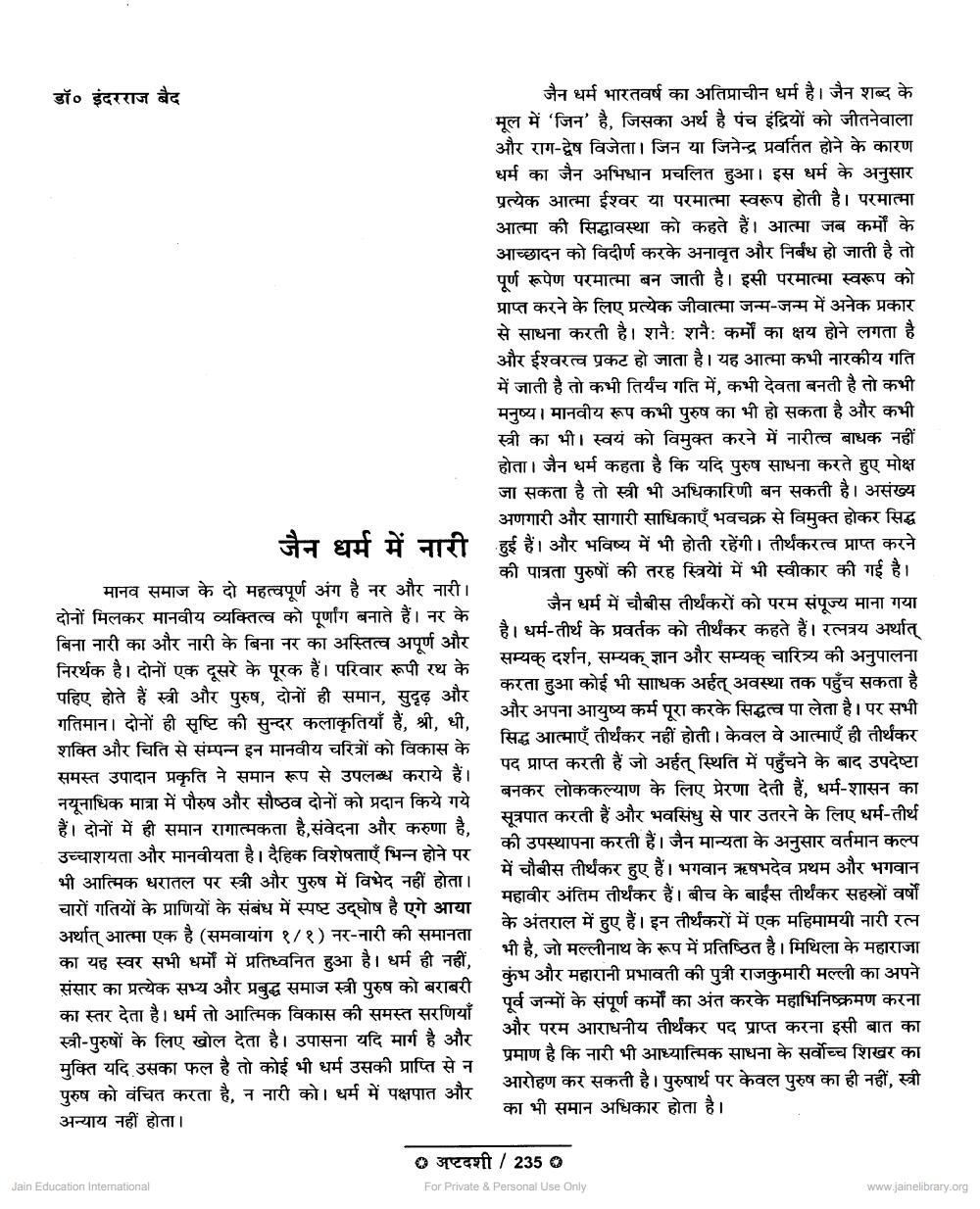________________
डॉ० इंदरराज बैद
मानव समाज के दो महत्वपूर्ण अंग है नर और नारी। दोनों मिलकर मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णांग बनाते हैं। नर के बिना नारी का और नारी के बिना नर का अस्तित्व अपूर्ण और निरर्थक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार रूपी रथ के पहिए होते हैं स्त्री और पुरुष, दोनों ही समान, सुदृढ़ और गतिमान। दोनों ही सृष्टि की सुन्दर कलाकृतियाँ हैं, श्री, धी, शक्ति और चिति से सम्पन्न इन मानवीय चरित्रों को विकास के समस्त उपादान प्रकृति ने समान रूप से उपलब्ध कराये हैं। नयूनाधिक मात्रा में पौरुष और सौष्ठव दोनों को प्रदान किये गये हैं। दोनों में ही समान रागात्मकता है,संवेदना और करुणा है, उच्चाशयता और मानवीयता है। दैहिक विशेषताएँ भिन्न होने पर भी आत्मिक धरातल पर स्त्री और पुरुष में विभेद नहीं होता। चारों गतियों के प्राणियों के संबंध में स्पष्ट उद्घोष है एगे आया अर्थात् आत्मा एक है (समवायांग १/१) नर-नारी की समानता का यह स्वर सभी धर्मों में प्रतिध्वनित हुआ है। धर्म ही नहीं, संसार का प्रत्येक सभ्य और प्रबुद्ध समाज स्त्री पुरुष को बराबरी का स्तर देता है। धर्म तो आत्मिक विकास की समस्त सरणियाँ स्त्री-पुरुषों के लिए खोल देता है। उपासना यदि मार्ग है और मुक्ति यदि उसका फल है तो कोई भी धर्म उसकी प्राप्ति से न पुरुष को वंचित करता है, न नारी को। धर्म में पक्षपात और अन्याय नहीं होता।
जैन धर्म भारतवर्ष का अतिप्राचीन धर्म है। जैन शब्द के मूल में 'जिन' है, जिसका अर्थ है पंच इंद्रियों को जीतनेवाला
और राग-द्वेष विजेता। जिन या जिनेन्द्र प्रवर्तित होने के कारण धर्म का जैन अभिधान प्रचलित हुआ। इस धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा ईश्वर या परमात्मा स्वरूप होती है। परमात्मा आत्मा की सिद्धावस्था को कहते हैं। आत्मा जब कर्मों के आच्छादन को विदीर्ण करके अनावृत और निर्बध हो जाती है तो पूर्ण रूपेण परमात्मा बन जाती है। इसी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा जन्म-जन्म में अनेक प्रकार से साधना करती है। शनैः शनैः कर्मों का क्षय होने लगता है
और ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। यह आत्मा कभी नारकीय गति में जाती है तो कभी तिर्यंच गति में, कभी देवता बनती है तो कभी मनुष्य। मानवीय रूप कभी पुरुष का भी हो सकता है और कभी स्त्री का भी। स्वयं को विमुक्त करने में नारीत्व बाधक नहीं होता। जैन धर्म कहता है कि यदि पुरुष साधना करते हुए मोक्ष जा सकता है तो स्त्री भी अधिकारिणी बन सकती है। असंख्य अणगारी और सागारी साधिकाएँ भवचक्र से विमुक्त होकर सिद्ध हुई हैं। और भविष्य में भी होती रहेंगी। तीर्थंकरत्व प्राप्त करने की पात्रता पुरुषों की तरह स्त्रियों में भी स्वीकार की गई है।
जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों को परम संपूज्य माना गया है। धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। रत्नत्रय अर्थात् सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की अनुपालना करता हुआ कोई भी साधक अर्हत् अवस्था तक पहुँच सकता है
और अपना आयुष्य कर्म पूरा करके सिद्धत्व पा लेता है। पर सभी सिद्ध आत्माएँ तीर्थंकर नहीं होती। केवल वे आत्माएँ ही तीर्थंकर पद प्राप्त करती हैं जो अर्हत् स्थिति में पहुँचने के बाद उपदेष्टा बनकर लोककल्याण के लिए प्रेरणा देती हैं, धर्म-शासन का सूत्रपात करती हैं और भवसिंधु से पार उतरने के लिए धर्म-तीर्थ की उपस्थापना करती हैं। जैन मान्यता के अनुसार वर्तमान कल्प में चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। भगवान ऋषभदेव प्रथम और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं। बीच के बाईंस तीर्थंकर सहस्रों वर्षों के अंतराल में हुए हैं। इन तीर्थंकरों में एक महिमामयी नारी रत्न भी है, जो मल्लीनाथ के रूप में प्रतिष्ठित है। मिथिला के महाराजा कुंभ और महारानी प्रभावती की पुत्री राजकुमारी मल्ली का अपने पूर्व जन्मों के संपूर्ण कर्मों का अंत करके महाभिनिष्क्रमण करना
और परम आराधनीय तीर्थंकर पद प्राप्त करना इसी बात का प्रमाण है कि नारी भी आध्यात्मिक साधना के सर्वोच्च शिखर का आरोहण कर सकती है। पुरुषार्थ पर केवल पुरुष का ही नहीं, स्त्री का भी समान अधिकार होता है।
० अष्टदशी / 2350 For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org