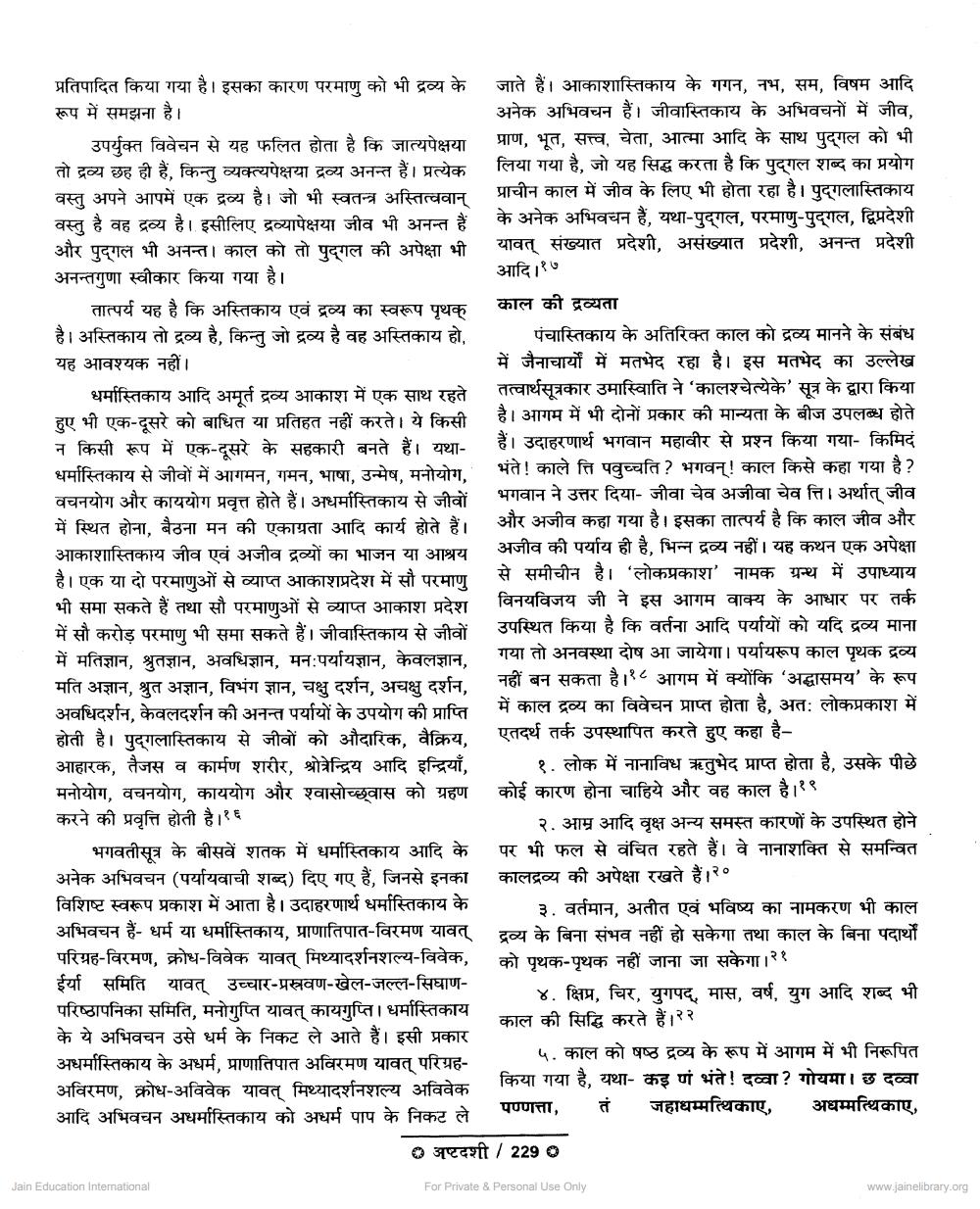________________
प्रतिपादित किया गया है। इसका कारण परमाणु को भी द्रव्य के रूप में समझना है।
उपर्युक्त विवेचन से यह फलित होता है कि जात्यपेक्षया तो द्रव्य छह ही हैं, किन्तु व्यक्त्यपेक्षया द्रव्य अनन्त है। प्रत्येक अपने आपमें एक द्रव्य है। जो भी स्वतन्त्र अस्तित्ववान् वस्तु वस्तु है वह द्रव्य है इसीलिए द्रव्यापेक्षया जीव भी अनन्त हैं। और पुद्गल भी अनन्त । काल को तो पुद्गल की अपेक्षा भी अनन्तगुणा स्वीकार किया गया है।
तात्पर्य यह है कि अस्तिकाय एवं द्रव्य का स्वरूप पृथक् है। अस्तिकाय तो द्रव्य है, किन्तु जो द्रव्य है वह अस्तिकाय हो, यह आवश्यक नहीं ।
धर्मास्तिकाय आदि अमूर्त द्रव्य आकाश में एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरे को बाधित या प्रतिहत नहीं करते। ये किसी न किसी रूप में एक-दूसरे के सहकारी बनते हैं। यथाधर्मास्तिकाय से जीवों में आगमन, गमन, भाषा, उन्मेष, मनोयोग, वचनयोग और काययोग प्रवृत्त होते हैं । अधर्मास्तिकाय से जीवों में स्थित होना, बैठना मन की एकाग्रता आदि कार्य होते हैं। आकाशास्तिकाय जीव एवं अजीव द्रव्यों का भाजन या आश्रय है। एक या दो परमाणुओं से व्याप्त आकाशप्रदेश में सौ परमाणु भी समा सकते हैं तथा सौ परमाणुओं से व्याप्त आकाश प्रदेश में सौ करोड़ परमाणु भी समा सकते हैं जीवास्तिकाय से जीवों में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन: पर्यायज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन की अनन्त पर्यायों के उपयोग की प्राप्ति होती है। पुद्गलास्तिकाय से जीवों को औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस व कार्मण शरीर श्रोत्रेन्द्रिय आदि इन्द्रियाँ, मनोयोग, वचनयोग, काययोग और श्वासोच्छ्वास को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है।१६
भगवतीसूत्र के बीसवें शतक में धर्मास्तिकाय आदि के अनेक अभिवचन (पर्यायवाची शब्द) दिए गए हैं, जिनसे इनका विशिष्ट स्वरूप प्रकाश में आता है। उदाहरणार्थ धर्मास्तिकाय के अभिवचन है- धर्म या धर्मास्तिकाय, प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह - विरमण, क्रोध - विवेक यावत् मिथ्यादर्शनशल्य-विवेक, ईर्ष्या समिति यावत् उच्चार-प्रस्रवण खेल जल्ल- सिघाणपरिष्ठापनिका समिति, मनोगुप्ति यावत् कायगुप्ति । धर्मास्तिकाय
ये अभिवचन उसे धर्म के निकट ले आते हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के अधर्म, प्राणातिपात अविरमण यावत् परिग्रहअविरमण, क्रोध- अविवेक यावत् मिथ्यादर्शनशल्य अविवेक आदि अभिवचन अधर्मास्तिकाय को अधर्म पाप के निकट ले
Jain Education International
जाते हैं। आकाशास्तिकाय के गगन, नभ, सम, विषम आदि अनेक अभिवचन हैं। जीवास्तिकाय के अभिवचनों में जीव, प्राण, भूत, सत्त्व, चेता, आत्मा आदि के साथ पुद्गल को भी लिया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि पुद्गल शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में जीव के लिए भी होता रहा है। पुद्गलास्तिकाय के अनेक अभिवचन हैं, यथा- पुद्गल, परमाणु- पुद्गल, द्विप्रदेशी यावत् संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनन्त प्रदेशी आदि । १७
काल की द्रव्यता
पंचास्तिकाय के अतिरिक्त काल को द्रव्य मानने के संबंध में जैनाचार्यों में मतभेद रहा है। इस मतभेद का उल्लेख तत्वार्थसूत्रकार उमास्विाति ने 'कालश्चेत्येके' सूत्र के द्वारा किया है । आगम में भी दोनों प्रकार की मान्यता के बीज उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ भगवान महावीर से प्रश्न किया गया किमिदं भंते! काले त्ति पवुच्चति ? भगवन्! काल किसे कहा गया है ? भगवान ने उत्तर दिया- जीवा चेव अजीवा चेव त्ति । अर्थात् जीव और अजीव कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि काल जीव और अजीव की पर्याय ही है, भिन्न द्रव्य नहीं । यह कथन एक अपेक्षा से समीचीन है । 'लोकप्रकाश' नामक ग्रन्थ में उपाध्याय विनयविजय जी ने इस आगम वाक्य के आधार पर तर्क उपस्थित किया है कि वर्तना आदि पर्यायों को यदि द्रव्य माना गया तो अनवस्था दोष आ जायेगा। पर्यायरूप काल पृथक द्रव्य नहीं बन सकता है। १८ आगम में क्योंकि 'अद्धासमय' के रूप में काल द्रव्य का विवेचन प्राप्त होता है, अत: लोकप्रकाश में एतदर्थ तर्क उपस्थापित करते हुए कहा है
१. लोक में नानाविध ऋतुभेद प्राप्त होता है, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिये और वह काल है। १९
२. आम्र आदि वृक्ष अन्य समस्त कारणों के उपस्थित होने पर भी फल से वंचित रहते हैं। वे नानाशक्ति से समन्वित कालद्रव्य की अपेक्षा रखते हैं । २०
३. वर्तमान, अतीत एवं भविष्य का नामकरण भी काल द्रव्य के बिना संभव नहीं हो सकेगा तथा काल के बिना पदार्थों को पृथक-पृथक नहीं जाना जा सकेगा । २१
४. क्षिम, चिर, युगपद् मास, वर्ष, युग आदि शब्द भी काल की सिद्धि करते हैं। २२
५. काल को षष्ठ द्रव्य के रूप में आगम में भी निरूपित किया गया है, यथा- कड् णं भंते! दव्वा ? गोयमा । छ दव्वा पण्णत्ता, तं जहाधम्मत्थिकाए, अथम्मत्थिकाए,
छ अष्टदशी / 229
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org