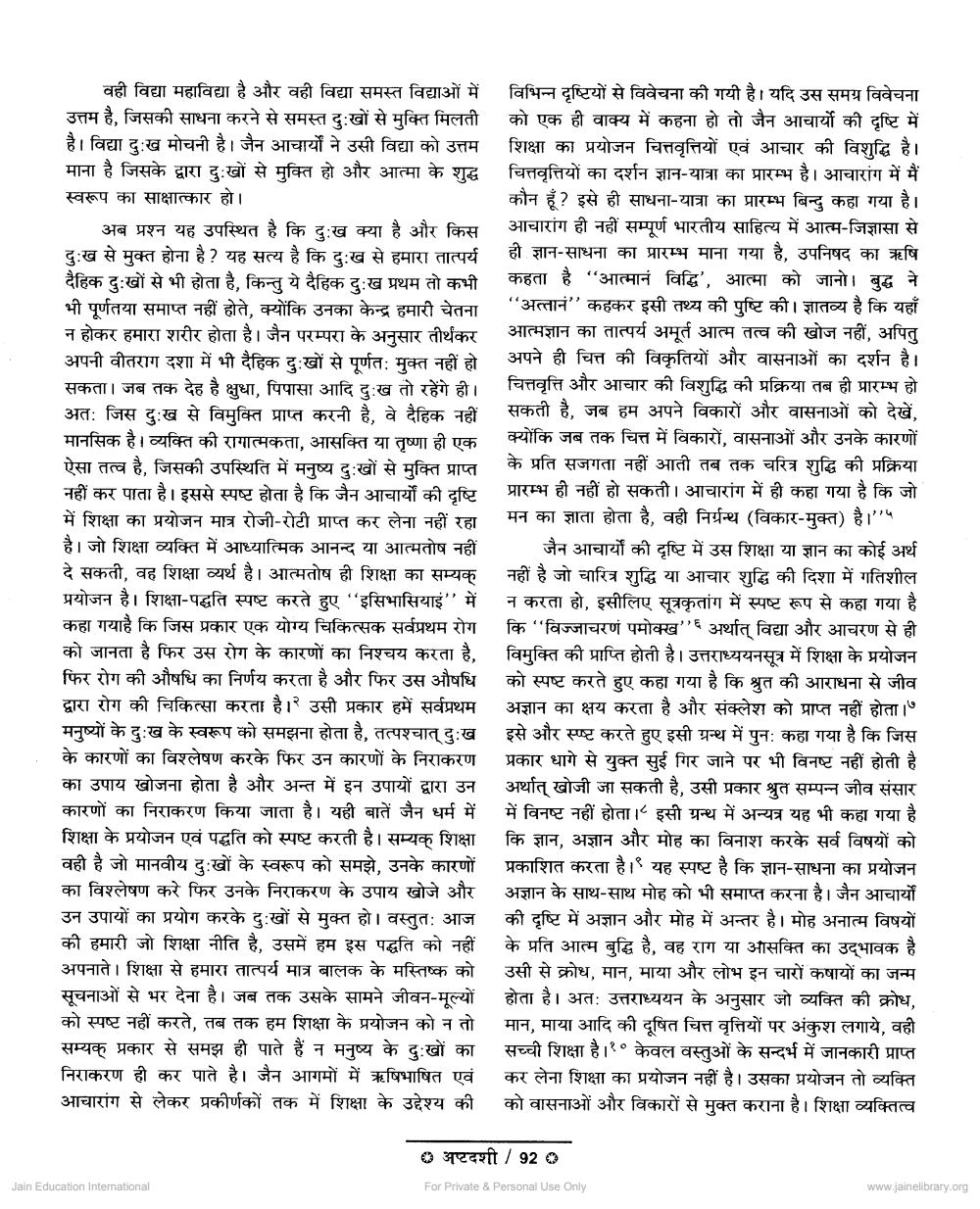________________
वही विद्या महाविद्या है और वही विद्या समस्त विद्याओं में उत्तम है, जिसकी साधना करने से समस्त दुःखों से मुक्ति मिलती है । विद्या दुःख मोचनी है। जैन आचार्यों ने उसी विद्या को उत्तम माना है जिसके द्वारा दुःखों से मुक्ति हो और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो ।
I
अब प्रश्न यह उपस्थित है कि दुःख क्या है और किस दुःख से मुक्त होना है? यह सत्य है कि दुःख से हमारा तात्पर्य दैहिक दुःखों से भी होता है, किन्तु ये दैहिक दुःख प्रथम तो कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं होते, क्योंकि उनका केन्द्र हमारी चेतना न होकर हमारा शरीर होता है जैन परम्परा के अनुसार तीर्थंकर अपनी वीतराग दशा में भी दैहिक दुःखों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। जब तक देह है क्षुधा, पिपासा आदि दुःख तो रहेंगे ही। अतः जिस दुःख से विमुक्ति प्राप्त करनी है, वे दैहिक नहीं मानसिक है। व्यक्ति की रागात्मकता, आसक्ति या तृष्णा ही एक ऐसा तत्व है, जिसकी उपस्थिति में मनुष्य दुःखों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन आचार्यों की दृष्टि में शिक्षा का प्रयोजन मात्र रोजी-रोटी प्राप्त कर लेना नहीं रहा है । जो शिक्षा व्यक्ति में आध्यात्मिक आनन्द या आत्मतोष नहीं दे सकती, वह शिक्षा व्यर्थ है। आत्मतोष ही शिक्षा का सम्यक् प्रयोजन है शिक्षा पद्धति स्पष्ट करते हुए "इसिभासियाई" में कहा गया है कि जिस प्रकार एक योग्य चिकित्सक सर्वप्रथम रोग को जानता है फिर उस रोग के कारणों का निश्चय करता है, फिर रोग की औषधि का निर्णय करता है और फिर उस औषधि द्वारा रोग की चिकित्सा करता है । उसी प्रकार हमें सर्वप्रथम मनुष्यों के दुःख के स्वरूप को समझना होता है, तत्पश्चात् दुःख के कारणों का विश्लेषण करके फिर उन कारणों के निराकरण का उपाय खोजना होता है और अन्त में इन उपायों द्वारा उन कारणों का निराकरण किया जाता है। यही बातें जैन धर्म में शिक्षा के प्रयोजन एवं पद्धति को स्पष्ट करती है। सम्यक् शिक्षा वही है जो मानवीय दुःखों के स्वरूप को समझे, उनके कारणों का विश्लेषण करे फिर उनके निराकरण के उपाय खोजे और उन उपायों का प्रयोग करके दुःखों से मुक्त हो । वस्तुतः आज की हमारी जो शिक्षा नीति है, उसमें हम इस पद्धति को नहीं अपनाते । शिक्षा से हमारा तात्पर्य मात्र बालक के मस्तिष्क को सूचनाओं से भर देना है। जब तक उसके सामने जीवन-मूल्यों को स्पष्ट नहीं करते, तब तक हम शिक्षा के प्रयोजन को न तो सम्यक् प्रकार से समझ ही पाते हैं न मनुष्य के दुःखों का निराकरण ही कर पाते है। जैन आगमों में ऋषिभाषित एवं आचारांग से लेकर प्रकीर्णकों तक में शिक्षा के उद्देश्य की
Jain Education International
विभिन्न दृष्टियों से विवेचना की गयी है। यदि उस समग्र विवेचना को एक ही वाक्य में कहना हो तो जैन आचार्यो की दृष्टि में शिक्षा का प्रयोजन चित्तवृत्तियों एवं आचार की विशुद्धि है। चित्तवृत्तियों का दर्शन ज्ञान- यात्रा का प्रारम्भ है। आचारांग में मैं कौन हूँ? इसे ही साधना - यात्रा का प्रारम्भ बिन्दु कहा गया है। आचारांग ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में आत्म-जिज्ञासा से ही ज्ञान-साधना का प्रारम्भ माना गया है, उपनिषद का ऋषि कहता है "आत्मानं विद्धि' आत्मा को जानो बुद्ध ने " अत्तानं " कहकर इसी तथ्य की पुष्टि की। ज्ञातव्य है कि यहाँ आत्मज्ञान का तात्पर्य अमूर्त आत्म तत्व की खोज नहीं, अपितु अपने ही चित्त की विकृतियों और वासनाओं का दर्शन है। चित्तवृत्ति और आधार की विशुद्धि की प्रक्रिया तब ही प्रारम्भ हो सकती है, जब हम अपने विकारों और वासनाओं को देखें, क्योंकि जब तक चित्त में विकारों, वासनाओं और उनके कारणों के प्रति सजगता नहीं आती तब तक चरित्र शुद्धि की प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं हो सकती। आचारांग में ही कहा गया है कि जो मन का ज्ञाता होता है, वही निर्ग्रन्थ ( विकार मुक्त) है। "५
जैन आचार्यों की दृष्टि में उस शिक्षा या ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जो चारित्र शुद्धि या आचार शुद्धि की दिशा में गतिशील न करता हो, इसीलिए सूत्रकृतांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है। कि "विज्जाचरणं पमोक्ख६ अर्थात् विद्या और आचरण से ही विमुक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तराध्ययनसूत्र में शिक्षा के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान का क्षय करता है और संक्लेश को प्राप्त नहीं होता । ७ इसे और स्पष्ट करते हुए इसी ग्रन्थ में पुन: कहा गया है कि जिस प्रकार धागे से युक्त सुई गिर जाने पर भी विनष्ट नहीं होती है। अर्थात् खोजी जा सकती है, उसी प्रकार श्रुत सम्पन्न जीव संसार में विनष्ट नहीं होता।' इसी ग्रन्थ में अन्यत्र यह भी कहा गया है। कि ज्ञान, अज्ञान और मोह का विनाश करके सर्व विषयों को प्रकाशित करता है। यह स्पष्ट है कि ज्ञान-साधना का प्रयोजन अज्ञान के साथ-साथ मोह को भी समाप्त करना है। जैन आचार्यों की दृष्टि में अज्ञान और मोह में अन्तर है मोह अनात्म विषयों के प्रति आत्म बुद्धि है, वह राग या आसक्ति का उद्भावक है उसी से क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों का जन्म होता है अतः उत्तराध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति की क्रोध, मान, माया आदि की दूषित चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगाये, वही सच्ची शिक्षा है। केवल वस्तुओं के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेना शिक्षा का प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन तो व्यक्ति को वासनाओं और विकारों से मुक्त कराना है। शिक्षा व्यक्तित्व
० अष्टदशी / 920
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org