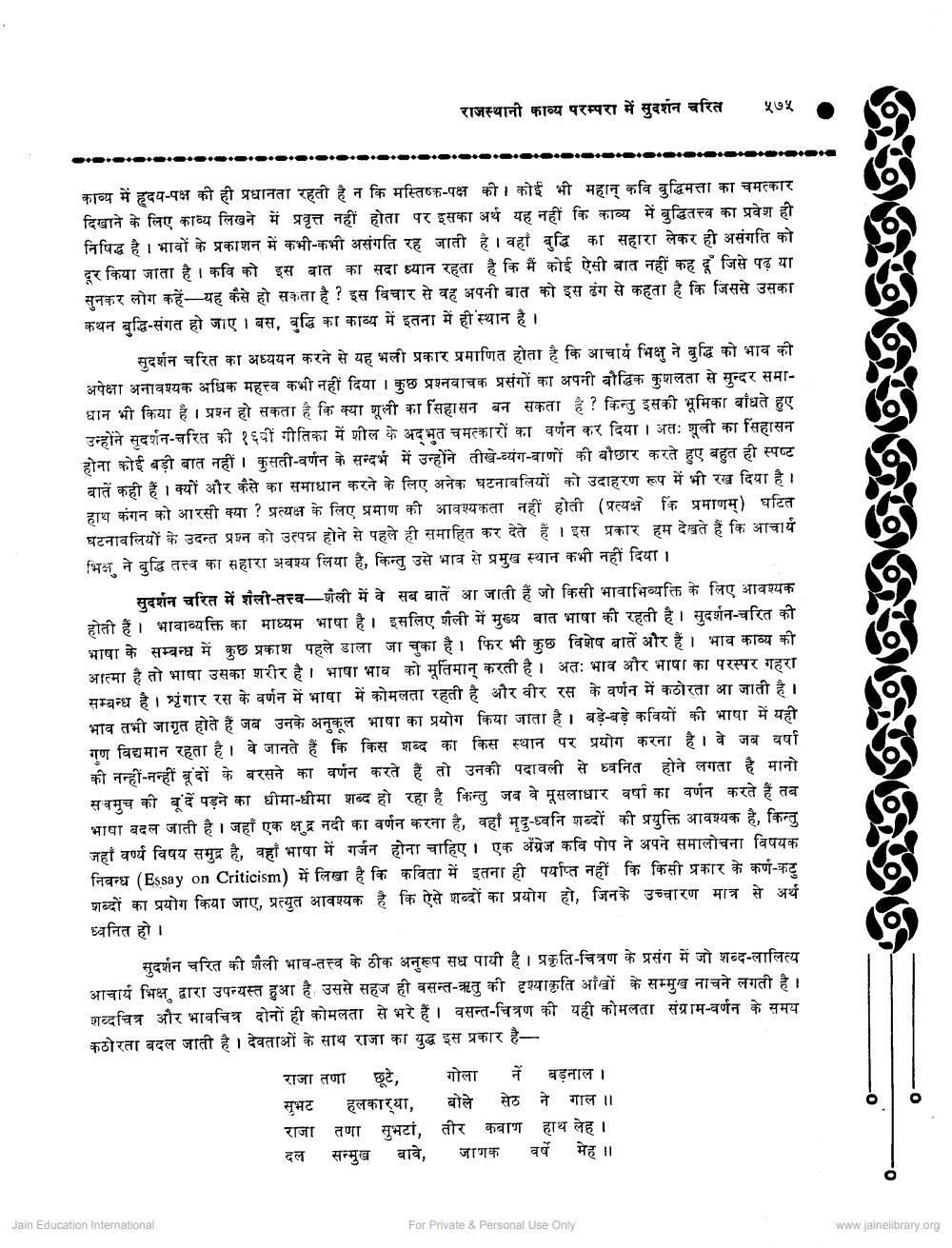________________
राजस्थानी काव्य परम्परा में सुदर्शन चरित
1
काव्य में हृदय-पक्ष की ही प्रधानता रहती है न कि मस्तिष्क पक्ष को कोई भी महान कवि बुद्धिमत्ता का चमत्कार दिखाने के लिए काव्य लिखने में प्रवृत्त नहीं होता पर इसका अर्थ यह नहीं कि काव्य में बुद्धितत्त्व का प्रवेश ही निषिद्ध है। भावों के प्रकाशन में कभी-कभी असंगति रह जाती है। वहाँ बुद्धि का सहारा लेकर ही असंगति को दूर किया जाता है । कवि को इस बात का सदा ध्यान रहता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह दूँ जिसे पढ़ या सुनकर लोग कहें - यह कैसे हो सकता है ? इस विचार से वह अपनी बात को इस ढंग से कहता है कि जिससे उसका कथन बुद्धि-संगत हो जाए। बस, बुद्धि का काव्य में इतना में ही स्थान है ।
सुदर्शन चरित का अध्ययन करने से यह भली प्रकार प्रमाणित होता है कि आचार्य भिक्षु ने बुद्धि को भाव की अपेक्षा अनावश्यक अधिक महत्त्व कभी नहीं दिया। कुछ प्रश्नवाचक प्रसंगों का अपनी बौद्धिक कुशलता से सुन्दर समाधान भी किया है। प्रश्न हो सकता है कि क्या शूली का सिंहासन बन सकता है ? किन्तु इसकी भूमिका बांधते हुए उन्होंनेकी १६ गीतिका में फीस के अद्भुत चमत्कारों का वर्णन कर दिया। अतः मूली का सिंहासन होना कोई बड़ी बात नहीं । कुसती वर्णन के सन्दर्भ में उन्होंने तीखे व्यंग-बाणों की बौछार करते हुए बहुत ही स्पष्ट बातें कही हैं। क्यों और कैसे का समाधान करने के लिए अनेक घटनावलियों को उदाहरण रूप में भी रख दिया है । हाथ कंगन को आरसी क्या ? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ( प्रत्यक्ष किं प्रमाणम् ) घटित घटनावलियों के उदन्त प्रश्न को उत्पन्न होने से पहले ही समाहित कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भिक्षु ने बुद्धि तत्त्व का सहारा अवश्य लिया है, किन्तु उसे भाव से प्रमुख स्थान कभी नहीं दिया ।
Jain Education International
सब बातें आ जाती हैं जो किसी भावाभिव्यक्ति के लिए आवश्यक इसलिए शैली में मुख्य बात भाषा की रहती है। सुदर्शन-चरित की जा चुका है। फिर भी कुछ विशेष बातें और हैं। भाव काव्य की अतः भाव और भाषा का परस्पर गहरा
सुदर्शन चरित में शैली-तस्य शैली में वे होती है। भावाव्यक्ति का माध्यम भाषा है भाषा के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पहले डाला आत्मा है तो भाषा उसका शरीर है। भाषा भाव को मूर्तिमान् करती है। सम्बन्ध है । शृंगार रस के वर्णन में भाषा में कोमलता रहती है और वीर रस के वर्णन में कठोरता आ जाती है । भाव तभी जागृत होते हैं जब उनके अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है। बड़े-बड़े कवियों की भाषा में यही गुण विद्यमान रहता है । वे जानते हैं कि किस शब्द का किस स्थान पर प्रयोग करना है । वे जब वर्षा की नन्हीं-नन्हीं बूंदों के बरसने का वर्णन करते हैं तो उनकी पदावली से ध्वनित होने लगता है मानो समुच की बूंदें पड़ने का धीमा-धीमा शब्द हो रहा है किन्तु जब वे मूसलाधार वर्षा का वर्णन करते हैं तब भाषा बदल जाती है । जहाँ एक क्षुद्र नदी का वर्णन करना है, वहाँ मृदु-ध्वनि शब्दों की प्रयुक्ति आवश्यक है, किन्तु होना चाहिए। एक अंग्रेज कवि पोप ने अपने समालोचना विषयक कविता में इतना ही पर्याप्त नहीं कि किसी प्रकार के कर्ण-न कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जिनके उच्चारण मात्र से अर्थ
जहाँ वर्ण्य विषय समुद्र है, वहाँ भाषा में गर्जन निबन्ध (Essay on Criticism) में लिखा है कि शब्दों का प्रयोग किया जाए, प्रत्युत आवश्यक है ध्वनित हो ।
सुदर्शन चरित की शैली भाव-तत्व के ठीक अनुरूप सच पायी है। प्रकृति-चित्रण के प्रसंग में जो शब्दलालित्य आचार्य भिक्षु द्वारा उपन्यस्त हुआ है उससे सहज ही वसन्त की दृस्याकृतियों के सम्मु नाचने लगती है। शब्दचित्र और भावचित्र दोनों ही कोमलता से भरे हैं। वसन्त-चित्रण की यही कोमलता संग्राम-वर्णन के समय कठोरता बदल जाती है। देवताओं के साथ राजा का युद्ध इस प्रकार है
नॅ बड़नाल ।
५७५
राजा तणा सुभट
छूटे, गोला हलकार्या, बोले सेठ राजा तणा सुभटां, तीर कबाग बावे, जाणक
दल सन्मुख
+++++
ने गाल ॥
हाथ लेह |
वर्षे मेह ॥
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.