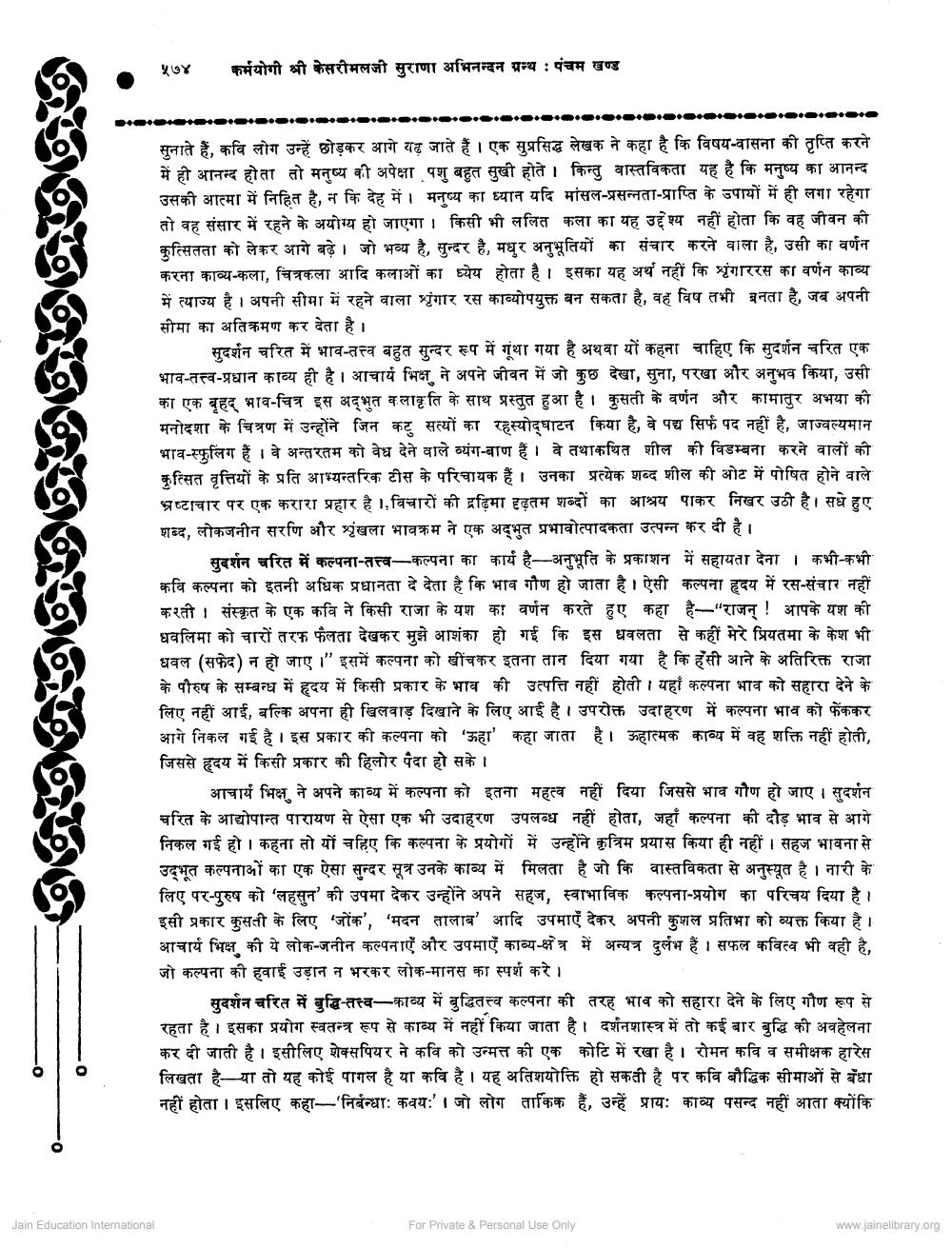________________
५७४
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
.........................................................................
सुनाते हैं, कवि लोग उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं । एक सुप्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि विषय-वासना की तृप्ति करने में ही आनन्द होता तो मनुष्य की अपेक्षा पशु बहुत सुखी होते। किन्तु बास्तविकता यह है कि मनुष्य का आनन्द उसकी आत्मा में निहित है, न कि देह में। मनुष्य का ध्यान यदि मांसल-प्रसन्नता-प्राप्ति के उपायों में ही लगा रहेगा तो वह संसार में रहने के अयोग्य हो जाएगा। किसी भी ललित कला का यह उद्देश्य नहीं होता कि वह जीवन की कुत्सितता को लेकर आगे बढ़े। जो भव्य है, सुन्दर है, मधुर अनुभूतियों का संचार करने वाला है, उसी का वर्णन करना काव्य-कला, चित्रकला आदि कलाओं का ध्येय होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि श्रृंगाररस का वर्णन काव्य में त्याज्य है। अपनी सीमा में रहने वाला शृंगार रस काव्योपयुक्त बन सकता है, वह विष तभी बनता है, जब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देता है।
सुदर्शन चरित में भाव-तत्त्व बहुत सुन्दर रूप में गूंथा गया है अथवा यों कहना चाहिए कि सुदर्शन चरित एक भाव-तत्त्व-प्रधान काव्य ही है। आचार्य भिक्ष ने अपने जीवन में जो कुछ देखा, सुना, परखा और अनुभव किया, उसी का एक बृहद् भाव-चित्र इस अद्भुत कलाकृति के साथ प्रस्तुत हुआ है। कुसती के वर्णन और कामातुर अभया की मनोदशा के चित्रण में उन्होंने जिन कटु सत्यों का रहस्योद्घाटन किया है, वे पद्य सिर्फ पद नहीं है, जाज्वल्यमान भाव-स्फुलिंग हैं । वे अन्तरतम को वेध देने वाले व्यंग-बाण हैं। वे तथाकथित शील की विडम्बना करने वालों की कुत्सित वृत्तियों के प्रति आभ्यन्तरिक टीस के परिचायक हैं। उनका प्रत्येक शब्द शील की ओट में पोषित होने वाले भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार है । विचारों की द्रढिमा दृढ़तम शब्दों का आश्रय पाकर निखर उठी है। सधे हुए शब्द, लोकजनीन सरणि और शृंखला भावक्रम ने एक अद्भुत प्रभावोत्पादकता उत्पन्न कर दी है।
___ सुदर्शन चरित में कल्पना-तत्त्व-कल्पना का कार्य है-अनुभूति के प्रकाशन में सहायता देना । कभी-कभी कवि कल्पना को इतनी अधिक प्रधानता दे देता है कि भाव गौण हो जाता है। ऐसी कल्पना हृदय में रस-संचार नहीं करती। संस्कृत के एक कवि ने किसी राजा के यश का वर्णन करते हुए कहा है-"राजन् ! आपके यश की धवलिमा को चारों तरफ फैलता देखकर मुझे आशंका हो गई कि इस धवलता से कहीं मेरे प्रियतमा के केश भी धवल (सफेद) न हो जाए।" इसमें कल्पना को खींचकर इतना तान दिया गया है कि हँसी आने के अतिरिक्त राजा के पौरुष के सम्बन्ध में हृदय में किसी प्रकार के भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ कल्पना भाव को सहारा देने के लिए नहीं आई, बल्कि अपना ही खिलवाड़ दिखाने के लिए आई है। उपरोक्त उदाहरण में कल्पना भाव को फेंककर आगे निकल गई है। इस प्रकार की कल्पना को 'ऊहा' कहा जाता है। ऊहात्मक काव्य में वह शक्ति नहीं होती, जिससे हृदय में किसी प्रकार की हिलोर पैदा हो सके ।
आचार्य भिक्ष ने अपने काव्य में कल्पना को इतना महत्व नहीं दिया जिससे भाव गौण हो जाए । सुदर्शन चरित के आद्योपान्त पारायण से ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, जहाँ कल्पना की दौड़ भाव से आगे निकल गई हो । कहना तो यों चहिए कि कल्पना के प्रयोगों में उन्होंने कृत्रिम प्रयास किया ही नहीं। सहज भावना से उद्भुत कल्पनाओं का एक ऐसा सुन्दर सूत्र उनके काव्य में मिलता है जो कि वास्तविकता से अनुस्यूत है। नारी के लिए पर-पुरुष को 'लहसुन' की उपमा देकर उन्होंने अपने सहज, स्वाभाविक कल्पना-प्रयोग का परिचय दिया है। इसी प्रकार कुसती के लिए 'जोंक', 'मदन तालाब' आदि उपमाएँ देकर अपनी कुशल प्रतिभा को व्यक्त किया है। आचार्य भिक्षु की ये लोक-जनीन कल्पनाएँ और उपमाएँ काव्य-क्षेत्र में अन्यत्र दुर्लभ हैं । सफल कवित्व भी वही है, जो कल्पना की हवाई उड़ान न भरकर लोक-मानस का स्पर्श करे।
सुदर्शन चरित में बुद्धि-तत्व-काव्य में बुद्धितत्त्व कल्पना की तरह भाव को सहारा देने के लिए गौण रूप से रहता है। इसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से काव्य में नहीं किया जाता है। दर्शनशास्त्र में तो कई बार बुद्धि की अवहेलना कर दी जाती है। इसीलिए शेक्सपियर ने कवि को उन्मत्त की एक कोटि में रखा है। रोमन कवि व समीक्षक हारेस लिखता है या तो यह कोई पागल है या कवि है। यह अतिशयोक्ति हो सकती है पर कवि बौद्धिक सीमाओं से बँधा नहीं होता। इसलिए कहा-'निर्बन्धाः कवयः' । जो लोग ताकिक हैं, उन्हें प्रायः काव्य पसन्द नहीं आता क्योंकि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org