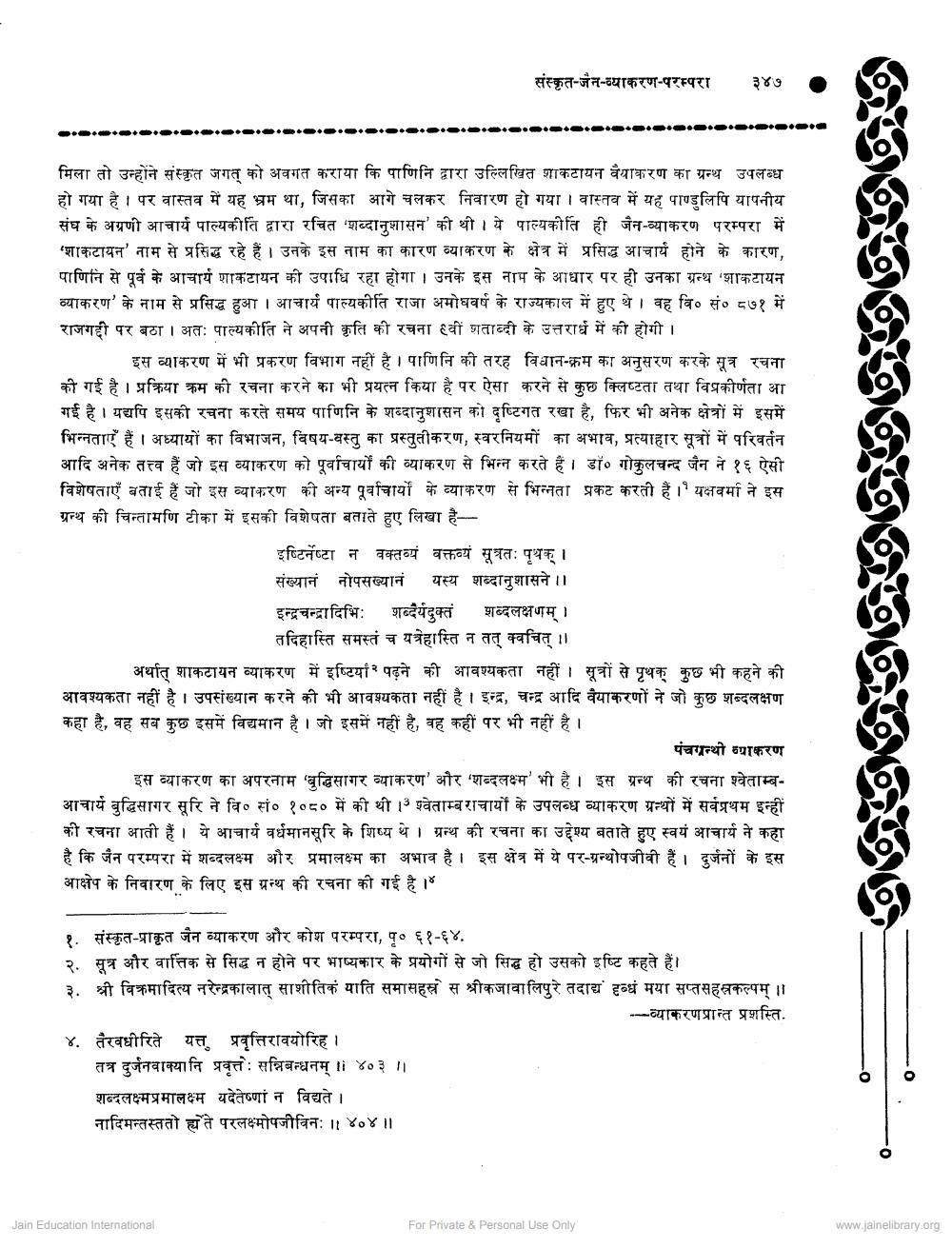________________
संस्कृत-जैन-व्याकरण-परम्परा
३४७
मिला तो उन्होंने संस्कृत जगत् को अवगत कराया कि पाणिनि द्वारा उल्लिखित शाकटायन वैयाकरण का ग्रन्थ उपलब्ध हो गया है। पर वास्तव में यह भ्रम था, जिसका आगे चलकर निवारण हो गया । वास्तव में यह पाण्डुलिपि यापनीय संघ के अग्रणी आचार्य पाल्यकीर्ति द्वारा रचित 'शब्दानुशासन' की थी। ये पाल्यकीति ही जैन-व्याकरण परम्परा में 'शाकटायन' नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। उनके इस नाम का कारण व्याकरण के क्षेत्र में प्रसिद्ध आचार्य होने के कारण, पाणिनि से पूर्व के आचार्य शाकटायन की उपाधि रहा होगा। उनके इस नाम के आधार पर ही उनका ग्रन्थ 'शाकटायन व्याकरण' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आचार्य पाल्यकीर्ति राजा अमोघवर्ष के राज्यकाल में हुए थे। वह वि० सं०८७१ में राजगद्दी पर बठा । अत: पाल्यकीर्ति ने अपनी कृति की रचना हवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की होगी।
इस व्याकरण में भी प्रकरण विभाग नहीं है। पाणिनि की तरह विधान-क्रम का अनुसरण करके सूत्र रचना की गई है । प्रक्रिया क्रम की रचना करने का भी प्रयत्न किया है पर ऐसा करने से कुछ क्लिष्टता तथा विप्रकीर्णता आ गई है । यद्यपि इसकी रचना करते समय पाणिनि के शब्दानुशासन को दृष्टिगत रखा है, फिर भी अनेक क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएँ हैं । अध्यायों का विभाजन, विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण, स्वरनियमों का अभाव, प्रत्याहार सूत्रों में परिवर्तन आदि अनेक तत्त्व हैं जो इस व्याकरण को पूर्वाचार्यों की व्याकरण से भिन्न करते हैं। डॉ० गोकुलचन्द जैन ने १६ ऐसी विशेषताएं बताई हैं जो इस व्याकरण की अन्य पूर्वाचार्यों के व्याकरण से भिन्नता प्रकट करती हैं। यक्षवर्मा ने इस ग्रन्थ की चिन्तामणि टीका में इसकी विशेषता बताते हुए लिखा है
इष्टिर्नेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः पृथक् । संख्यानं नोपसख्यानं यस्य शब्दानुशासने ।। इन्द्रचन्द्रादिभिः शब्दर्यदुक्तं शब्दलक्षणम् ।
तदिहास्ति समस्तं च यत्रेहास्ति न तत् क्वचित् ।। अर्थात् शाकटायन व्याकरण में इष्टियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सूत्रों से पृथक् कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है । उपसंख्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इन्द्र, चन्द्र आदि वैयाकरणों ने जो कुछ शब्दलक्षण कहा है, वह सब कुछ इसमें विद्यमान है । जो इसमें नहीं है, वह कहीं पर भी नहीं है।
पंचग्रन्थी व्याकरण इस व्याकरण का अपरनाम 'बुद्धिसागर व्याकरण' और 'शब्दलक्ष्म' भी है। इस ग्रन्थ की रचना श्वेताम्बआचार्य बुद्धिसागर सूरि ने वि० सं० १०८० में की थी। श्वेताम्बराचार्यों के उपलब्ध व्याकरण ग्रन्थों में सर्वप्रथम इन्हीं की रचना आती हैं। ये आचार्य वर्धमानसूरि के शिष्य थे। ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य बताते हुए स्वयं आचार्य ने कहा है कि जैन परम्परा में शब्दलक्ष्म और प्रमालक्ष्म का अभाव है। इस क्षेत्र में ये पर-ग्रन्थोपजीवी हैं। दुर्जनों के इस आक्षेप के निवारण के लिए इस ग्रन्थ की रचना की गई है।
१. संस्कृत-प्राकृत जैन व्याकरण और कोश परम्परा, पृ० ६१-६४. २. सूत्र और वात्तिक से सिद्ध न होने पर भाष्यकार के प्रयोगों से जो सिद्ध हो उसको इष्टि कहते हैं। ३. श्री विक्रमादित्य नरेन्द्रकालात् साशीतिकं याति समासहस्र स श्रीकजावा लिपुरे तदाद्य दृब्धं मया सप्तसहस्रकल्पम् ।।
-व्याकरणप्रान्त प्रशस्ति. ४. तैरवधीरिते यत्तु प्रवृत्तिरावयोरिह ।
तत्र दुर्जनवाक्या नि प्रवृत्त : सन्निबन्धनम् ॥ ४०३ ।। शब्दलक्ष्मप्रमालक्ष्म यदेतेष्णां न विद्यते । नादिमन्तस्ततो ह्य ते परलक्ष्मोपजीविनः ।। ४०४ ॥
-
0
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org