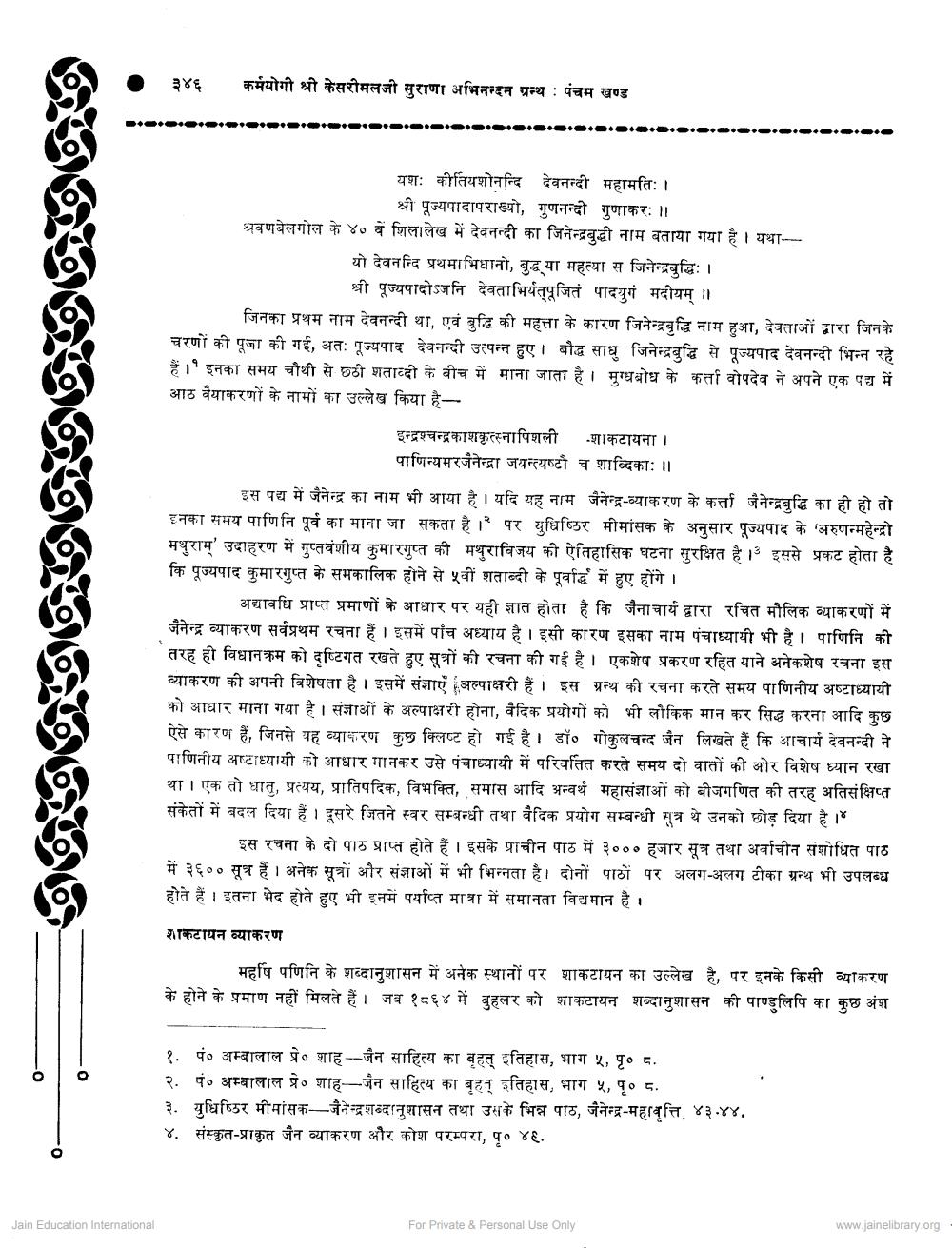________________
३४६
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-............................................
यशः कीतियशोनन्दि देवनन्दी महामतिः ।
श्री पूज्यपादापराख्यो, गुणनन्दो गुणाकरः ॥ श्रवणबेलगोल के ४० वे शिलालेख में देवनन्दी का जिनेन्द्रबुद्धी नाम बताया गया है । यथा---
यो देवनन्दि प्रथमाभिधानो, बुद्ध या महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ।
श्री पूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्पूजितं पादयुगं मदीयम् ॥ जिनका प्रथम नाम देवनन्दी था, एवं बुद्धि की महत्ता के कारण जिनेन्द्रबुद्धि नाम हुआ, देवताओं द्वारा जिनके चरणों की पूजा की गई, अतः पूज्यपाद देवनन्दी उत्पन्न हुए। बौद्ध साधु जिनेन्द्रबुद्धि से पूज्यपाद देवनन्दी भिन्न रहे हैं। इनका समय चौथी से छठी शताब्दी के बीच में माना जाता है। मुग्धबोध के कर्ता वोपदेव ने अपने एक पद्य में आठ वैयाकरणों के नामों का उल्लेख किया है
इन्द्रश्चन्द्रकाशकृत्स्नापिशली -शाकटायना ।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ।। इस पद्य में जैनेन्द्र का नाम भी आया है। यदि यह नाम जैनेन्द्र-व्याकरण के कर्ता जैनेन्द्रबुद्धि का ही हो तो इनका समय पाणिनि पूर्व का माना जा सकता है। पर युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पूज्यपाद के 'अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्' उदाहरण में गुप्तवंशीय कुमारगुप्त की मथुराविजय की ऐतिहासिक घटना सुरक्षित है। इससे प्रकट होता है कि पूज्यपाद कुमारगुप्त के समकालिक होने से ५वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए होंगे।
अद्यावधि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यही ज्ञात होता है कि जैनाचार्य द्वारा रचित मौलिक व्याकरणों में जैनेन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम रचना हैं । इसमें पांच अध्याय है। इसी कारण इसका नाम पंचाध्यायी भी है। पाणिनि की तरह ही विधानक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सूत्रों की रचना की गई है। एकशेष प्रकरण रहित याने अनेकशेष रचना इस व्याकरण की अपनी विशेषता है। इसमें संज्ञाएँ अल्पाक्षरी हैं। इस ग्रन्थ की रचना करते समय पाणिनीय अष्टाध्यायी को आधार माना गया है। संज्ञाओं के अल्पाक्षरी होना, वैदिक प्रयोगों को भी लौकिक मान कर सिद्ध करना आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे यह व्याकरण कुछ क्लिष्ट हो गई है। डॉ० गोकुलचन्द जैन लिखते हैं कि आचार्य देवनन्दी ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को आधार मानकर उसे पंचाध्यायी में परिवर्तित करते समय दो वातों की ओर विशेष ध्यान रखा था। एक तो धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, विभक्ति, समास आदि अन्वर्थ महासंज्ञाओं को बीजगणित की तरह अतिसंक्षिप्त संकेतों में बदल दिया हैं । दूसरे जितने स्वर सम्बन्धी तथा वैदिक प्रयोग सम्बन्धी मूत्र थे उनको छोड़ दिया है।
इस रचना के दो पाठ प्राप्त होते हैं । इसके प्राचीन पाठ में ३००० हजार सूत्र तथा अर्वाचीन संशोधित पाठ में ३६०० सूत्र हैं । अनेक सूत्रों और संज्ञाओं में भी भिन्नता है। दोनों पाठों पर अलग-अलग टीका ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं । इतना भेद होते हुए भी इनमें पर्याप्त मात्रा में समानता विद्यमान है।
शाकटायन व्याकरण
महर्षि पणिनि के शब्दानुशासन में अनेक स्थानों पर शाकटायन का उल्लेख है, पर इनके किसी व्याकरण के होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। जब १८६४ में बुहलर को शाकटायन शब्दानुशासन की पाण्डुलिपि का कुछ अंश
१. पं० अम्बालाल प्रे० शाह --जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ५, पृ०८. २. पं० अम्बालाल प्रे० शाह-जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ५, पृ० ८. ३. युधिष्ठिर मीमांसक-जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके भिन्न पाठ, जैनेन्द्र-महावृत्ति, ४३.४४. ४. संस्कृत-प्राकृत जैन व्याकरण और कोश परम्परा, पृ० ४६.
Jain Education International
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only