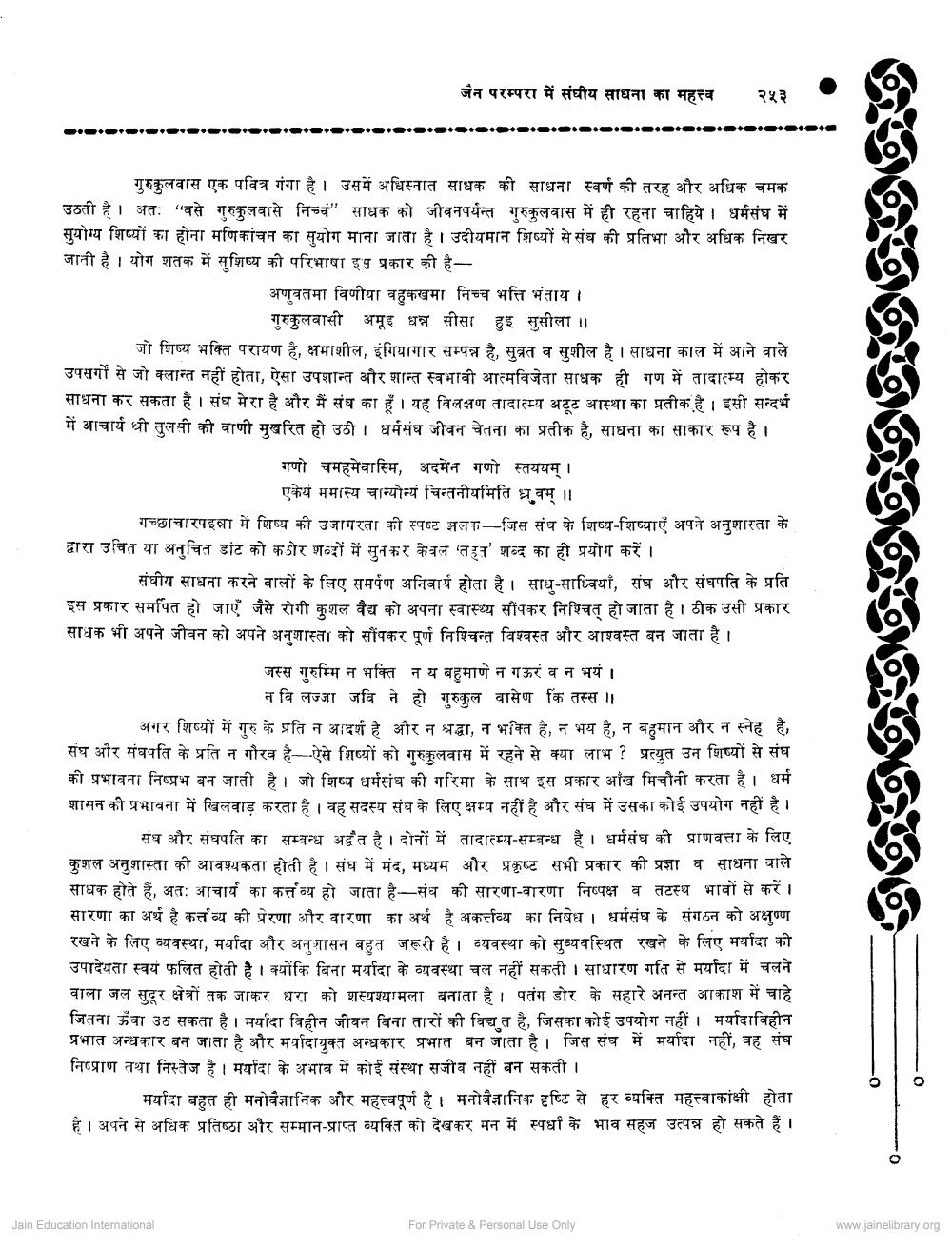________________
जैन परम्परा में संघीय साधना का महत्त्व
२५३
....
....
........
........
......
........
......
......
..
......
.
....
....
..
गुरुकुलवास एक पवित्र गंगा है। उसमें अधिस्नात साधक की साधना स्वर्ण की तरह और अधिक चमक उठती है। अत: "वसे गुरुकुलवासे निच्चं" साधक को जीवनपर्यन्त गुरुकुलवास में ही रहना चाहिये। धर्मसंघ में सुयोग्य शिष्यों का होना मणिकांचन का सुयोग माना जाता है। उदीयमान शिष्यों से संघ की प्रतिभा और अधिक निखर जाती है। योग शतक में सुशिष्य की परिभाषा इस प्रकार की है
अणुवतमा विणीया वहुकखमा निच्च भत्ति भंताय ।
गुरुकुलवासी अमूइ धन्न सीसा हुइ सुसीला ॥ जो शिष्य भक्ति परायण है, क्षमाशील, इंगियागार सम्पन्न है, सुव्रत व सुशील है । साधना काल में आने वाले उपसर्गों से जो क्लान्त नहीं होता, ऐसा उपशान्त और शान्त स्वभावी आत्मविजेता साधक ही गण में तादात्म्य होकर साधना कर सकता है । संघ मेरा है और मैं संघ का हूँ। यह विलक्षण तादात्म्य अटूट आस्था का प्रतीक है। इसी सन्दर्भ में आचार्य श्री तुलसी की वाणी मुखरित हो उठी। धर्मसंघ जीवन चेतना का प्रतीक है, साधना का साकार रूप है।
गणो चमहमेवास्मि, अदमेन गणो स्तययम् ।
एकेयं ममास्य चान्योन्यं चिन्तनीयमिति ध्रुवम् ॥ गच्छाचारपइन्ना में शिष्य की उजागरता की स्पष्ट झलक-जिस संघ के शिष्य-शिष्याएँ अपने अनुशास्ता के द्वारा उचित या अनुचित डांट को कठोर शब्दों में सुनकर केवल 'तहर' शब्द का ही प्रयोग करें।
संघीय साधना करने वालों के लिए समर्पण अनिवार्य होता है। साध-साध्वियाँ, संघ और संघपति के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाएँ जैसे रोगी कुशल वैद्य को अपना स्वास्थ्य सौंपकर निश्चित् हो जाता है । ठीक उसी प्रकार साधक भी अपने जीवन को अपने अनुशास्ता को सौंपकर पूर्ण निश्चिन्त विश्वस्त और आश्वस्त बन जाता है।
जस्स गुरुम्मि न भक्ति न य बहुमाणे न गऊरं व न भयं ।
न वि लज्जा जवि ने हो गुरुकुल वासेण कि तस्स ।। अगर शिष्यों में गुरु के प्रति न आदर्श है और न श्रद्धा, न भक्ति है, न भय है, न बहुमान और न स्नेह है, संघ और संघपति के प्रति न गौरव है.--.ऐसे शिष्यों को गुरुकूलवास में रहने से क्या लाभ ? प्रत्युत उन शिष्यों से संघ की प्रभाबना निष्प्रभ बन जाती है। जो शिष्य धर्मसंघ की गरिमा के साथ इस प्रकार आँख मिचौनी करता है। धर्म शासन की प्रभावना में खिलवाड़ करता है । वह सदस्य संघ के लिए क्षम्य नहीं है और संघ में उसका कोई उपयोग नहीं है।
संघ और संघपति का सम्बन्ध अद्वैत है। दोनों में तादात्म्य-सम्बन्ध है। धर्मसंघ की प्राणवत्ता के लिए कुशल अनुशास्ता की आवश्यकता होती है। संघ में मंद, मध्यम और प्रकृष्ट सभी प्रकार की प्रज्ञा व साधना वाले साधक होते हैं, अत: आचार्य का कर्तव्य हो जाता है-संघ की सारणा-वारणा निष्पक्ष व तटस्थ भावों से करें। सारणा का अर्थ है कर्तव्य की प्रेरणा और वारणा का अर्थ है अकर्त्तव्य का निषेध । धर्मसंघ के संगठन को अक्षुण्ण रखने के लिए व्यवस्था, मर्यादा और अनुशासन बहत जरूरी है। व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए मर्यादा की उपादेयता स्वयं फलित होती है । क्योंकि बिना मर्यादा के व्यवस्था चल नहीं सकती । साधारण गति से मर्यादा में चलने वाला जल सुदूर क्षेत्रों तक जाकर धरा को शस्यश्यामला बनाता है। पतंग डोर के सहारे अनन्त आकाश में चाहे जितना ऊँचा उठ सकता है। मर्यादा विहीन जीवन बिना तारों की विद्य त है, जिसका कोई उपयोग नहीं। मर्यादाविहीन प्रभात अन्धकार बन जाता है और मर्यादायुक्त अन्धकार प्रभात बन जाता है। जिस संघ में मर्यादा नहीं, वह संघ निष्प्राण तथा निस्तेज है। मर्यादा के अभाव में कोई संस्था सजीव नहीं बन सकती।
मर्यादा बहुत ही मनोवैज्ञानिक और महत्त्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हर व्यक्ति महत्त्वाकांक्षी होता है। अपने से अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान-प्राप्त व्यक्ति को देखकर मन में स्पर्धा के भाव सहज उत्पन्न हो सकते हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org