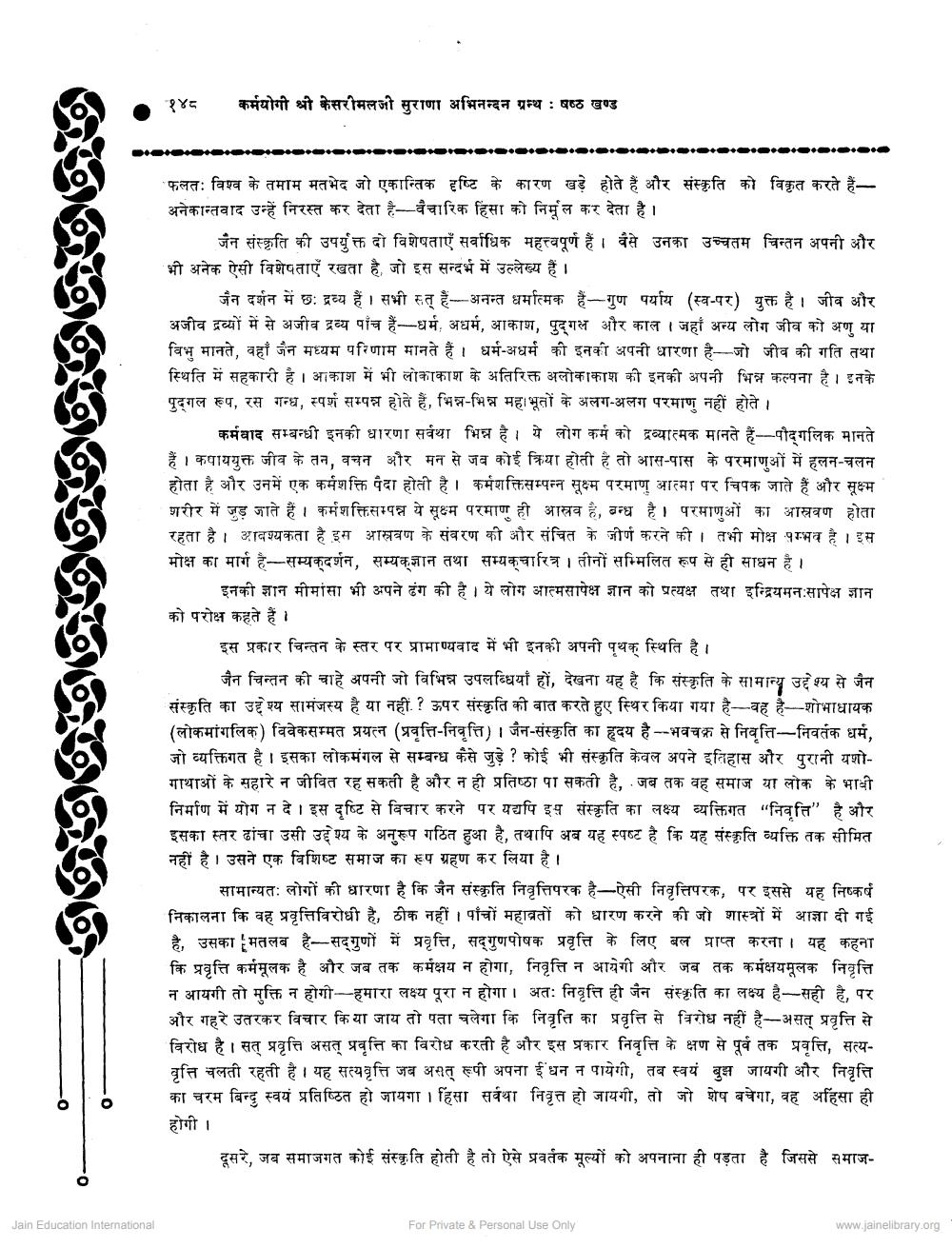________________
०
O
.०
Jain Education International
१४८
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठ खण्ड
फलतः विश्व के तमाम मतभेद जो एकान्तिक दृष्टि के कारण खड़े होते हैं और संस्कृति को विकृत करते हैंअनेकान्तबाद उन्हें निरस्त कर देता है—वैचारिक हिंसा को निर्मूल कर देता है।
जैन संस्कृति की उपर्युक्त दो विशेषताएँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं । वैसे उनका उच्चतम चिन्तन अपनी और भी अनेक ऐसी विशेषताएँ रखता है, जो इस सन्दर्भ में उल्लेख्य हैं ।
जैन दर्शन में छः द्रव्य हैं। सभी सत् हैं - अनन्त धर्मात्मक हैं—गुण पर्याय ( स्व-पर) युक्त है। जीव और अजीव द्रव्यों में से अजीव द्रव्य पाँच हैं-धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल । जहाँ अन्य लोग जीव को अणु या विभु मानते, वहाँ जैन मध्यम परिणाम मानते हैं । धर्म-अधर्म की इनकी अपनी धारणा है—जो जीव की गति तथा स्थिति में सहकारी है । आकाश में भी लोकाकाश के अतिरिक्त अलोकाकाश की इनकी अपनी भिन्न कल्पना है । इनके पुद्गल रूप, रस गन्ध, स्पर्श सम्पन्न होते हैं, भिन्न-भिन्न महाभूतों के अलग-अलग परमाणु नहीं होते ।
कर्मवाद सम्बन्धी इनकी धारणा सर्वथा भिन्न है । ये लोग कर्म को द्रव्यात्मक मानते हैं- पौद्गलिक मानते हैं । कपाययुक्त जीव के तन, वचन और मन से जब कोई क्रिया होती है तो आस-पास के परमाणुओं में हलन चलन होता है और उनमें एक कर्मशक्ति पैदा होती है। कर्मक्तिसम्पन्न सूक्ष्म परमाणु आत्मा पर चिपक जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में जुड़ जाते हैं । कर्मशक्तिसम्पन्न ये सूक्ष्म परमाणु ही आस्रव है, बन्ध है । परमाणुओं का आस्रवण होता रहता है । आवश्यकता है इस आस्रवण के संवरण की और संचित के जीर्ण करने की। तभी मोक्ष सम्भव है । इस मोक्ष का मार्ग है- सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक्चारिण तीनों सम्मिलित रूप से ही साधन है।
इनकी ज्ञान मीमांसा भी अपने ढंग की है। ये लोग आत्मसापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा इन्द्रियमनः सापेक्ष ज्ञान को परोक्ष कहते हैं।
इस प्रकार चिन्तन के स्तर पर प्रामाण्यवाद में भी इनकी अपनी पृथक् स्थिति है ।
जैन चिन्तन की चाहे अपनी जो विभिन्न उपलब्धियाँ हों, देखना यह है कि संस्कृति के सामान्य उद्देश्य से जैन संस्कृति का उद्देश्य सामंजस्य है या नहीं ? ऊपर संस्कृति की बात करते हुए स्थिर किया गया है - वह है— शोभाधायक (लोकमांगलिक) विवेकसम्मत प्रयत्न ( प्रवृत्ति निवृत्ति ) । जैन संस्कृति का हृदय है -- भवचक्र से निवृत्ति - निवर्तक धर्म, जो व्यक्तिगत है । इसका लोकमंगल से सम्बन्ध कैसे जुड़े ? कोई भी संस्कृति केवल अपने इतिहास और पुरानी यशोगाथाओं के सहारे न जीवित रह सकती है और न ही प्रतिष्ठा पा सकती है, जब तक वह समाज या लोक के भावी निर्माण में योग न दे । इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि इस संस्कृति का लक्ष्य व्यक्तिगत "निवृत्ति" है और इसका स्तर ढांचा उसी उद्देश्य के अनुरूप गठित हुआ है, तथापि अब यह स्पष्ट है कि यह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उसने एक विशिष्ट समाज का रूप ग्रहण कर लिया है ।
सामान्यतः लोगों की धारणा है कि जैन संस्कृति निवृतिपरक है-ऐसी निवृत्तिपरक, पर इससे यह निष्कर्ष निकालना कि वह प्रवृत्तिविरोधी है, ठीक नहीं। पांचों महाव्रतों को धारण करने की जो शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, उसका मतलब है- सद्गुणों में प्रवृत्ति, सद्गुणपोषक प्रवृत्ति के लिए बल प्राप्त करना। यह कहना कि प्रवृत्ति कर्ममूलक है और जब तक कर्मक्षय न होगा, निवृत्ति न आयेगी और जब तक कर्मक्षयमूलक निवृत्ति न आयगी तो मुक्ति न होगी - हमारा लक्ष्य पूरा न होगा। अतः निवृत्ति ही जैन संस्कृति का लक्ष्य है - सही है, पर और गहरे उतरकर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि निवृत्ति का प्रवृत्ति से विरोध नहीं है-असत् प्रवृत्ति से विरोध है । सत्प्रवृत्ति असत् प्रवृत्ति का विरोध करती है और इस प्रकार निवृत्ति के क्षण से पूर्व तक प्रवृत्ति, सत्यवृत्ति चलती रहती है। यह सत्यवृत्ति जब असत् रूपी अपना ईंधन न पायेंगी, तब स्वयं बुझ जायगी और निवृत्ति का चरम बिन्दु स्वयं प्रतिष्ठित हो जायगा । हिंसा सर्वथा निवृत्त हो जायगी, तो जो शेष बचेगा, वह अहिंसा ही होगी ।
दूसरे, जब समाजगत कोई संस्कृति होती है तो ऐसे प्रवर्तक मूल्यों को अपनाना ही पड़ता है जिससे समाज
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org