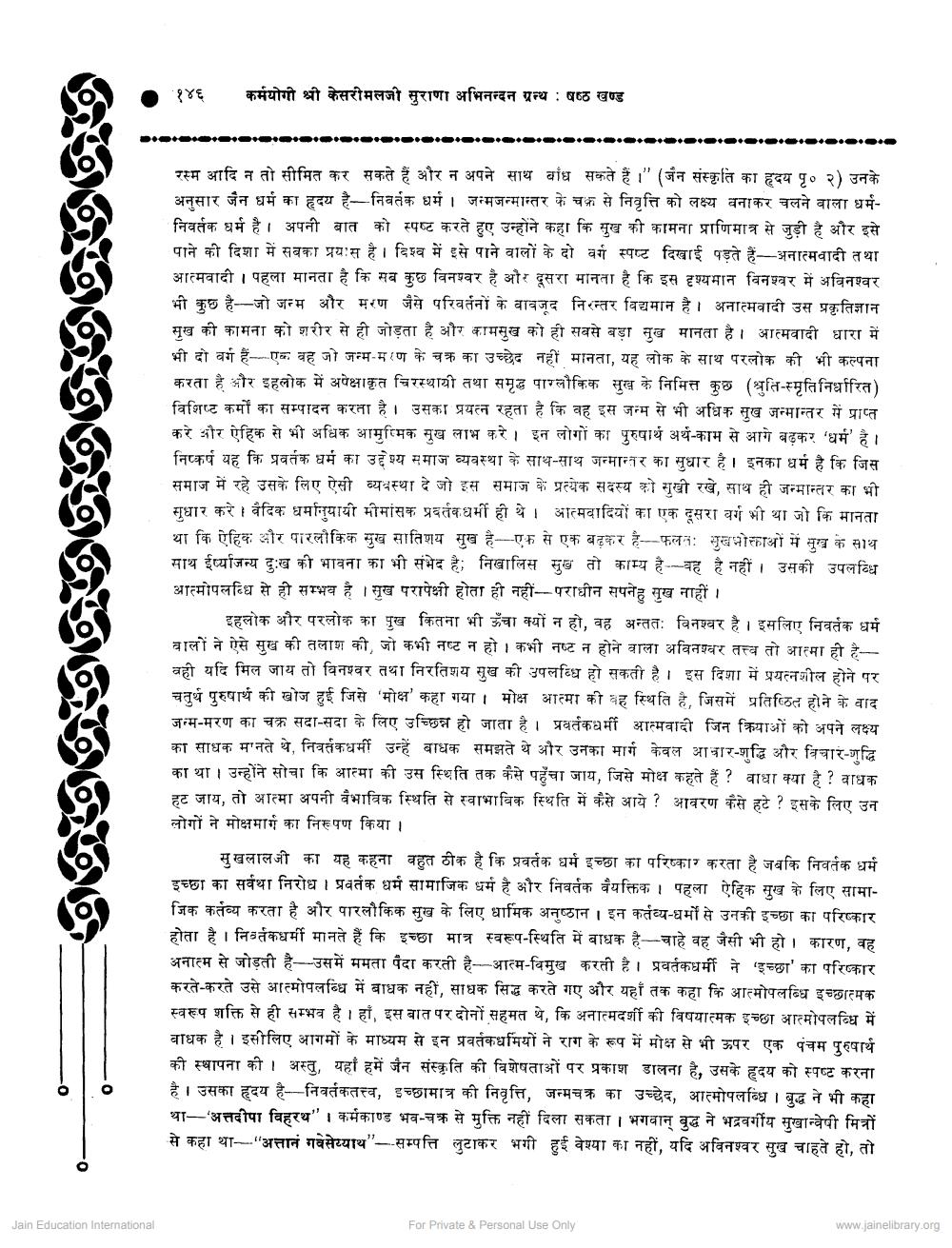________________
१४६
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठ खण्ड
...........................................
रस्म आदि न तो सीमित कर सकते हैं और न अपने साथ बाँध सकते हैं।" (जैन संस्कृति का हृदय पृ० २) उनके अनुसार जैन धर्म का हृदय है-निवर्तक धर्म । जन्मजन्मान्तर के चक्र से निवृत्ति को लक्ष्य बनाकर चलने वाला धर्मनिवर्तक धर्म है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सुख की कामना प्राणिमात्र से जुड़ी है और इसे पाने की दिशा में सबका प्रयास है। विश्व में इसे पाने वालों के दो वर्ग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं-अनात्मवादी तथा आत्मवादी । पहला मानता है कि सब कुछ विनश्वर है और दूसरा मानता है कि इस दृश्यमान विनश्वर में अविनश्वर भी कुछ है-जो जन्म और मरण जैसे परिवर्तनों के बावजूद निरन्तर विद्यमान है। अनात्मवादी उस प्रकृतिज्ञान सुख की कामना को शरीर से ही जोड़ता है और कामसुख को ही सबसे बड़ा सुख मानता है। आत्मवादी धारा में भी दो वर्ग हैं ---एक वह जो जन्म-मरण के चक्र का उच्छेद नहीं मानता, यह लोक के साथ परलोक की भी कल्पना करता है और इहलोक में अपेक्षाकृत चिरस्थायी तथा समृद्ध पारलौकिक सुख के निमित्त कुछ (श्रुति-स्मृति निर्धारित) विशिष्ट कर्मों का सम्पादन करता है। उसका प्रयत्न रहता है कि वह इस जन्म से भी अधिक सुख जन्मान्तर में प्राप्त करे और ऐहिक से भी अधिक आमुग्मिक सुख लाभ करे। इन लोगों का पुरुषार्थ अर्थ-काम से आगे बढ़कर 'धर्म' है। निष्कर्ष यह कि प्रवर्तक धर्म का उद्देश्य समाज व्यवस्था के साथ-साथ जन्मान्तर का सुधार है। इनका धर्म है कि जिस समाज में रहे उसके लिए ऐसी व्यवस्था दे जो इस समाज के प्रत्येक सदस्य को सुखी रखे, साथ ही जन्मान्तर का भी सुधार करे। वैदिक धर्मानुयायी मीमांसक प्रवर्तकधर्मी ही थे। आत्मवादियों का एक दूसरा वर्ग भी था जो कि मानता था कि ऐहिक और पारलौकिक सुख सातिशय सुख है-एक से एक बढ़कर है-फलतः सुखभोक्ताओं में सुख के साथ साथ ईर्ष्याजन्य दुःख की भावना का भी संभेद है; निखालिस सुख तो काम्य है---वह है नहीं। उसकी उपलब्धि आत्मोपलब्धि से ही सम्भव है । सुख परापेक्षी होता ही नहीं-पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।
इहलोक और परलोक का पुख कितना भी ऊँचा क्यों न हो, वह अन्तत: विनश्वर है। इसलिए निवर्तक धर्म बालों ने ऐसे सुख की तलाश की, जो कभी नष्ट न हो। कभी नष्ट न होने वाला अविनश्वर तत्त्व तो आत्मा ही हैवही यदि मिल जाय तो विनश्वर तथा निरतिशय सुख की उपलब्धि हो सकती है। इस दिशा में प्रयत्नशील होने पर चतुर्थ पुरुषार्थ की खोज हुई जिसे 'मोक्ष' कहा गया। मोक्ष आत्मा की यह स्थिति है, जिसमें प्रतिष्ठित होने के बाद जन्म-मरण का चक्र सदा-सदा के लिए उच्छिन्न हो जाता है। प्रवर्तकधर्मी आत्मवादी जिन क्रियाओं को अपने लक्ष्य का साधक मानते थे, निवर्तकधर्मी उन्हें बाधक समझते थे और उनका मार्ग केवल आचार-शुद्धि और विचार-गुद्धि का था। उन्होंने सोचा कि आत्मा की उस स्थिति तक कैसे पहुँचा जाय, जिसे मोक्ष कहते हैं ? वाधा क्या है ? वाधक हट जाय, तो आत्मा अपनी वैभाविक स्थिति से स्वाभाविक स्थिति में कैसे आये? आवरण कैसे हटे ? इसके लिए उन लोगों ने मोक्षमार्ग का निरूपण किया।
सुखलालजी का यह कहना बहुत ठीक है कि प्रवर्तक धर्म इच्छा का परिष्कार करता है जबकि निवर्तक धर्म इच्छा का सर्वथा निरोध । प्रवर्तक धर्म सामाजिक धर्म है और निवर्तक वैयक्तिक । पहला ऐहिक सुख के लिए सामाजिक कर्तव्य करता है और पारलौकिक सुख के लिए धार्मिक अनुष्ठान । इन कर्तव्य-धर्मों से उनकी इच्छा का परिष्कार होता है । निवर्तकधर्मी मानते हैं कि इच्छा मात्र स्वरूप-स्थिति में बाधक है--चाहे वह जैसी भी हो। कारण, वह अनात्म से जोड़ती है--उसमें ममता पैदा करती है----आत्म-विमुख करती है। प्रवर्तकधर्मी ने 'इच्छा' का परिष्कार करते-करते उसे आत्मोपलब्धि में बाधक नहीं, साधक सिद्ध करते गए और यहाँ तक कहा कि आत्मोपलब्धि इच्छात्मक स्वरूप शक्ति से ही सम्भव है। हाँ, इस बात पर दोनों सहमत थे, कि अनात्मदर्शी की विषयात्मक इच्छा आत्मोपलब्धि में बाधक है। इसीलिए आगमों के माध्यम से इन प्रवर्तकर्मियों ने राग के रूप में मोक्ष से भी ऊपर एक पंचम पुरुषार्थ की स्थापना की। अस्तु, यहाँ हमें जैन संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, उसके हृदय को स्पष्ट करना है। उसका हृदय है.----निवर्तकतत्त्व, इच्छामात्र की निवृत्ति, जन्मचक्र का उच्छेद, आत्मोपलब्धि । बुद्ध ने भी कहा था-'अत्तदीपा विहरथ" । कर्मकाण्ड भव-चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता । भगवान् बुद्ध ने भद्रवर्गीय सुखान्वेषी मित्रों से कहा था-"अत्तानं गवसेय्याथ"-सम्पत्ति लुटाकर भगी हुई वेश्या का नहीं, यदि अविनश्वर सुख चाहते हो, तो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org