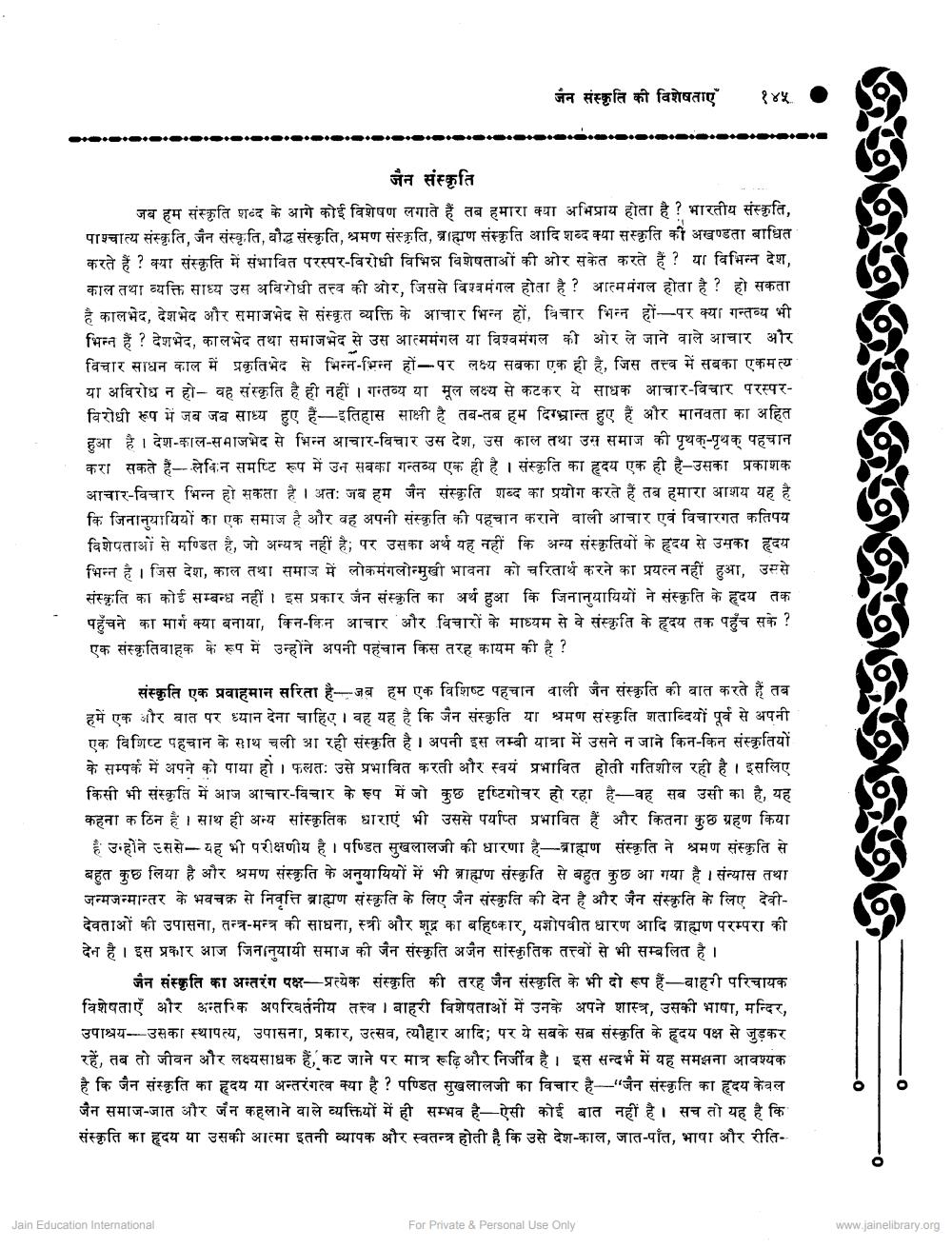________________
जैन संस्कृति की विशेषताएँ
१४५ .
-.-.-.-.-...........................................................
.
....
__ जैन संस्कृति जब हम संस्कृति शब्द के आगे कोई विशेषण लगाते हैं तब हमारा क्या अभिप्राय होता है ? भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति आदि शब्द क्या सस्कृति की अखण्डता बाधित करते हैं ? क्या संस्कृति में संभावित परस्पर-विरोधी विभिन्न विशेषताओं की ओर सकेत करते हैं ? या विभिन्न देश, काल तथा व्यक्ति साध्य उस अविरोधी तत्त्व की ओर, जिससे विश्वमंगल होता है ? आत्ममंगल होता है ? हो सकता है कालभेद, देशभेद और समाजभेद से संस्कृत व्यक्ति के आचार भिन्न हों, विचार भिन्न हों-पर क्या गन्तव्य भी भिन्न हैं ? देशभेद, कालभेद तथा समाजभेद से उस आत्ममंगल या विश्वमंगल की ओर ले जाने वाले आचार और विचार साधन काल में प्रकृतिभेद से भिन्न-भिन्न हों-पर लक्ष्य सबका एक ही है, जिस तत्त्व में सबका एकम त्य या अविरोध न हो- वह संस्कृति है ही नहीं । गन्तव्य या मूल लक्ष्य से कटकर ये साधक आचार-विचार परस्परविरोधी रूप में जब जब साध्य हुए हैं-इतिहास साक्षी है तब-तब हम दिग्भ्रान्त हुए हैं और मानवता का अहित हुआ है। देश-काल-समाजभेद से भिन्न आचार-विचार उस देश, उस काल तथा उस समाज की पृथक्-पृथक् पहचान करा सकते हैं-- लेविन समष्टि रूप में उन सबका गन्तव्य एक ही है । संस्कृति का हृदय एक ही है-उसका प्रकाशक आचार-विचार भिन्न हो सकता है । अत: जब हम जैन संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा आशय यह है कि जिनानुयायियों का एक समाज है और वह अपनी संस्कृति की पहचान कराने वाली आचार एवं विचारगत कतिपय विशेषताओं से मण्डित है, जो अन्यत्र नहीं है; पर उसका अर्थ यह नहीं कि अन्य संस्कृतियों के हृदय से उसका हृदय भिन्न है । जिस देश, काल तथा समाज में लोकमंगलोन्मुखी भावना को चरितार्थ करने का प्रयत्न नहीं हुआ, उससे संस्कृति का कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार जैन संस्कृति का अर्थ हुआ कि जिनानुयायियों ने संस्कृति के हृदय तक पहुँचने का मार्ग क्या बनाया, किन-किन आचार और विचारों के माध्यम से वे संस्कृति के हृदय तक पहुँच सके ? एक संस्कृतिबाहक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान किस तरह कायम की है ?
संस्कृति एक प्रवाहमान सरिता है-जब हम एक विशिष्ट पहचान वाली जैन संस्कृति की बात करते हैं तब हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। वह यह है कि जैन संस्कृति या श्रमण संस्कृति शताब्दियों पूर्व से अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ चली आ रही संस्कृति है। अपनी इस लम्बी यात्रा में उसने न जाने किन-किन संस्कृतियों के सम्पर्क में अपने को पाया हो । फलत: उसे प्रभावित करती और स्वयं प्रभावित होती गतिशील रही है । इसलिए किसी भी संस्कृति में आज आचार-विचार के रूप में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब उसी का है, यह कहना कठिन है । साथ ही अन्य सांस्कृतिक धाराएं भी उससे पर्याप्त प्रभावित हैं और कितना कुछ ग्रहण किया
है उन्होंने उससे-यह भी परीक्षणीय है। पण्डित सुखलालजी की धारणा है-ब्राह्मण संस्कृति ने श्रमण संस्कृति से बहुत कुछ लिया है और श्रमण संस्कृति के अनुयायियों में भी ब्राह्मण संस्कृति से बहुत कुछ आ गया है । संन्यास तथा जन्मजन्मान्तर के भवचक्र से निवृत्ति ब्राह्मण संस्कृति के लिए जैन संस्कृति की देन है और जैन संस्कृति के लिए देवीदेवताओं की उपासना, तन्त्र-मन्त्र की साधना, स्त्री और शूद्र का बहिष्कार, यज्ञोपवीत धारण आदि ब्राह्मण परम्परा की देन है । इस प्रकार आज जिनानुयायी समाज की जैन संस्कृति अजैन सांस्कृतिक तत्त्वों से भी सम्बलित है।
जैन संस्कृति का अन्तरंग पक्ष-प्रत्येक संस्कृति की तरह जैन संस्कृति के भी दो रूप हैं—बाहरी परिचायक विशेषताएँ और अन्तरिक अपरिवर्तनीय तत्त्व । बाहरी विशेषताओं में उनके अपने शास्त्र, उसकी भाषा, मन्दिर, उपाश्रय----उसका स्थापत्य, उपासना, प्रकार, उत्सव, त्यौहार आदि; पर ये सबके सब संस्कृति के हृदय पक्ष से जुड़कर रहें, तब तो जीवन और लक्ष्यसाधक हैं, कट जाने पर मात्र रूढ़ि और निर्जीव है। इस सन्दर्भ में यह समझना आवश्यक है कि जैन संस्कृति का हृदय या अन्तरंगत्व क्या है ? पण्डित सुखलालजी का विचार है-"जैन संस्कृति का हृदय केबल जैन समाज-जात और जैन कहलाने वाले व्यक्तियों में ही सम्भव है—ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि संस्कृति का हृदय या उसकी आत्मा इतनी व्यापक और स्वतन्त्र होती है कि उसे देश-काल, जात-पात, भाषा और रीति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org