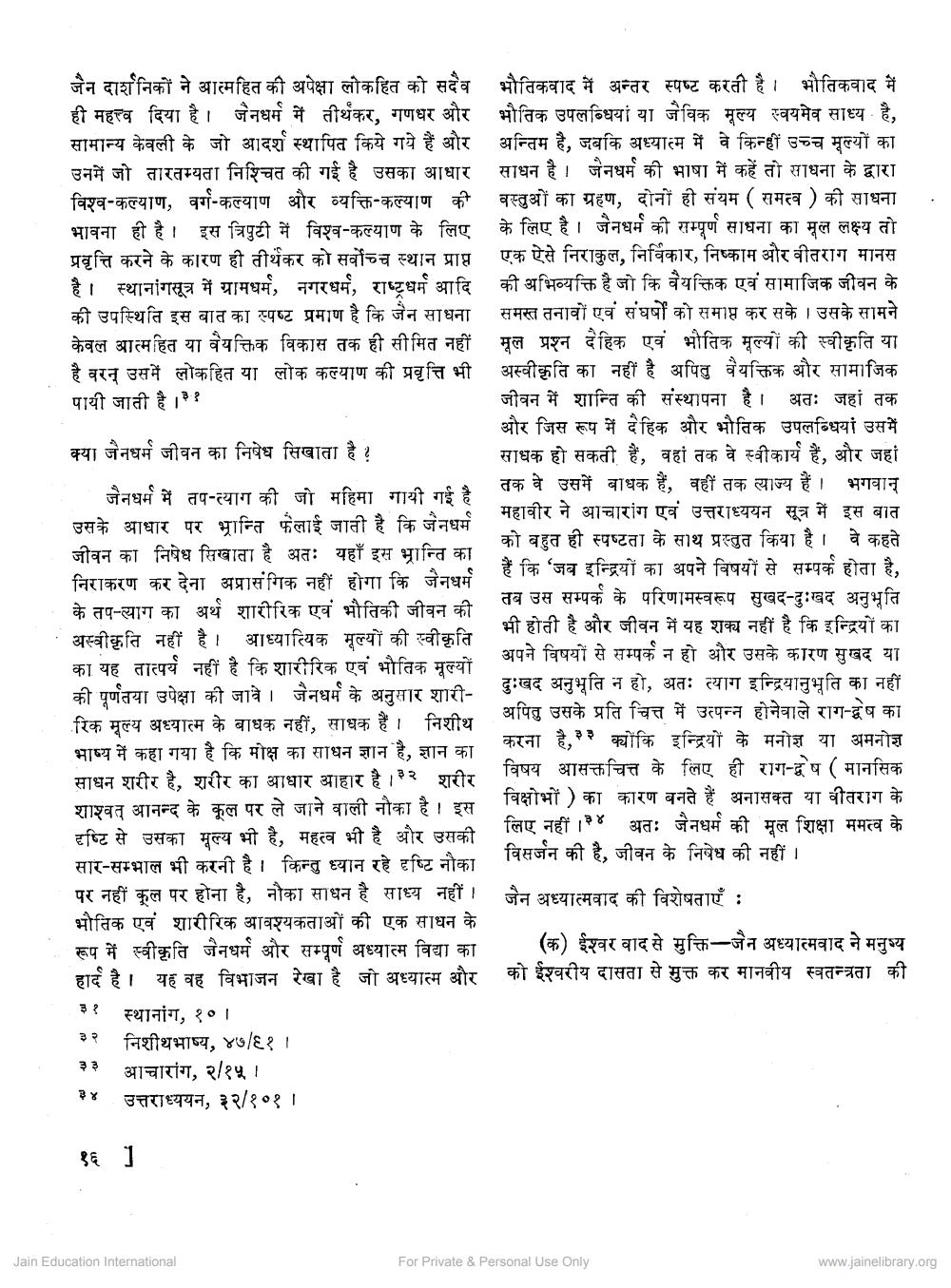________________
जैन दार्शनिकों ने आत्महित की अपेक्षा लोकहित को सदैव ही महत्त्व दिया है । जैनधर्म में तीर्थंकर, गणधर और सामान्य केवली के जो आदर्श स्थापित किये गये हैं और उनमें जो तारतम्यता निश्चित की गई है उसका आधार विश्व-कल्याण, वर्ग-कल्याण और व्यक्ति-कल्याण की भावना ही है । इस त्रिपुटी में विश्व कल्याण के लिए प्रवृत्ति करने के कारण ही तीर्थंकर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । स्थानांगसूत्र में ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म आदि की उपस्थिति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जैन साधना केवल आत्महित या वैयक्तिक विकास तक ही सीमित नहीं है वरन् उसमें लोकहित या लोक कल्याण की प्रवृत्ति भी पायी जाती है । ३१
क्या जैनधर्म जीवन का निषेध सिखाता है ?
जैनधर्म में तप-त्याग की जो महिमा गायी गई है। उसके आधार पर भ्रान्ति फैलाई जाती है कि जैनधर्म जीवन का निषेध सिखाता है अतः यहाँ इस भ्रान्ति का निराकरण कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जैनधर्म के तप-त्याग का अर्थ शारीरिक एवं भौतिकी जीवन की अस्वीकृति नहीं है। आध्यात्यिक मूल्यों की स्वीकृति का यह तात्पर्य नहीं है कि शारीरिक एवं भौतिक मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की जावे। जैनधर्म के अनुसार शारीरिक मूल्य अध्यात्म के बाधक नहीं, साधक हैं । निशीथ भाष्य में कहा गया है कि मोक्ष का साधन ज्ञान है, ज्ञान का साधन शरीर है, शरीर का आधार आहार है । ३२ शरीर शाश्वत आनन्द के कूल पर ले जाने वाली नौका है। इस दृष्टि से उसका मूल्य भी है, महत्व भी है और उसकी सार-सम्भाल भी करनी है । किन्तु ध्यान रहे दृष्टि नौका पर नहीं कूल पर होना है, नौका साधन है साध्य नहीं । भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की एक साधन के रूप में स्वीकृति जैनधर्म और सम्पूर्ण अध्यात्म विद्या का हार्द है । यह वह विभाजन रेखा है जो अध्यात्म और स्थानांग, १० ।
३१
निशीथभाष्य, ४७ /६१ ।
३३
आचारांग, २ / १५ ।
३४ उत्तराध्ययन, ३२ / १०१ ।
३२
१६]
भौतिकवाद में अन्तर स्पष्ट करती है। भौतिकवाद में भौतिक उपलब्धियां या जैविक मूल्य स्वयमेव साध्य है, अन्तिम है, जबकि अध्यात्म में वे किन्हीं उच्च मूल्यों का साधन है। जैनधर्म की भाषा में कहें तो साधना के द्वारा वस्तुओं का ग्रहण, दोनों ही संयम ( समत्व ) की साधना के लिए है। जैनधर्म की सम्पूर्ण साधना का मूल लक्ष्य तो एक ऐसे निराकुल, निर्विकार, निष्काम और वीतराग मानस की अभिव्यक्ति है जो कि वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन के समस्त तनावों एवं संघर्षो को समाप्त कर सके । उसके सामने मूल प्रश्न दैहिक एवं भौतिक मूल्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति का नहीं है अपितु वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में शान्ति की संस्थापना है । अतः जहां तक और जिस रूप में दैहिक और भौतिक उपलब्धियां उसमें साधक हो सकती हैं, वहां तक वे स्वीकार्य हैं, और जहां तक वे उसमें बाधक हैं, वहीं तक त्याज्य हैं । भगवान् महावीर ने आचारांग एवं उत्तराध्ययन सूत्र में इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है । वे कहते हैं कि 'जब इन्द्रियों का अपने विषयों से सम्पर्क होता है, तब उस सम्पर्क के परिणामस्वरूप सुखद - दुःखद अनुभूति भी होती है और जीवन में यह शक्य नहीं है कि इन्द्रियों का अपने विषयों से सम्पर्क न हो और उसके कारण सुखद या दुःखद अनुभूति न हो, अतः त्याग इन्द्रियानुभूति का नहीं अपितु उसके प्रति चित्त में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेष का करना है, ३३ क्योंकि इन्द्रियों के मनोज्ञ या अमनोज्ञ विषय आसक्तचित्त के लिए ही राग-द्वेष ( मानसिक विक्षोभों ) का कारण बनते हैं अनासक्त या वीतराग के लिए नहीं । ३४ अतः जैनधर्म की मूल शिक्षा ममत्व के विसर्जन की जीवन के निषेध की नहीं ।
जैन अध्यात्मवाद की विशेषताएँ :
Jain Education International
(क) ईश्वर वाद से मुक्ति - जैन अध्यात्मवाद ने मनुष्य को ईश्वरीय दासता से मुक्त कर मानवीय स्वतन्त्रता की
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org