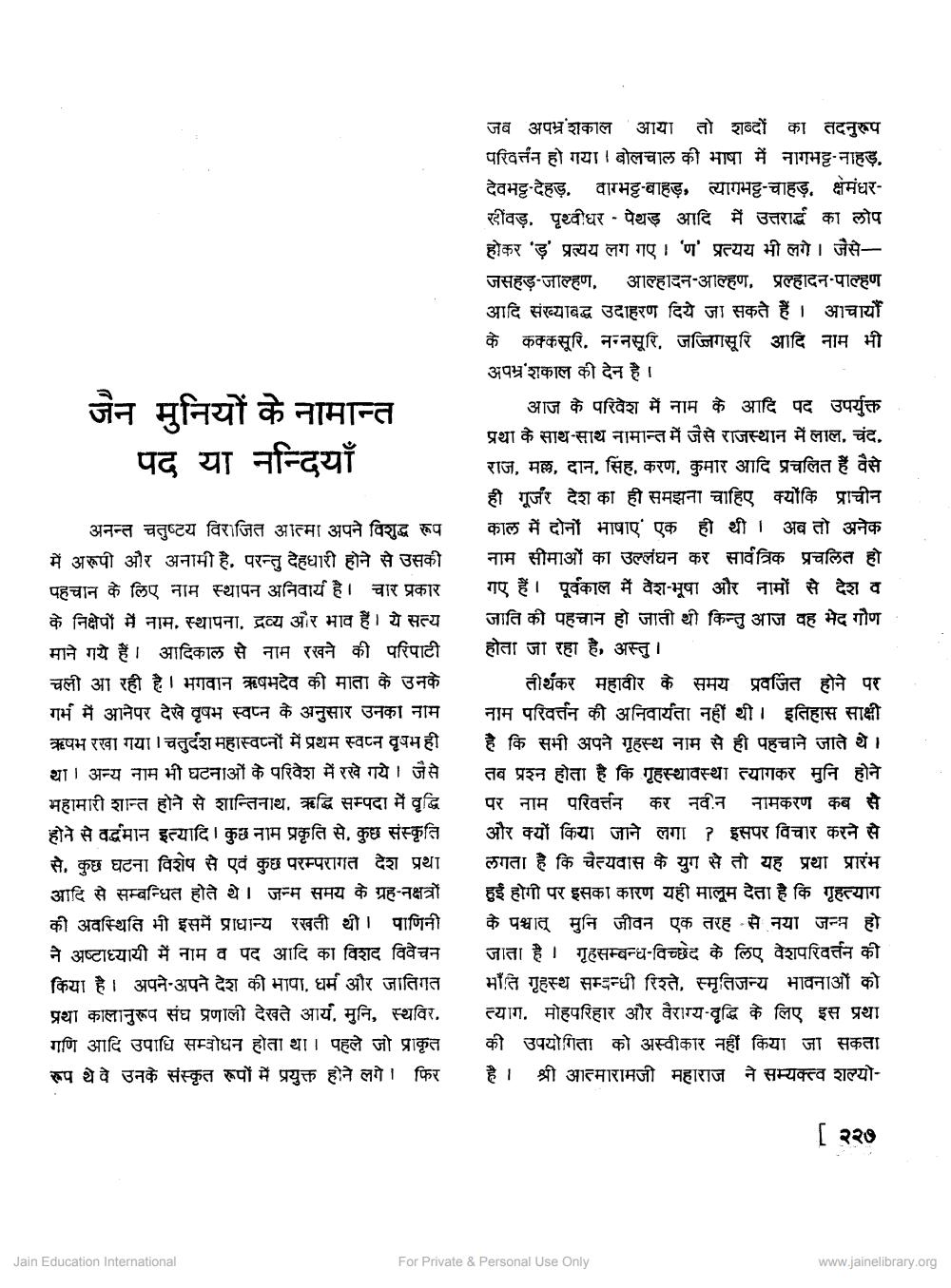________________
जैन मुनियों के नामान्त पद या नन्दियाँ
अनन्त चतुष्टय विराजित आत्मा अपने विशुद्ध रूप में अरूपी और अनामी है, परन्तु देहधारी होने से उसकी पहचान के लिए नाम स्थापन अनिवार्य है। चार प्रकार के निक्षेपों में नाम. स्थापना. द्रव्य और भाव हैं। ये सत्य माने गये हैं। आदिकाल से नाम रखने की परिपाटी चली आ रही है। भगवान ऋषभदेव की माता के उनके गर्भ में आनेपर देखे वृषभ स्वप्न के अनुसार उनका नाम ऋषभ रखा गया । चतुर्दश महास्वप्नों में प्रथम स्वप्न वृषम ही था। अन्य नाम भी घटनाओं के परिवेश में रखे गये। जैसे महामारी शान्त होने से शान्तिनाथ, ऋद्धि सम्पदा में वृद्धि होने से वर्द्धमान इत्यादि । कुछ नाम प्रकृति से, कुछ संस्कृति से, कुछ घटना विशेष से एवं कुछ परम्परागत देश प्रथा आदि से सम्बन्धित होते थे। जन्म समय के ग्रह-नक्षत्रों की अवस्थिति भी इसमें प्राधान्य रखती थी। पाणिनी ने अष्टाध्यायी में नाम व पद आदि का विशद विवेचन किया है। अपने-अपने देश की भाषा, धर्म और जातिगत प्रथा कालानुरूप संघ प्रणाली देखते आर्य, मुनि, स्थविर, गणि आदि उपाधि सम्बोधन होता था। पहले जो प्राकृत रूप थे वे उनके संस्कृत रूपों में प्रयुक्त होने लगे। फिर
जब अपभ्रंशकाल आया तो शब्दों का तदनुरुप परिवर्तन हो गया । बोलचाल की भाषा में नागभट्ट नाहड़, देवमट्ट-देहड़, वाग्भट्ट-बाहड़, त्यागभट्ट-चाहड़, मंधरटींवड़, पृथ्वीधर - पेथड़ आदि में उत्तरार्द्ध का लोप होकर 'ड' प्रत्यय लग गए। 'ण' प्रत्यय भी लगे। जैसेजसहड़-जालहण, आल्हादन-आल्हण, प्रल्हादन-पाल्हण आदि संख्याबद्ध उदाहरण दिये जा सकते हैं। आचार्यों के कक्कसूरि. नन्नसूरि, जजिगसूरि आदि नाम भी अपभ्रशकाल की देन है।
आज के परिवेश में नाम के आदि पद उपर्युक्त प्रथा के साथ-साथ नामान्त में जैसे राजस्थान में लाल, चंद, राज, मल्ल, दान. सिंह, करण, कुमार आदि प्रचलित हैं वैसे ही गूर्जर देश का ही समझना चाहिए क्योंकि प्राचीन काल में दोनों भाषाए एक ही थी । अब तो अनेक नाम सीमाओं का उल्लंघन कर सार्वत्रिक प्रचलित हो गए हैं। पूर्वकाल में वेश-भूषा और नामों से देश व जाति की पहचान हो जाती थी किन्तु आज वह भेद गौण . होता जा रहा है, अस्तु ।
तीर्थंकर महावीर के समय प्रवर्जित होने पर नाम परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं थी। इतिहास साक्षी है कि सभी अपने गृहस्थ नाम से ही पहचाने जाते थे। तब प्रश्न होता है कि गृहस्थावस्था त्यागकर मुनि होने पर नाम परिवर्तन कर नवीन नामकरण कब से और क्यों किया जाने लगा ? इसपर विचार करने से लगता है कि चैत्यवास के युग से तो यह प्रथा प्रारंभ हुई होगी पर इसका कारण यही मालूम देता है कि गृहत्याग के पश्चात् मुनि जीवन एक तरह से नया जन्म हो जाता है । गृहसम्बन्ध-विच्छेद के लिए वेशपरिवर्तन की माँति गृहस्थ सम्बन्धी रिश्ते, स्मृतिजन्य भावनाओं को त्याग. मोहपरिहार और वैराग्य वृद्धि के लिए इस प्रथा की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री आत्मारामजी महाराज ने सम्यक्त्व शल्यो
[ २२७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org