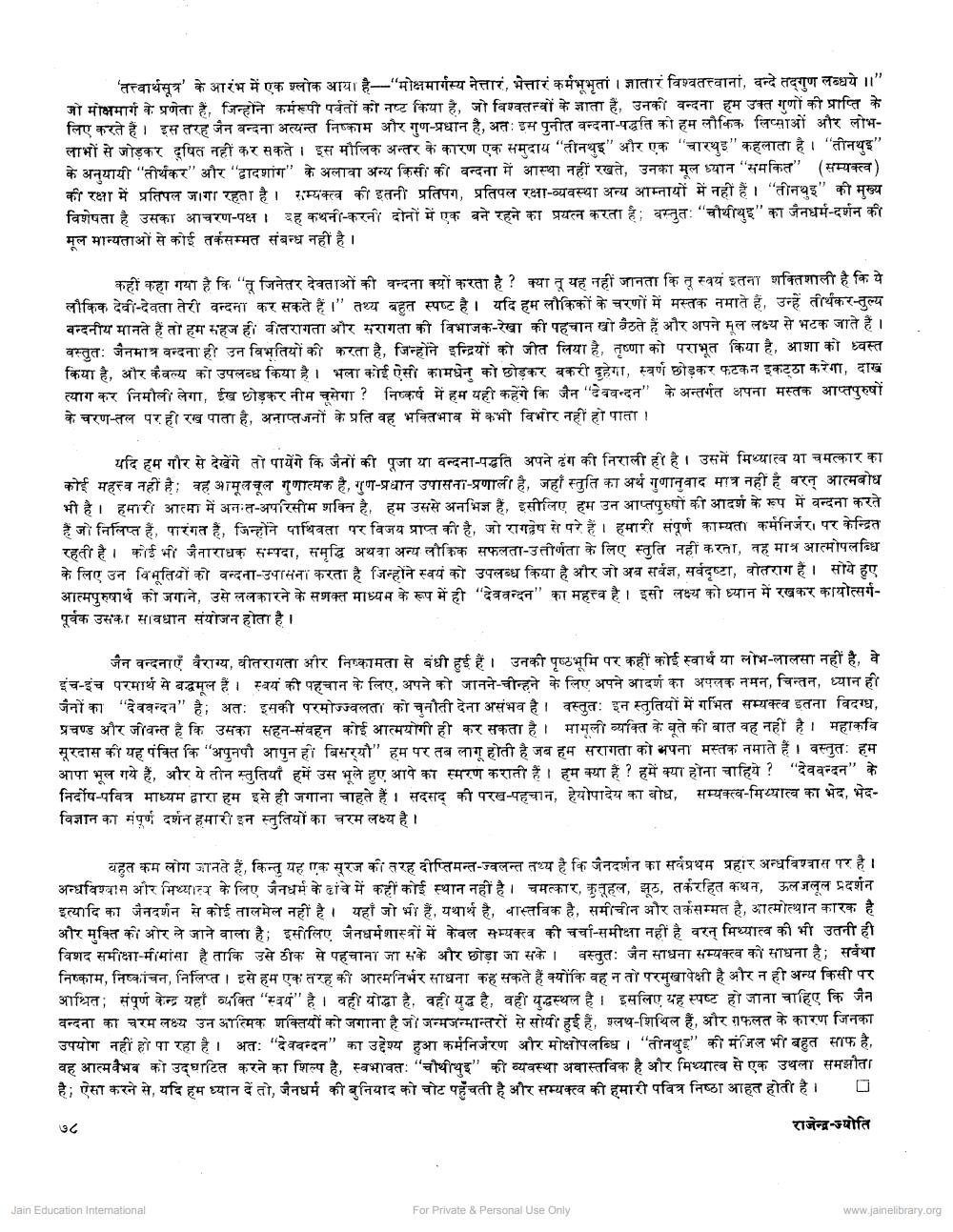________________
'तत्त्वार्थसूत्र' के आरंभ में एक श्लोक आया है-"मोक्षमार्गस्य नेत्तार, भेत्तारं कर्मभूभृतां । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुण लब्धये ॥" जो मोक्षमार्ग के प्रणेता हैं, जिन्होंने कर्मरूपी पर्वतों को नष्ट किया है, जो विश्वतत्वों के ज्ञाता हैं, उनकी वन्दना हम उक्त गणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस तरह जैन वन्दना अत्यन्त निष्काम और गुण-प्रधान है, अतः इस पुनीत वन्दना-पद्धति को हम लौकिक लिप्साओं और लोभलाभों से जोड़कर दुषित नहीं कर सकते। इस मौलिक अन्तर के कारण एक समुदाय “तीनथुइ" और एक “चारथुइ" कहलाता है । “तीनथुइ" के अनुयायी "तीर्थकर" और "द्वादशांग" के अलावा अन्य किसी की वन्दना में आस्था नहीं रखते, उनका मूल ध्यान “समकित" (सम्यक्त्व) की रक्षा में प्रतिपल जागा रहता है। सम्यक्त्व की इतनी प्रतिपग, प्रतिपल रक्षा-व्यवस्था अन्य आम्नायों में नहीं हैं। "तीनथुइ" की मुख्य विशेषता है उसका आचरण-पक्ष। वह कथनी-करनी दोनों में एक बने रहने का प्रयत्न करता है; वस्तुतः “चौथीथुइ" का जैनधर्म-दर्शन की मुल मान्यताओं से कोई तर्कसम्मत संबन्ध नहीं है।
कहीं कहा गया है कि " जिनेतर देवताओं की वन्दना क्यों करता है ? क्या तू यह नहीं जानता कि तू स्वयं इतना शक्तिशाली है कि ये लौकिक देवी-देवता तेरी वन्दना कर सकते हैं।" तथ्य बहुत स्पष्ट है। यदि हम लौकिकों के चरणों में मस्तक नमाते हैं, उन्हें तीर्थंकर-तुल्य वन्दनीय मानते हैं तो हम सहज ही वीतरागता और सरागता की विभाजक-रेखा की पहचान खो बैठते हैं और अपने मूल लक्ष्य से भटक जाते हैं । वस्तुतः जैनमात्र वन्दना ही उन विभतियों की करता है, जिन्होंने इन्द्रियों को जीत लिया है, तृष्णा को पराभूत किया है, आशा को ध्वस्त किया है, और कैवल्य को उपलब्ध किया है। भला कोई ऐसी कामधेन को छोड़कर बकरी दुहेगा, स्वर्ण छोड़कर फटक न इकट्ठा करेगा, दाख त्याग कर निमौली लेगा, ईख छोड़कर नीम चसेगा? निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि जैन "देवबन्दन" के अन्तर्गत अपना मस्तक आप्तपुरुषों के चरण-तल पर ही रख पाता है, अनाप्तजनों के प्रति वह भक्तिभाव में कभी विभोर नहीं हो पाता।
यदि हम गौर से देखेंगे तो पायेंगे कि जैनों की पूजा या वन्दना-पद्धति अपने ढंग की निराली ही है। उसमें मिथ्यात्व या चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है। वह आमूलचूल गुणात्मक है, गुण-प्रधान उपासना-प्रणाली है, जहाँ स्तुति का अर्थ गुणानुवाद मात्र नहीं है वरन् आत्मबोध भी है। हमारी आत्मा में अन-त-अपरिसीम शक्ति है, हम उससे अनभिज्ञ हैं, इसीलिए हम उन आप्तपुरुषों की आदर्श के रूप में वन्दना करते हैं जो निलिप्त हैं, पारंगत हैं, जिन्होंने पार्थिवता पर विजय प्राप्त की है, जो रागद्वेष से परे हैं। हमारी संपूर्ण काम्यता कर्मनिर्जर। पर केन्द्रित रहती है। कोई भी जैनाराधक सम्पदा, समृद्धि अथवा अन्य लौकिक सफलता-उत्तीर्णता के लिए स्तुति नहीं करता, तह मात्र आत्मोपलब्धि के लिए उन विभूतियों को वन्दना-उपासना करता है जिन्होंने स्वयं को उपलब्ध किया है और जो अब सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, बोतराग हैं। सोये हुए आत्मपुरुषार्थ को जगाने, उसे ललकारने के सशक्त माध्यम के रूप में ही “देववन्दन" का महत्त्व है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर कायोत्सर्गपूर्वक उसका सावधान संयोजन होता है।
जैन वन्दनाएँ वैराग्य, वीतरागता और निष्कामता से बंधी हुई हैं। उनकी पृष्ठभूमि पर कहीं कोई स्वार्थ या लोभ-लालसा नहीं है, वे इंच-इंच परमार्थ से बद्धमूल हैं। स्वयं की पहचान के लिए, अपने को जानने-चीन्हने के लिए अपने आदर्श का अपलक नमन, चिन्तन, ध्यान ही जैनों का “देववन्दन" है। अतः इसकी परमोज्ज्वलता को चनौती देना असंभव है। वस्तुतः इन स्तुतियों में गभित सम्यक्त्व इतना विदग्ध, प्रचण्ड और जीवन्त है कि उसका सहन-संवहन कोई आत्मयोगी ही कर सकता है। मामूली व्यक्ति के बूते की बात वह नहीं है। महाकवि सूरदास की यह पंक्ति कि "अपुनपौ आपुन ही बिसर्यो" हम पर तब लागू होती है जब हम सरागता को अपना मस्तक नमाते हैं। वस्तुतः हम आपा भूल गये हैं, और ये तीन स्तुतियाँ हमें उस भूले हुए आपे का स्मरण कराती हैं। हम क्या हैं ? हमें क्या होना चाहिये? "देववन्दन" के निर्दोष-पवित्र माध्यम द्वारा हम इसे ही जगाना चाहते हैं। सदसद् की परख-पहचान, हेयोपादेय का बोध, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व का भेद, भेदविज्ञान का मंपूर्ण दर्शन हमारी इन स्तुतियों का चरम लक्ष्य है।
बहुत कम लोग जानते हैं, किन्तु यह एक सुरज की तरह दीप्तिमन्त-ज्वलन्त तथ्य है कि जैनदर्शन का सर्वप्रथम प्रहार अन्धविश्वास पर है। अन्धविश्वास और मिथ्यात्य के लिए जैनधर्म के ढांचे में कहीं कोई स्थान नहीं है। चमत्कार, कुतूहल, झूठ, तर्करहित कथन, ऊलजलूल प्रदर्शन इत्यादि का जैनदर्शन से कोई तालमेल नहीं है। यहाँ जो भी हैं, यथार्थ है, वास्तविक है, समीचीन और तर्कसम्मत है, आत्मोत्थान कारक है और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए जैनधर्मशास्त्रों में केवल सम्यक्त्व की चर्चा-समीक्षा नहीं है वरन् मिथ्यात्व की भी उतनी ही विशद समीक्षा-मीमांसा है ताकि उसे ठीक से पहचाना जा सके और छोड़ा जा सके। वस्तुत: जैन साधना सम्यक्त्व को साधना है; सर्वथा निष्काम, निष्कांचन, निलिप्त । इसे हम एक तरह की आत्मनिर्भर साधना कह सकते हैं क्योंकि वह न तो परमुखापेक्षी है और न ही अन्य किसी पर आथित; संपूर्ण केन्द्र यहाँ व्यक्ति "स्वयं" है। वही योद्धा है, वहीं युद्ध है, वही युद्धस्थल है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जैन वन्दना का चरम लक्ष्य उन आत्मिक शक्तियों को जगाना है जो जन्मजन्मान्तरों से सोयी हुई हैं, श्लथ-शिथिल हैं, और गफलत के कारण जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः "देववन्दन" का उद्देश्य हुआ कर्मनिर्जरण और मोक्षोपलब्धि । “तीनथुइ" की मंजिल भी बहुत साफ है, वह आत्मवैभव को उद्घाटित करने का शिल्प है, स्वभावतः "चौथीथुइ" की व्यवस्था अवास्तविक है और मिथ्यात्व से एक उथला समझौता है। ऐसा करने से, यदि हम ध्यान दें तो, जैनधर्म की बुनियाद को चोट पहुँचती है और सम्यक्त्व की हमारी पवित्र निष्ठा आहत होती है।
राजेन्द्र-ज्योति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org