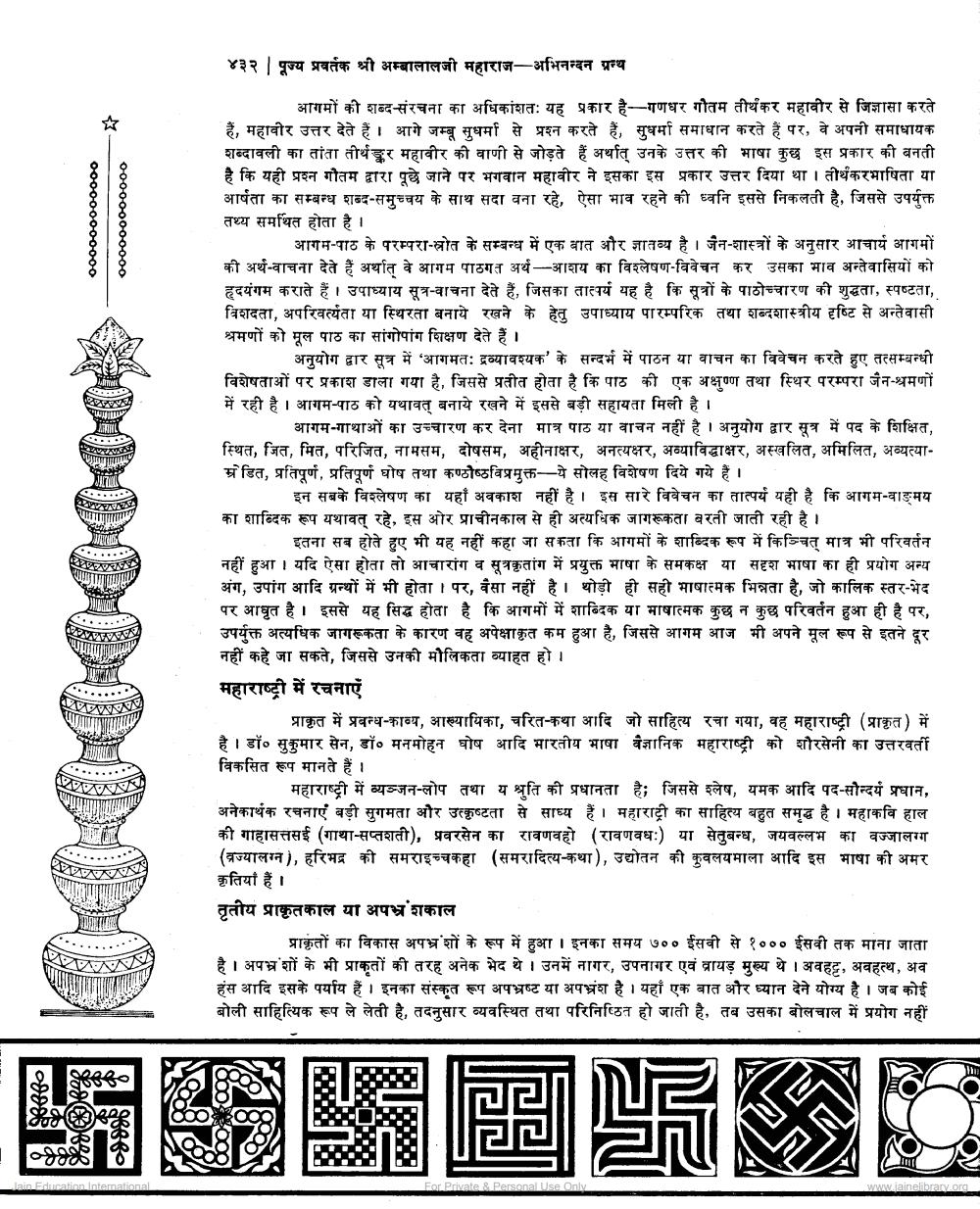________________
४३२ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
००००००००००००
००००००००००००
Corte
HERBERGC
4...
___आगमों की शब्द-संरचना का अधिकांशतः यह प्रकार है-गणधर गौतम तीर्थंकर महावीर से जिज्ञासा करते हैं, महावीर उत्तर देते हैं। आगे जम्बू सुधर्मा से प्रश्न करते हैं, सुधर्मा समाधान करते हैं पर, वे अपनी समाधायक शब्दावली का तांता तीर्थङ्कर महावीर की वाणी से जोड़ते हैं अर्थात् उनके उत्तर की भाषा कुछ इस प्रकार की बनती है कि यही प्रश्न गौतम द्वारा पूछे जाने पर भगवान महावीर ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया था । तीर्थंकरभाषिता या आर्षता का सम्बन्ध शब्द-समुच्चय के साथ सदा बना रहे, ऐसा भाव रहने की ध्वनि इससे निकलती है, जिससे उपर्युक्त तथ्य समर्थित होता है।
आगम-पाठ के परम्परा-स्रोत के सम्बन्ध में एक बात और ज्ञातव्य है । जैन-शास्त्रों के अनुसार आचार्य आगमों की अर्थ-वाचना देते हैं अर्थात् वे आगम पाठगत अर्थ-आशय का विश्लेषण-विवेचन कर उसका भाव अन्तेवासियों को हृदयंगम कराते हैं । उपाध्याय सूत्र-वाचना देते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि सूत्रों के पाठोच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता, विशदता, अपरिवर्त्यता या स्थिरता बनाये रखने के हेतु उपाध्याय पारम्परिक तथा शब्दशास्त्रीय दृष्टि से अन्तेवासी श्रमणों को मूल पाठ का सांगोपांग शिक्षण देते हैं।
अनुयोग द्वार सूत्र में 'आगमत: द्रव्यावश्यक' के सन्दर्भ में पाठन या वाचन का विवेचन करते हुए तत्सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे प्रतीत होता है कि पाठ की एक अक्षुण्ण तथा स्थिर परम्परा जैन-श्रमणों में रही है । आगम-पाठ को यथावत् बनाये रखने में इससे बड़ी सहायता मिली है।
आगम-गाथाओं का उच्चारण कर देना मात्र पाठ या वाचन नहीं है । अनुयोग द्वार सूत्र में पद के शिक्षित, स्थित, जित, मित, परिजित, नामसम, दोषसम, अहीनाक्षर, अनत्यक्षर, अव्याविद्धाक्षर, अस्खलित, अमिलित, अव्यत्यादंडित, प्रतिपूर्ण, प्रतिपूर्ण घोष तथा कण्ठोष्ठविप्रमुक्त-ये सोलह विशेषण दिये गये हैं।
इन सबके विश्लेषण का यहाँ अवकाश नहीं है। इस सारे विवेचन का तात्पर्य यही है कि आगम-वाङ्मय का शाब्दिक रूप यथावत् रहे, इस ओर प्राचीनकाल से ही अत्यधिक जागरूकता बरती जाती रही है।
. इतना सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि आगमों के शाब्दिक रूप में किञ्चित् मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो आचारांग व सूत्रकृतांग में प्रयुक्त भाषा के समकक्ष या सदृश भाषा का ही प्रयोग अन्य अंग, उपांग आदि ग्रन्थों में भी होता । पर, वैसा नहीं है। थोड़ी ही सही भाषात्मक भिन्नता है, जो कालिक स्तर-भेद पर आघृत है। इससे यह सिद्ध होता है कि आगमों में शाब्दिक या भाषात्मक कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ ही है पर, उपर्युक्त अत्यधिक जागरूकता के कारण वह अपेक्षाकृत कम हुआ है, जिससे आगम आज भी अपने मूल रूप से इतने दूर नहीं कहे जा सकते, जिससे उनकी मौलिकता व्याहत हो। महाराष्ट्री में रचनाएँ
प्राकृत में प्रबन्ध-काव्य, आख्यायिका, चरित-कथा आदि जो साहित्य रचा गया, वह महाराष्ट्री (प्राकृत) में है । डॉ० सुकुमार सेन, डॉ. मनमोहन घोष आदि भारतीय भाषा वैज्ञानिक महाराष्ट्री को शौरसेनी का उत्तरवर्ती विकसित रूप मानते हैं।
महाराष्ट्री में व्यञ्जन-लोप तथा य श्रुति की प्रधानता है। जिससे श्लेष, यमक आदि पद-सौन्दर्य प्रधान, अनेकार्थक रचनाएं बड़ी सुगमता और उत्कृष्टता से साध्य हैं। महाराट्री का साहित्य बहुत समृद्ध है । महाकवि हाल की गाहासत्तसई (गाथा-सप्तशती), प्रवरसेन का रावणवहो (रावणवधः) या सेतुबन्ध, जयवल्लभ का वज्जालग्ग (व्रज्यालग्न), हरिभद्र की समराइच्चकहा (समरादित्य-कथा), उद्योतन की कुवलयमाला आदि इस भाषा की अमर कृतियां हैं। तृतीय प्राकृतकाल या अपभ्रंशकाल
प्राकृतों का विकास अपभ्रंशों के रूप में हुआ । इनका समय ७०० ईसवी से १००० ईसवी तक माना जाता है। अपभ्र'शों के भी प्राक़तों की तरह अनेक भेद थे। उनमें नागर, उपनागर एवं व्रायड़ मुख्य थे । अवहट्ट, अवहत्थ, अव हंस आदि इसके पर्याय हैं। इनका संस्कृत रूप अपभ्रष्ट या अपभ्रंश है । यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । जब कोई बोली साहित्यिक रूप ले लेती है, तदनुसार व्यवस्थित तथा परिनिष्ठित हो जाती है, तब उसका बोलचाल में प्रयोग नहीं
METARAN
A
VIR
M.DO
Lain Education Interational
For Private
Personal use only
www.iainelibrary.org