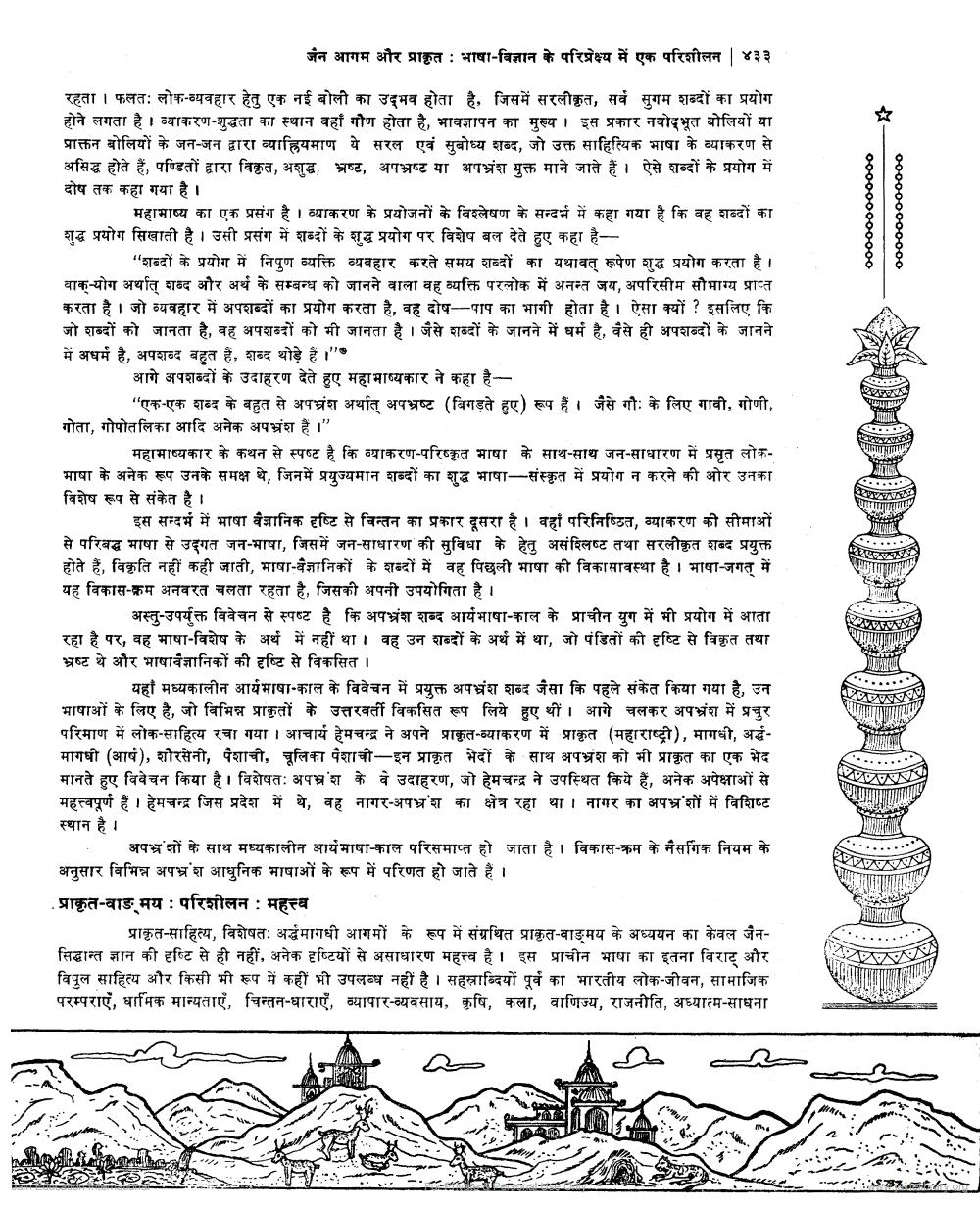________________
जैन आगम और प्राकृत भाषा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक परिशीलन | ४३३ रहता। फलतः सो व्यवहार हेतु एक नई बोली का उद्भव होता है, जिसमें सरलीकृत सर्व सुगम शब्दों का प्रयोग होने लगता है । व्याकरण शुद्धता का स्थान वहाँ गौण होता है, भावज्ञापन का मुख्य । इस प्रकार नवोद्भुत बोलियों या सरल एवं सुबोध्य शब्द, जो उक्त साहित्यिक भाषा के व्याकरण से अपभ्रष्ट या अपभ्रंश युक्त माने जाते हैं । ऐसे शब्दों के प्रयोग में
प्राक्तन बोलियों के जन-जन द्वारा व्याह्रियमाण ये afe होते हैं, पण्डितों द्वारा विकृत, अशुद्ध, भ्रष्ट, दोष तक कहा गया है ।
महाभाष्य का एक प्रसंग है । व्याकरण के प्रयोजनों के विश्लेषण के सन्दर्भ में कहा गया है कि वह शब्दों का प्रयोग सिखाती है। उसी प्रसंग में शब्दों के शुद्ध प्रयोग पर विशेष बल देते हुए कहा है
शुद्ध
"शब्दों के प्रयोग में निपुण व्यक्ति व्यवहार करते समय शब्दों का यथावत् रूपेण शुद्ध प्रयोग करता है । वाक्-योग अर्थात् शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानने वाला वह व्यक्ति परलोक में अनन्त जय, अपरिसीम सौभाग्य प्राप्त करता है । जो व्यवहार में अपशब्दों का प्रयोग करता है, वह दोष-पाप का भागी होता है। ऐसा क्यों ? इसलिए कि जो शब्दों को जानता है, वह अपशब्दों को भी जानता है । जैसे शब्दों के जानने में धर्म है, वैसे ही अपशब्दों के जानने में अधर्म है, अपशब्द बहुत हैं, शब्द थोड़े हैं।"
आगे अपशब्दों के उदाहरण देते हुए महामाष्यकार ने कहा है
"एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश अर्थात् अपभ्रष्ट (बिगड़ते हुए ) रूप है जैसे गौ के लिए गावी गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अनेक अपभ्रंश हैं ।"
महाभाष्यकार के कथन से स्पष्ट है कि व्याकरण- परिष्कृत भाषा के साथ-साथ जन साधारण में प्रसृत लोकभाषा के अनेक रूप उनके समक्ष थे, जिनमें प्रयुज्यमान शब्दों का शुद्ध भाषा-संस्कृत में प्रयोग न करने की ओर उनका विशेष रूप से संकेत है ।
इस सन्दर्भ में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से चिन्तन का प्रकार दूसरा है । वहाँ परिनिष्ठित, व्याकरण की सीमाओं से परिबद्ध भाषा से उद्गत जन-भाषा, जिसमें जन-साधारण की सुविधा के हेतु असंश्लिष्ट तथा सरलीकृत शब्द प्रयुक्त होते हैं, विकृति नहीं कही जाती, भाषा वैज्ञानिकों के शब्दों में वह पिछली भाषा की विकासावस्था है । भाषा जगत् में यह विकास क्रम अनवरत चलता रहता है, जिसकी अपनी उपयोगिता है ।
अस्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपभ्रंश शब्द आर्यभाषा काल के प्राचीन युग में भी प्रयोग में आता रहा है पर, वह भाषा - विशेष के अर्थ में नहीं था । वह उन शब्दों के अर्थ में था, जो पंडितों की दृष्टि से विकृत तथा भ्रष्ट थे और भाषावैज्ञानिकों की दृष्टि से विकसित ।
यहाँ मध्यकालीन आर्यभाषा - काल के विवेचन में प्रयुक्त अपभ्रंश शब्द जैसा कि पहले संकेत किया गया है, उन भाषाओं के लिए है, जो विभिन्न प्राकृतों के उत्तरवर्ती विकसित रूप लिये हुए थीं। आगे चलकर अपभ्रंश में प्रचुर परिमाण में लोक-साहित्य रचा गया। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में प्राकृत (महाराष्ट्री), मागधी, अर्द्धमागधी (आर्ष), शौरसेनी, पैशाची, चूलिका पैशाची - इन प्राकृत भेदों के साथ अपभ्रंश को भी प्राकृत का एक भेद मानते हुए विवेचन किया है। विशेषतः अपभ्रंश के वे उदाहरण, जो हेमचन्द्र ने उपस्थित किये हैं, अनेक अपेक्षाओं से महत्त्वपूर्ण हैं । हेमचन्द्र जिस प्रदेश में थे, वह नागर- अपभ्रंश का क्षेत्र रहा था। नागर का अपभ्रंशों में विशिष्ट
स्थान है ।
अपभ्रंशों के साथ मध्यकालीन आर्यभाषा-काल परिसमाप्त हो जाता है । विकास क्रम के नैसर्गिक नियम के अनुसार विभिन्न अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के रूप में परिणत हो जाते हैं ।
प्राकृत वाङमय: परिशीलन महत्व
+4
प्राकृत-साहित्य, विशेषतः अर्द्धमागधी आगमों के रूप में संबंधित प्राकृत वाङ्मय के अध्ययन का केवल जैनसिद्धान्त ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, अनेक दृष्टियों से असाधारण महत्त्व है। इस प्राचीन भाषा का इतना विराट् और विपुल साहित्य और किसी भी रूप में कहीं भी उपलब्ध नहीं है । सहस्राब्दियों पूर्व का भारतीय लोक-जीवन, सामाजिक परम्पराएँ, धार्मिक मान्यताएँ, चिन्तन धाराएँ, व्यापार-व्यवसाय, कृषि, कला, वाणिज्य, राजनीति, अध्यात्म-साधना
Moral me
The
2
*
000000000000 000000000000
400bbbbbbbt