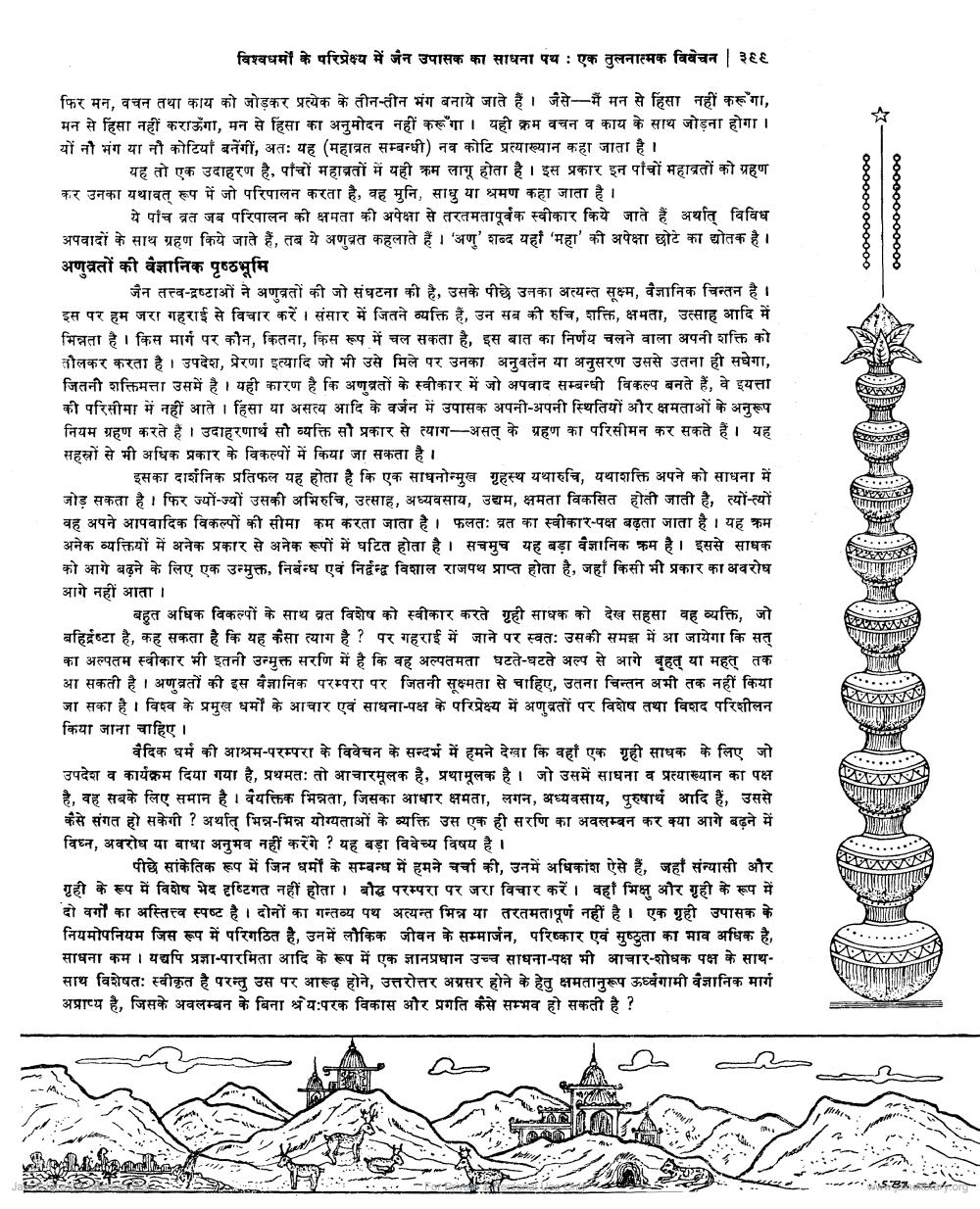________________
विश्वधर्मो के परिप्रेक्ष्य में जैन उपासक का साधना पथ : एक तुलनात्मक विवेचन | ३६६ फिर मन, वचन तथा काय को जोड़कर प्रत्येक के तीन-तीन भंग बनाये जाते हैं। जैसे- मैं मन से हिंसा नहीं करूँगा, मन से हिंसा नहीं कराऊँगा, मन से हिंसा का अनुमोदन नहीं करूँगा । यही क्रम वचन व काय के साथ जोड़ना होगा । यों नौ भंग या नौ कोटियाँ बनेंगीं, अतः यह (महाव्रत सम्बन्धी ) नव कोटि प्रत्याख्यान कहा जाता है ।
यह तो एक उदाहरण है, पाँचों महाव्रतों में यही क्रम लागू होता है। इस प्रकार इन पाँचों महाव्रतों को ग्रहण कर उनका यथावत् रूप में जो परिपालन करता है, वह मुनि, साधु या श्रमण कहा जाता है ।
ये पाँच व्रत जब परिपालन की क्षमता की अपेक्षा से तरतमतापूर्वक स्वीकार किये जाते हैं अर्थात् विविध अपवादों के साथ ग्रहण किये जाते हैं, तब ये अणुव्रत कहलाते हैं। 'अणु' शब्द यहाँ 'महा' की अपेक्षा छोटे का द्योतक है । अणुव्रतों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि
जैन तत्त्व-द्रष्टाओं ने अणुव्रतों की जो संघटना की है, उसके पीछे उनका अत्यन्त सूक्ष्म, वैज्ञानिक चिन्तन है । इस पर हम जरा गहराई से विचार करें। संसार में जितने व्यक्ति हैं, उन सब की रुचि, शक्ति, क्षमता, उत्साह आदि में भिन्नता है । किस मार्ग पर कौन, कितना, किस रूप में चल सकता है, इस बात का निर्णय चलने वाला अपनी शक्ति को तौलकर करता है । उपदेश, प्रेरणा इत्यादि जो भी उसे मिले पर उनका अनुवर्तन या अनुसरण उससे उतना ही सघेगा, जितनी शक्तिमत्ता उसमें है । यही कारण है कि अणुव्रतों के स्वीकार में जो अपवाद सम्बन्धी विकल्प बनते हैं, वे इयत्ता की परिसीमा में नहीं आते। हिंसा या असत्य आदि के वर्जन में उपासक अपनी-अपनी स्थितियों और क्षमताओं के अनुरूप नियम ग्रहण करते हैं । उदाहरणार्थं सौ व्यक्ति सौ प्रकार से त्याग — असत् के ग्रहण का परिसीमन कर सकते हैं । यह सहस्रों से भी अधिक प्रकार के विकल्पों में किया जा सकता है ।
इसका दार्शनिक प्रतिफल यह होता है कि एक साधनोन्मुख गृहस्थ यथारुचि, यथाशक्ति अपने को साधना में जोड़ सकता है । फिर ज्यों-ज्यों उसकी अभिरुचि, उत्साह, अध्यवसाय, उद्यम, क्षमता विकसित होती जाती है, त्यों-त्यों वह अपने आपवादिक विकल्पों की सीमा कम करता जाता है । फलतः व्रत का स्वीकार पक्ष बढ़ता जाता है । यह क्रम अनेक व्यक्तियों में अनेक प्रकार से अनेक रूपों में घटित होता है । सचमुच यह बड़ा वैज्ञानिक क्रम है। इससे साधक को आगे बढ़ने के लिए एक उन्मुक्त, निर्बन्ध एवं निर्द्वन्द्व विशाल राजपथ प्राप्त होता है, जहाँ किसी भी प्रकार का अवरोध आगे नहीं आता ।
बहुत अधिक विकल्पों के साथ व्रत विशेष को स्वीकार करते गृही साधक को देख सहसा वह व्यक्ति, जो बहिर्द्रष्टा है, कह सकता है कि यह कैसा त्याग है ? पर गहराई में जाने पर स्वतः उसकी समझ में आ जायेगा कि सत् का अल्पतम स्वीकार भी इतनी उन्मुक्त सरणि में है कि वह अल्पतमता घटते घटते अल्प से आगे बृहत् या महत् तक आ सकती है । अणुव्रतों की इस वैज्ञानिक परम्परा पर जितनी सूक्ष्मता से चाहिए, उतना चिन्तन अभी तक नहीं किया जा सका है । विश्व के प्रमुख धर्मों के आचार एवं साधना-पक्ष के परिप्रेक्ष्य में अणुव्रतों पर विशेष तथा विशद परिशीलन किया जाना चाहिए ।
वैदिक धर्म की आश्रम-परम्परा के विवेचन के सन्दर्भ में हमने देखा कि वहाँ एक गृही साधक के लिए जो उपदेश व कार्यक्रम दिया गया है, प्रथमतः तो आचारमूलक है, प्रथामूलक है। जो उसमें साधना व प्रत्याख्यान का पक्ष है, वह सबके लिए समान है। वैयक्तिक भिन्नता, जिसका आधार क्षमता, लगन, अध्यवसाय, पुरुषार्थं आदि हैं, उससे कैसे संगत हो सकेगी ? अर्थात् भिन्न-भिन्न योग्यताओं के व्यक्ति उस एक ही सरणि का अवलम्बन कर क्या आगे बढ़ने में विघ्न, अवरोध या बाधा अनुभव नहीं करेंगे ? यह बड़ा विवेच्य विषय है ।
पीछे सांकेतिक रूप में जिन धर्मो के सम्बन्ध में हमने चर्चा की, उनमें अधिकांश ऐसे हैं, जहाँ संन्यासी और गृही के रूप में विशेष भेद दृष्टिगत नहीं होता । बौद्ध परम्परा पर जरा विचार करें। वहाँ भिक्षु और गृही के रूप में दो वर्गों का अस्तित्त्व स्पष्ट है । दोनों का गन्तव्य पथ अत्यन्त भिन्न या तरतमतापूर्ण नहीं है । एक गृही उपासक के नियमोपनियम जिस रूप में परिगठित है, उनमें लौकिक जीवन के सम्मार्जन, परिष्कार एवं सुष्ठुता का भाव अधिक है, साधना कम । यद्यपि प्रज्ञापारमिता आदि के रूप में एक ज्ञानप्रधान उच्च साधना-पक्ष भी आचार -शोधक पक्ष के साथसाथ विशेषतः स्वीकृत है परन्तु उस पर आरूढ़ होने, उत्तरोत्तर अग्रसर होने के हेतु क्षमतानुरूप ऊर्ध्वगामी वैज्ञानिक मार्ग अप्राप्य है, जिसके अवलम्बन के बिना श्रेयःपरक विकास और प्रगति कैसे सम्भव हो सकती है ?
000000000000
Hin
*
000000000000
*CODEDCODE
Basterorg