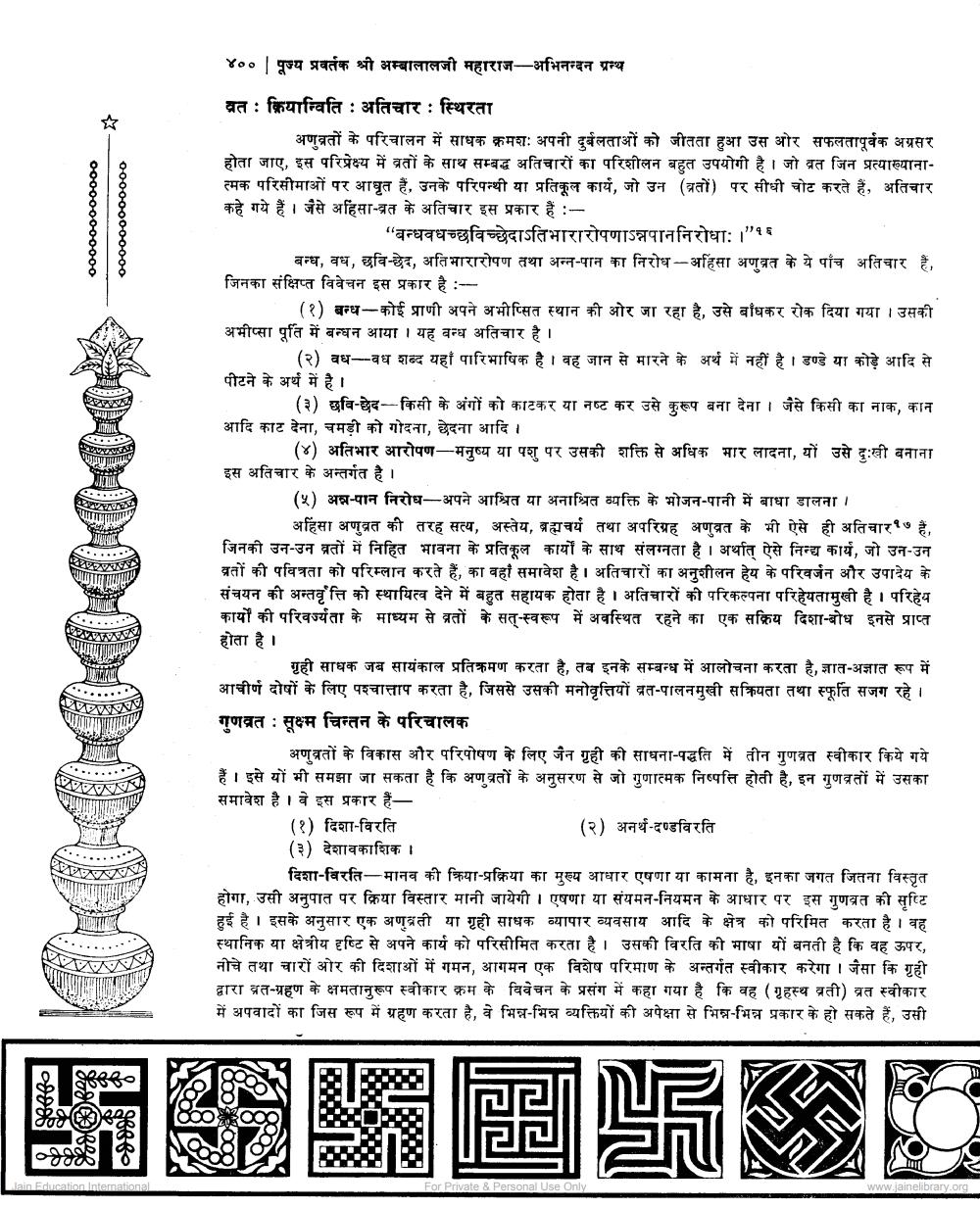________________
४०० | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
००००००००००००
००००००००००००
व्रत : क्रियान्विति : अतिचार : स्थिरता
अणुव्रतों के परिचालन में साधक क्रमशः अपनी दुर्बलताओं को जीतता हुआ उस ओर सफलतापूर्वक अग्रसर होता जाए, इस परिप्रेक्ष्य में व्रतों के साथ सम्बद्ध अतिचारों का परिशीलन बहुत उपयोगी है । जो व्रत जिन प्रत्याख्यानात्मक परिसीमाओं पर आघृत हैं, उनके परिपन्थी या प्रतिकूल कार्य, जो उन (व्रतों) पर सीधी चोट करते हैं, अतिचार कहे गये हैं। जैसे अहिंसा-व्रत के अतिचार इस प्रकार हैं :
"बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः ।"१६ बन्ध, वध, छवि-छेद, अतिभारारोपण तथा अन्न-पान का निरोध-अहिंसा अणुव्रत के ये पाँच अतिचार हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है :
(१) बन्ध-कोई प्राणी अपने अभीप्सित स्थान की ओर जा रहा है, उसे बाँधकर रोक दिया गया । उसकी अभीप्सा पूर्ति में बन्धन आया । यह बन्ध अतिचार है।
(२) वध-वध शब्द यहाँ पारिभाषिक है। वह जान से मारने के अर्थ में नहीं है । डण्डे या कोड़े आदि से पीटने के अर्थ में है।
(३) छवि-छेद-किसी के अंगों को काटकर या नष्ट कर उसे कुरूप बना देना। जैसे किसी का नाक, कान आदि काट देना, चमड़ी को गोदना, छेदना आदि ।
(४) अतिभार आरोपण-मनुष्य या पशु पर उसकी शक्ति से अधिक मार लादना, यों उसे दुःखी बनाना इस अतिचार के अन्तर्गत है।
(५) अन्न-पान निरोध-अपने आश्रित या अनाश्रित व्यक्ति के भोजन-पानी में बाधा डालना।
अहिंसा अणुव्रत की तरह सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह अणुव्रत के भी ऐसे ही अतिचार१७ हैं, जिनकी उन-उन व्रतों में निहित भावना के प्रतिकूल कार्यों के साथ संलग्नता है । अर्थात् ऐसे निन्द्य कार्य, जो उन-उन व्रतों की पवित्रता को परिम्लान करते हैं, का वहाँ समावेश है। अतिचारों का अनुशीलन हेय के परिवर्जन और उपादेय के संचयन की अन्तवृत्ति को स्थायित्व देने में बहुत सहायक होता है । अतिचारों की परिकल्पना परिहेयतामुखी है । परिहेय कार्यों की परिवर्यता के माध्यम से व्रतों के सत्-स्वरूप में अवस्थित रहने का एक सक्रिय दिशा-बोध इनसे प्राप्त होता है।
गृही साधक जब सायंकाल प्रतिक्रमण करता है, तब इनके सम्बन्ध में आलोचना करता है, ज्ञात-अज्ञात रूप में आचीर्ण दोषों के लिए पश्चात्ताप करता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियों व्रत-पालनमुखी सक्रियता तथा स्फूति सजग रहे । गुणवत : सूक्ष्म चिन्तन के परिचालक
अणुव्रतों के विकास और परिपोषण के लिए जैन गृही की साधना-पद्धति में तीन गुणव्रत स्वीकार किये गये हैं । इसे यों भी समझा जा सकता है कि अणुव्रतों के अनुसरण से जो गुणात्मक निष्पत्ति होती है, इन गुणव्रतों में उसका समावेश है। वे इस प्रकार हैं(१) दिशा-विरति
(२) अनर्थ-दण्डविरति (३) देशावकाशिक ।
दिशा-विरति-मानव की क्रिया-प्रक्रिया का मुख्य आधार एषणा या कामना है, इनका जगत जितना विस्तृत होगा, उसी अनुपात पर क्रिया विस्तार मानी जायेगी। एषणा या संयमन-नियमन के आधार पर इस गुणव्रत की सृष्टि हुई है। इसके अनुसार एक अणुव्रती या गृही साधक व्यापार व्यवसाय आदि के क्षेत्र को परिमित करता है। वह स्थानिक या क्षेत्रीय दृष्टि से अपने कार्य को परिसीमित करता है। उसकी विरति की भाषा यों बनती है कि वह ऊपर, नीचे तथा चारों ओर की दिशाओं में गमन, आगमन एक विशेष परिमाण के अन्तर्गत स्वीकार करेगा । जैसा कि गृही द्वारा व्रत-ग्रहण के क्षमतानुरूप स्वीकार क्रम के विवेचन के प्रसंग में कहा गया है कि वह (गृहस्थ व्रती) व्रत स्वीकार में अपवादों का जिस रूप में ग्रहण करता है, वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उसी
lain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org