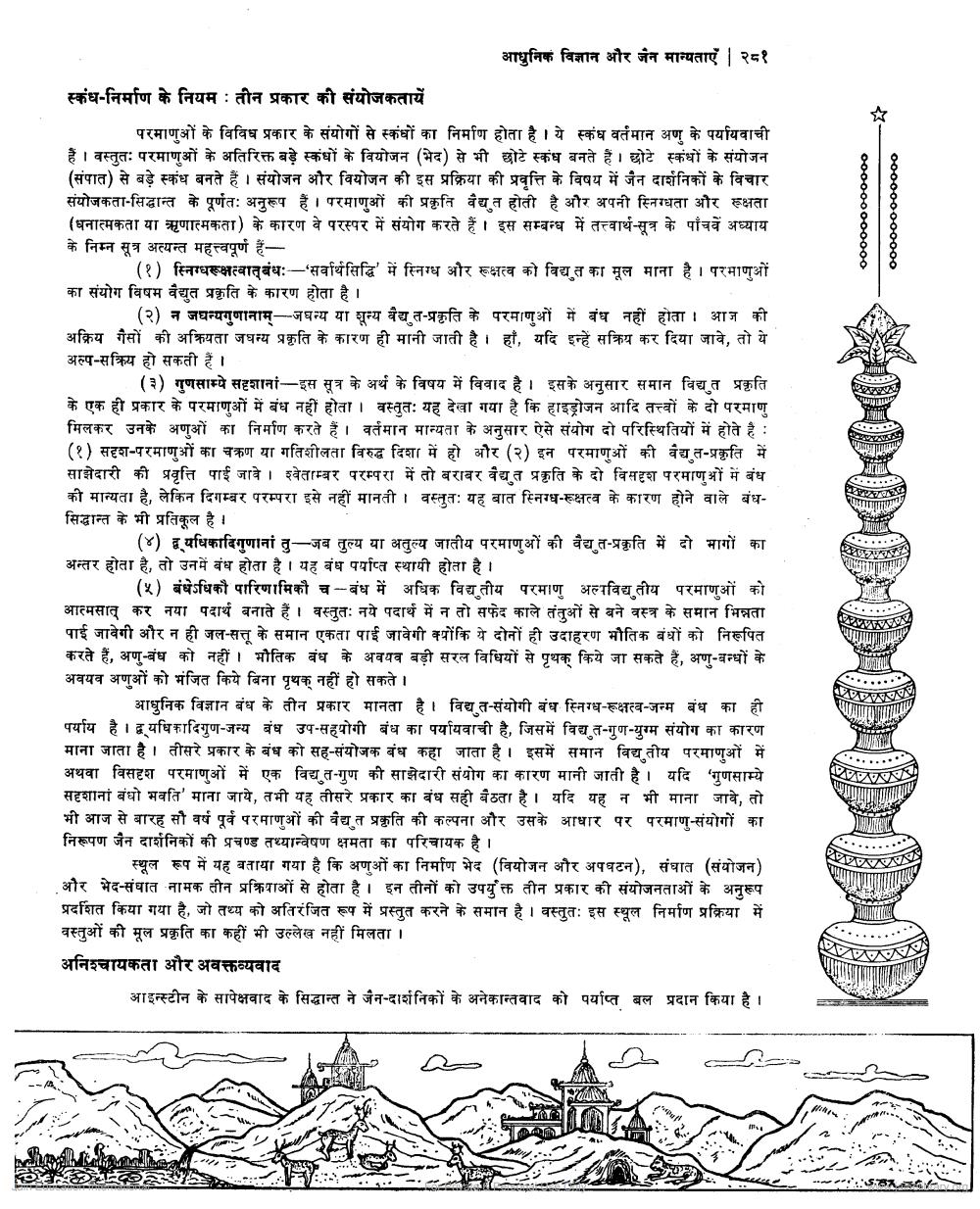________________
आधुनिक विज्ञान और जैन मान्यताएँ | २८१
००००००००००००
००००००००००००
JAIIMIRE Corno
MADE
JAMIL
THS
MLEN .....
..
JUTTAMIL
JALAN
स्कंध-निर्माण के नियम : तीन प्रकार की संयोजकतायें
परमाणुओं के विविध प्रकार के संयोगों से स्कंधों का निर्माण होता है। ये स्कंध वर्तमान अणु के पर्यायवाची हैं । वस्तुतः परमाणुओं के अतिरिक्त बड़े स्कंधों के वियोजन (भेद) से भी छोटे स्कंध बनते हैं। छोटे स्कंधों के संयोजन (संपात) से बड़े स्कंध बनते हैं । संयोजन और वियोजन की इस प्रक्रिया की प्रवृत्ति के विषय में जैन दार्शनिकों के विचार संयोजकता-सिद्धान्त के पूर्णत: अनुरूप हैं । परमाणुओं की प्रकृति वैधुत होती है और अपनी स्निग्धता और रूक्षता (धनात्मकता या ऋणात्मकता) के कारण वे परस्पर में संयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में तत्त्वार्थ-सूत्र के पांचवें अध्याय के निम्न सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं
(१) स्निग्धरूक्षत्वात्बंधः–'सर्वार्थसिद्धि' में स्निग्ध और रूक्षत्व को विद्युत का मूल माना है। परमाणुओं का संयोग विषम वैद्युत प्रकृति के कारण होता है ।
(२) न जघन्यगुणानाम्-जघन्य या शून्य वैद्य त-प्रकृति के परमाणुओं में बंध नहीं होता। आज की अक्रिय गैसों की अक्रियता जघन्य प्रकृति के कारण ही मानी जाती है। हाँ, यदि इन्हें सक्रिय कर दिया जावे, तो ये अल्प-सक्रिय हो सकती हैं।
(३) गुणसाम्ये सदृशानां-इस सूत्र के अर्थ के विषय में विवाद है। इसके अनुसार समान विद्युत प्रकृति के एक ही प्रकार के परमाणुओं में बंध नहीं होता। वस्तुतः यह देखा गया है कि हाइड्रोजन आदि तत्त्वों के दो परमाणु मिलकर उनके अणुओं का निर्माण करते हैं। वर्तमान मान्यता के अनुसार ऐसे संयोग दो परिस्थितियों में होते है : (१) सदृश-परमाणुओं का चक्रण या गतिशीलता विरुद्ध दिशा में हो और (२) इन परमाणुओं की वैद्य त-प्रकृति में साझेदारी की प्रवृत्ति पाई जावे। श्वेताम्बर परम्परा में तो बराबर वैद्युत प्रकृति के दो विसदृश परमाणुओं में बंध की मान्यता है, लेकिन दिगम्बर परम्परा इसे नहीं मानती। वस्तुत: यह बात स्निग्ध-रूक्षत्व के कारण होने वाले बंधसिद्धान्त के भी प्रतिकूल है।
(४) दयधिकादिगुणानां तु-जब तुल्य या अतुल्य जातीय परमाणुओं की वैद्य त-प्रकृति में दो भागों का अन्तर होता है, तो उनमें बंध होता है । यह बंध पर्याप्त स्थायी होता है।
(५) बंधेऽधिको पारिणामिको च-बंध में अधिक विद्युतीय परमाणु अल्लविद्युतीय परमाणुओं को आत्मसात् कर नया पदार्थ बनाते हैं। वस्तुतः नये पदार्थ में न तो सफेद काले तंतुओं से बने वस्त्र के समान भिन्नता पाई जावेगी और न ही जल-सत्तू के समान एकता पाई जावेगी क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण भौतिक बंधों को निरूपित करते हैं, अणु-बंध को नहीं। भौतिक बंध के अवयव बड़ी सरल विधियों से पृथक् किये जा सकते हैं, अणु-बन्धों के अवयव अणुओं को भंजित किये बिना पृथक् नहीं हो सकते।
आधुनिक विज्ञान बंध के तीन प्रकार मानता है। विद्युत-संयोगी बंध स्निग्ध-रूक्षत्व-जन्म बंध का ही पर्याय है । द्वयधिकादिगुण-जन्य बंध उप-सहयोगी बंध का पर्यायवाची है, जिसमें विद्यु त-गुण-युग्म संयोग का कारण माना जाता है। तीसरे प्रकार के बंध को सह-संयोजक बंध कहा जाता है। इसमें समान विद्युतीय परमाणुओं में अथवा विसदृश परमाणुओं में एक विद्युत-गुण की साझेदारी संयोग का कारण मानी जाती है। यदि 'गुणसाम्ये सदृशानां बंधो भवति' माना जाये, तभी यह तीसरे प्रकार का बंध सही बैठता है। यदि यह न भी माना जावे, तो भी आज से बारह सौ वर्ष पूर्व परमाणुओं की वैद्युत प्रकृति की कल्पना और उसके आधार पर परमाणु-संयोगों का निरूपण जैन दार्शनिकों की प्रचण्ड तथ्यान्वेषण क्षमता का परिचायक है।
स्थूल रूप में यह बताया गया है कि अणुओं का निर्माण भेद (वियोजन और अपघटन), संघात (संयोजन) और भेद-संघात नामक तीन प्रक्रियाओं से होता है। इन तीनों को उपयुक्त तीन प्रकार की संयोजनताओं के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है, जो तथ्य को अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करने के समान है । वस्तुतः इस स्थूल निर्माण प्रक्रिया में वस्तुओं की मूल प्रकृति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। अनिश्चायकता और अवक्तव्यवाद
आइन्स्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धान्त ने जैन-दार्शनिकों के अनेकान्तवाद को पर्याप्त बल प्रदान किया है।
16KWS AUTAMAND
ThmMaina
AMBAKMAITAN