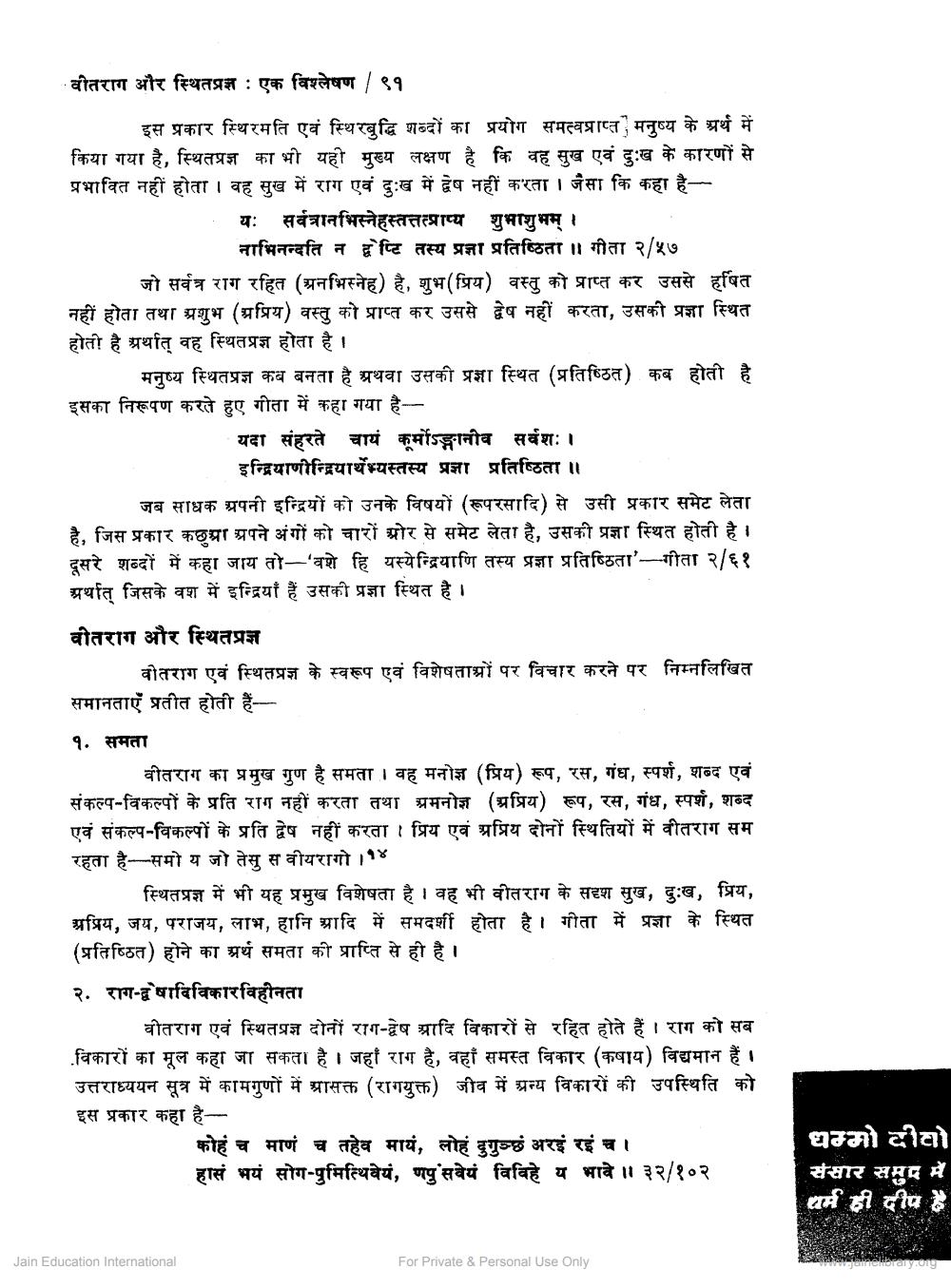________________
वीतराग और स्थितप्रज्ञ : एक विश्लेषण | ९१
इस प्रकार स्थिरमति एवं स्थिरबुद्धि शब्दों का प्रयोग समत्वप्राप्त, मनुष्य के अर्थ में किया गया है, स्थितप्रज्ञ का भी यही मुख्य लक्षण है कि वह सुख एवं दु:ख के कारणों से प्रभावित नहीं होता। वह सुख में राग एवं दुःख में द्वेष नहीं करता । जैसा कि कहा है
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वप्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ गीता २/५७ जो सर्वत्र राग रहित (अनभिस्नेह) है, शुभ(प्रिय) वस्तु को प्राप्त कर उससे हर्षित नहीं होता तथा अशुभ (अप्रिय) वस्तु को प्राप्त कर उससे द्वेष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा स्थित होती है अर्थात् वह स्थितप्रज्ञ होता है ।
मनुष्य स्थितप्रज्ञ कब बनता है अथवा उसकी प्रज्ञा स्थित (प्रतिष्ठित) कब होती है इसका निरूपण करते हुए गीता में कहा गया है
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ जब साधक अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों (रूपरसादि) से उसी प्रकार समेट लेता है, जिस प्रकार कछपा अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसकी प्रज्ञा स्थित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो-'वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'-गीता २/६१ अर्थात जिसके वश में इन्द्रियाँ हैं उसकी प्रज्ञा स्थित है।
वीतराग और स्थितप्रज्ञ
वीतराग एवं स्थितप्रज्ञ के स्वरूप एवं विशेषताओं पर विचार करने पर निम्नलिखित समानताएँ प्रतीत होती हैं१. समता
वीतराग का प्रमुख गुण है समता । वह मनोज्ञ (प्रिय) रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द एवं संकल्प-विकल्पों के प्रति राग नहीं करता तथा अमनोज्ञ (अप्रिय) रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द एवं संकल्प-विकल्पों के प्रति द्वेष नहीं करता । प्रिय एवं अप्रिय दोनों स्थितियों में वीतराग सम रहता है-समो य जो तेसु स वीयरागो।'
स्थितप्रज्ञ में भी यह प्रमुख विशेषता है । वह भी वीतराग के सदृश सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय, जय, पराजय, लाभ, हानि आदि में समदर्शी होता है। गीता में प्रज्ञा के स्थित (प्रतिष्ठित) होने का अर्थ समता की प्राप्ति से ही है।
२. राग-द्वषादिविकारविहीनता
वीतराग एवं स्थितप्रज्ञ दोनों राग-द्वेष प्रादि विकारों से रहित होते हैं। राग को सब विकारों का मूल कहा जा सकता है। जहाँ राग है, वहाँ समस्त विकार (कषाय) विद्यमान हैं । उत्तराध्ययन सूत्र में कामगुणों में आसक्त (रागयुक्त) जीव में अन्य विकारों की उपस्थिति को इस प्रकार कहा है
कोहं च माणं च तहेव माय, लोहं दुगुञ्छं अरइं रइं च । हासं भयं सोग-पुमित्थिवेयं, णपुसवेयं विविहे य भावे ।। ३२/१०२
धम्मो दीयो संसार समुद्र में धर्म ही दीप
COM
Jain Education International
For Private & Personal Use Only