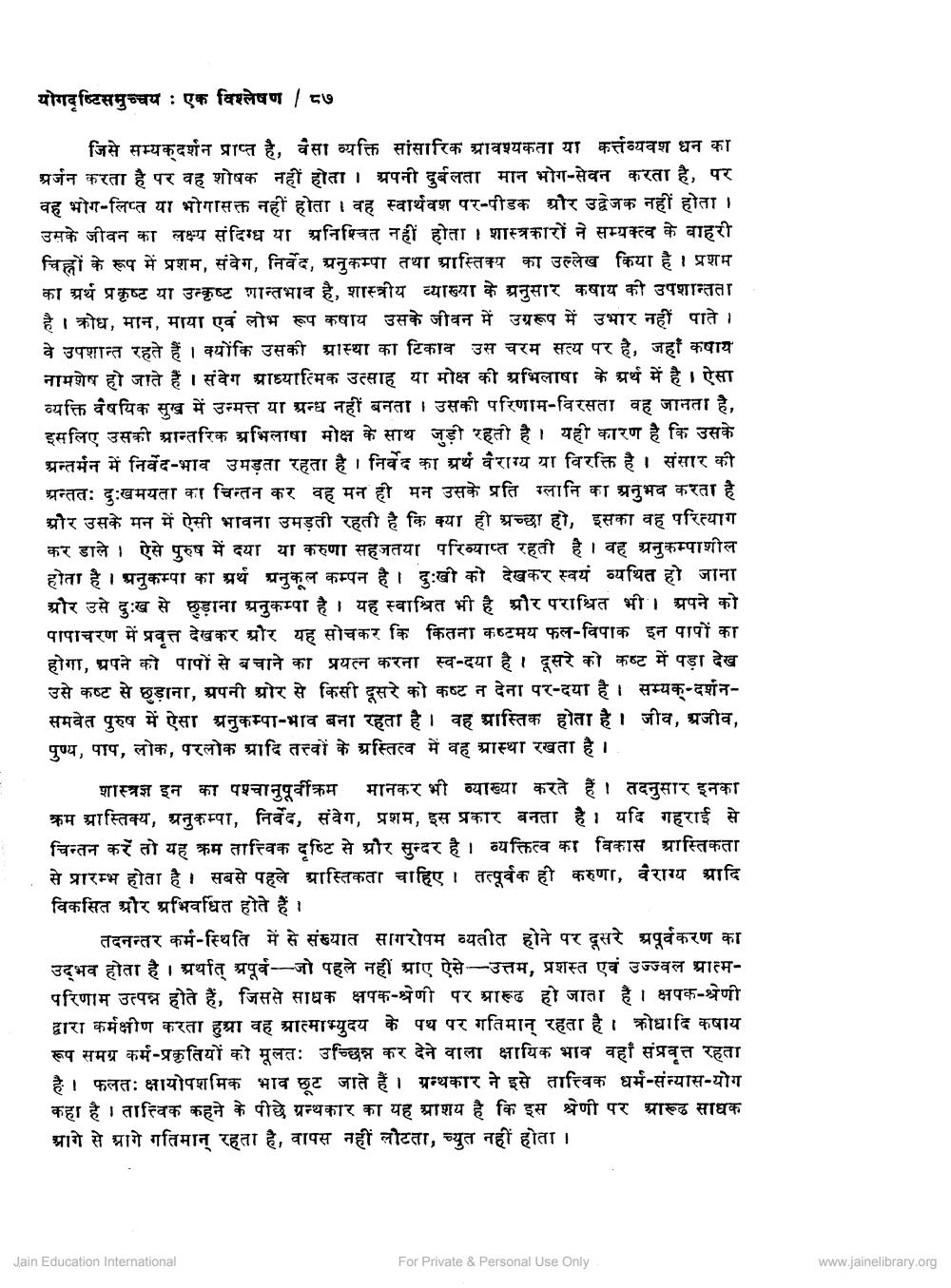________________
योगदृष्टिसमुच्चय : एक विश्लेषण | ८७
जिसे सम्यकदर्शन प्राप्त है, वैसा व्यक्ति सांसारिक आवश्यकता या कर्तव्यवश धन का अर्जन करता है पर वह शोषक नहीं होता। अपनी दुर्बलता मान भोग-सेवन करता है, पर वह भोग-लिप्त या भोगासक्त नहीं होता। वह स्वार्थवश पर-पीडक और उद्वेजक नहीं होता। उसके जीवन का लक्ष्य संदिग्ध या अनिश्चित नहीं होता । शास्त्रकारों ने सम्यक्त्व के बाहरी चिह्नों के रूप में प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा तथा प्रास्तिक्य का उल्लेख किया है। प्रशम का अर्थ प्रकृष्ट या उत्कृष्ट गान्तभाव है, शास्त्रीय व्याख्या के अनुसार कषाय की उपशान्तता है । क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप कषाय उसके जीवन में उग्ररूप में उभार नहीं पाते । वे उपशान्त रहते हैं। क्योंकि उसकी प्रास्था का टिकाव उस चरम सत्य पर है, जहां कषाय नामशेष हो जाते हैं । संवेग प्राध्यात्मिक उत्साह या मोक्ष की अभिलाषा के अर्थ में है। ऐसा व्यक्ति वैषयिक सुख में उन्मत्त या अन्ध नहीं बनता । उसकी परिणाम-विरसता वह जानता है, इसलिए उसकी प्रान्तरिक अभिलाषा मोक्ष के साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि उसके अन्तर्मन में निर्वेद-भाव उमड़ता रहता है। निर्वेद का अर्थ वैराग्य या विरक्ति है। संसार की अन्ततः दु:खमयता का चिन्तन कर वह मन ही मन उसके प्रति ग्लानि का अनुभव करता है और उसके मन में ऐसी भावना उमड़ती रहती है कि क्या ही अच्छा हो, इसका वह परित्याग कर डाले। ऐसे पुरुष में दया या करुणा सहजतया परिव्याप्त रहती है। वह अनुकम्पाशील होता है। अनुकम्पा का अर्थ अनुकूल कम्पन है। दु:खी को देखकर स्वयं व्यथित हो जाना और उसे दुःख से छुड़ाना अनुकम्पा है। यह स्वाश्रित भी है और पराश्रित भी। अपने को पापाचरण में प्रवृत्त देखकर और यह सोचकर कि कितना कष्टमय फल-विपाक इन पापों का होगा, अपने को पापों से बचाने का प्रयत्न करना स्व-दया है। दूसरे को कष्ट में पड़ा देख उसे कष्ट से छुड़ाना, अपनी ओर से किसी दूसरे को कष्ट न देना पर-दया है। सम्यक्-दर्शनसमवेत पुरुष में ऐसा अनुकम्पा-भाव बना रहता है। वह पास्तिक होता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, लोक, परलोक आदि तत्वों के अस्तित्व में वह आस्था रखता है।
शास्त्रज्ञ इन का पश्चानुपूर्वीक्रम मानकर भी व्याख्या करते हैं। तदनुसार इनका क्रम आस्तिक्य, अनुकम्पा, निर्वेद, संवेग, प्रशम, इस प्रकार बनता है। यदि गहराई से चिन्तन करें तो यह क्रम तात्त्विक दृष्टि से और सुन्दर है। व्यक्तित्व का विकास प्रास्तिकता . से प्रारम्भ होता है। सबसे पहले प्रास्तिकता चाहिए। तत्पूर्वक ही करुणा, वैराग्य आदि विकसित और अभिवधित होते हैं।
___ तदनन्तर कर्म-स्थिति में से संख्यात सागरोपम व्यतीत होने पर दूसरे अपूर्वकरण का उद्भव होता है । अर्थात् अपूर्व-जो पहले नहीं पाए ऐसे-उत्तम, प्रशस्त एवं उज्ज्वल प्रात्मपरिणाम उत्पन्न होते हैं, जिससे साधक क्षपक-श्रेणी पर आरूढ हो जाता है। क्षपक-श्रेणी द्वारा कर्मक्षीण करता हुआ वह आत्माभ्युदय के पथ पर गतिमान् रहता है। क्रोधादि कषाय रूप समग्र कर्म-प्रकृतियों को मूलतः उच्छिन्न कर देने वाला क्षायिक भाव वहाँ संप्रवृत्त रहता है। फलतः क्षायोपशमिक भाव छूट जाते हैं। ग्रन्थकार ने इसे तात्त्विक धर्म-संन्यास-योग कहा है । तात्त्विक कहने के पीछे ग्रन्थकार का यह आशय है कि इस श्रेणी पर आरूढ साधक मागे से प्रागे गतिमान् रहता है, वापस नहीं लौटता, च्यूत नहीं होता।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org