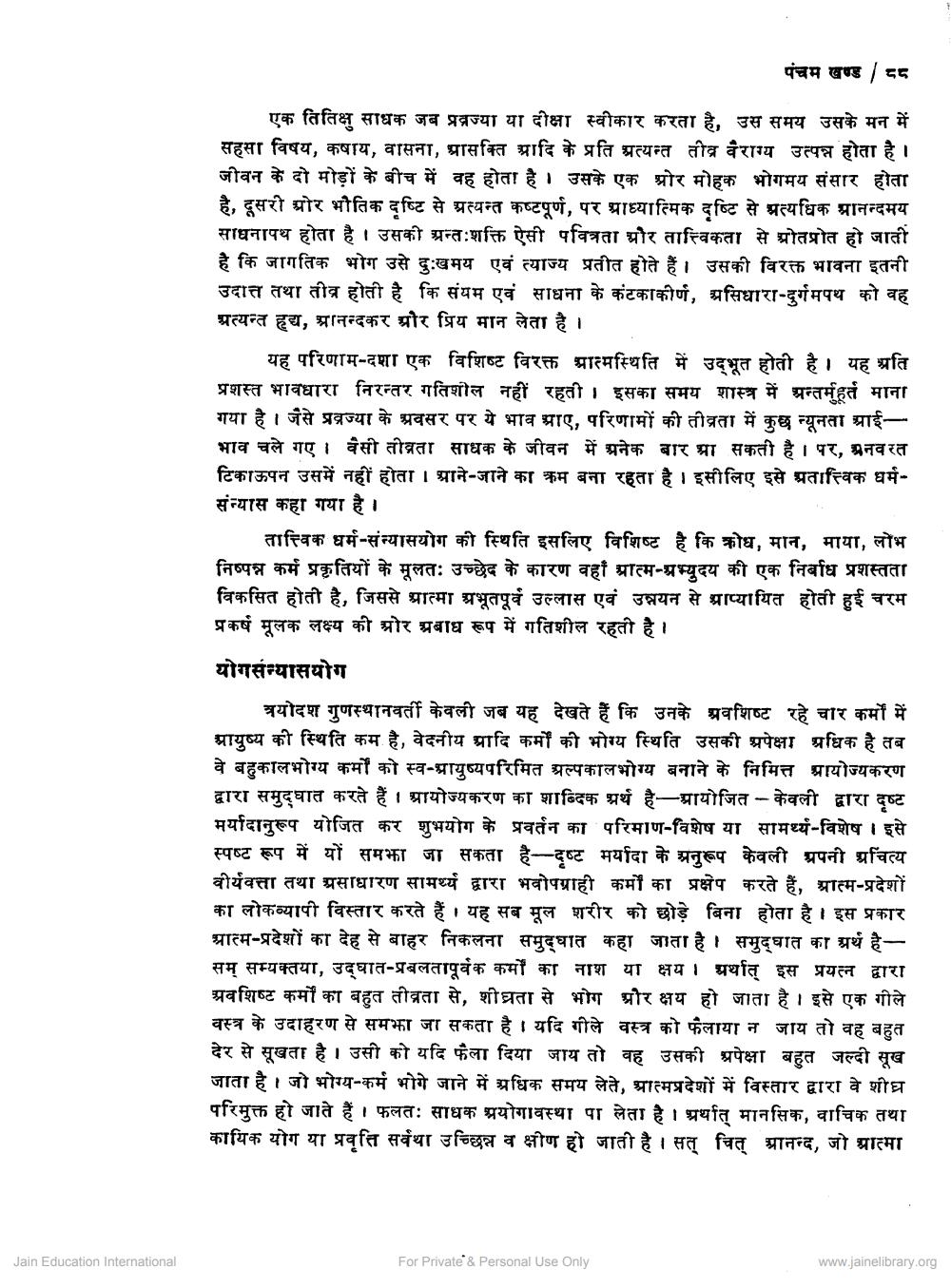________________
पंचम खण्ड / ८८
एक तितिक्षु साधक जब प्रव्रज्या या दीक्षा स्वीकार करता है, उस समय उसके मन में सहसा विषय, कषाय, वासना, प्रासक्ति आदि के प्रति अत्यन्त तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है । जीवन के दो मोड़ों के बीच में वह होता है। उसके एक ओर मोहक भोगमय संसार होता है, दूसरी ओर भौतिक दृष्टि से अत्यन्त कष्टपूर्ण, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक प्रानन्दमय साधनापथ होता है। उसकी अन्तःशक्ति ऐसी पवित्रता और तात्त्विकता से अोतप्रोत हो जाती है कि जागतिक भोग उसे दु:खमय एवं त्याज्य प्रतीत होते हैं। उसकी विरक्त भावना इतनी उदात्त तथा तीव्र होती है कि संयम एवं साधना के कंटकाकीर्ण, असिधारा-दुर्गमपथ को वह अत्यन्त हृद्य, प्रानन्दकर और प्रिय मान लेता है।
यह परिणाम-दशा एक विशिष्ट विरक्त आत्मस्थिति में उद्भूत होती है। यह अति प्रशस्त भावधारा निरन्तर गतिशील नहीं रहती। इसका समय शास्त्र में अन्तर्मुहुर्त माना गया है। जैसे प्रव्रज्या के अवसर पर ये भाव आए, परिणामों की तीव्रता में कुछ न्यूनता आईभाव चले गए। वैसी तीव्रता साधक के जीवन में अनेक बार पा सकती है। पर, अनवरत टिकाऊपन उसमें नहीं होता । आने-जाने का क्रम बना रहता है। इसीलिए इसे प्रतात्त्विक धर्मसंन्यास कहा गया है।
तात्त्विक धर्म-संन्यासयोग की स्थिति इसलिए विशिष्ट है कि क्रोध, मान, माया, लोभ निष्पन्न कर्म प्रकृतियों के मुलतः उच्छेद के कारण वहां प्रात्म-प्रभ्युदय की एक निर्बाध प्रशस्तता विकसित होती है, जिससे प्रात्मा अभूतपूर्व उल्लास एवं उन्नयन से प्राप्यायित होती हई चरम प्रकर्ष मूलक लक्ष्य की ओर अबाध रूप में गतिशील रहती है।
योगसंन्यासयोग
त्रयोदश गुणस्थानवर्ती केवली जब यह देखते हैं कि उनके प्रवशिष्ट रहे चार कर्मों में आयुष्य की स्थिति कम है, वेदनीय आदि कर्मों की भोग्य स्थिति उसकी अपेक्षा अधिक है तब वे बहुकालभोग्य कर्मों को स्व-प्रायुष्यपरिमित अल्पकालभोग्य बनाने के निमित्त प्रायोज्यकरण द्वारा समुद्घात करते हैं । प्रायोज्यकरण का शाब्दिक अर्थ है-प्रायोजित -केवली द्वारा दृष्ट मर्यादानुरूप योजित कर शुभयोग के प्रवर्तन का परिमाण-विशेष या सामर्थ्य-विशेष । इसे स्पष्ट रूप में यों समझा जा सकता है-दृष्ट मर्यादा के अनुरूप केवली अपनी प्रचित्य वीर्यवत्ता तथा असाधारण सामर्थ्य द्वारा भवोपनाही कर्मों का प्रक्षेप करते हैं, आत्म-प्रदेशों का लोकव्यापी विस्तार करते हैं। यह सब मूल शरीर को छोड़े बिना होता है। इस प्रकार आत्म-प्रदेशों का देह से बाहर निकलना समुद्घात कहा जाता है। समुद्घात का अर्थ हैसम् सम्यक्तया, उद्घात-प्रबलतापूर्वक कर्मों का नाश या क्षय । अर्थात् इस प्रयत्न द्वारा अवशिष्ट कर्मों का बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से भोग और क्षय हो जाता है । इसे एक गीले वस्त्र के उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि गीले वस्त्र को फैलाया न जाय तो वह बहुत देर से सूखता है। उसी को यदि फैला दिया जाय तो वह उसकी अपेक्षा बहुत जल्दी सूख जाता है। जो भोग्य-कर्म भोगे जाने में अधिक समय लेते, आत्मप्रदेशों में विस्तार द्वारा वे शीघ्र परिमुक्त हो जाते हैं। फलत: साधक प्रयोगावस्था पा लेता है । अर्थात् मानसिक, वाचिक तथा कायिक योग या प्रवृत्ति सर्वथा उच्छिन्न व क्षीण हो जाती है। सत् चित् आनन्द, जो प्रात्मा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org