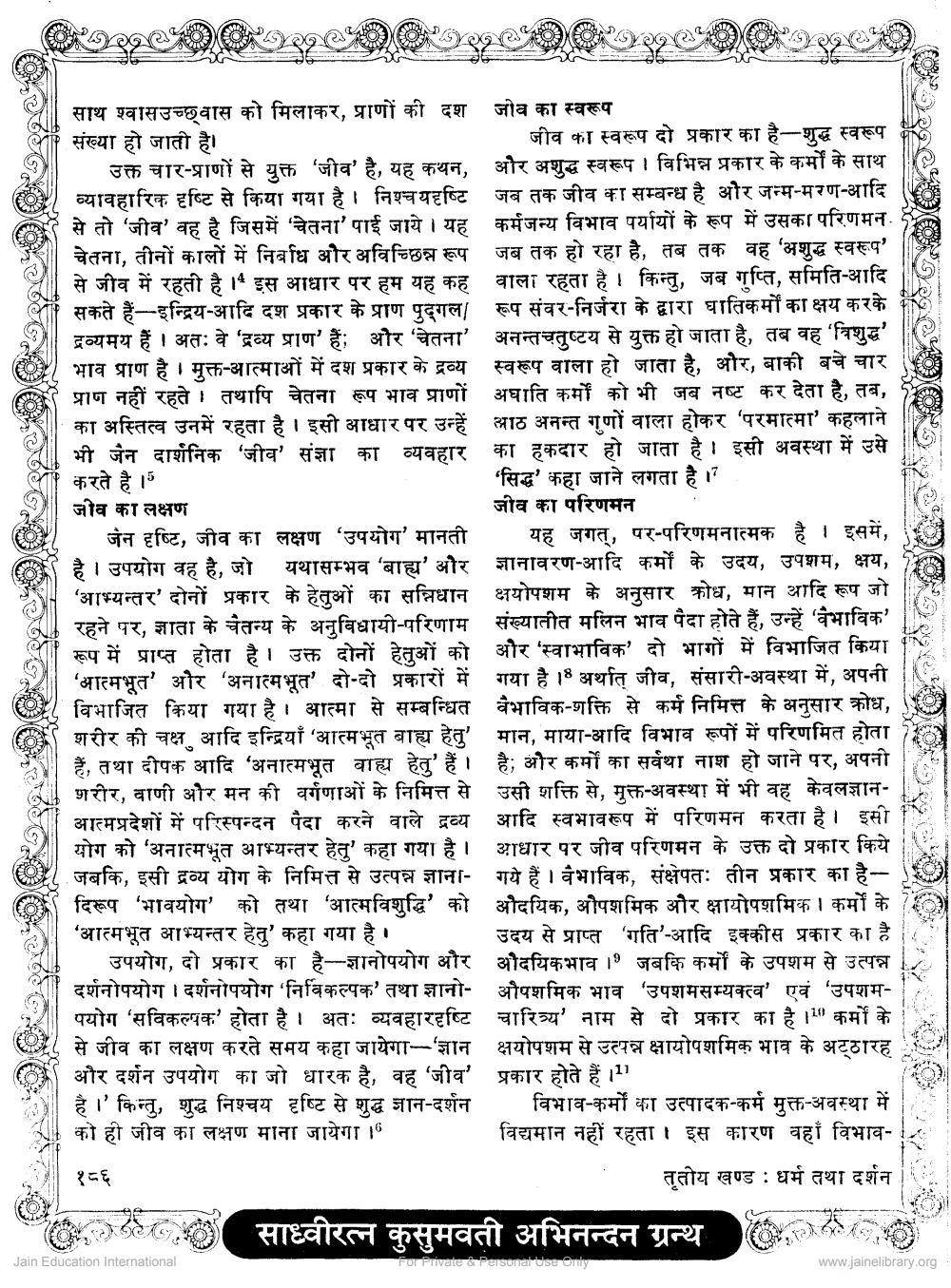________________
साथ श्वासउच्छ्वास को मिलाकर, प्राणों की दश संख्या हो जाती है।
उक्त चार-प्राणों से युक्त 'जीव' है, यह कथन, व्यावहारिक दृष्टि से किया गया है । निश्चयदृष्टि से तो 'जीव' वह है जिसमें 'चेतना' पाई जाये । यह चेतना, तीनों कालों में निर्बाध और अविच्छिन्न रूप से जीव में रहती है । इस आधार पर हम यह कह सकते हैं - इन्द्रिय-आदि दश प्रकार के प्राण पुद्गल / द्रव्यमय हैं । अतः वे 'द्रव्य प्राण' हैं; और 'चेतना' भाव प्राण है। मुक्त आत्माओं में दश प्रकार के द्रव्य प्राण नहीं रहते । तथापि चेतना रूप भाव प्राणों का अस्तित्व उनमें रहता है । इसी आधार पर उन्हें भी जैन दार्शनिक 'जीव' संज्ञा का व्यवहार करते है ।
जीव का लक्षण
जैन दृष्टि, जीव का लक्षण 'उपयोग' मानती है । उपयोग वह है, जो यथासम्भव ‘'बाह्य' और 'आभ्यन्तर' दोनों प्रकार के हेतुओं का सन्निधान रहने पर ज्ञाता के चैतन्य के अनुविधायी - परिणाम रूप में प्राप्त होता है । उक्त दोनों हेतुओं को 'आत्मभूत' और 'अनात्मभूत' दो-दो प्रकारों में विभाजित किया गया है । आत्मा से सम्बन्धित शरीर की चक्ष, आदि इन्द्रियाँ 'आत्मभूत बाह्य हेतु' हैं, तथा दीपक आदि 'अनात्मभूत वाह्य हेतु' हैं । शरीर, वाणी और मन की वर्गणाओं के निमित्त से आत्मप्रदेशों में परिस्पन्दन पैदा करने वाले द्रव्य योग को 'अनात्मभूत आभ्यन्तर हेतु' कहा गया है । . जबकि, इसी द्रव्य योग के निमित्त से उत्पन्न ज्ञानादिरूप 'भावयोग' को तथा 'आत्मविशुद्धि' को 'आत्मभूत आभ्यन्तर हेतु' कहा गया है ।
उपयोग, दो प्रकार का है-ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । दर्शनोपयोग 'निर्विकल्पक' तथा ज्ञानोपयोग 'सविकल्पक' होता है। अतः व्यवहारदृष्टि से जीव का लक्षण करते समय कहा जायेगा - 'ज्ञान और दर्शन उपयोग का जो धारक है, वह 'जीव' है ।' किन्तु, शुद्ध निश्चय दृष्टि से को ही जीव का लक्षण माना जायेगा ।"
१८६
Jain Education International
जीव का स्वरूप
जीव का स्वरूप दो प्रकार का है - शुद्ध स्वरूप और अशुद्ध स्वरूप । विभिन्न प्रकार के कर्मों के साथ जब तक जीव का सम्बन्ध है और जन्म-मरण- आदि कर्मजन्य विभाव पर्यायों के रूप में उसका परिणमनजब तक हो रहा है, तब तक वह 'अशुद्ध स्वरूप' वाला रहता है । किन्तु जब गुप्ति, समिति-आदि रूप संवर - निर्जरा के द्वारा घातिकर्मों का क्षय करके अनन्तचतुष्टय से युक्त हो जाता है, तब वह 'विशुद्ध' स्वरूप वाला हो जाता है, ओर, बाकी बचे चार अघाति कर्मों को भी जब नष्ट कर देता है, तब, आठ अनन्त गुणों वाला होकर 'परमात्मा' कहलाने का हकदार हो जाता है । इसी अवस्था में उसे 'सिद्ध' कहा जाने लगता है ।" जीव का परिणमन
यह जगत्, पर-परिणमनात्मक है । इसमें, ज्ञानावरण- आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के अनुसार क्रोध, मान आदि रूप जो संख्यातीत मलिन भाव पैदा होते हैं, उन्हें 'वैभाविक ' और 'स्वाभाविक' दो भागों में विभाजित किया गया है । अर्थात् जीव, संसारी अवस्था में, अपनी वैभाविक शक्ति से कर्म निमित्त के अनुसार क्रोध, मान, माया आदि विभाव रूपों में परिणमित होता है; और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाने पर, अपनी उसी शक्ति से, मुक्त-अवस्था में भी वह केवलज्ञानआदि स्वभावरूप में परिणमन करता है । इसी आधार पर जीव परिणमन के उक्त दो प्रकार किये गये हैं । वैभाविक, संक्षेपतः तीन प्रकार का हैओदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक । कर्मों के उदय से प्राप्त 'गति' आदि इक्कीस प्रकार का है औदयिकभाव। जबकि कर्मों के उपशम से उत्पन्न औपशमिक भाव 'उपशमसम्यक्त्व' एवं 'उपशमचारित्र्य' नाम से दो प्रकार का है । 2 कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न क्षायोपशमिक भाव के अट्ठारह प्रकार होते हैं ।" विभाव- कर्मों का उत्पादक-कर्म शुद्ध ज्ञान-दर्शन में मुक्त-अवस्था विद्यमान नहीं रहता । इस कारण वहाँ विभाव
तृतीय खण्ड : धर्म तथा दर्शन
A
साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org