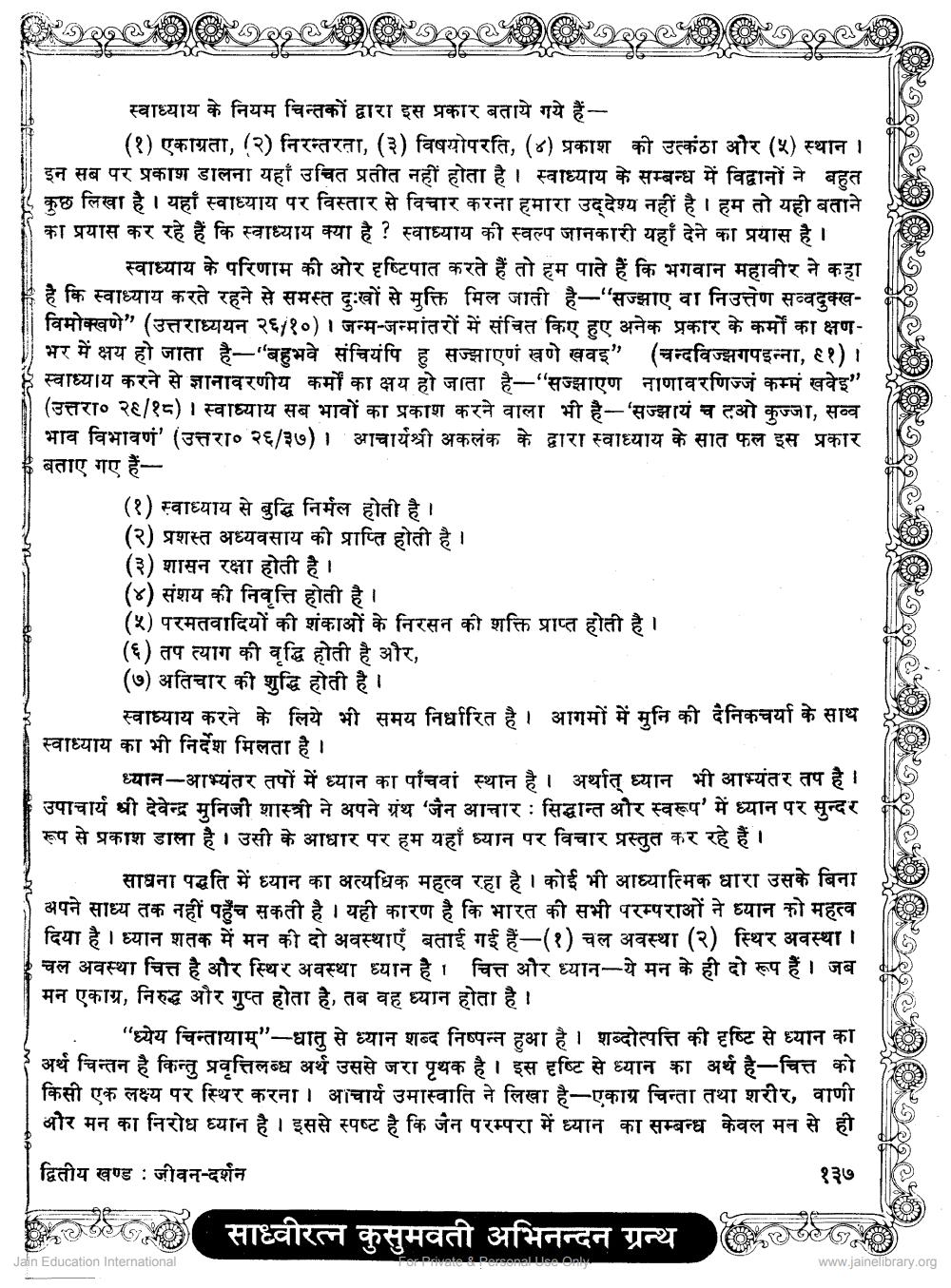________________
स्वाध्याय के नियम चिन्तकों द्वारा इस प्रकार बताये गये हैं
(१) एकाग्रता, (२) निरन्तरता, (३) विषयोपरति, (४) प्रकाश की उत्कंठा और (५) स्थान । इन सब पर प्रकाश डालना यहाँ उचित प्रतीत नहीं होता है। स्वाध्याय के सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है । यहाँ स्वाध्याय पर विस्तार से विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है । हम तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वाध्याय क्या है ? स्वाध्याय की स्वल्प जानकारी यहाँ देने का प्रयास है।
स्वाध्याय के परिणाम की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान महावीर ने कहा है कि स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति मिल जाती है-"सज्झाए वा निउत्तेण सव्वदुक्खविमोक्खणे” (उत्तराध्ययन २६/१०) । जन्म-जन्मांतरों में संचित किए हुए अनेक प्रकार के कर्मों का क्षणभर में क्षय हो जाता है-"बहुभवे संचियंपि हु सज्झाएणं खणे खवइ" (चन्दविज्झगपइन्ना, ६१)। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाता है-"सज्झाएण नाणावरणिज्जं कम्म खवेइ" (उत्तरा० २६/१८) । स्वाध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला भी है-'सज्झायं च दओ कुज्जा, सव्व भाव विभावणं' (उत्तरा० २६/३७)। आचार्यश्री अकलंक के द्वारा स्वाध्याय के सात फल इस प्रकार बताए गए हैं
(१) स्वाध्याय से बुद्धि निर्मल होती है। (२) प्रशस्त अध्यवसाय की प्राप्ति होती है। (३) शासन रक्षा होती है। (४) संशय की निवृत्ति होती है। (५) परमतवादियों की शंकाओं के निरसन की शक्ति प्राप्त होती है। (६) तप त्याग की वृद्धि होती है और, (७) अतिचार की शुद्धि होती है।
स्वाध्याय करने के लिये भी समय निर्धारित है। आगमों में मुनि की दैनिकचर्या के साथ स्वाध्याय का भी निर्देश मिलता है।
ध्यान-आभ्यंतर तपों में ध्यान का पांचवां स्थान है। अर्थात् ध्यान भी आभ्यंतर तप है । उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री ने अपने ग्रंथ 'जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप' में ध्यान पर सुन्दर रूप से प्रकाश डाला है । उसी के आधार पर हम यहाँ ध्यान पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं ।
. साधना पद्धति में ध्यान का अत्यधिक महत्व रहा है। कोई भी आध्यात्मिक धारा उसके बिना अपने साध्य तक नहीं पहुँच सकती है । यही कारण है कि भारत की सभी परम्पराओं ने ध्यान को महत्व दिया है । ध्यान शतक में मन की दो अवस्थाएं बताई गई हैं-(१) चल अवस्था (२) स्थिर अवस्था । चल अवस्था चित्त है और स्थिर अवस्था ध्यान है । चित्त और ध्यान-ये मन के ही दो रूप हैं। जब मन एकाग्र, निरुद्ध और गुप्त होता है, तब वह ध्यान होता है ।
__ "ध्येय चिन्तायाम्"-धातु से ध्यान शब्द निष्पन्न हआ है। शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान का अर्थ चिन्तन है किन्तु प्रवृत्तिलब्ध अर्थ उससे जरा पृथक है । इस दृष्टि से ध्यान का अर्थ है-चित्त को किसी एक लक्ष्य पर स्थिर करना। आचार्य उमास्वाति ने लिखा है-एकाग्र चिन्ता तथा शरीर, वाणी
और मन का निरोध ध्यान है । इससे स्पष्ट है कि जैन परम्परा में ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ही द्वितीय खण्ड : जीवन-दर्शन
१३७ ट साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International
Orivate a personaldeeonly
HOROSCOPEOPORORRORSC
www.jainelibrary.org