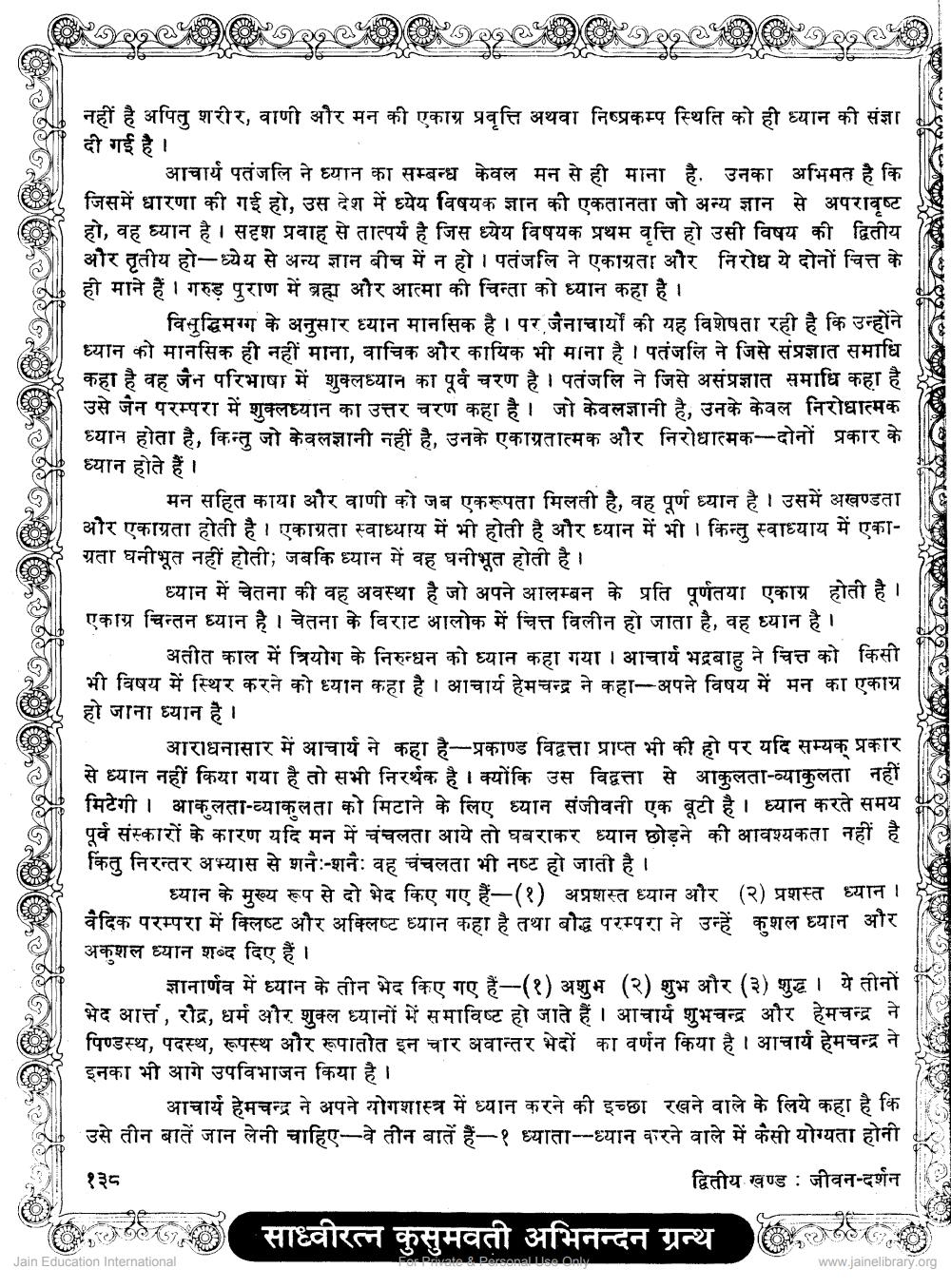________________
ANSATORICA
नहीं है अपितु शरीर, वाणी और मन की एकाग्र प्रवृत्ति अथवा निष्प्रकम्प स्थिति को ही ध्यान की संज्ञा । दी गई है।
आचार्य पतंजलि ने ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ही माना है. उनका अभिमत है कि जिसमें धारणा की गई हो, उस देश में ध्येय विषयक ज्ञान की एकतानता जो अन्य ज्ञान से अपरावृष्ट हो, वह ध्यान है । सदृश प्रवाह से तात्पर्य है जिस ध्येय विषयक प्रथम वत्ति हो उसी विषय की द्वितीय और तृतीय हो-ध्येय से अन्य ज्ञान बीच में न हो । पतंजलि ने एकाग्रता और निरोध ये दोनों चित्त के ही माने हैं । गरुड़ पुराण में ब्रह्म और आत्मा की चिन्ता को ध्यान कहा है ।
विसुद्धिमग्ग के अनुसार ध्यान मानसिक है। पर जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने ध्यान को मानसिक ही नहीं माना, वाचिक और कायिक भी माना है । पतंजलि ने जिसे संप्रज्ञात समाधि कहा है वह जैन परिभाषा में शुक्लध्यान का पूर्व चरण है। पतंजलि ने जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा है उसे जैन परम्परा में शुक्लध्यान का उत्तर चरण कहा है। जो केवलज्ञानी है, उनके केवल निरोधात्मक ध्यान होता है, किन्तु जो केवलज्ञानी नहीं है, उनके एकाग्रतात्मक और निरोधात्मक-दोनों प्रकार के ध्यान होते हैं।
मन सहित काया और वाणी को जब एकरूपता मिलती है, वह पूर्ण ध्यान है । उसमें अखण्डता और एकाग्रता होती है । एकाग्रता स्वाध्याय में भी होती है और ध्यान में भी । किन्तु स्वाध्याय में एकाग्रता घनीभूत नहीं होती; जबकि ध्यान में वह घनीभूत होती है।
ध्यान में चेतना की वह अवस्था है जो अपने आलम्बन के प्रति पूर्णतया एकान होती है। एकाग्र चिन्तन ध्यान है । चेतना के विराट आलोक में चित्त विलीन हो जाता है, वह ध्यान है।
अतीत काल में त्रियोग के निरुन्धन को ध्यान कहा गया । आचार्य भद्रबाहु ने चित्त को किसी भी विषय में स्थिर करने को ध्यान कहा है । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा-अपने विषय में मन का एकाग्र हो जाना ध्यान है।
आराधनासार में आचार्य ने कहा है-प्रकाण्ड विद्वत्ता प्राप्त भी की हो पर यदि सम्यक् प्रकार से ध्यान नहीं किया गया है तो सभी निरर्थक है । क्योंकि उस विद्वत्ता से आकुलता-व्याकुलता नहीं मिटेगी। आकुलता-व्याकुलता को मिटाने के लिए ध्यान संजीवनी एक बूटी है। ध्यान करते समय पूर्व संस्कारों के कारण यदि मन में चंचलता आये तो घबराकर ध्यान छोडने की आवश किंतु निरन्तर अभ्यास से शनैः-शनैः वह चंचलता भी नष्ट हो जाती है।
ध्यान के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं-(१) अनशस्त ध्यान और (२) प्रशस्त ध्यान । वैदिक परम्परा में क्लिष्ट और अक्लिष्ट ध्यान कहा है तथा बौद्ध परम्परा ने उन्हें कुशल ध्यान और अकुशल ध्यान शब्द दिए हैं।
ज्ञानार्णव में ध्यान के तीन भेद किए गए हैं-(१) अशुभ (२) शुभ और (३) शुद्ध । ये तीनों भेद आतं, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यानों में समाविष्ट हो जाते हैं । आचार्य शुभचन्द्र और हेमचन्द्र ने पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार अवान्तर भेदों का वर्णन किया है । आचार्य हेमचन्द्र ने इनका भी आगे उपविभाजन किया है।
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में ध्यान करने की इच्छा रखने वाले के लिये कहा है कि उसे तीन बातें जान लेनी चाहिए-वे तीन बातें हैं-१ ध्याता-ध्यान करने वाले में कैसी योग्यता होनी १३८
द्वितीय खण्ड : जीवन-दर्शन
हे
साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Parete 3 Personalilee Only
www.jainelibrary.org