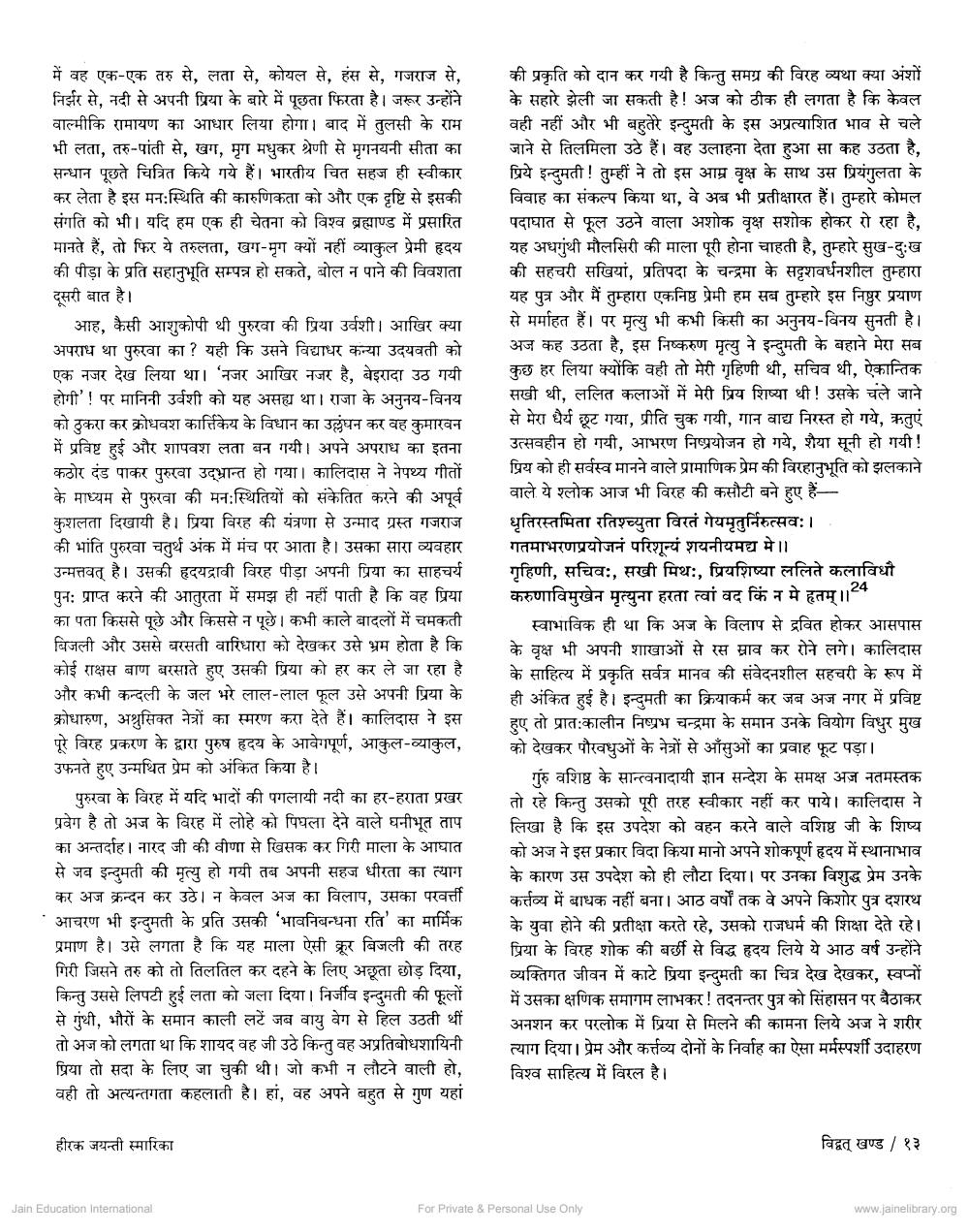________________
में वह एक-एक तरु से, लता से, कोयल से, हंस से, गजराज से, निर्झर से, नदी से अपनी प्रिया के बारे में पूछता फिरता है। जरूर उन्होंने वाल्मीकि रामायण का आधार लिया होगा। बाद में तुलसी के राम भी लता, तरु-पांती से, खग, मृग मधुकर श्रेणी से मृगनयनी सीता का सन्धान पूछते चित्रित किये गये हैं। भारतीय चित सहज ही स्वीकार कर लेता है इस मन:स्थिति की कारुणिकता को और एक दृष्टि से इसकी संगति को भी। यदि हम एक ही चेतना को विश्व ब्रह्माण्ड में प्रसारित मानते हैं, तो फिर ये तरुलता, खग-मृग क्यों नहीं व्याकुल प्रेमी हृदय की पीड़ा के प्रति सहानुभूति सम्पन्न हो सकते, बोल न पाने की विवशता दूसरी बात है। __ आह, कैसी आशुकोपी थी पुरुरवा की प्रिया उर्वशी। आखिर क्या अपराध था पुरुरवा का? यही कि उसने विद्याधर कन्या उदयवती को एक नजर देख लिया था। 'नजर आखिर नजर है, बेइरादा उठ गयी होगी'! पर मानिनी उर्वशी को यह असह्य था। राजा के अनुनय-विनय को ठुकरा कर क्रोधवश कार्तिकेय के विधान का उल्लंघन कर वह कुमारवन में प्रविष्ट हुई और शापवश लता बन गयी। अपने अपराध का इतना कठोर दंड पाकर पुरुरवा उद्धान्त हो गया। कालिदास ने नेपथ्य गीतों के माध्यम से पुरुरवा की मन:स्थितियों को संकेतित करने की अपूर्व कुशलता दिखायी है। प्रिया विरह की यंत्रणा से उन्माद ग्रस्त गजराज की भांति पुरुरवा चतुर्थ अंक में मंच पर आता है। उसका सारा व्यवहार उन्मत्तवत् है। उसकी हृदयद्रावी विरह पीड़ा अपनी प्रिया का साहचर्य पुनः प्राप्त करने की आतुरता में समझ ही नहीं पाती है कि वह प्रिया का पता किससे पूछे और किससे न पूछे। कभी काले बादलों में चमकती बिजली और उससे बरसती वारिधारा को देखकर उसे भ्रम होता है कि कोई राक्षस बाण बरसाते हुए उसकी प्रिया को हर कर ले जा रहा है और कभी कन्दली के जल भरे लाल-लाल फूल उसे अपनी प्रिया के क्रोधारुण, अश्रुसिक्त नेत्रों का स्मरण करा देते हैं। कालिदास ने इस पूरे विरह प्रकरण के द्वारा पुरुष हृदय के आवेगपूर्ण, आकुल-व्याकुल, उफनते हुए उन्मथित प्रेम को अंकित किया है।
पुरुरवा के विरह में यदि भादों की पगलायी नदी का हर-हराता प्रखर प्रवेग है तो अज के विरह में लोहे को पिघला देने वाले घनीभूत ताप का अन्तर्दाह। नारद जी की वीणा से खिसक कर गिरी माला के आघात । से जब इन्दुमती की मृत्यु हो गयी तब अपनी सहज धीरता का त्याग कर अज क्रन्दन कर उठे। न केवल अज का विलाप, उसका परवर्ती आचरण भी इन्दुमती के प्रति उसकी 'भावनिबन्धना रति' का मार्मिक प्रमाण है। उसे लगता है कि यह माला ऐसी क्रूर बिजली की तरह गिरी जिसने तरु को तो तिलतिल कर दहने के लिए अछूता छोड़ दिया, किन्तु उससे लिपटी हुई लता को जला दिया। निर्जीव इन्दुमती की फूलों से गुंथी, भौरों के समान काली लटें जब वायु वेग से हिल उठती थीं तो अज को लगता था कि शायद वह जी उठे किन्तु वह अप्रतिबोधशायिनी प्रिया तो सदा के लिए जा चुकी थी। जो कभी न लौटने वाली हो, वही तो अत्यन्तगता कहलाती है। हां, वह अपने बहुत से गुण यहां
की प्रकृति को दान कर गयी है किन्तु समग्र की विरह व्यथा क्या अंशों के सहारे झेली जा सकती है! अज को ठीक ही लगता है कि केवल वही नहीं और भी बहुतेरे इन्दुमती के इस अप्रत्याशित भाव से चले जाने से तिलमिला उठे हैं। वह उलाहना देता हुआ सा कह उठता है, प्रिये इन्दुमती ! तुम्हीं ने तो इस आम्र वृक्ष के साथ उस प्रियंगुलता के विवाह का संकल्प किया था, वे अब भी प्रतीक्षारत हैं। तुम्हारे कोमल पदाघात से फूल उठने वाला अशोक वृक्ष सशोक होकर रो रहा है, यह अधगुंथी मौलसिरी की माला पूरी होना चाहती है, तुम्हारे सुख-दुःख की सहचरी सखियां, प्रतिपदा के चन्द्रमा के सदृशवर्धनशील तुम्हारा यह पुत्र और मैं तुम्हारा एकनिष्ठ प्रेमी हम सब तुम्हारे इस निष्ठुर प्रयाण से मर्माहत हैं। पर मृत्यु भी कभी किसी का अनुनय-विनय सुनती है। अज कह उठता है, इस निष्करुण मृत्यु ने इन्दुमती के बहाने मेरा सब कुछ हर लिया क्योंकि वही तो मेरी गृहिणी थी, सचिव थी, ऐकान्तिक सखी थी, ललित कलाओं में मेरी प्रिय शिष्या थी ! उसके चले जाने से मेरा धैर्य छूट गया, प्रीति चुक गयी, गान वाद्य निरस्त हो गये, ऋतुएं उत्सवहीन हो गयी, आभरण निष्प्रयोजन हो गये, शैया सूनी हो गयी! प्रिय को ही सर्वस्व मानने वाले प्रामाणिक प्रेम की विरहानुभूति को झलकाने वाले ये श्लोक आज भी विरह की कसौटी बने हुए हैंधृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सवः। . गतमाभरणप्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे।। गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम्॥4
स्वाभाविक ही था कि अज के विलाप से द्रवित होकर आसपास के वृक्ष भी अपनी शाखाओं से रस स्राव कर रोने लगे। कालिदास के साहित्य में प्रकृति सर्वत्र मानव की संवेदनशील सहचरी के रूप में ही अंकित हुई है। इन्दुमती का क्रियाकर्म कर जब अज नगर में प्रविष्ट हुए तो प्रात:कालीन निष्प्रभ चन्द्रमा के समान उनके वियोग विधुर मुख को देखकर पौरवधुओं के नेत्रों से आँसुओं का प्रवाह फूट पड़ा।
गुरु वशिष्ठ के सान्त्वनादायी ज्ञान सन्देश के समक्ष अज़ नतमस्तक तो रहे किन्तु उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाये। कालिदास ने लिखा है कि इस उपदेश को वहन करने वाले वशिष्ठ जी के शिष्य को अज ने इस प्रकार विदा किया मानो अपने शोकपूर्ण हृदय में स्थानाभाव के कारण उस उपदेश को ही लौटा दिया। पर उनका विशुद्ध प्रेम उनके कर्तव्य में बाधक नहीं बना। आठ वर्षों तक वे अपने किशोर पुत्र दशरथ के युवा होने की प्रतीक्षा करते रहे, उसको राजधर्म की शिक्षा देते रहे। प्रिया के विरह शोक की बर्थी से विद्ध हृदय लिये ये आठ वर्ष उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में काटे प्रिया इन्दुमती का चित्र देख देखकर, स्वप्नों में उसका क्षणिक समागम लाभकर! तदनन्तर पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर अनशन कर परलोक में प्रिया से मिलने की कामना लिये अज ने शरीर त्याग दिया। प्रेम और कर्त्तव्य दोनों के निर्वाह का ऐसा मर्मस्पर्शी उदाहरण विश्व साहित्य में विरल है।
हीरक जयन्ती स्मारिका
विद्वत् खण्ड / १३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org