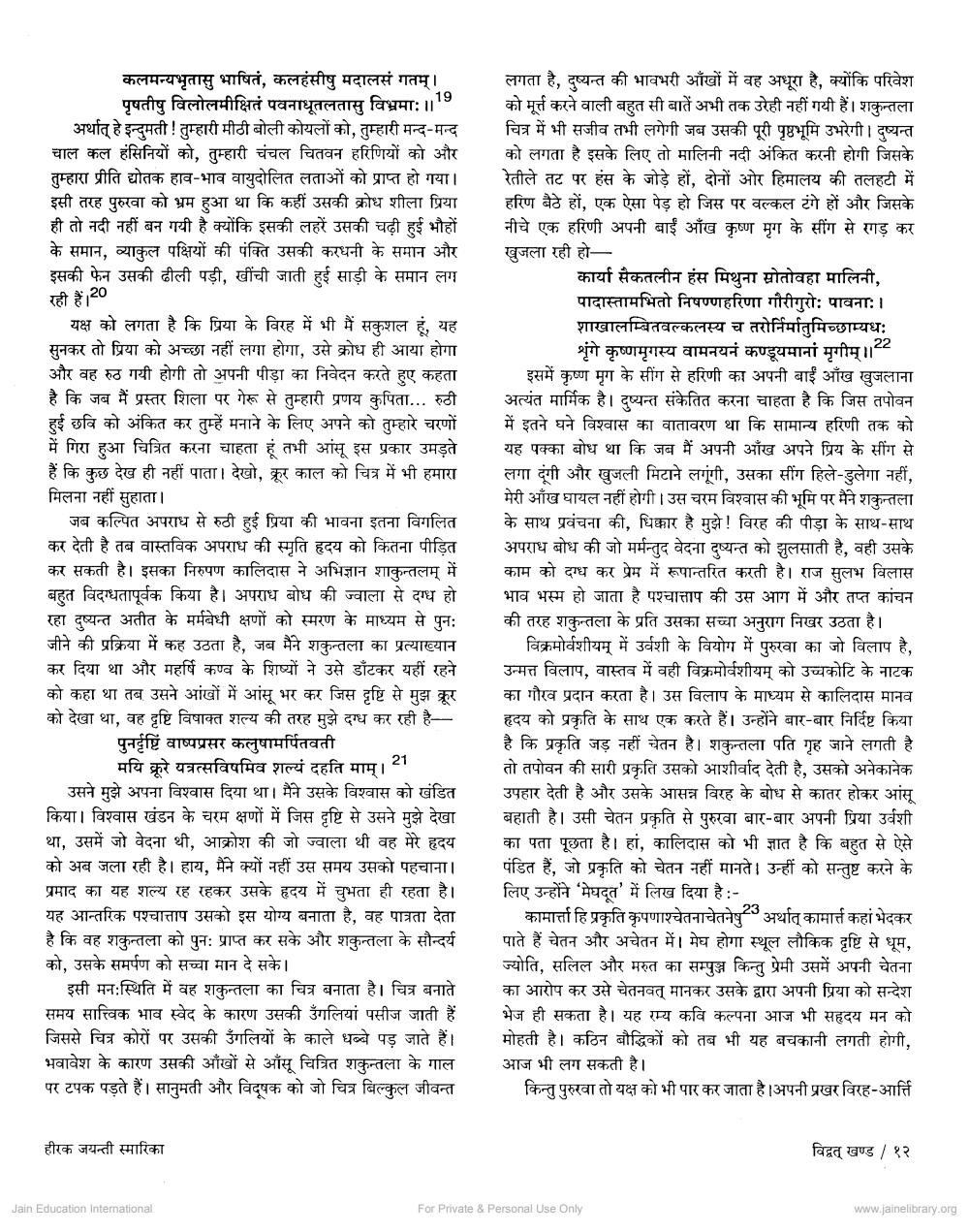________________
कलमन्यभृतासु भाषितं, कलहंसीषु मदालसं गतम्।
पृषतीषु विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विभ्रमाः॥ अर्थात् हे इन्दुमती ! तुम्हारी मीठी बोली कोयलों को, तुम्हारी मन्द-मन्द चाल कल हंसिनियों को, तुम्हारी चंचल चितवन हरिणियों को और तुम्हारा प्रीति द्योतक हाव-भाव वायुदोलित लताओं को प्राप्त हो गया। इसी तरह पुरुरवा को भ्रम हुआ था कि कहीं उसकी क्रोध शीला प्रिया ही तो नदी नहीं बन गयी है क्योंकि इसकी लहरें उसकी चढ़ी हुई भौहों के समान, व्याकुल पक्षियों की पंक्ति उसकी करधनी के समान और इसकी फेन उसकी ढीली पड़ी, खींची जाती हुई साड़ी के समान लग
रही हैं।20
यक्ष को लगता है कि प्रिया के विरह में भी मैं सकुशल हूं, यह सुनकर तो प्रिया को अच्छा नहीं लगा होगा, उसे क्रोध ही आया होगा
और वह रुठ गयी होगी तो अपनी पीड़ा का निवेदन करते हुए कहता है कि जब मैं प्रस्तर शिला पर गेरू से तुम्हारी प्रणय कुपिता... रुठी हुई छवि को अंकित कर तुम्हें मनाने के लिए अपने को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ चित्रित करना चाहता हूं तभी आंसू इस प्रकार उमड़ते हैं कि कुछ देख ही नहीं पाता। देखो, क्रूर काल को चित्र में भी हमारा मिलना नहीं सुहाता।
जब कल्पित अपराध से रुठी हुई प्रिया की भावना इतना विगलित कर देती है तब वास्तविक अपराध की स्मृति हृदय को कितना पीड़ित कर सकती है। इसका निरुपण कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में बहुत विदग्धतापूर्वक किया है। अपराध बोध की ज्वाला से दग्ध हो रहा दुष्यन्त अतीत के मर्मबेधी क्षणों को स्मरण के माध्यम से पुनः जीने की प्रक्रिया में कह उठता है, जब मैंने शकुन्तला का प्रत्याख्यान कर दिया था और महर्षि कण्व के शिष्यों ने उसे डाँटकर यहीं रहने को कहा था तब उसने आंखों में आंसू भर कर जिस दृष्टि से मुझ क्रूर को देखा था, वह दृष्टि विषाक्त शल्य की तरह मुझे दग्ध कर रही है
पुनर्दृष्टिं वाष्पप्रसर कलुषामर्पितवती ___मयि क्रूरे यत्रत्सविषमिव शल्यं दहति माम्। 21 उसने मुझे अपना विश्वास दिया था। मैंने उसके विश्वास को खंडित किया। विश्वास खंडन के चरम क्षणों में जिस दृष्टि से उसने मुझे देखा था, उसमें जो वेदना थी, आक्रोश की जो ज्वाला थी वह मेरे हृदय को अब जला रही है। हाय, मैने क्यों नहीं उस समय उसको पहचाना। प्रमाद का यह शल्य रह रहकर उसके हृदय में चुभता ही रहता है। यह आन्तरिक पश्चात्ताप उसको इस योग्य बनाता है, वह पात्रता देता है कि वह शकुन्तला को पुन: प्राप्त कर सके और शकुन्तला के सौन्दर्य को, उसके समर्पण को सच्चा मान दे सके।
इसी मन:स्थिति में वह शकुन्तला का चित्र बनाता है। चित्र बनाते समय सात्त्विक भाव स्वेद के कारण उसकी उँगलियां पसीज जाती हैं जिससे चित्र कोरों पर उसकी उँगलियों के काले धब्बे पड़ जाते हैं। भवावेश के कारण उसकी आँखों से आँसू चित्रित शकुन्तला के गाल पर टपक पड़ते हैं। सानुमती और विदूषक को जो चित्र बिल्कुल जीवन्त
लगता है, दुष्यन्त की भावभरी आँखों में वह अधूरा है, क्योंकि परिवेश को मूर्त करने वाली बहुत सी बातें अभी तक उरेही नहीं गयी हैं। शकुन्तला चित्र में भी सजीव तभी लगेगी जब उसकी पूरी पृष्ठभूमि उभरेगी। दुष्यन्त को लगता है इसके लिए तो मालिनी नदी अंकित करनी होगी जिसके रेतीले तट पर हंस के जोड़े हों, दोनों ओर हिमालय की तलहटी में हरिण बैठे हों, एक ऐसा पेड़ हो जिस पर वल्कल टंगे हों और जिसके नीचे एक हरिणी अपनी बाईं आँख कृष्ण मृग के सींग से रगड़ कर खुजला रही हो
कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतोवहा मालिनी, पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः। शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः
शृंगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्॥2 इसमें कृष्ण मृग के सींग से हरिणी का अपनी बाईं आँख खुजलाना अत्यंत मार्मिक है। दुष्यन्त संकेतित करना चाहता है कि जिस तपोवन में इतने घने विश्वास का वातावरण था कि सामान्य हरिणी तक को यह पक्का बोध था कि जब मैं अपनी आँख अपने प्रिय के सींग से लगा दूंगी और खुजली मिटाने लगूंगी, उसका सींग हिले-डुलेगा नहीं, मेरी आँख घायल नहीं होगी। उस चरम विश्वास की भूमि पर मैंने शकुन्तला के साथ प्रवंचना की, धिक्कार है मुझे! विरह की पीड़ा के साथ-साथ अपराध बोध की जो मर्मन्तुद वेदना दुष्यन्त को झुलसाती है, वही उसके काम को दग्ध कर प्रेम में रूपान्तरित करती है। राज सुलभ विलास भाव भस्म हो जाता है पश्चात्ताप की उस आग में और तप्त कांचन की तरह शकुन्तला के प्रति उसका सच्चा अनुराग निखर उठता है।
विक्रमोर्वशीयम् में उर्वशी के वियोग में पुरुरवा का जो विलाप है, उन्मत्त विलाप, वास्तव में वही विक्रमोर्वशीयम् को उच्चकोटि के नाटक का गौरव प्रदान करता है। उस विलाप के माध्यम से कालिदास मानव हृदय को प्रकृति के साथ एक करते हैं। उन्होंने बार-बार निर्दिष्ट किया है कि प्रकृति जड़ नहीं चेतन है। शकुन्तला पति गृह जाने लगती है तो तपोवन की सारी प्रकृति उसको आशीर्वाद देती है, उसको अनेकानेक उपहार देती है और उसके आसन्न विरह के बोध से कातर होकर आंसू बहाती है। उसी चेतन प्रकृति से पुरुरवा बार-बार अपनी प्रिया उर्वशी का पता पूछता है। हां, कालिदास को भी ज्ञात है कि बहुत से ऐसे पंडित हैं, जो प्रकृति को चेतन नहीं मानते। उन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिए उन्होंने 'मेघदूत' में लिख दिया है :
कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु अर्थात् कामात कहां भेदकर पाते हैं चेतन और अचेतन में। मेघ होगा स्थूल लौकिक दृष्टि से धूम, ज्योति, सलिल और मरुत का सम्पुञ्ज किन्तु प्रेमी उसमें अपनी चेतना का आरोप कर उसे चेतनवत् मानकर उसके द्वारा अपनी प्रिया को सन्देश भेज ही सकता है। यह रम्य कवि कल्पना आज भी सहृदय मन को मोहती है। कठिन बौद्धिकों को तब भी यह बचकानी लगती होगी, आज भी लग सकती है। किन्तु पुरुरवा तो यक्ष को भी पार कर जाता है।अपनी प्रखर विरह-आर्ति
हीरक जयन्ती स्मारिका
विद्वत् खण्ड / १२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org