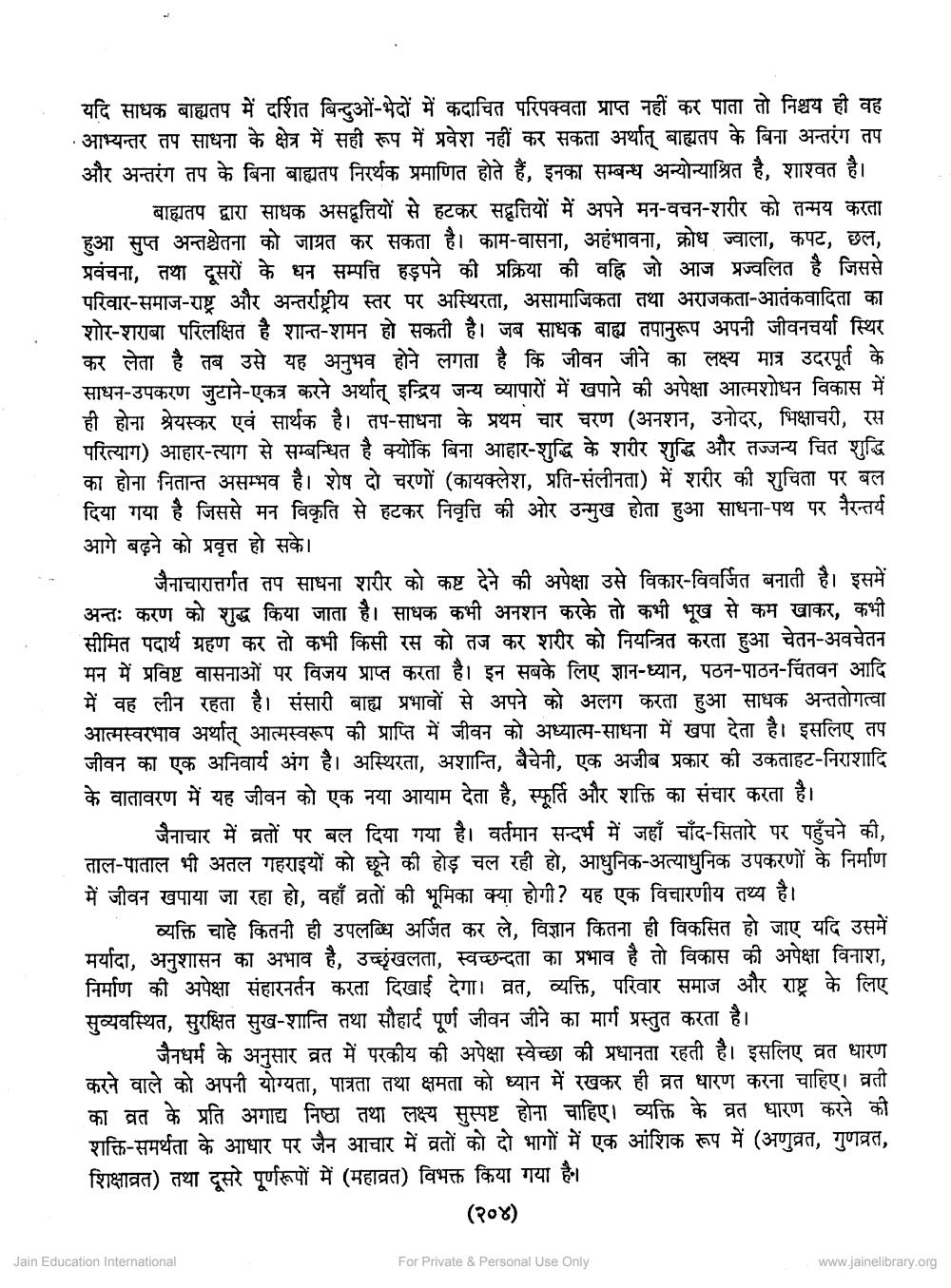________________
यदि साधक बाह्यतप में दर्शित बिन्दुओं-भेदों में कदाचित परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाता तो निश्चय ही वह • आभ्यन्तर तप साधना के क्षेत्र में सही रूप में प्रवेश नहीं कर सकता अर्थात् बाह्यतप के बिना अन्तरंग तप और अन्तरंग तप के बिना बाह्यतप निरर्थक प्रमाणित होते हैं, इनका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है, शाश्वत है।
___बाह्यतप द्वारा साधक असदृत्तियों से हटकर सद्वृत्तियों में अपने मन-वचन-शरीर को तन्मय करता हुआ सुप्त अन्तश्चेतना को जाग्रत कर सकता है। काम-वासना, अहंभावना, क्रोध ज्वाला, कपट, छल, प्रवंचना, तथा दूसरों के धन सम्पत्ति हड़पने की प्रक्रिया की वह्नि जो आज प्रज्वलित है जिससे परिवार-समाज-राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता, असामाजिकता तथा अराजकता-आतंकवादिता का शोर-शराबा परिलक्षित है शान्त-शमन हो सकती है। जब साधक बाह्य तपानुरूप अपनी जीवनचर्या स्थिर कर लेता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन जीने का लक्ष्य मात्र उदरपूर्त के साधन-उपकरण जुटाने-एकत्र करने अर्थात् इन्द्रिय जन्य व्यापारों में खपाने की अपेक्षा आत्मशोधन विकास में ही होना श्रेयस्कर एवं सार्थक है। तप-साधना के प्रथम चार चरण (अनशन, उनोदर, भिक्षाचरी, रस परित्याग) आहार-त्याग से सम्बन्धित है क्योंकि बिना आहार-शुद्धि के शरीर शुद्धि और तज्जन्य चित शुद्धि का होना नितान्त असम्भव है। शेष दो चरणों (कायक्लेश, प्रति-संलीनता) में शरीर की शुचिता पर बल दिया गया है जिससे मन विकृति से हटकर निवृत्ति की ओर उन्मुख होता हुआ साधना-पथ पर नैरन्तर्य आगे बढ़ने को प्रवृत्त हो सके।
जैनाचारात्तर्गत तप साधना शरीर को कष्ट देने की अपेक्षा उसे विकार-विवर्जित बनाती है। इसमें अन्तः करण को शुद्ध किया जाता है। साधक कभी अनशन करके तो कभी भूख से कम खाकर, कभी सीमित पदार्थ ग्रहण कर तो कभी किसी रस को तज कर शरीर को नियन्त्रित करता हुआ चेतन-अवचेतन मन में प्रविष्ट वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है। इन सबके लिए ज्ञान-ध्यान, पठन-पाठन-चिंतवन आदि में वह लीन रहता है। संसारी बाह्य प्रभावों से अपने को अलग करता हुआ साधक अन्ततोगत्वा आत्मस्वरभाव अर्थात् आत्मस्वरूप की प्राप्ति में जीवन को अध्यात्म-साधना में खपा देता है। इसलिए तप जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अस्थिरता, अशान्ति, बैचेनी, एक अजीब प्रकार की उकताहट-निराशादि के वातावरण में यह जीवन को एक नया आयाम देता है, स्फूर्ति और शक्ति का संचार करता है।
जैनाचार में व्रतों पर बल दिया गया है। वर्तमान सन्दर्भ में जहाँ चाँद-सितारे पर पहुँचने की, ताल-पाताल भी अतल गहराइयों को छूने की होड़ चल रही हो, आधुनिक-अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण में जीवन खपाया जा रहा हो, वहाँ व्रतों की भूमिका क्या होगी? यह एक विचारणीय तथ्य है।
व्यक्ति चाहे कितनी ही उपलब्धि अर्जित कर ले, विज्ञान कितना ही विकसित हो जाए यदि उसमें मर्यादा, अनुशासन का अभाव है, उच्छंखलता, स्वच्छन्दता का प्रभाव है तो विकास की अपेक्षा विनाश, निर्माण की अपेक्षा संहारनर्तन करता दिखाई देगा। व्रत, व्यक्ति, परिवार समाज और राष्ट्र के लिए सुव्यवस्थित, सुरक्षित सुख-शान्ति तथा सौहार्द पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत करता है।
जैनधर्म के अनुसार व्रत में परकीय की अपेक्षा स्वेच्छा की प्रधानता रहती है। इसलिए व्रत धारण करने वाले को अपनी योग्यता, पात्रता तथा क्षमता को ध्यान में रखकर ही व्रत धारण करना चाहिए। व्रती का व्रत के प्रति अगाद्य निष्ठा तथा लक्ष्य सुस्पष्ट होना चाहिए। व्यक्ति के व्रत धारण करने की शक्ति-समर्थता के आधार पर जैन आचार में व्रतों को दो भागों में एक आंशिक रूप में (अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत) तथा दूसरे पूर्णरूपों में (महाव्रत) विभक्त किया गया है।
(२०४)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org