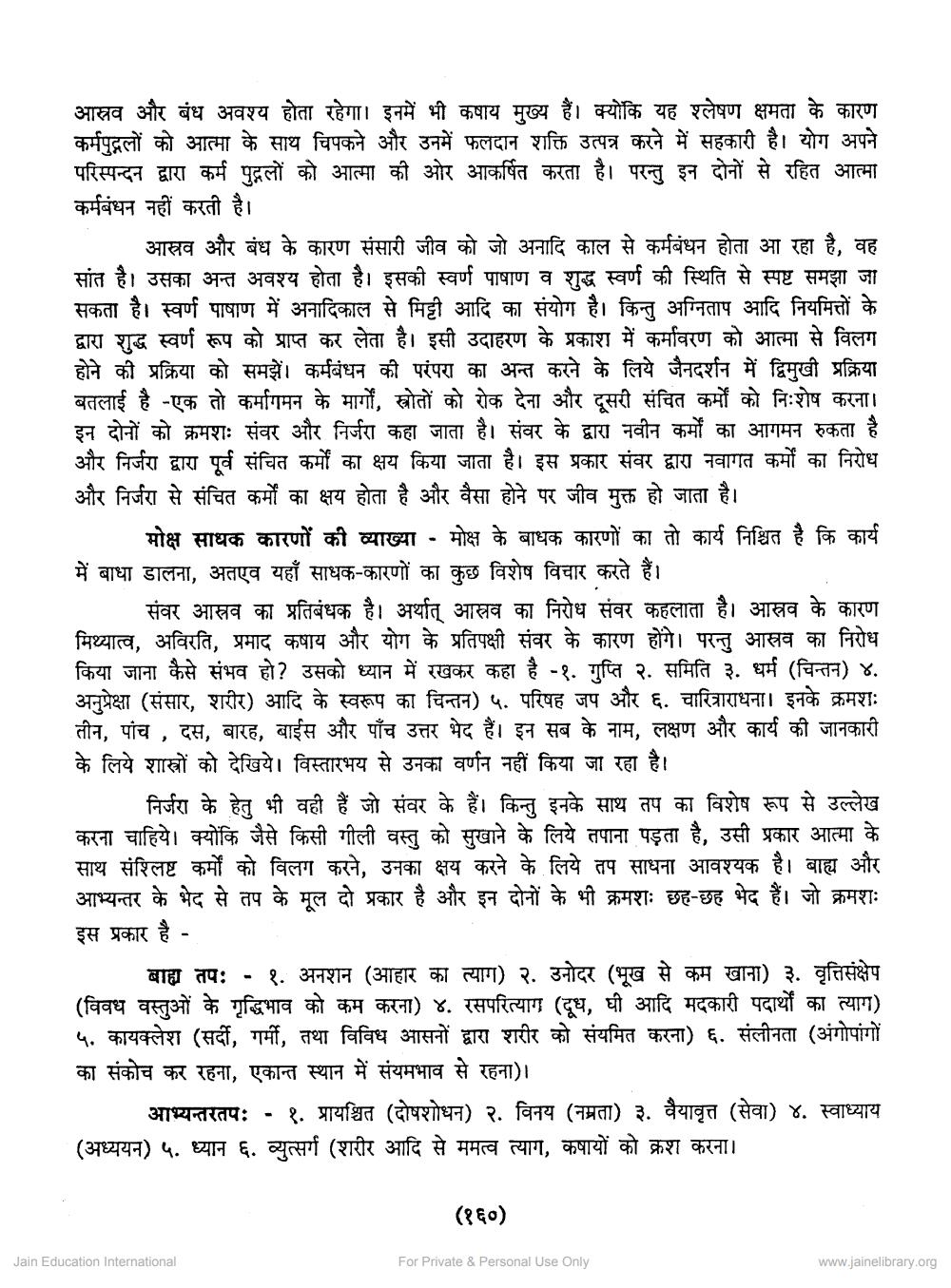________________
आस्रव और बंध अवश्य होता रहेगा। इनमें भी कषाय मुख्य हैं। क्योंकि यह श्लेषण क्षमता के कारण कर्मपुद्गलों को आत्मा के साथ चिपकने और उनमें फलदान शक्ति उत्पन्न करने में सहकारी है। योग अपने परिस्पन्दन द्वारा कर्म पुद्गलों को आत्मा की ओर आकर्षित करता है। परन्तु इन दोनों से रहित आत्मा कर्मबंधन नहीं करती है।
__ आस्रव और बंध के कारण संसारी जीव को जो अनादि काल से कर्मबंधन होता आ रहा है, वह सांत है। उसका अन्त अवश्य होता है। इसकी स्वर्ण पाषाण व शुद्ध स्वर्ण की स्थिति से स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वर्ण पाषाण में अनादिकाल से मिट्टी आदि का संयोग है। किन्तु अग्निताप आदि नियमित्तों के द्वारा शुद्ध स्वर्ण रूप को प्राप्त कर लेता है। इसी उदाहरण के प्रकाश में कर्मावरण को आत्मा से विलग होने की प्रक्रिया को समझें। कर्मबंधन की परंपरा का अन्त करने के लिये जैनदर्शन में द्विमुखी प्रक्रिया बतलाई है -एक तो कर्मागमन के मार्गों, स्रोतों को रोक देना और दूसरी संचित कर्मों को निःशेष करना। इन दोनों को क्रमशः संवर और निर्जरा कहा जाता है। संवर के द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रुकता है और निर्जरा द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय किया जाता है। इस प्रकार संवर द्वारा नवागत कर्मों का निरोध और निर्जरा से संचित कर्मों का क्षय होता है और वैसा होने पर जीव मुक्त हो जाता है।
मोक्ष साधक कारणों की व्याख्या • मोक्ष के बाधक कारणों का तो कार्य निश्चित है कि कार्य में बाधा डालना, अतएव यहाँ साधक-कारणों का कुछ विशेष विचार करते हैं।
संवर आस्रव का प्रतिबंधक है। अर्थात् आस्रव का निरोध संवर कहलाता है। आस्रव के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय और योग के प्रतिपक्षी संवर के कारण होंगे। परन्तु आस्रव का निरोध किया जाना कैसे संभव हो? उसको ध्यान में रखकर कहा है -१. गुप्ति २. समिति ३. धर्म (चिन्तन) ४. अनुप्रेक्षा (संसार, शरीर) आदि के स्वरूप का चिन्तन) ५. परिषह जप और ६. चारित्राराधना। इनके क्रमशः तीन, पांच , दस, बारह, बाईस और पाँच उत्तर भेद हैं। इन सब के नाम, लक्षण और कार्य की जानकारी के लिये शास्त्रों को देखिये। विस्तारभय से उनका वर्णन नहीं किया जा रहा है।
निर्जरा के हेतु भी वही हैं जो संवर के हैं। किन्तु इनके साथ तप का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिये। क्योंकि जैसे किसी गीली वस्तु को सुखाने के लिये तपाना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ संश्लिष्ट कर्मों को विलग करने, उनका क्षय करने के लिये तप साधना आवश्यक है। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप के मूल दो प्रकार है और इन दोनों के भी क्रमशः छह-छह भेद हैं। जो क्रमशः इस प्रकार है -
बाह्य तपः - १. अनशन (आहार का त्याग) २. उनोदर (भूख से कम खाना) ३. वृत्तिसंक्षेप (विवध वस्तुओं के गृद्धिभाव को कम करना) ४. रसपरित्याग (दूध, घी आदि मदकारी पदार्थों का त्याग) ५. कायक्लेश (सर्दी, गर्मी, तथा विविध आसनों द्वारा शरीर को संयमित करना) ६. संलीनता (अंगोपांगों का संकोच कर रहना, एकान्त स्थान में संयमभाव से रहना)।
आभ्यन्तरतपः - १. प्रायश्चित (दोषशोधन) २. विनय (नम्रता) ३. वैयावृत्त (सेवा) ४. स्वाध्याय (अध्ययन) ५. ध्यान ६. व्युत्सर्ग (शरीर आदि से ममत्व त्याग, कषायों को क्रश करना।
(१६०)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org