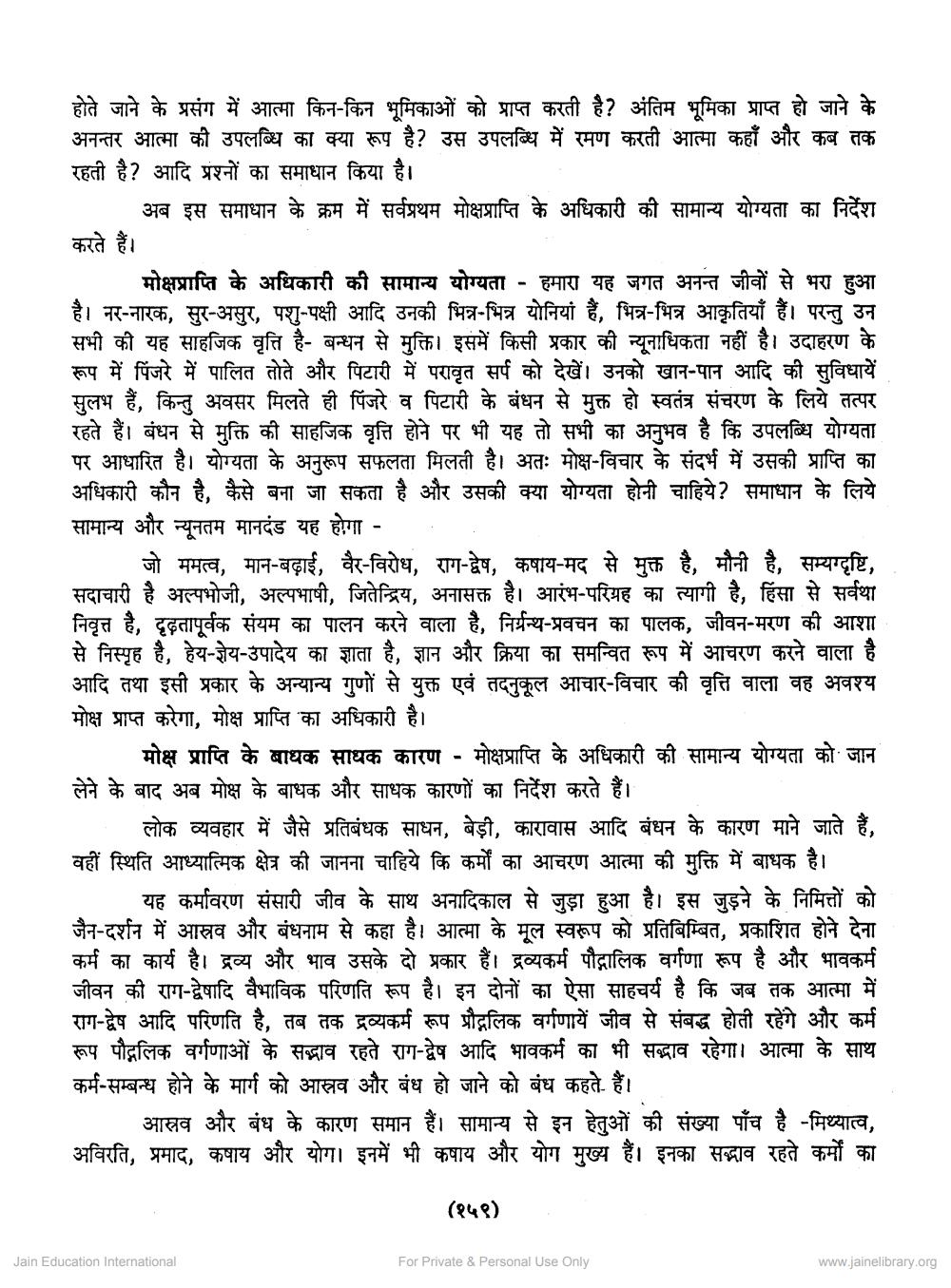________________
होते जाने के प्रसंग में आत्मा किन-किन भूमिकाओं को प्राप्त करती है? अंतिम भूमिका प्राप्त हो जाने के अनन्तर आत्मा की उपलब्धि का क्या रूप है? उस उपलब्धि में रमण करती आत्मा कहाँ और कब तक रहती है? आदि प्रश्नों का समाधान किया है।
__ अब इस समाधान के क्रम में सर्वप्रथम मोक्षप्राप्ति के अधिकारी की सामान्य योग्यता का निर्देश करते हैं।
मोक्षप्राप्ति के अधिकारी की सामान्य योग्यता - हमारा यह जगत अनन्त जीवों से भरा हआ है। नर-नारक, सुर-असुर, पशु-पक्षी आदि उनकी भिन्न-भिन्न योनियां हैं, भिन्न-भिन्न आकृतियाँ हैं। परन्तु उन सभी की यह साहजिक वत्ति है- बन्धन से मक्ति। इसमें किसी प्रकार की न्यनाधिकता नहीं है। उदाहरण के रूप में पिंजरे में पालित तोते और पिटारी में परावृत सर्प को देखें। उनको खान-पान आदि की सुविधायें सुलभ हैं, किन्तु अवसर मिलते ही पिंजरे व पिटारी के बंधन से मुक्त हो स्वतंत्र संचरण के लिये तत्पर रहते हैं। बंधन से मुक्ति की साहजिक वृत्ति होने पर भी यह तो सभी का अनुभव है कि उपलब्धि योग्यता पर आधारित है। योग्यता के अनुरूप सफलता मिलती है। अतः मोक्ष-विचार के संदर्भ में उसकी प्राप्ति का अधिकारी कौन है, कैसे बना जा सकता है और उसकी क्या योग्यता होनी चाहिये? समाधान के लिये सामान्य और न्यूनतम मानदंड यह होगा -
जो ममत्व, मान-बढ़ाई, वैर-विरोध, राग-द्वेष, कषाय-मद से मुक्त है, मौनी है, सम्यग्दृष्टि, सदाचारी है अल्पभोजी, अल्पभाषी, जितेन्द्रिय, अनासक्त है। आरंभ-परिग्रह का त्यागी है, हिंसा से सर्वथा निवृत्त है, दृढ़तापूर्वक संयम का पालन करने वाला है, निम्रन्थ-प्रवचन का पालक, जीवन-मरण की आशा से निस्पृह है, हेय-ज्ञेय-उपादेय का ज्ञाता है, ज्ञान और क्रिया का समन्वित रूप में आचरण करने वाला है आदि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य गुणों से युक्त एवं तदनुकूल आचार-विचार की वृत्ति वाला वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है।
___मोक्ष प्राप्ति के बाधक साधक कारण - मोक्षप्राप्ति के अधिकारी की सामान्य योग्यता को जान लेने के बाद अब मोक्ष के बाधक और साधक कारणों का निर्देश करते हैं।
लोक व्यवहार में जैसे प्रतिबंधक साधन, बेड़ी, कारावास आदि बंधन के कारण माने जाते हैं, वहीं स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र की जानना चाहिये कि कर्मों का आचरण आत्मा की मुक्ति में बाधक है।
यह कर्मावरण संसारी जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। इस जुड़ने के निमित्तों को जैन-दर्शन में आस्रव और बंधनाम से कहा है। आत्मा के मूल स्वरूप को प्रतिबिम्बित, प्रकाशित होने देना कर्म का कार्य है। द्रव्य और भाव उसके दो प्रकार हैं। द्रव्यकर्म पौगालिक वर्गणा रूप है और भावकर्म जीवन की राग-द्वेषादि वैभाविक परिणति रूप है। इन दोनों का ऐसा साहचर्य है कि जब तक आत्मा में राग-द्वेष आदि परिणति है, तब तक द्रव्यकर्म रूप प्रौद्गलिक वर्गणायें जीव से संबद्ध होती रहेंगे और कर्म रूप पौगलिक वर्गणाओं के सद्भाव रहते राग-द्वेष आदि भावकर्म का भी सद्भाव रहेगा। आत्मा के साथ कर्म-सम्बन्ध होने के मार्ग को आस्रव और बंध हो जाने को बंध कहते हैं।
आस्रव और बंध के कारण समान हैं। सामान्य से इन हेतुओं की संख्या पाँच है -मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें भी कषाय और योग मुख्य हैं। इनका सद्भाव रहते कर्मों का
(१५९)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org