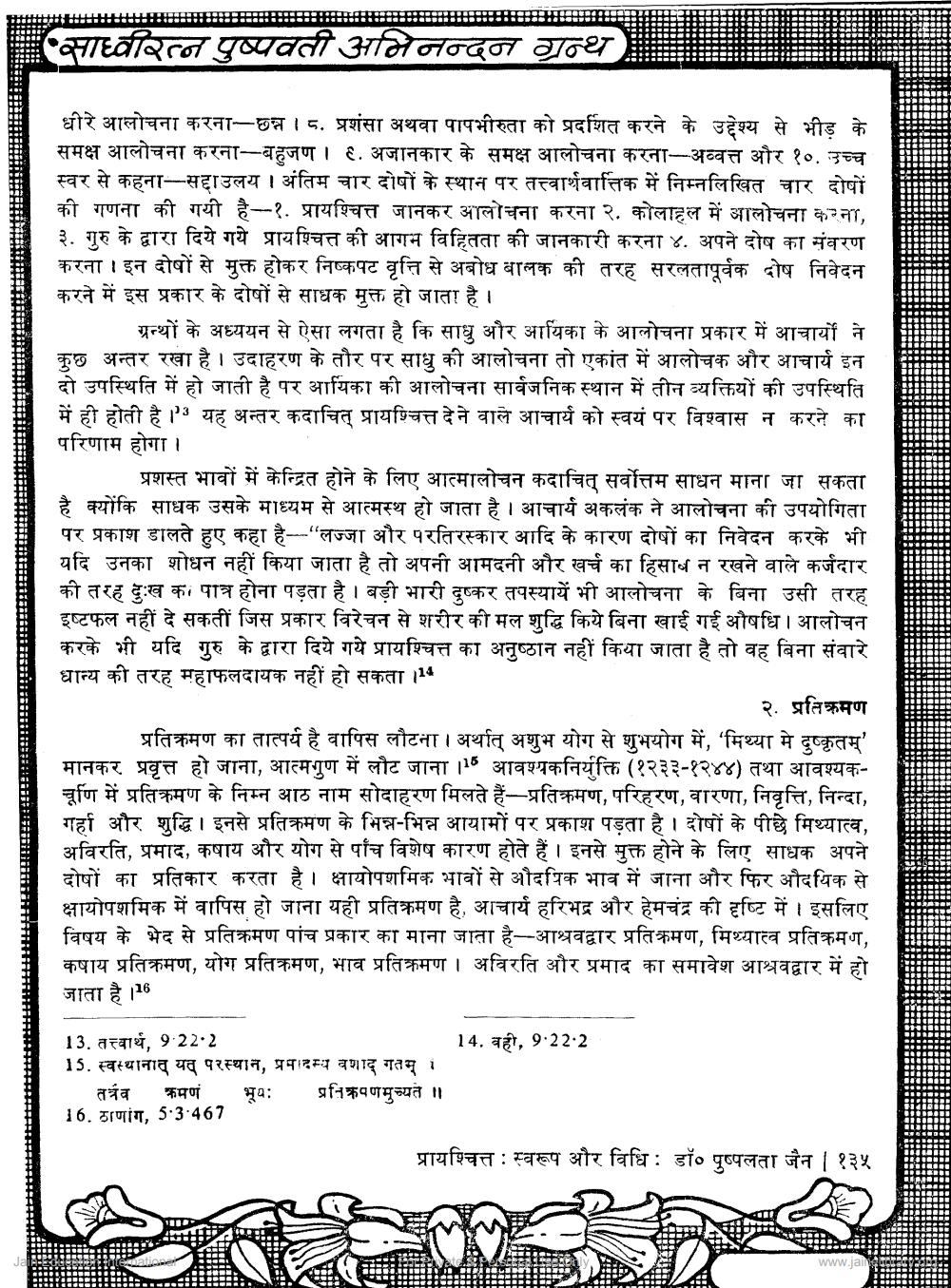________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
धीरे आलोचना करना - छन्न । ८ प्रशंसा अथवा पापभीरुता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भीड़ के समक्ष आलोचना करना - बहुजण । ६. अजानकार के समक्ष आलोचना करना -अव्वत्त और १०. उच्च स्वर से कहना - सद्दाउलय | अंतिम चार दोषों के स्थान पर तत्त्वार्थवात्र्तिक में निम्नलिखित चार दोषों की गणना की गयी है -- १. प्रायश्चित्त जानकर आलोचना करना २. कोलाहल में आलोचना करना, ३. गुरु के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त की आगन विहितता की जानकारी करना ४. अपने दोष का संवरण करना । इन दोषों से मुक्त होकर निष्कपट वृत्ति से अबोध बालक की तरह सरलतापूर्वक दोष निवेदन करने में इस प्रकार के दोषों से साधक मुक्त हो जाता है।
ग्रन्थों के अध्ययन से ऐसा लगता है कि साधु और आर्यिका के आलोचना प्रकार में आचार्यों ने कुछ अन्तर रखा है । उदाहरण के तौर पर साधु की आलोचना तो एकांत में आलोचक और आचार्य इन दो उपस्थिति में हो जाती है पर आर्यिका की आलोचना सार्वजनिक स्थान में तीन व्यक्तियों की उपस्थिति में ही होती है ।" यह अन्तर कदाचित् प्रायश्चित्त देने वाले आचार्य को स्वयं पर विश्वास न करने का परिणाम होगा ।
प्रशस्त भावों में केन्द्रित होने के लिए आत्मालोचन कदाचित् सर्वोत्तम साधन माना जा सकता है क्योंकि साधक उसके माध्यम से आत्मस्थ हो जाता है । आचार्य अकलंक ने आलोचना की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा है- “लज्जा और परतिरस्कार आदि के कारण दोषों का निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब न रखने वाले कर्जदार की तरह दुःख का पात्र होना पड़ता है । बड़ी भारी दुष्कर तपस्यायें भी आलोचना के बिना उसी तरह इष्टफल नहीं दे सकतीं जिस प्रकार विरेचन से शरीर की मल शुद्धि किये बिना खाई गई औषधि । आलोचन करके भी यदि गुरु के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वह बिना संवारे धान्य की तरह महाफलदायक नहीं हो सकता 1214
२. प्रतिक्रमण
प्रतिक्रमण का तात्पर्य है वापिस लौटना । अर्थात् अशुभ योग से शुभयोग में, 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' मानकर प्रवृत्त हो जाना, आत्मगुण में लौट जाना । 15 आवश्यकनिर्युक्ति (१२३३ - १२४४) तथा आवश्यकचूर्ण में प्रतिक्रमण के निम्न आठ नाम सोदाहरण मिलते हैं-प्रतिक्रमण, परिहरण, वारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि । इनसे प्रतिक्रमण के भिन्न-भिन्न आयामों पर प्रकाश पड़ता है । दोषों के पीछे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से पाँच विशेष कारण होते हैं । इनसे मुक्त होने के लिए साधक अपने दोषों का प्रतिकार करता है । क्षायोपशमिक भावों से औदपिक भाव में जाना और फिर औदयिक से क्षायोपशमिक में वापिस हो जाना यही प्रतिक्रमण है, आचार्य हरिभद्र और हेमचंद्र की दृष्टि में । इसलिए विषय के भेद से प्रतिक्रमण पांच प्रकार का माना जाता है-आश्रवद्वार प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, कषाय प्रतिक्रमण, योग प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण । अविरति और प्रमाद का समावेश आश्रवद्वार में हो जाता है | 26
13. तत्त्वार्थ, 9-22-2
15. स्वस्थानात् यत् परस्थान, प्रमादस्य वशाद् गतम् ।
भूयः प्रतिपणमुच्यते ॥
तत्रैव कमण 16. ठाणांग, 5.3.467
14. वही, 9.22.2
प्रायश्चित्त: स्वरूप और विधि : डॉ० पुष्पलता जैन | १३५
www.jaih