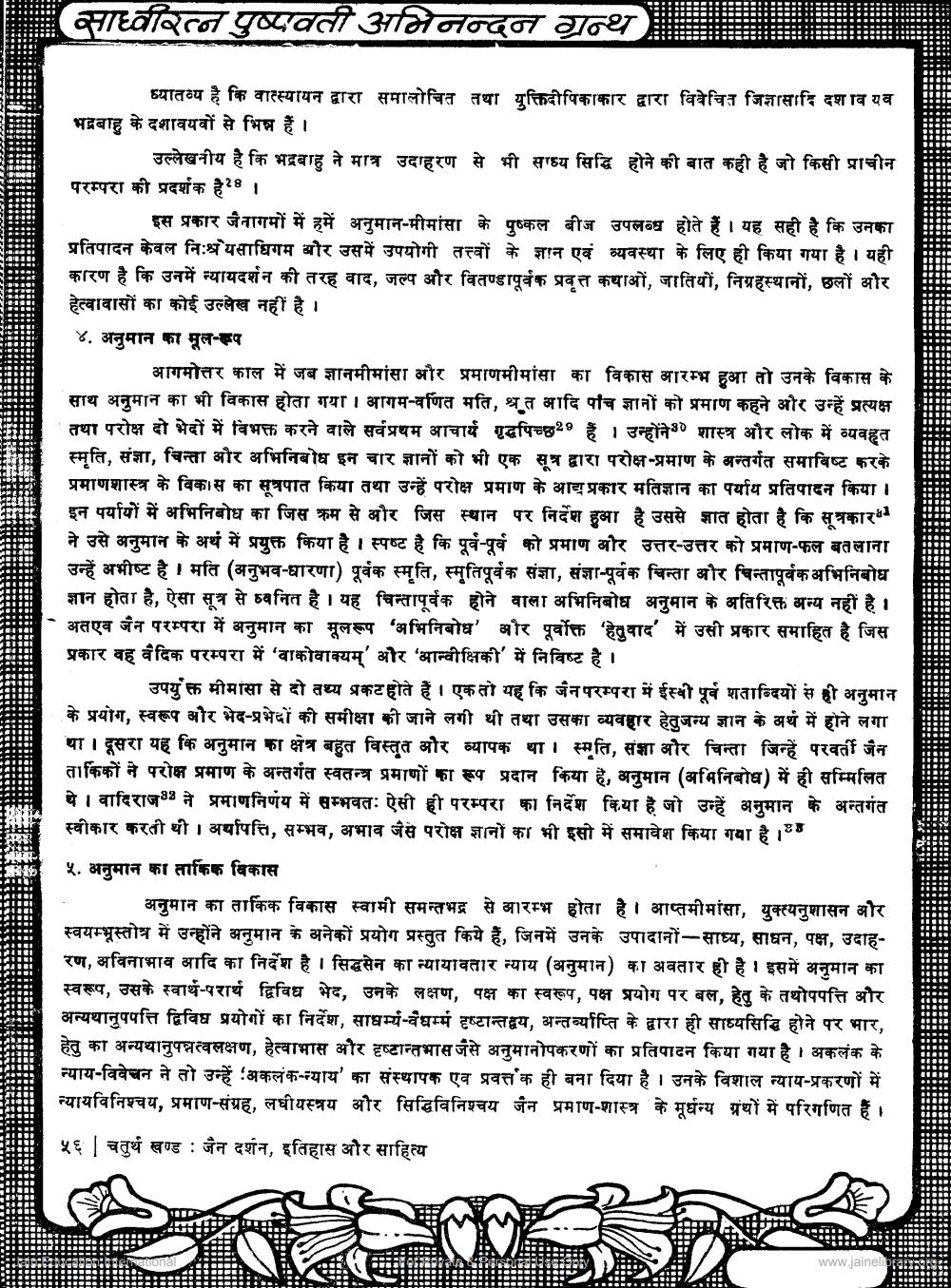________________
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
...
IC
...
ध्यातव्य है कि वात्स्यायन द्वारा समालोचित तथा युक्तिदीपिकाकार द्वारा विवेचित जिज्ञासादि दशाव यव भद्रबाहु के दशावयवों से भिन्न हैं।
उल्लेखनीय है कि भद्रबाह ने मात्र उदाहरण से भी साध्य सिद्धि होने की बात कही है जो किसी प्राचीन परम्परा की प्रदर्शक है ।
इस प्रकार जैनागमों में हमें अनुमान-मीमांसा के पुष्कल बीज उपलब्ध होते हैं। यह सही है कि उनका प्रतिपादन केवल निःश्रेयसाधिगम और उसमें उपयोगी तत्त्वों के ज्ञान एवं व्यवस्था के लिए ही किया गया है । यही कारण है कि उनमें न्यायदर्शन की तरह वाद, जल्प और वितण्डापूर्वक प्रवृत्त कथाओं, जातियों, निग्रहस्थानों, छलों और हेत्वावासों का कोई उल्लेख नहीं है। ४. अनुमान का मूल-रूप
आगमोत्तर काल में जब ज्ञानमीमांसा और प्रमाणमीमांसा का विकास आरम्भ हुआ तो उनके विकास के साथ अनुमान का भी विकास होता गया। आगम-वर्णित मति, श्रुत आदि पांच ज्ञानों को प्रमाण कहने और उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो भेदों में विभक्त करने वाले सर्वप्रथम आचार्य गृद्धपिच्छ29 हैं । उन्होंने शास्त्र और लोक में व्यवहृत स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध इन चार ज्ञानों को भी एक सूत्र द्वारा परोक्ष-प्रमाण के अन्तर्गत समाविष्ट करके प्रमाणशास्त्र के विकास का सूत्रपात किया तथा उन्हें परोक्ष प्रमाण के आय प्रकार मतिज्ञान का पर्याय प्रतिपादन किया। इन पर्यायों में अभिनिबोध का जिस क्रम से और जिस स्थान पर निर्देश हुआ है उससे ज्ञात होता है कि सूत्रकार ने उसे अनुमान के अर्थ में प्रयुक्त किया है । स्पष्ट है कि पूर्व-पूर्व को प्रमाण और उत्तर-उत्तर को प्रमाण-फल बतलाना उन्हें अभीष्ट है। मति (अनुभव-धारणा) पूर्वक स्मृति, स्मृतिपूर्वक संज्ञा, संज्ञा-पूर्वक चिन्ता और चिन्तापूर्वक अभिनिबोध ज्ञान होता है, ऐसा सूत्र से ध्वनित है। यह चिन्तापूर्वक होने वाला अभिनिबोध अनुमान के अतिरिक्त अन्य नहीं है। अतएव जैन परम्परा में अनुमान का मूलरूप 'अभिनिबोध' और पूर्वोक्त 'हेतवाद' में उसी प्रकार समाहित है जिस प्रकार वह वैदिक परम्परा में 'वाकोवाक्यम्' और 'आन्वीक्षिकी' में निविष्ट है।
उपयुक्त मीमासा से दो तथ्य प्रकट होते हैं । एक तो यह कि जैनपरम्परा में ईस्वी पूर्व शताब्दियों से ही अनुमान के प्रयोग, स्वरूप और भेद-प्रभेदों की समीक्षा की जाने लगी थी तथा उसका व्यवहार हेतुजन्य ज्ञान के अर्थ में होने लगा था। दूसरा यह कि अनुमान का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक था। स्मति, संज्ञा और चिन्ता जिन्हें परवर्ती जैन ताकिकों ने परोक्ष प्रमाण के अन्तर्गत स्वतन्त्र प्रमाणों का रूप प्रदान किया है, अनुमान (अमिनिबोध) में ही सम्मिलित थे । वादिराज ने प्रमाणनिर्णय में सम्भवतः ऐसी ही परम्परा का निर्देश किया है जो उन्हें अनुमान के अन्तर्गत स्वीकार करती थी। अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव जैसे परोक्ष ज्ञानों का भी इसो में समावेश किया गया है। ५. अनुमान का तार्किक विकास
___ अनुमान का तार्किक विकास स्वामी समन्तभद्र से आरम्भ होता है। आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूस्तोत्र में उन्होंने अनुमान के अनेकों प्रयोग प्रस्तुत किये हैं, जिनमें उनके उपादानों-साध्य, साधन, पक्ष, उदाहरण, अविनाभाव आदि का निर्देश है । सिद्धसेन का न्यायावतार न्याय (अनुमान) का अवतार ही है । इसमें अनुमान का स्वरूप, उसके स्वार्थ-परार्थ द्विविध भेद, उनके लक्षण, पक्ष का स्वरूप, पक्ष प्रयोग पर बल, हेतु के तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति द्विविध प्रयोगों का निर्देश, साधर्म्य-वैधर्म दृष्टान्तद्वय, अन्तर्व्याप्ति के द्वारा ही साध्यसिद्धि होने पर भार, हेतु का अन्यथानुपन्नत्वलक्षण, हेत्वाभास और दृष्टान्तभास जैसे अनुमानोपकरणों का प्रतिपादन किया गया है । अकलंक के न्याय-विवेचन ने तो उन्हें अकलंक-न्याय' का संस्थापक एव प्रवर्तक ही बना दिया है । उनके विशाल न्याय-प्रकरणों में न्यायविनिश्चय, प्रमाण-संग्रह, लघीयस्त्रय और सिद्धिविनिश्चय जैन प्रमाण-शास्त्र के मूर्धन्य ग्रंथों में परिगणित हैं।
५६ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
www.jainelibrat