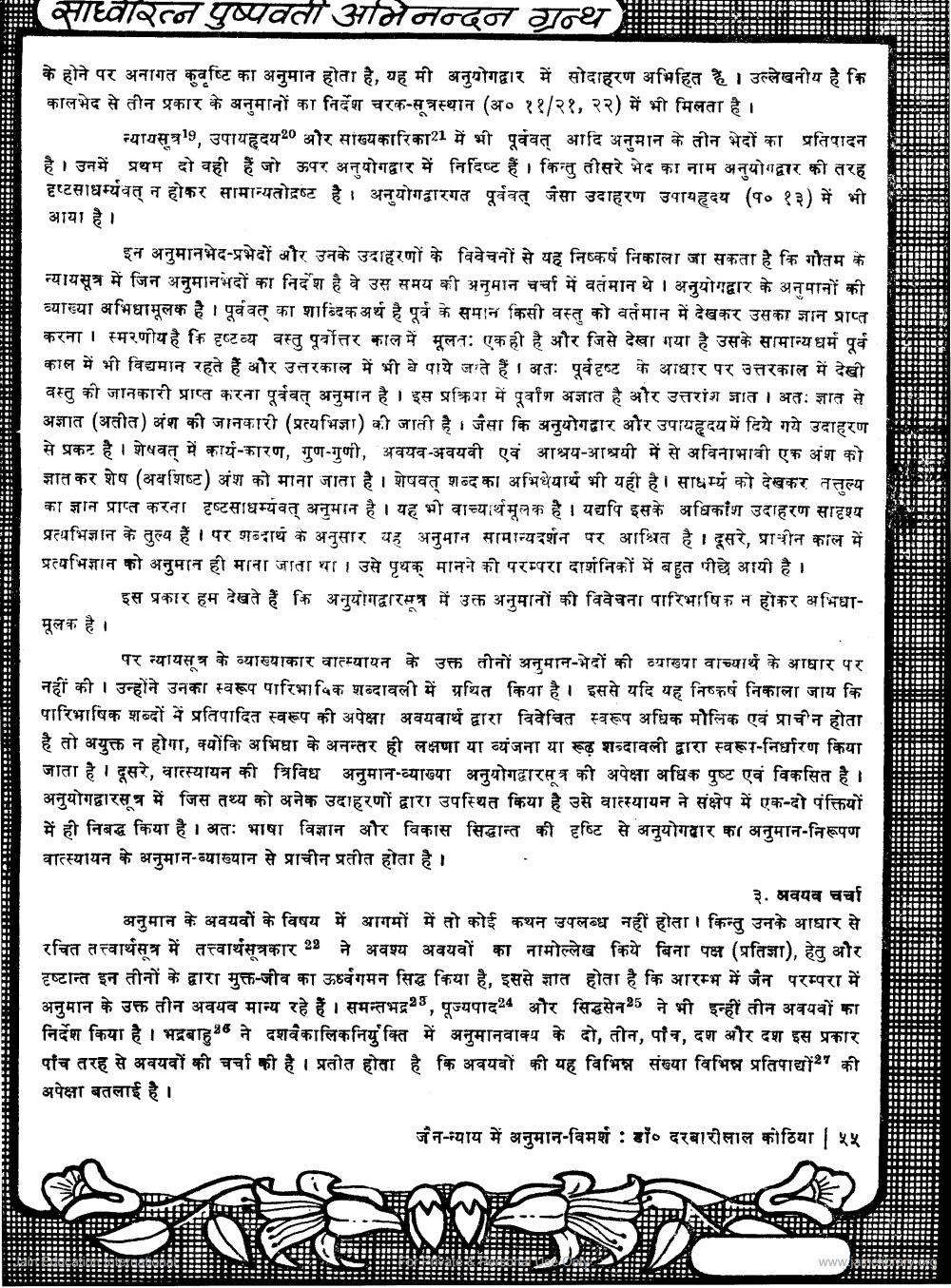________________
साध्वारत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
iiiiiiiiii
के होने पर अनागत कुवृष्टि का अनुमान होता है, यह मी अनुयोगद्वार में सोदाहरण अभिहित है । उल्लेखनीय है कि कालभेद से तीन प्रकार के अनुमानों का निर्देश चरक-सूत्रस्थान (अ० ११/२१, २२) में भी मिलता है।
न्यायसूत्र, उपायहृदय20 और सांख्यकारिका में भी पूर्ववत् आदि अनुमान के तीन भेदों का प्रतिपादन है। उनमें प्रथम दो वही हैं जो ऊपर अनुयोगद्वार में निर्दिष्ट हैं। किन्तु तीसरे भेद का नाम अनुयोगद्वार की तरह दृष्टसाधर्म्यवत् न होकर सामान्यतोद्रष्ट है। अनुयोगद्वारगत पूर्ववत् जैसा उदाहरण उपायहृदय (प. १३) में भी आया है।
इन अनुमानभेद-प्रभेदों और उनके उदाहरणों के विवेचनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गौतम के न्यायसूत्र में जिन अनुमानभेदों का निर्देश है वे उस समय की अनुमान चर्चा में वर्तमान थे । अनुयोगद्वार के अनमानों की व्याख्या अभिधामूलक है । पूर्ववत् का शाब्दिक अर्थ है पूर्व के समान किसी वस्तु को वर्तमान में देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना । स्मरणीय है कि दृष्ट व्य वस्तु पूर्वोत्तर काल में मूलतः एक ही है और जिसे देखा गया है उसके सामान्य धर्म पूर्व काल में भी विद्यमान रहते हैं और उत्तरकाल में भी वे पाये जाते हैं । अतः पूर्व दृष्ट के आधार पर उत्तरकाल में देखी वस्तु की जानकारी प्राप्त करना पूर्ववत् अनुमान है । इस प्रक्रिया में पूर्वांश अज्ञात है और उत्तरांश जात । अतः ज्ञात से अज्ञात (अतीत) अंश की जानकारी (प्रत्यभिज्ञा) की जाती है। जैसा कि अनुयोगद्वार और उपायहृदय में दिये गये उदाहरण से प्रकट है । शेषवत् में कार्य-कारण, गुण-गुणी, अवयव-अवयवी एवं आश्रय-आश्रयी में से अविनाभावी एक अंश को ज्ञात कर शेष (अवशिष्ट) अंश को माना जाता है । शेषवत् शब्द का अभिधेयार्थ भी यही है। साधर्म्य को देखकर तत्तुल्य का ज्ञान प्राप्त करना दृष्टसाधम्यवत् अनुमान है। यह भी वाच्यार्थमूलक है । यद्यपि इसके अधिकांश उदाहरण सादृश्य प्रत्यभिज्ञान के तुल्य हैं । पर शब्दार्थ के अनुसार यह अनुमान सामान्यदर्शन पर आश्रित है। दूसरे, प्राचीन काल में प्रत्यभिज्ञान को अनुमान ही माना जाता था। उसे पृथक् मानने की परम्परा दार्शनिकों में बहुत पीछे आयो है ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुयोगद्वारसत्र में उक्त अनुमानों की विवेचना पारिभाषिक न होकर अभिधामूलक है।
पर न्यायसूत्र के व्याख्याकार वात्स्यायन के उक्त तीनों अनुमान-भेदों की व्याख्या वाच्यार्थ के आधार पर नहीं की। उन्होंने उनका स्वरूप पारिभाषिक शब्दावली में ग्रथित किया है। इससे यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि पारिभाषिक शब्दों में प्रतिपादित स्वरूप की अपेक्षा अवयवार्थ द्वारा विवेचित स्वरूप अधिक मौलिक एवं प्राचीन होता है तो अयुक्त न होगा, क्योंकि अभिधा के अनन्तर ही लक्षणा या व्यंजना या रूढ़ शब्दावली द्वारा स्वरूप-निर्धारण किया जाता है । दूसरे, वात्स्यायन की त्रिविध अनुमान-व्याख्या अनुयोगद्वारसूत्र की अपेक्षा अधिक पुष्ट एवं विकसित है। अनुयोगद्वारसूत्र में जिस तथ्य को अनेक उदाहरणों द्वारा उपस्थित किया है उसे वात्स्यायन ने संक्षेप में एक-दो पंक्तियों में ही निबद्ध किया है। अतः भाषा विज्ञान और विकास सिद्धान्त की दृष्टि से अनुयोगद्वार का अनुमान-निरूपण वात्स्यायन के अनुमान-व्याख्यान से प्राचीन प्रतीत होता है।
३. अवयव चर्चा अनुमान के अवयवों के विषय में आगमों में तो कोई कथन उपलब्ध नहीं होता। किन्तु उनके आधार से रचित तत्त्वार्थसत्र में तत्त्वार्थसत्रकार ने अवश्य अवयवों का नामोल्लेख किये बिना पक्ष (प्रतिज्ञा), हेतु और दृष्टान्त इन तीनों के द्वारा मुक्त-जीव का ऊर्ध्वगमन सिद्ध किया है, इससे ज्ञात होता है कि आरम्भ में जैन परम्परा में अनुमान के उक्त तीन अवयव मान्य रहे हैं। समन्तभद्र, पूज्यपाद24 और सिद्धसेन25 ने भी इन्हीं तीन अवयवों का निर्देश किया है। भद्रबाहु ने दशवकालिकनियुक्ति में अनुमानवाक्य के दो, तीन, पांच, दश और दश इस प्रकार पांच तरह से अवयवों की चर्चा की है । प्रतीत होता है कि अवयवों की यह विभिन्न संख्या विभिन्न प्रतिपाद्यों की अपेक्षा बतलाई है।
जैन-न्याय में अनुमान-विमर्श : डॉ० दरबारीलाल कोठिया | ५५