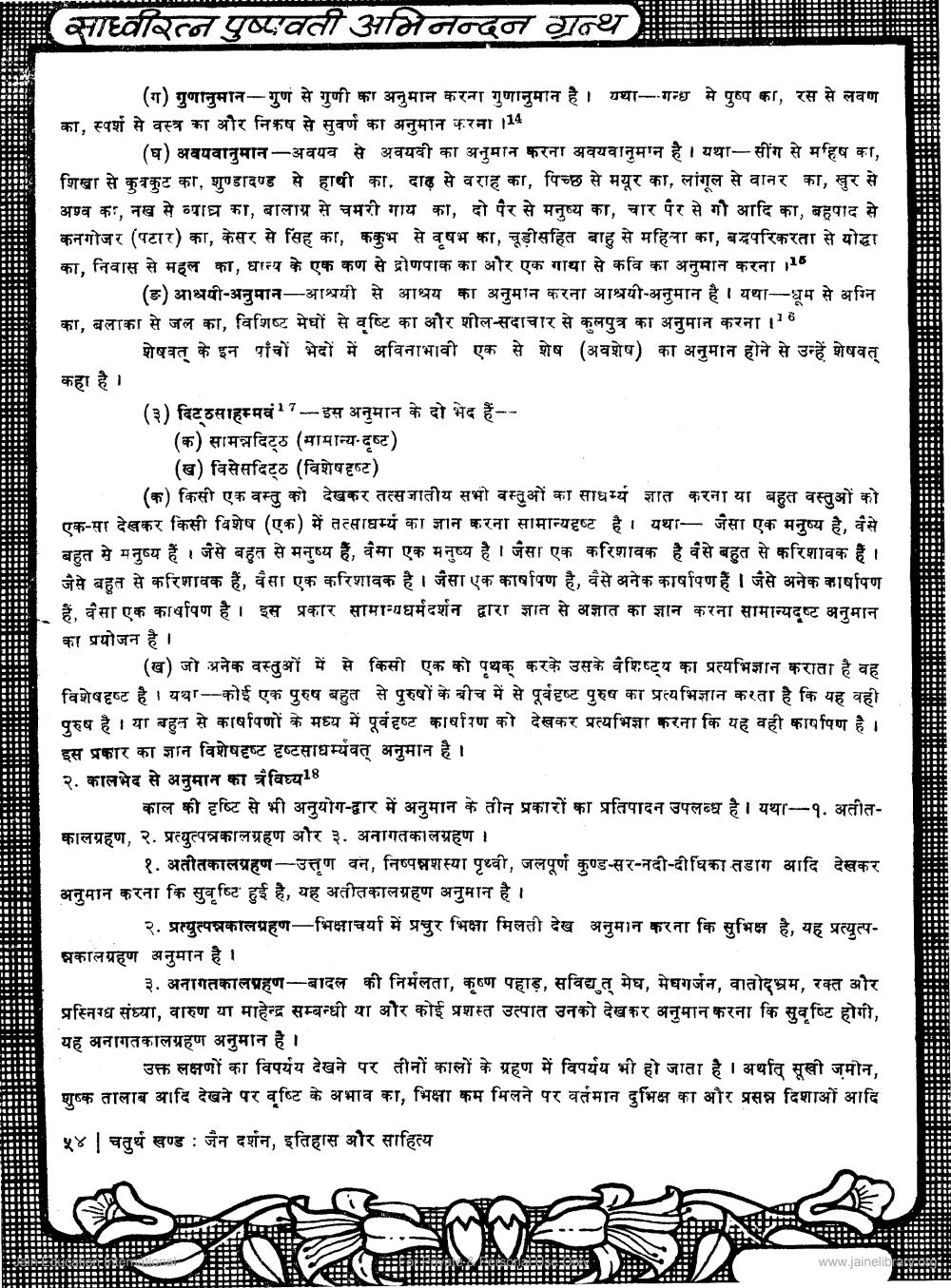________________
साध्वीरत्न पुष्वती अभिनन्दन ग्रन्थ ।
(ग) गुणानुमान-गुण से गुणी का अनुमान करना गुणानुमान है। यथा---गन्ध से पुष्प का, रस से लवण का, स्पर्श से वस्त्र का और निकष से सुवर्ण का अनुमान करना ।14
(घ) अवयवानुमान-अवयव से अवयवी का अनुमान करना अवयवानुमान है । यथा-सींग से महिष का, शिखा से वकुट का, शुण्डादण्ड से हाथी का, दाढ़ से वराह का, पिच्छ से मयूर का, लांगूल से वानर का, खुर से अश्व का, नख से व्याघ्र का, बालाग्र से चमरी गाय का, दो पैर से मनुष्य का, चार पर से गौ आदि का, बहपाद से कनगोजर (पटार) का, केसर से सिंह का, ककुभ से वृषभ का, चूड़ीसहित बाहु से महिला का, बद्धपरिकरता से योद्धा का, निवास से महल का, धान्य के एक कण से द्रोणपाक का और एक गाथा से कवि का अनुमान करना ।
(ङ) आश्रयी-अनुमान-आश्रयी से आश्रय का अनुमान करना आश्रयी-अनुमान है । यथा-धूम से अग्नि का, बलाका से जल का, विशिष्ट मेघों से वृष्टि का और शील-सदाचार से कुलपुत्र का अनुमान करना ।18
शेषवत के इन पांचों भेदों में अविनाभावी एक से शेष (अवशेष) का अनुमान होने से उन्हें शेषवत कहा है।
(३) विट ठसाहम्मवं17--इस अनुमान के दो भेद हैं---
(क) सामन्नदिट्ठ (मामान्य दृष्ट)
(ख) विसेसदिट्ठ (विशेषदृष्ट)
(क) किसी एक वस्तु को देखकर तत्सजातीय सभी वस्तुओं का साधर्म्य ज्ञात करना या बहुत वस्तुओं को कमा देखकर किसी विशेष (एक) में तत्साधर्म्य का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट है। यथा- जैसा एक मनुष्य है. वैसे बहत मे मनुष्य हैं । जैसे बहुत से मनुष्य हैं, वैसा एक मनुष्य है । जैसा एक करिशावक है वैसे बहुत से करिशावक हैं । जैसे बहुत से करिशावक हैं, वैसा एक करिशावक है । जैसा एक कार्षापण है, वैसे अनेक कार्षापण हैं । जैसे अनेक कार्षापण हैं. वैसा एक कार्षापण है। इस प्रकार सामान्यधर्मदर्शन द्वारा ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमान का प्रयोजन है।
(ख) जो अनेक वस्तुओं में से किसी एक को पृथक् करके उसके वैशिष्ट्य का प्रत्यभिज्ञान कराता है वह विशेषदृष्ट है। यथा--कोई एक पुरुष बहुत से पुरुषों के बीच में से पूर्वदृष्ट पुरुष का प्रत्यभिज्ञान करता है कि यह वही .
या बहुत से कार्षापणों के मध्य में पूर्वदृष्ट कार्षापण को देखकर प्रत्यभिज्ञा करना कि यह वही कार्षापण है। इस प्रकार का ज्ञान विशेषदृष्ट दृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान है। २. कालभेद से अनुमान का वैविध्य18
काल की दृष्टि से भी अनुयोग-द्वार में अनुमान के तीन प्रकारों का प्रतिपादन उपलब्ध है। यथा-१. अतीतकालग्रहण, २. प्रत्युत्पन्नकालग्रहण और ३. अनागतकालग्रहण ।।
१. अतीतकालग्रहण-उत्तृण वन, निष्पन्नशस्या पृथ्वी, जलपूर्ण कुण्ड-सर-नदी-दीपिका तडाग आदि देखकर अनुमान करना कि सुवृष्टि हुई है, यह अतीतकालग्रहण अनुमान है।
२. प्रत्युत्पन्नकालग्रहण-भिक्षाचर्या में प्रचुर भिक्षा मिलती देख अनुमान करना कि सुभिक्ष है, यह प्रत्युत्पप्रकालग्रहण अनुमान है ।
३. अनागतकालग्रहण-बादल की निर्मलता, कृष्ण पहाड़, सविद्युत् मेघ, मेघगर्जन, वातोभ्रम, रक्त और प्रस्निग्ध संध्या, वारुण या माहेन्द्र सम्बन्धी या और कोई प्रशस्त उत्पात उनको देखकर अनुमान करना कि सुवष्टि होगी, यह अनागतकालग्रहण अनुमान है।
उक्त लक्षणों का विपर्यय देखने पर तीनों कालों के ग्रहण में विपर्यय भी हो जाता है । अर्थात् सूखी जमीन, शुष्क तालाब आदि देखने पर वृष्टि के अभाव का, भिक्षा कम मिलने पर वर्तमान दुभिक्ष का और प्रसन्न दिशाओं आदि
:::
:::
:::
:
५४ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य
www.jainelibrariete