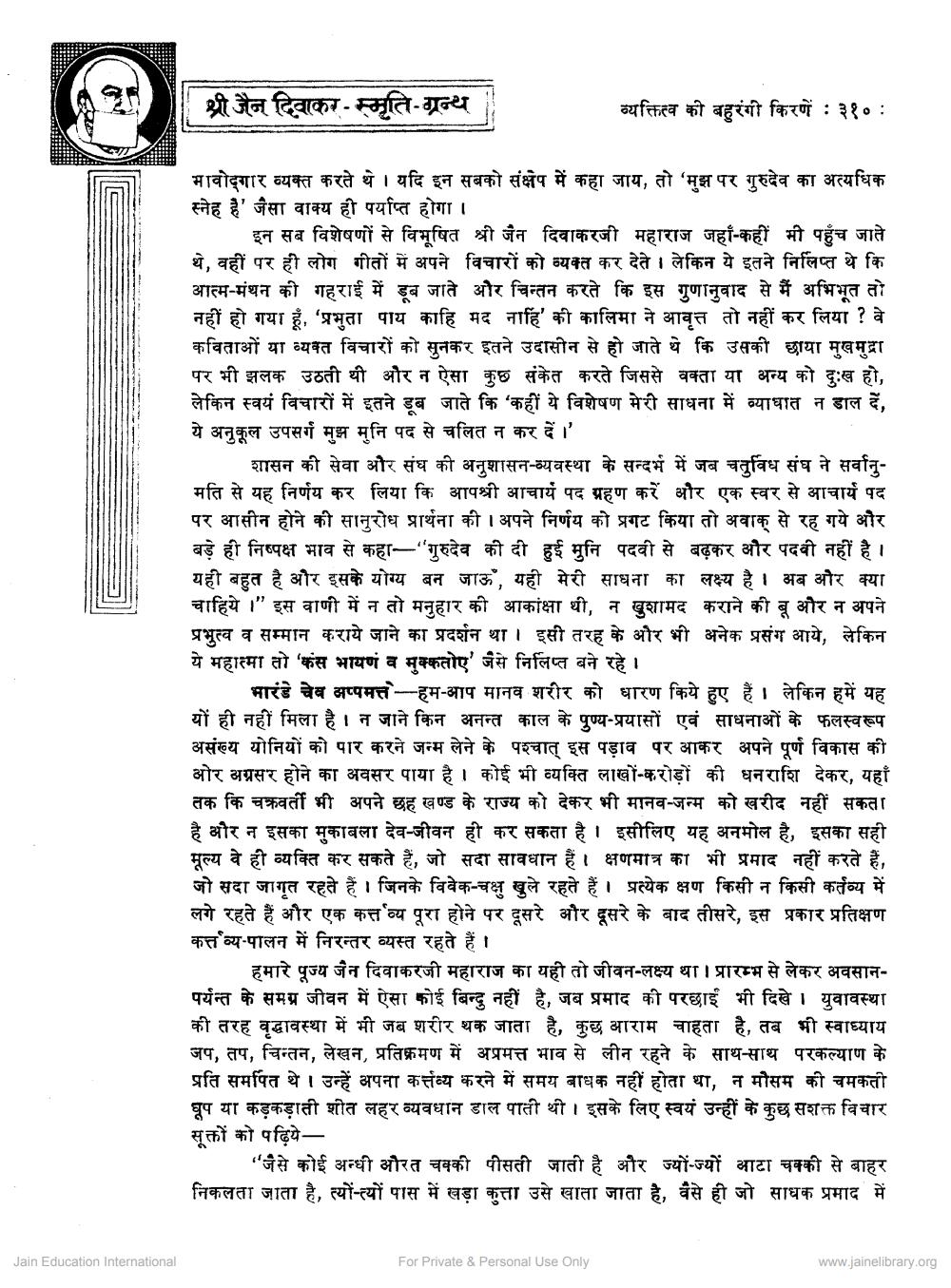________________
श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ
व्यक्तित्व की बहरंगी किरणे : ३१० :
भावोद्गार व्यक्त करते थे । यदि इन सबको संक्षेप में कहा जाय, तो 'मुझ पर गुरुदेव का अत्यधिक स्नेह है' जैसा वाक्य ही पर्याप्त होगा।
इन सब विशेषणों से विभूषित श्री जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ-कहीं भी पहुंच जाते थे, वहीं पर ही लोग गीतों में अपने विचारों को व्यक्त कर देते। लेकिन ये इतने निलिप्त थे कि आत्म-मंथन की गहराई में डूब जाते और चिन्तन करते कि इस गुणानुवाद से मैं अभिभूत तो नहीं हो गया है, 'प्रभुता पाय काहि मद नाहिं' की कालिमा ने आवृत्त तो नहीं कर लिया? वे कविताओं या व्यक्त विचारों को सुनकर इतने उदासीन से हो जाते थे कि उसकी छाया मुखमुद्रा पर भी झलक उठती थी और न ऐसा कुछ संकेत करते जिससे वक्ता या अन्य को दुःख हो, लेकिन स्वयं विचारों में इतने डूब जाते कि 'कहीं ये विशेषण मेरी साधना में व्याघात न डाल दें, ये अनुकूल उपसर्ग मुझ मुनि पद से चलित न कर दें।'
शासन की सेवा और संघ की अनुशासन-व्यवस्था के सन्दर्भ में जब चतुर्विध संघ ने सर्वानुमति से यह निर्णय कर लिया कि आपश्री आचार्य पद ग्रहण करें और एक स्वर से आचार्य पद पर आसीन होने की सानुरोध प्रार्थना की । अपने निर्णय को प्रगट किया तो अवाक् से रह गये और बड़े ही निष्पक्ष भाव से कहा-"गुरुदेव की दी हुई मुनि पदवी से बढ़कर और पदवी नहीं है। यही बहुत है और इसके योग्य बन जाऊँ, यही मेरी साधना का लक्ष्य है। अब और क्या चाहिये ।" इस वाणी में न तो मनुहार की आकांक्षा थी, न खुशामद कराने की बू और न अपने प्रभूत्व व सम्मान कराये जाने का प्रदर्शन था। इसी तरह के और भी अनेक प्रसंग आये, लेकिन ये महात्मा तो 'कस भायणं व मुक्कतोए' जैसे निर्लिप्त बने रहे।
भारंडे चेव अप्पमत्त-हम-आप मानव शरीर को धारण किये हुए हैं। लेकिन हमें यह यों ही नहीं मिला है । न जाने किन अनन्त काल के पुण्य-प्रयासों एवं साधनाओं के फलस्वरूप असंख्य योनियों को पार करने जन्म लेने के पश्चात् इस पड़ाव पर आकर अपने पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर पाया है। कोई भी व्यक्ति लाखों-करोड़ों की धनराशि देकर, यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी अपने छह खण्ड के राज्य को देकर भी मानव-जन्म को खरीद नहीं सकता है और न इसका मुकाबला देव-जीवन ही कर सकता है। इसीलिए यह अनमोल है, इसका सही मूल्य वे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो सदा सावधान हैं। क्षणमात्र का भी प्रमाद नहीं करते हैं, जो सदा जागत रहते हैं। जिनके विवेक-चक्षु खुले रहते हैं। प्रत्येक क्षण किसी न किसी कर्तव्य में लगे रहते हैं और एक कत्तव्य पूरा होने पर दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, इस प्रकार प्रतिक्षण कर्तव्य-पालन में निरन्तर व्यस्त रहते हैं।
हमारे पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज का यही तो जीवन-लक्ष्य था। प्रारम्भ से लेकर अवसानपर्यन्त के समग्र जीवन में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, जब प्रमाद की परछाईं भी दिखे । युवावस्था की तरह वृद्धावस्था में भी जब शरीर थक जाता है, कुछ आराम चाहता है, तब भी स्वाध्याय जप, तप, चिन्तन, लेखन, प्रतिक्रमण में अप्रमत्त भाव से लीन रहने के साथ-साथ परकल्याण के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपना कर्त्तव्य करने में समय बाधक नहीं होता था, न मौसम की चमकती धूप या कड़कड़ाती शीत लहर व्यवधान डाल पाती थी। इसके लिए स्वयं उन्हीं के कुछ सशक्त विचार सूक्तों को पढ़िये
"जैसे कोई अन्धी औरत चक्की पीसती जाती है और ज्यों-ज्यों आटा चक्की से बाहर निकलता जाता है, त्यों-त्यों पास में खड़ा कुत्ता उसे खाता जाता है, वैसे ही जो साधक प्रमाद में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org