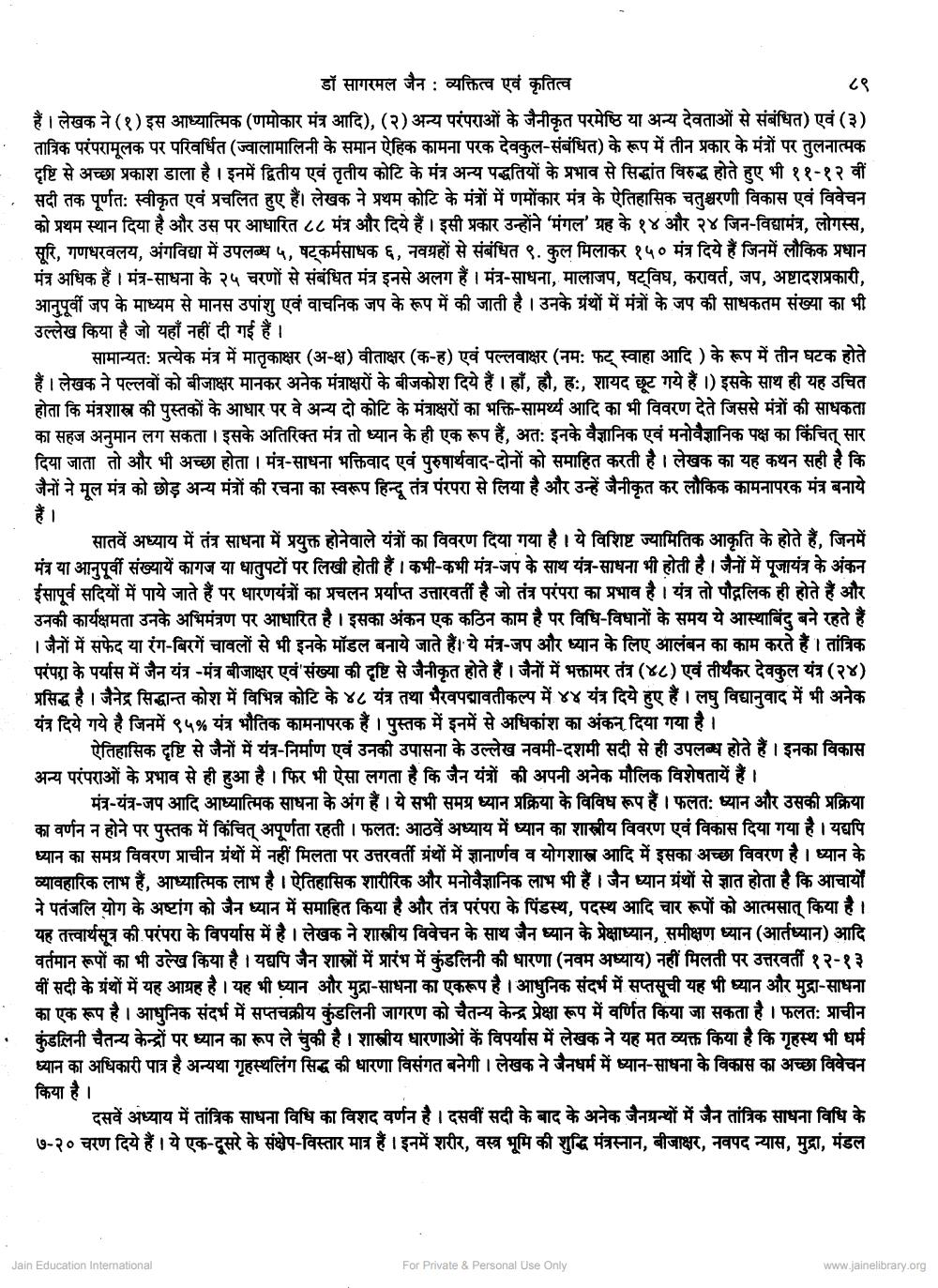________________
८९
डॉ सागरमल जैन : व्यक्तित्व एवं कृतित्व हैं। लेखक ने (१) इस आध्यात्मिक (णमोकार मंत्र आदि), (२) अन्य परंपराओं के जैनीकृत परमेष्ठि या अन्य देवताओं से संबंधित) एवं (३) तात्रिक परंपरामूलक पर परिवर्धित (ज्वालामालिनी के समान ऐहिक कामना परक देवकुल-संबंधित) के रूप में तीन प्रकार के मंत्रों पर तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा प्रकाश डाला है । इनमें द्वितीय एवं तृतीय कोटि के मंत्र अन्य पद्धतियों के प्रभाव से सिद्धांत विरुद्ध होते हुए भी ११-१२ वीं सदी तक पूर्णतः स्वीकृत एवं प्रचलित हुए हैं। लेखक ने प्रथम कोटि के मंत्रों में णमोकार मंत्र के ऐतिहासिक चतुश्चरणी विकास एवं विवेचन को प्रथम स्थान दिया है और उस पर आधारित ८८ मंत्र और दिये हैं। इसी प्रकार उन्होंने 'मंगल' ग्रह के १४ और २४ जिन-विद्यामंत्र, लोगस्स, सूरि, गणधरवलय, अंगविद्या में उपलब्ध ५, षट्कर्मसाधक ६, नवग्रहों से संबंधित ९. कुल मिलाकर १५० मंत्र दिये हैं जिनमें लौकिक प्रधान मंत्र अधिक हैं। मंत्र-साधना के २५ चरणों से संबंधित मंत्र इनसे अलग हैं । मंत्र-साधना, मालाजप, ट्विघ, करावर्त, जप, अष्टादशप्रकारी, आनपूर्वी जप के माध्यम से मानस उपांशु एवं वाचनिक जप के रूप में की जाती है। उनके ग्रंथों में मंत्रों के जप की साधकतम संख्या का भी उल्लेख किया है जो यहाँ नहीं दी गई हैं।
सामान्यत: प्रत्येक मंत्र में मातृकाक्षर (अ-क्ष) वीताक्षर (क-ह) एवं पल्लवाक्षर (नमः फट् स्वाहा आदि ) के रूप में तीन घटक होते हैं । लेखक ने पल्लवों को बीजाक्षर मानकर अनेक मंत्राक्षरों के बीजकोश दिये हैं। हाँ, हौ, ह्रः, शायद छूट गये हैं।) इसके साथ ही यह उचित होता कि मंत्रशास्त्र की पुस्तकों के आधार पर वे अन्य दो कोटि के मंत्राक्षरों का भक्ति-सामर्थ्य आदि का भी विवरण देते जिससे मंत्रों की साधकता का सहज अनुमान लग सकता। इसके अतिरिक्त मंत्र तो ध्यान के ही एक रूप हैं, अत: इनके वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष का किंचित् सार दिया जाता तो और भी अच्छा होता । मंत्र-साधना भक्तिवाद एवं पुरुषार्थवाद-दोनों को समाहित करती है। लेखक का यह कथन सही है कि जैनों ने मूल मंत्र को छोड़ अन्य मंत्रों की रचना का स्वरूप हिन्दू तंत्र पंरपरा से लिया है और उन्हें जैनीकृत कर लौकिक कामनापरक मंत्र बनाये
सातवें अध्याय में तंत्र साधना में प्रयुक्त होनेवाले यंत्रों का विवरण दिया गया है। ये विशिष्ट ज्यामितिक आकृति के होते हैं, जिनमें मंत्र या आनुपूर्वी संख्यायें कागज या धातुपटों पर लिखी होती हैं। कभी-कभी मंत्र-जप के साथ यंत्र-साधना भी होती है। जैनों में पूजायंत्र के अंकन
दियों में पाये जाते हैं पर धारणयंत्रों का प्रचलन प्रर्याप्त उत्तारवती है जो तंत्र परंपरा का प्रभाव है। यंत्र तो पौद्रलिक ही होते हैं और उनकी कार्यक्षमता उनके अभिमंत्रण पर आधारित है। इसका अंकन एक कठिन काम है पर विधि-विधानों के समय ये आस्थाबिंदु बने रहते हैं । जैनों में सफेद या रंग-बिरगें चावलों से भी इनके मॉडल बनाये जाते हैं। ये मंत्र-जप और ध्यान के लिए आलंबन का काम करते हैं। तांत्रिक परंपरा के पर्यास में जैन यंत्र -मंत्र बीजाक्षर एवं संख्या की दृष्टि से जैनीकृत होते हैं । जैनों में भक्तामर तंत्र (४८) एवं तीर्थंकर देवकुल यंत्र (२४) प्रसिद्ध है । जैनेद्र सिद्धान्त कोश में विभिन्न कोटि के ४८ यंत्र तथा भैरवपद्मावतीकल्प में ४४ यंत्र दिये हुए हैं । लघु विद्यानुवाद में भी अनेक यंत्र दिये गये है जिनमें ९५% यंत्र भौतिक कामनापरक हैं । पुस्तक में इनमें से अधिकांश का अंकन दिया गया है।
ऐतिहासिक दृष्टि से जैनों में यंत्र-निर्माण एवं उनकी उपासना के उल्लेख नवमी-दशमी सदी से ही उपलब्ध होते हैं। इनका विकास अन्य परंपराओं के प्रभाव से ही हुआ है । फिर भी ऐसा लगता है कि जैन यंत्रों की अपनी अनेक मौलिक विशेषतायें हैं।
आध्यात्मिक साधना के अंग हैं। ये सभी समग्र ध्यान प्रक्रिया के विविध रूप हैं। फलत: ध्यान और उसकी प्रक्रिया का वर्णन न होने पर पुस्तक में किंचित् अपूर्णता रहती । फलत: आठवें अध्याय में ध्यान का शास्त्रीय विवरण एवं विकास दिया गया है । यद्यपि ध्यान का समग्र विवरण प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता पर उत्तरवर्ती ग्रंथों में ज्ञानार्णव व योगशास्त्र आदि में इसका अच्छा विवरण है । ध्यान के व्यावहारिक लाभ हैं, आध्यात्मिक लाभ है । ऐतिहासिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। जैन ध्यान ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आचार्यों ने पतंजलि योग के अष्टांग को जैन ध्यान में समाहित किया है और तंत्र परंपरा के पिंडस्थ, पदस्थ आदि चार रूपों को आत्मसात् किया है। यह तत्त्वार्थसूत्र की परंपरा के विपर्यास में है । लेखक ने शास्त्रीय विवेचन के साथ जैन ध्यान के प्रेक्षाध्यान, समीक्षण ध्यान (आर्तध्यान) आदि वर्तमान रूपों का भी उल्ख किया है । यद्यपि जैन शास्त्रों में प्रारंभ में कुंडलिनी की धारणा (नवम अध्याय) नहीं मिलती पर उत्तरवर्ती १२-१३ वीं सदी के ग्रंथों में यह आग्रह है। यह भी ध्यान और मुद्रा-साधना का एकरूप है। आधुनिक संदर्भ में सप्तसूची यह भी ध्यान और मुद्रा-साधना का एक रूप है । आधुनिक संदर्भ में सप्तचक्रीय कुंडलिनी जागरण को चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा रूप में वर्णित किया जा सकता है । फलत: प्राचीन कुंडलिनी चैतन्य केन्द्रों पर ध्यान का रूप ले चुकी है। शास्त्रीय धारणाओं के विपर्यास में लेखक ने यह मत व्यक्त किया है कि गृहस्थ भी धर्म ध्यान का अधिकारी पात्र है अन्यथा गृहस्थलिंग सिद्ध की धारणा विसंगत बनेगी। लेखक ने जैनधर्म में ध्यान-साधना के विकास का अच्छा विवेचन किया है।
दसवें अध्याय में तांत्रिक साधना विधि का विशद वर्णन है । दसवीं सदी के बाद के अनेक जैनग्रन्थों में जैन तांत्रिक साधना विधि के ७-२० चरण दिये हैं। ये एक-दूसरे के संक्षेप-विस्तार मात्र हैं। इनमें शरीर, वस्त्र भूमि की शुद्धि मंत्रस्नान, बीजाक्षर, नवपद न्यास, मुद्रा, मंडल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org