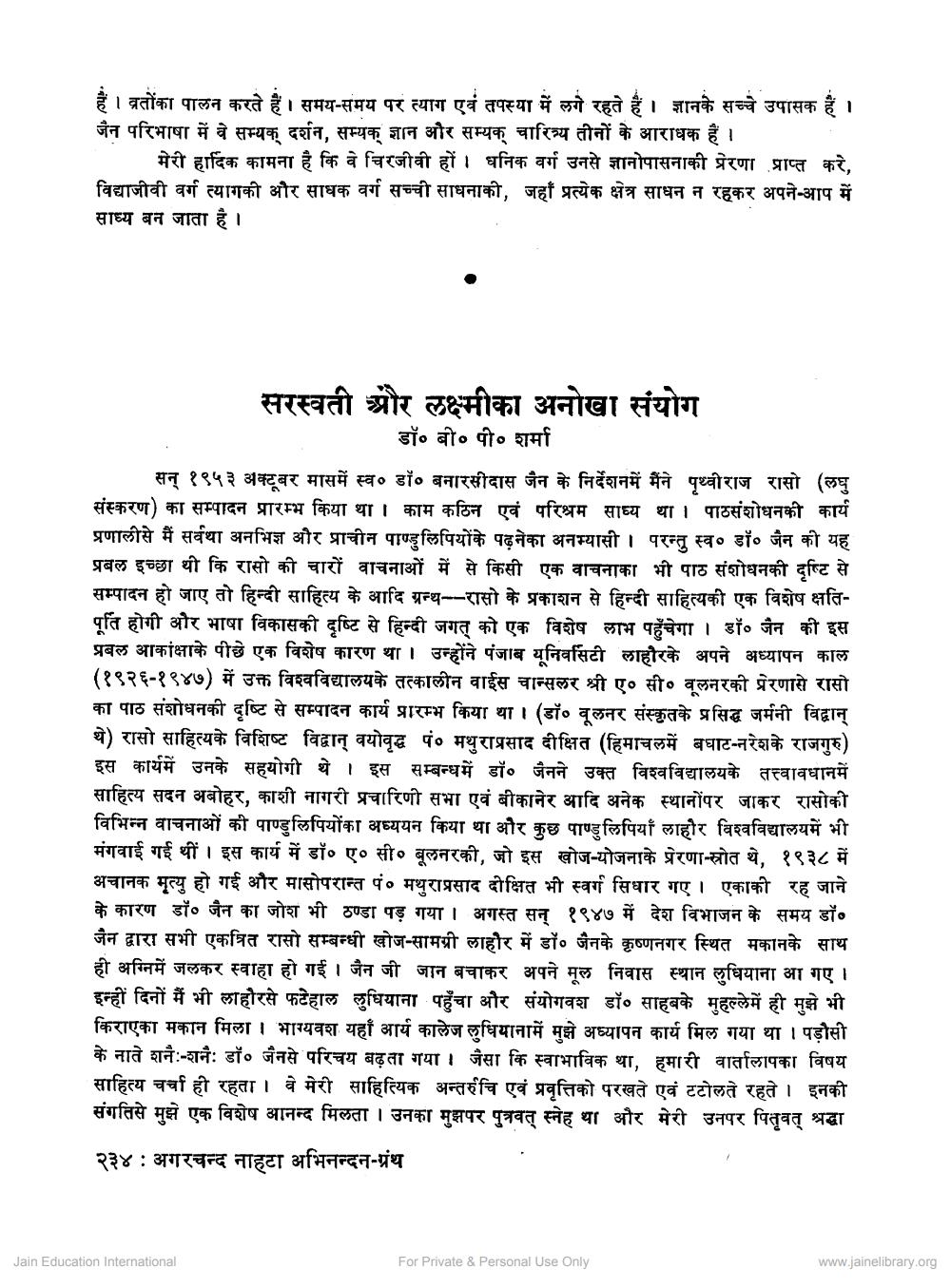________________
हैं । व्रतोंका पालन करते हैं। समय-समय पर त्याग एवं तपस्या में लगे रहते हैं। ज्ञानके सच्चे उपासक हैं । जैन परिभाषा में वे सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य तीनों के आराधक हैं।।
मेरी हादिक कामना है कि वे चिरजीवी हों। धनिक वर्ग उनसे ज्ञानोपासनाकी प्रेरणा प्राप्त करे, विद्याजीवी वर्ग त्यागकी और साधक वर्ग सच्ची साधनाकी, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र साधन न रहकर अपने-आप में साध्य बन जाता है।
सरस्वती और लक्ष्मीका अनोखा संयोग
डॉ० बी० पी० शर्मा सन् १९५३ अक्टूबर मासमें स्व० डॉ० बनारसीदास जैन के निर्देशनमें मैंने पृथ्वीराज रासो (लघु संस्करण) का सम्पादन प्रारम्भ किया था। काम कठिन एवं परिश्रम साध्य था। पाठसंशोधनकी कार्य प्रणालीसे मैं सर्वथा अनभिज्ञ और प्राचीन पाण्डुलिपियोंके पढ़नेका अनम्यासी। परन्तु स्व० डॉ० जैन की यह प्रबल इच्छा थी कि रासो की चारों वाचनाओं में से किसी एक वाचनाका भी पाठ संशोधनकी दृष्टि से सम्पादन हो जाए तो हिन्दी साहित्य के आदि ग्रन्थ-रासो के प्रकाशन से हिन्दी साहित्यकी एक विशेष क्षतिपूर्ति होगी और भाषा विकासकी दृष्टि से हिन्दी जगत् को एक विशेष लाभ पहुँचेगा । डॉ० जैन की इस प्रबल आकांक्षाके पीछे एक विशेष कारण था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौरके अपने अध्यापन काल (१९२६-१९४७) में उक्त विश्वविद्यालयके तत्कालीन वाईस चान्सलर श्री ए० सी० वूलनरकी प्रेरणासे रासो का पाठ संशोधनकी दृष्टि से सम्पादन कार्य प्रारम्भ किया था। (डॉ० वूलनर संस्कृतके प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान् थे) रासो साहित्यके विशिष्ट विद्वान् वयोवृद्ध पं० मथुराप्रसाद दीक्षित (हिमाचलमें बघाट-नरेशके राजगुरु) इस कार्यमें उनके सहयोगी थे । इस सम्बन्धमें डॉ. जैनने उक्त विश्वविद्यालयके तत्त्वावधानमें साहित्य सदन अबोहर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा एवं बीकानेर आदि अनेक स्थानोंपर जाकर रासोकी विभिन्न वाचनाओं की पाण्डुलिपियोंका अध्ययन किया था और कुछ पाण्डुलिपियाँ लाहौर विश्वविद्यालयमें भी मंगवाई गई थीं। इस कार्य में डॉ० ए० सी० बूलनरकी, जो इस खोज-योजनाके प्रेरणा-स्रोत थे, १९३८ में अचानक मृत्यु हो गई और मासोपरान्त पं० मथुराप्रसाद दीक्षित भी स्वर्ग सिधार गए। एकाकी रह जाने के कारण डॉ० जैन का जोश भी ठण्डा पड़ गया। अगस्त सन् १९४७ में देश विभाजन के समय डॉ. जैन द्वारा सभी एकत्रित रासो सम्बन्धी खोज-सामग्री लाहौर में डॉ. जैनके कृष्णनगर स्थित मकानके साथ ही अग्निमें जलकर स्वाहा हो गई । जैन जी जान बचाकर अपने मूल निवास स्थान लुधियाना आ गए। इन्हीं दिनों में भी लाहौरसे फटेहाल लुधियाना पहुँचा और संयोगवश डॉ० साहबके मुहल्लेमें ही मुझे भी किराएका मकान मिला । भाग्यवश यहाँ आर्य कालेज लुधियानामें मुझे अध्यापन कार्य मिल गया था । पड़ोसी के नाते शनैः-शनैः डॉ० जैनसे परिचय बढ़ता गया। जैसा कि स्वाभाविक था, हमारी वार्तालापका विषय साहित्य चर्चा ही रहता। वे मेरी साहित्यिक अन्तर्रुचि एवं प्रवृत्तिको परखते एवं टटोलते रहते । इनकी संगतिसे मुझे एक विशेष आनन्द मिलता । उनका मुझपर पुत्रवत् स्नेह था और मेरी उनपर पितृवत् श्रद्धा
२३४ : अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन-ग्रंथ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org