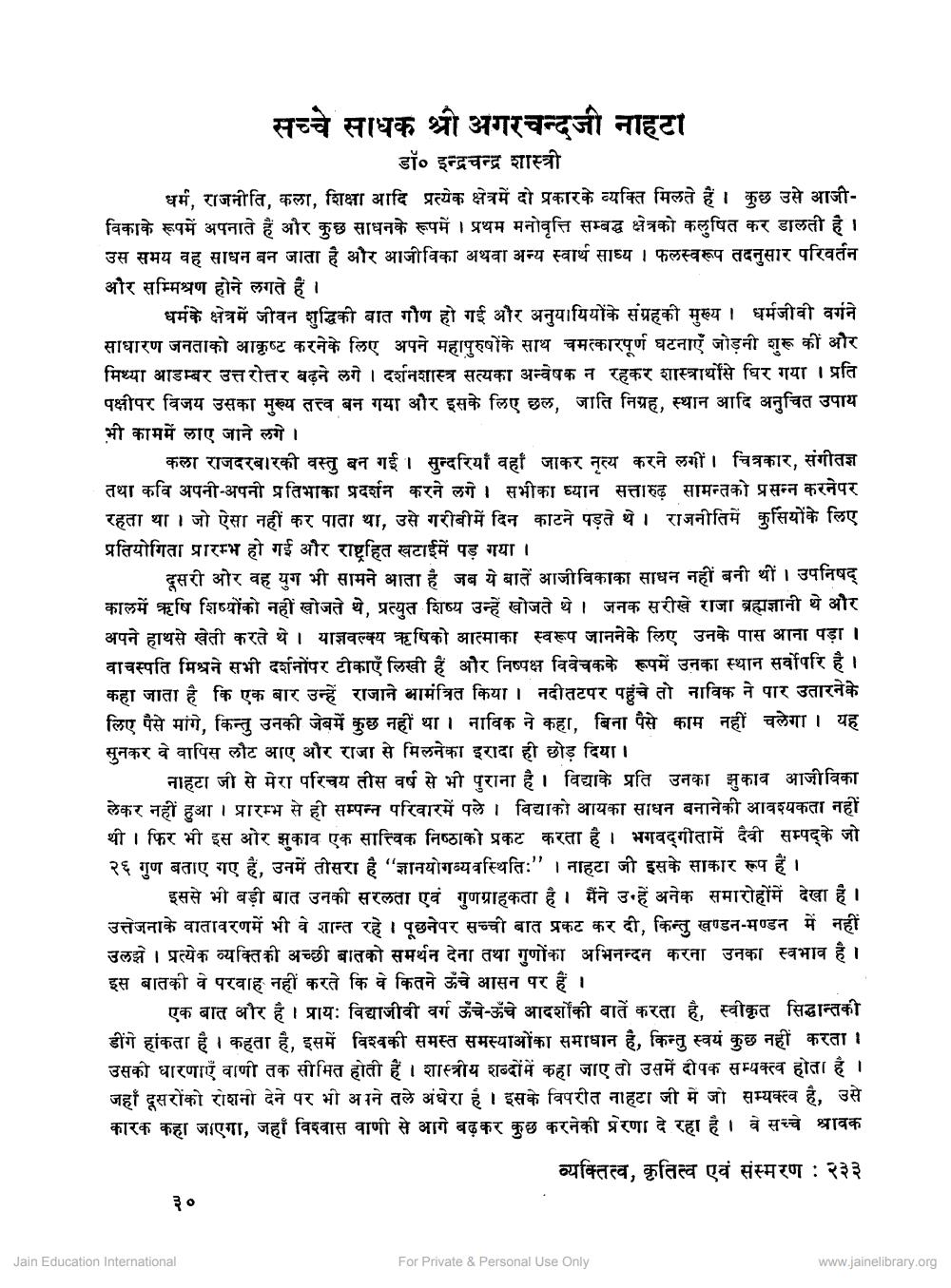________________
सच्चे साधक श्री अगरचन्दजी नाहटा
डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री धर्म, राजनीति, कला, शिक्षा आदि प्रत्येक क्षेत्रमें दो प्रकारके व्यक्ति मिलते हैं। कुछ उसे आजीविकाके रूपमें अपनाते हैं और कुछ साधनके रूपमें । प्रथम मनोवृत्ति सम्बद्ध क्षेत्रको कलुषित कर डालती है। उस समय वह साधन बन जाता है और आजीविका अथवा अन्य स्वार्थ साध्य । फलस्वरूप तदनुसार परिवर्तन और सम्मिश्रण होने लगते हैं।
धर्मके क्षेत्रमें जीवन शुद्धिकी बात गौण हो गई और अनुयायियोंके संग्रहकी मुख्य । धर्मजीवी वर्गने साधारण जनताको आकृष्ट करनेके लिए अपने महापुरुषोंके साथ चमत्कारपूर्ण घटनाएँ जोड़नी शुरू की और मिथ्या आडम्बर उत्तरोत्तर बढ़ने लगे । दर्शनशास्त्र सत्यका अन्वेषक न रहकर शास्त्रार्थोसे घिर गया । प्रति पक्षीपर विजय उसका मख्य तत्त्व बन गया और इसके लिए छल, जाति निग्रह. स्थान आदि अनुचित उपाय भी काममें लाए जाने लगे।
कला राजदरबारकी वस्तु बन गई। सुन्दरियाँ वहाँ जाकर नत्य करने लगीं। चित्रकार, संगीतज्ञ तथा कवि अपनी-अपनी प्रतिभाका प्रदर्शन करने लगे। सभीका ध्यान सत्तारुढ़ सामन्तको प्रसन्न करनेपर रहता था। जो ऐसा नहीं कर पाता था, उसे गरीबीमें दिन काटने पड़ते थे। राजनीतिमें कुर्सियोंके लिए प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई और राष्ट्रहित खटाईमें पड़ गया।
दूसरी ओर वह युग भी सामने आता है जब ये बातें आजीविकाका साधन नहीं बनी थीं। उपनिषद् कालमें ऋषि शिष्योंको नहीं खोजते थे, प्रत्युत शिष्य उन्हें खोजते थे। जनक सरीखे राजा ब्रह्मज्ञानी थे और अपने हाथसे खेती करते थे। याज्ञवल्क्य ऋषिको आत्माका स्वरूप जाननेके लिए उनके पास आना पड़ा। वाचस्पति मिश्रने सभी दर्शनोंपर टीकाएँ लिखी हैं और निष्पक्ष विवेचकके रूपमें उनका स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि एक बार उन्हें राजाने आमंत्रित किया। नदीतटपर पहुंचे तो नाविक ने पार उतारनेके लिए पैसे मांगे, किन्तु उनकी जेबमें कुछ नहीं था। नाविक ने कहा, बिना पैसे काम नहीं चलेगा। यह सुनकर वे वापिस लौट आए और राजा से मिलनेका इरादा ही छोड़ दिया।
नाहटा जी से मेरा परिचय तीस वर्ष से भी पुराना है। विद्याके प्रति उनका झुकाव आजीविका लेकर नहीं हुआ। प्रारम्भ से ही सम्पन्न परिवारमें पले। विद्याको आयका साधन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इस ओर झुकाव एक सात्त्विक निष्ठाको प्रकट करता है। भगवद्गीतामें दैवी सम्पद्के जो २६ गुण बताए गए हैं, उनमें तीसरा है "ज्ञानयोगव्यवस्थितिः" । नाहटा जी इसके साकार रूप हैं।।
इससे भी बड़ी बात उनकी सरलता एवं गुणग्राहकता है। मैंने उन्हें अनेक समारोहोंमें देखा है । उत्तेजनाके वातावरणमें भी वे शान्त रहे। पूछनेपर सच्ची बात प्रकट कर दी, किन्तु खण्डन-मण्डन में नहीं उलझे । प्रत्येक व्यक्तिकी अच्छी बातको समर्थन देना तथा गुणोंका अभिनन्दन करना उनका स्वभाव है। इस बातकी वे परवाह नहीं करते कि वे कितने ऊँचे आसन पर हैं ।
एक बात और है। प्राय: विद्याजीवी वर्ग ऊँचे-ऊँचे आदर्शोंकी बातें करता है. स्वीकृत सिद्धान्तकी डींगे हांकता है । कहता है, इसमें विश्वकी समस्त समस्याओंका समाधान है, किन्तु स्वयं कुछ नहीं करता। उसको धारणाएँ वाणी तक सीमित होती है । शास्त्रीय शब्दों में कहा जाए तो उसमें दीपक सम्यक्त्व होता है । जहाँ दूसरोंको रोशनो देने पर भी अपने तले अंधेरा है। इसके विपरीत नाहटा जी में जो सम्यक्त्व है, उसे कारक कहा जाएगा, जहाँ विश्वास वाणी से आगे बढ़कर कुछ करनेकी प्रेरणा दे रहा है। वे सच्चे श्रावक
व्यक्तित्व, कृतित्व एवं संस्मरण : २३३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org