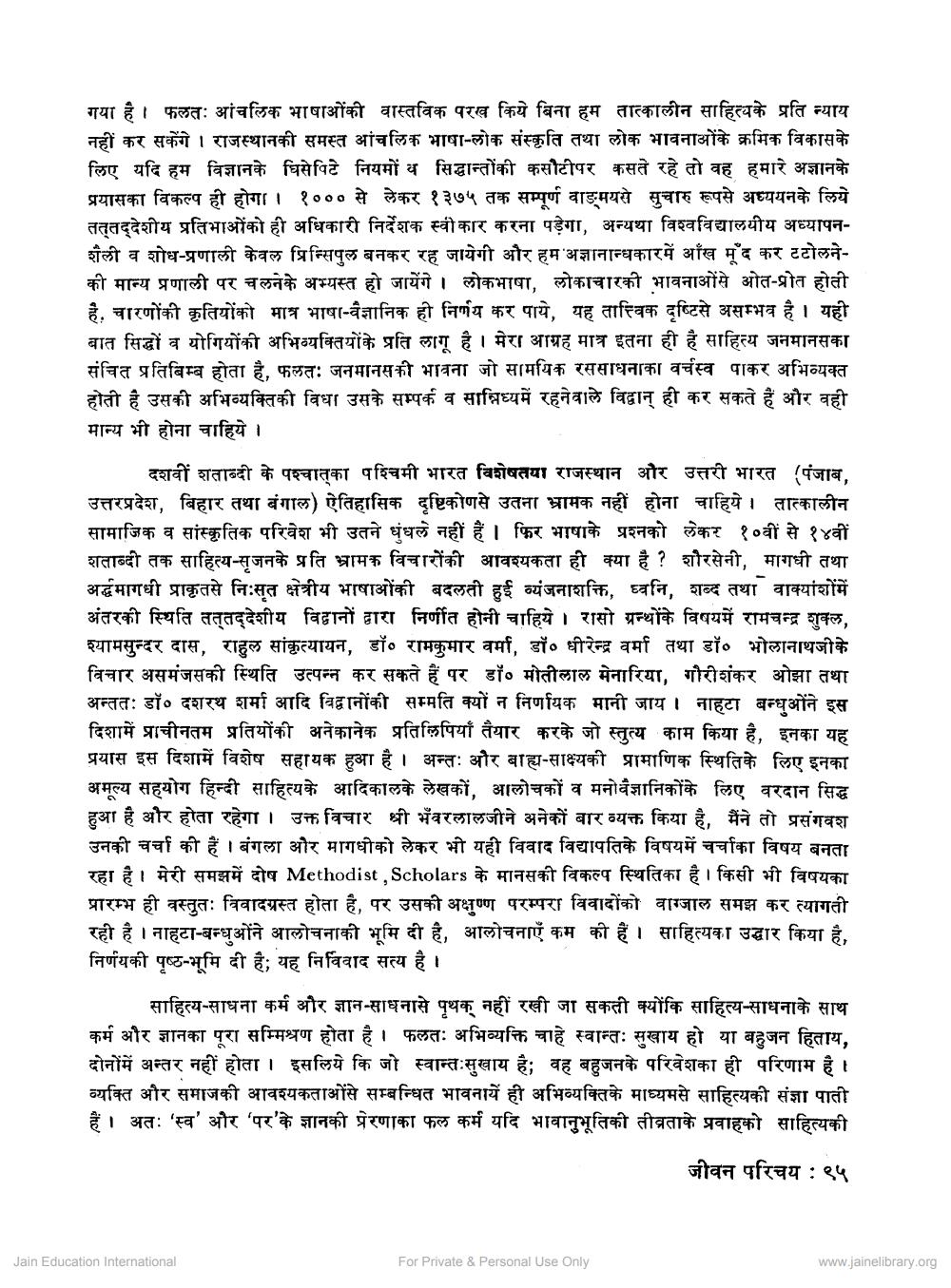________________
गया है। फलतः आंचलिक भाषाओंकी वास्तविक परख किये बिना हम तात्कालीन साहित्यके प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे। राजस्थानकी समस्त आंचलिक भाषा-लोक संस्कृति तथा लोक भावनाओंके क्रमिक विकासके लिए यदि हम विज्ञानके घिसेपिटे नियमों व सिद्धान्तोंकी कसौटीपर कसते रहे तो वह हमारे अज्ञानके प्रयासका विकल्प ही होगा। १००० से लेकर १३७५ तक सम्पूर्ण वाङ्मयसे सुचारु रूपसे अध्ययनके लिये तत्तद्देशीय प्रतिभाओंको ही अधिकारी निर्देशक स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा विश्वविद्यालयीय अध्यापनशैली व शोध-प्रणाली केवल प्रिन्सिपुल बनकर रह जायेगी और हम अज्ञानान्धकारमें आँख मद कर टटोलनेकी मान्य प्रणाली पर चलनेके अभ्यस्त हो जायेंगे। लोकभाषा, लोकाचारकी भावनाओंसे ओत-प्रोत होती है. चारणोंकी कृतियोंको मात्र भाषा-वैज्ञानिक ही निर्णय कर पाये, यह तात्त्विक दष्टिसे असम्भव है। यही बात सिद्धों व योगियोंकी अभिव्यक्तियों के प्रति लाग है। मेरा आग्रह मात्र इतना ही है साहित्य जनमानसका संचित प्रतिबिम्ब होता है, फलतः जनमानसकी भावना जो सामयिक रससाधनाका वर्चस्व पाकर अभिव्यक्त होती है उसकी अभिव्यक्तिकी विधा उसके सम्पर्क व सान्निध्य में रहनेवाले विद्वान् ही कर सकते हैं और वही मान्य भी होना चाहिये।
दशवीं शताब्दी के पश्चातका पश्चिमी भारत विशेषतया राजस्थान और उत्तरी भारत (पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा बंगाल) ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे उतना भ्रामक नहीं होना चाहिये। तात्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश भी उतने धुंधले नहीं हैं। फिर भाषाके प्रश्नको लेकर १०वीं से १४वीं शताब्दी तक साहित्य-सृजनके प्रति भ्रामक विचारोंकी आवश्यकता ही क्या है ? शौरसेनी, मागधी तथा अर्द्धमागधी प्राकृतसे नि:सत क्षेत्रीय भाषाओंकी बदलती हई व्यंजनाशक्ति, ध्वनि, शब्द तथा वाक्यांशोंमें अंतरकी स्थिति तत्तद्देशीय विद्वानों द्वारा निर्णीत होनी चाहिये । रासो ग्रन्थोंके विषयमें रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० भोलानाथजीके विचार असमंजसकी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं पर डॉ० मोतीलाल मेनारिया, गौरीशंकर ओझा तथा अन्ततः डॉ० दशरथ शर्मा आदि विद्वानोंकी सम्मति क्यों न निर्णायक मानी जाय । नाहटा बन्धुओंने इस दिशामें प्राचीनतम प्रतियोंकी अनेकानेक प्रतिलिपियाँ तैयार करके जो स्तुत्य काम किया है, इनका यह प्रयास इस दिशामें विशेष सहायक हुआ है। अन्तः और बाह्य-साक्ष्यकी प्रामाणिक स्थितिके लिए इनका अमूल्य सहयोग हिन्दी साहित्यके आदिकालके लेखकों, आलोचकों व मनोवैज्ञानिकोंके लिए वरदान सिद्ध हुआ है और होता रहेगा। उक्त विचार श्री भंवरलालजीने अनेकों बार व्यक्त किया है, मैंने तो प्रसंगवश उनकी चर्चा की हैं । बंगला और मागधीको लेकर भी यही विवाद विद्यापतिके विषयमें चर्चाका विषय बनता रहा है। मेरी समझमें दोष Methodist, Scholars के मानसकी विकल्प स्थितिका है। किसी भी विषयका प्रारम्भ ही वस्तुतः विवादग्रस्त होता है, पर उसकी अक्षुण्ण परम्परा विवादोंको वाग्जाल समझ कर त्यागती रही है । नाहटा-बन्धुओंने आलोचनाकी भूमि दी है, आलोचनाएँ कम की है। साहित्यका उद्धार किया है, निर्णयकी पृष्ठ-भूमि दी है; यह निर्विवाद सत्य है ।
साहित्य-साधना कर्म और ज्ञान-साधनासे पृथक् नहीं रखी जा सकती क्योंकि साहित्य-साधनाके साथ कर्म और ज्ञानका पूरा सम्मिश्रण होता है । फलतः अभिव्यक्ति चाहे स्वान्तः सुखाय हो या बहुजन हिताय, दोनोंमें अन्तर नहीं होता। इसलिये कि जो स्वान्तःसुखाय है; वह बहुजनके परिवेशका ही परिणाम है । व्यक्ति और समाजकी आवश्यकताओंसे सम्बन्धित भावनायें ही अभिव्यक्तिके माध्यमसे साहित्यकी संज्ञा पाती हैं। अतः 'स्व' और 'पर' के ज्ञानकी प्रेरणाका फल कर्म यदि भावानुभूतिकी तीव्रताके प्रवाहको साहित्यकी
जीवन परिचय : ९५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org